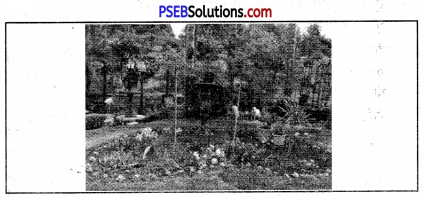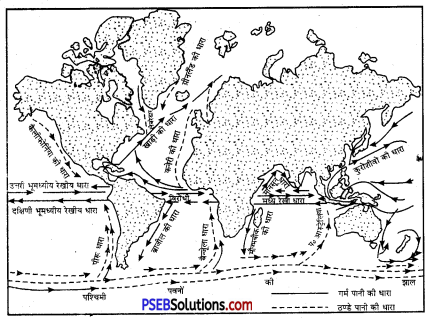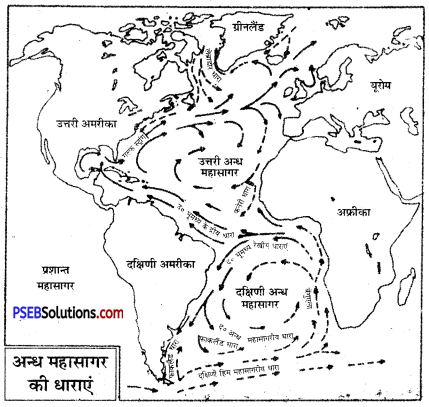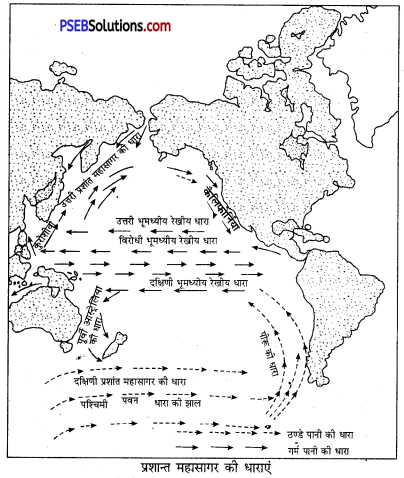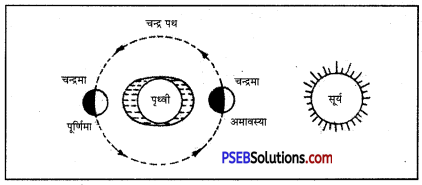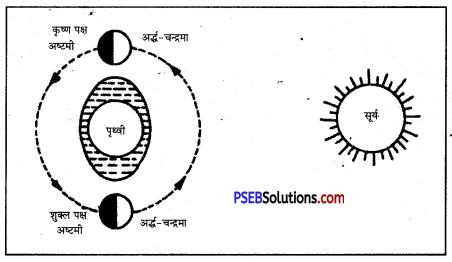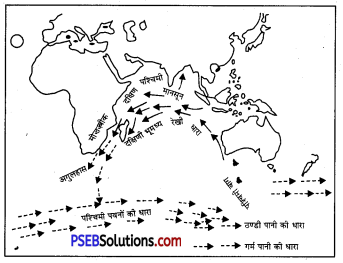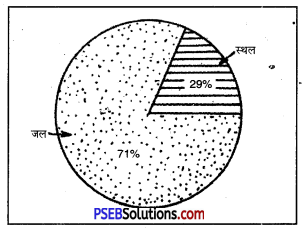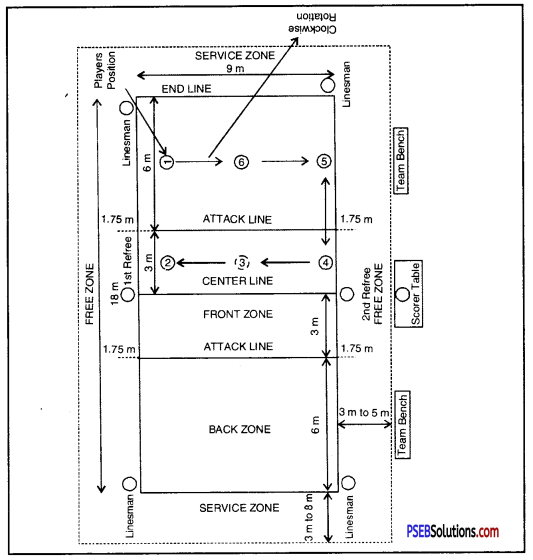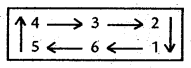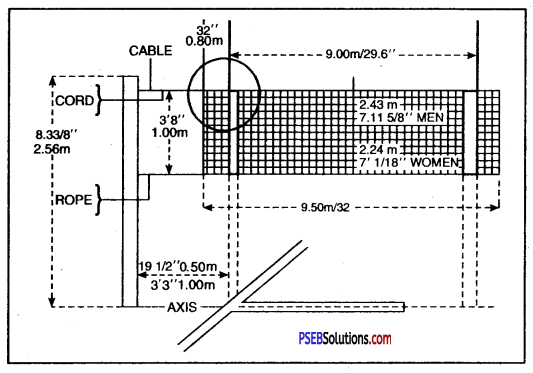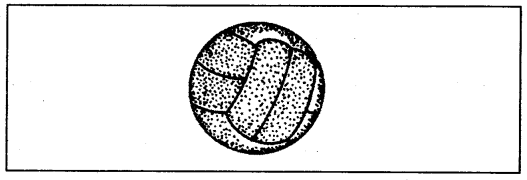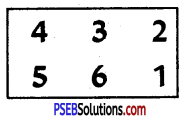Punjab State Board PSEB 12th Class History Book Solutions Chapter 9 गुरु तेग़ बहादुर जी और उनका बलिदान Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 12 History Chapter 9 गुरु तेग़ बहादुर जी और उनका बलिदान
निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)
गुरु तेग बहादुर जी का प्रारंभिक जीवन (Early Career of Guru Tegh Bahadur Ji)
प्रश्न 1.
गुरु तेग़ बहादुर जी के प्रारंभिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (Give a brief description of the early life of Guru Tegh Bahadur Ji.)
उत्तर-
गुरु तेग़ बहादुर जी सिखों के नवम् गुरु थे। उनका गुरुकाल 1664 ई० से 1675 ई० तक रहा। गुरु तेग़ बहादुर जी ने सिख धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अनेक प्रदेशों की यात्राएँ कीं। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देकर उन्होंने भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। गुरु जी के प्रारंभिक जीवन और यात्राओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—
1. जन्म तथा माता-पिता (Birth and Parentage)-गुरु तेग़ बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल, 1621 ई० को अमृतसर में हुआ। आप गुरु हरगोबिंद जी के पाँचवें तथा सबसे छोटे पुत्र थे। आपके माता जी का नाम नानकी था। आपके पिता जी ने आपके जन्म पर भविष्यवाणी की कि यह बालक सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलेगा तथा अत्याचार का डट कर मुकाबला करेगा। गुरु जी का यह कथन सत्य सिद्ध हुआ।
2. बाल्यकाल तथा शिक्षा (Childhood and Education)-बचपन में आपका नाम त्यागमल था। जब आप पाँच वर्ष के हुए तो आपने बाबा बुड्डा जी तथा भाई गुरदास जी से शिक्षा प्राप्त करनी आरंभ की। आपने पंजाबी, ब्रज, संस्कृत, इतिहास, दर्शन, गणित, संगीत आदि की शिक्षा प्राप्त की। आपको घुड़सवारी तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी गई। करतारपुर की लड़ाई में आपकी वीरता देखकर आपके पिता गुरु हरगोबिंद जी ने आपका नाम त्यागमल से बदल कर तेग़ बहादुर रख दिया।
3. विवाह (Marriage)-तेग़ बहादुर जी का विवाह करतारपुर वासी लाल चंद जी की सुपुत्री गुजरी से हुआ। आपके घर 1666 ई० में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस बालक का नाम गोबिंद राय अथवा गोबिंद दास रखा गया।
4. बाबा बकाला में निवास (Settlement at Baba Bakala)—ज्योति-जोत समाने से पूर्व गुरु हरगोबिंद जी ने अपने पौत्र हर राय जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने तेग़ बहादुर जी को अपनी पत्नी गुजरी तथा माता नानकी को लेकर बकाला चले जाने का आदेश दिया। यहाँ तेग़ बहादुर जी 20 वर्ष तक रहे।
5. गुरुगद्दी की प्राप्ति (Assumption of Guruship)-अपने ज्योति-जोत समाने से पूर्व गुरु हर कृष्ण जी ने यह संकेत दिया था कि सिखों का अगला गुरु बाबा बकाला में है। जब यह समाचार बकाला पहुँचा तो 22 सोढियों ने अपनी 22 मंजियाँ स्थापित कर लीं। हर कोई स्वयं को गुरु कहलवाने लगा। ऐसे समय में मक्खन शाह लुबाणा नामक एक सिख ने इसका समाधान ढूंढा। वह एक व्यापारी था। एक बार जब उसका समुद्री जहाज़ डूब रहा था तो उसने शुद्ध मन से गुरु साहिब के आगे अरदास की कि यदि उसका जहाज़ डूबने से बच जाए तो वह गुरु साहिब के चरणों में सोने की 500 मोहरें भेंट करेगा। उसका जहाज़ किनारे लग गया। वह गुरु साहिब को 500 मोहरें भेंट करने के लिए बाबा बकाला पहुँचा। यहाँ वह 22 गुरु देखकर चकित रह गया। वास्तविक गुरु को ढूंढने के लिए उसने बारी-बारी प्रत्येक गुरु को दो-दो मोहरें भेंट की। नकली गुरु दो-दो मोहरें लेकर प्रसन्न हो गए। जब मक्खन शाह ने अंत में श्री तेग़ बहादुर जी को दो मोहरें भेंट की तो गुरु साहिब ने कहा, “जहाज़ डूबते समय तो तूने 500 मोहरें भेंट करने का वचन दिया था,परंतु अब केवल दो मोहरें ही भेंट कर रहा है।” यह सुनकर मक्खन शाह एक मकान की छत पर चढ़कर ज़ोर-ज़ोर से कहने लगा, “गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे।” अर्थात् गुरु मिल गया है। इस प्रकार सिख संगतों ने गुरु तेग़ बहादुर जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु तेग़ बहादुर जी 1664 ई० से 1675 ई० तक गुरुगद्दी पर विराजमान रहे।
6. धीरमल का विरोध (Opposition of Dhir Mal)-धीरमल गुरु हरराय जी का बड़ा भाई था। बकाला में स्थापित 22 मंजियों में से एक धीरमल की भी थी। जब धीरमल को यह समाचार मिला कि सिख संगतों ने तेग़ बहादुर जी को अपना गुरु मान लिया है तो उसने कुछ गुंडों के साथ गुरु जी पर आक्रमण कर दिया। इस घटना से सिख रोष से भर उठे। वे धीरमल को पकड़कर गुरु जी के पास लाए। धीरमल द्वारा क्षमा याचना करने पर गुरु साहिब ने उसे क्षमा कर दिया।
गुरु तेग बहादुर जी की यात्राएँ
(Travels of Guru Tegh Bahadur Ji)
प्रश्न 2.
गुरु तेग़ बहादुर जी की धर्म यात्राओं का संक्षिप्त वर्णन करें। (Give a brief account of the religious tours of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की धार्मिक यात्राओं का संक्षेप वर्णन करें। (Narrate the travels undertaken by Guru Tegh Bahadur Ji for preaching Sikhism.)
उत्तर-
1664 ई० में गुरुगद्दी पर विराजमान होने के शीघ्र पश्चात् गुरु तेग़ बहादुर जी ने सिख धर्म के प्रचार के लिए पंजाब तथा पंजाब से बाहर की यात्राएँ आरंभ कर दीं। इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों को सत्य तथा प्रेम का संदेश देना था। गुरु साहिब की यात्राओं के उद्देश्य के संबंध में लिखते हुए विख्यात इतिहासकार एस० एस० जौहर का कहना है,
“गुरु तेग़ बहादुर ने लोगों को नया जीवन देने तथा उनके भीतर नई भावना उत्पन्न करना आवश्यक समझा।”1
1. “Guru Tegh Bahadur thought it necessary to infuse a new life and rekindle a new spirit among the people.” S.S. Johar, Guru Tegh Bahadur (New Delhi : 1975) p. 104.
I. पंजाब की यात्राएँ (Travels of Punjab)
1. अमृतसर (Amritsar)—गुरु तेग़ बहादुर जी ने अपनी यात्राओं का आरंभ 1664 ई० में अमृतसर से किया। उस समय हरिमंदिर साहिब में पृथी चंद का पौत्र हरजी मीणा कुछ भ्रष्टाचारी मसंदों के साथ मिलकर स्वयं गुरु बना बैठा था। गुरु साहिब के आने की सूचना मिलते ही उसने हरिमंदिर साहिब के सभी द्वार बंद करवा दिए। जब गुरु साहिब वहाँ पहुँचे तो द्वार बंद देखकर उन्हें दुःख हुआ। अतः वह अकाल तख्त के निकट एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। यहाँ पर अब एक छोटा-सा गुरुद्वारा बना हुआ है जिसे ‘थम्म साहिब’ कहते हैं।
2. वल्ला तथा घुक्केवाली (Walla and Ghukewali)-अमृतसर से गुरु तेग बहादुर जी वल्ला नामक गाँव गए। यहाँ लंगर में महिलाओं की अथक सेवा से प्रसन्न होकर गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा कहा “माईयाँ रब्ब रजाईयाँ”। वल्ला के पश्चात् गुरु जी घुक्केवाली गाँव गए। इस गाँव में अनगिनत वृक्षों के कारण गुरु जी ने इसका नाम ‘गुरु का बाग’ रख दिया।
3. खडूर साहिब, गोइंदवाल साहिब, तरन तारन तथा खेमकरन आदि (Khadur Sahib, Goindwal Sahib, Tarn Taran and Khemkaran etc.)-गुरु साहिब की यात्रा के अगले पड़ाव खडूर साहिब, गोइंदवाल साहिब तथा तरनतारन थे। यहाँ परं गुरु जी ने लोगों को प्रेम तथा भाईचारे का संदेश दिया। तत्पश्चात् गुरु साहिब खेमकरन गए। यहाँ के एक श्रद्धालु चौधरी रघुपति राय ने गुरु साहिब को एक घोड़ी भेंट की।
4. कीरतपुर साहिब और बिलासपुर (Kiratpur Sahib and Bilaspur)-माझा प्रदेश की यात्रा पूर्ण करने के पश्चात् गुरु तेग़ बहादुर जी कीरतपुर साहिब पहुँचे। वे रानी चंपा के निमंत्रण पर बिलासपुर पहुँचे। गुरु साहिब यहाँ तीन दिन ठहरे। गुरु साहिब ने रानी को 500 रुपए देकर माखोवाल में कुछ भूमि खरीदी तथा एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम उनकी माता जी के नाम पर “चक्क नानकी” रखा गया। बाद में यह स्थान गुरु गोबिंद सिंह जी के समय श्री आनंदपुर साहिब के नाम से विख्यात हुआ।
II. पूर्वी भारत की यात्राएँ । (Travels of Eastern India)
पंजाब की यात्राओं के पश्चात् गुरु तेग़ बहादुर साहिब ने पूर्वी भारत की यात्राएँ कीं। इन यात्राओं का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है—
5. सैफाबाद और धमधान (Saifabad and Dhamdhan)—अपनी पूर्वी भारत की यात्रा के दौरान सर्वप्रथम गुरु साहिब ने सैफाबाद तथा धमधान की यात्रा की। यहाँ गुरु साहिब के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। सिख धर्म के इस बढ़ते हुए प्रचार को देखकर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बना लिया।
6. मथुरा और वृंदावन (Mathura and Brindaban) अंबर के राजा राम सिंह के कहने पर औरंगजेब ने गुरु तेग़ बहादुर जी को छोड़ दिया। छूटने के बाद गुरु साहिब दिल्ली से मथुरा तथा वृंदावन पहुंचे। इन दोनों स्थानों पर गुरु साहिब ने धर्म प्रचार किया और संगतों को उपदेश दिए।
7. आगरा और प्रयाग (Agra and Paryag)—गुरु साहिब की यात्रा का अगला पड़ाव आगरा था। यहाँ पर वह एक बुजुर्ग श्रद्धालु माई जस्सी के घर ठहरे। तत्पश्चात् गुरु साहिब प्रयाग पहुँचे। यहाँ गुरु साहिब ने संन्यासियों, साधुओं और योगियों को उपदेश देते हुए फरमाया, “साधो मन का मान त्यागो।”
8. बनारस (Banaras)—प्रयाग की यात्रा के पश्चात् गुरु साहिब बनारस पहुँचे। यहाँ सिख संगतें प्रतिदिन बड़ी संख्या में गुरु साहिब के दर्शन और उनके उपदेश सुनने के लिए उपस्थित होतीं। यहाँ के लोगों का विश्वास था कि कर्मनाशा नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति के सभी अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। गुरु साहिब ने स्वयं इस नदी में स्नान किया और कहा कि नदी में स्नान करने से कुछ नहीं होता मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है।
9. ससराम और गया (Sasram and Gaya)-बनारस के पश्चात् गुरु साहिब ससराम पहुँचे। यहाँ पर एक श्रद्धालु सिख ‘मसंद फग्गू शाह’ ने गुरु साहिब की बहुत सेवा की। तत्पश्चात् गुरु साहिब गया पहुंचे। यह बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था। यहाँ गुरु साहिब ने लोगों को सत्य तथा परस्पर भ्रातृभाव का संदेश दिया।
10. पटना (Patna)गुरु साहिब 1666 ई० में पटना पहुँचे। यहाँ पर सिख संगतों (श्रद्धालुओं) ने गुरु साहिब का भव्य स्वागत किया। गुरु साहिब ने सिख सिद्धांतों पर प्रकाश डाला तथा पटना को ‘गुरु का घर’ कहकर सम्मानित किया। गुरु साहिब ने अपनी पत्नी और माता जी को यहाँ छोड़कर स्वयं मुंघेर के लिए प्रस्थान किया।
11. ढाका (Dhaka)-ढाका पूर्वी भारत में सिख धर्म का एक प्रमुख प्रचार केंद्र था। गुरु साहिब के आगमन के कारण बड़ी संख्या में लोग सिख-धर्म में शामिल हुए। गुरु साहिब ने यहाँ संगतों को जाति-पाति के बंधनों से ऊपर उठने और नाम स्मरण से जुड़ने का संदेश दिया।
12. असम (Assam)-ढाका की यात्रा के बाद गुरु साहिब अंबर के राजा राम सिंह के निवेदन पर असम गए। असमी लोग जादू-टोनों में बहुत कुशल थे। गुरु जी की उपस्थिति में जादू-टोने वाले प्रभावहीन होने लगे और उन्हें गुरु जी का लोहा मानना पड़ा। वे गुरु जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे और उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। तत्पश्चात् गुरु साहिब अपने परिवार सहित पंजाब लौट आए और चक्क नानकी में रहने लगे।
III. मालवा और बांगर प्रदेश की यात्राएँ (Tours of Malwa and Bangar Region)
1673 ई० के मध्य में गुरु तेग़ बहादुर जी ने पंजाब के मालवा और बांगर प्रदेश की दूसरी बार यात्रा आरंभ की। इस यात्रा के दौरान गुरु साहिब सैफ़ाबाद, मलोवाल, ढिल्लवां, भोपाली, खीवां, ख्यालां, तलवंडी, भठिंडा और धमधान आदि प्रदेशों में गए। इस यात्रा के दौरान गुरु साहिब ने स्थान-स्थान पर धर्म प्रचार के केंद्र खोले और गुरु नानक जी का संदेश घर-घर पहुँचाया। गुरु साहिब के सर्वपक्षीय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हज़ारों लोग गुरु साहिब के अनुयायी बन गए। अंत में, हम प्रसिद्ध इतिहासकार हरबंस सिंह के इन शब्दों से सहमत हैं,
“गुरु तेग़ बहादुर जी की यात्राओं ने देश में एक तूफान-सा ला दिया। यह न तो पहले जैसा देश रहा और न ही वे लोग। उनमें नई जागृति आ चुकी थी।”2

प्रश्न 3.
गुरु तेग़ बहादुर जी के आरंभिक जीवन तथा यात्राओं का विवरण दें।
(Give an account of the early career and travels of Guru Tegh Bahadur Ji.)
उत्तर-
गुरु तेग़ बहादुर जी सिखों के नवम् गुरु थे। उनका गुरुकाल 1664 ई० से 1675 ई० तक रहा। गुरु तेग़ बहादुर जी ने सिख धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अनेक प्रदेशों की यात्राएँ कीं। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देकर उन्होंने भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। गुरु जी के प्रारंभिक जीवन और यात्राओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—
1. जन्म तथा माता-पिता (Birth and Parentage)-गुरु तेग़ बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल, 1621 ई० को अमृतसर में हुआ। आप गुरु हरगोबिंद जी के पाँचवें तथा सबसे छोटे पुत्र थे। आपके माता जी का नाम नानकी था। आपके पिता जी ने आपके जन्म पर भविष्यवाणी की कि यह बालक सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलेगा तथा अत्याचार का डट कर मुकाबला करेगा। गुरु जी का यह कथन सत्य सिद्ध हुआ।
2. बाल्यकाल तथा शिक्षा (Childhood and Education)-बचपन में आपका नाम त्यागमल था। जब आप पाँच वर्ष के हुए तो आपने बाबा बुड्डा जी तथा भाई गुरदास जी से शिक्षा प्राप्त करनी आरंभ की। आपने पंजाबी, ब्रज, संस्कृत, इतिहास, दर्शन, गणित, संगीत आदि की शिक्षा प्राप्त की। आपको घुड़सवारी तथा शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी गई। करतारपुर की लड़ाई में आपकी वीरता देखकर आपके पिता गुरु हरगोबिंद जी ने आपका नाम त्यागमल से बदल कर तेग़ बहादुर रख दिया।
3. विवाह (Marriage)-तेग़ बहादुर जी का विवाह करतारपुर वासी लाल चंद जी की सुपुत्री गुजरी से हुआ। आपके घर 1666 ई० में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस बालक का नाम गोबिंद राय अथवा गोबिंद दास रखा गया।
4. बाबा बकाला में निवास (Settlement at Baba Bakala)—ज्योति-जोत समाने से पूर्व गुरु हरगोबिंद जी ने अपने पौत्र हर राय जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने तेग़ बहादुर जी को अपनी पत्नी गुजरी तथा माता नानकी को लेकर बकाला चले जाने का आदेश दिया। यहाँ तेग़ बहादुर जी 20 वर्ष तक रहे।
5. गुरुगद्दी की प्राप्ति (Assumption of Guruship)-अपने ज्योति-जोत समाने से पूर्व गुरु हर कृष्ण जी ने यह संकेत दिया था कि सिखों का अगला गुरु बाबा बकाला में है। जब यह समाचार बकाला पहुँचा तो 22 सोढियों ने अपनी 22 मंजियाँ स्थापित कर लीं। हर कोई स्वयं को गुरु कहलवाने लगा। ऐसे समय में मक्खन शाह लुबाणा नामक एक सिख ने इसका समाधान ढूंढा। वह एक व्यापारी था। एक बार जब उसका समुद्री जहाज़ डूब रहा था तो उसने शुद्ध मन से गुरु साहिब के आगे अरदास की कि यदि उसका जहाज़ डूबने से बच जाए तो वह गुरु साहिब के चरणों में सोने की 500 मोहरें भेंट करेगा। उसका जहाज़ किनारे लग गया। वह गुरु साहिब को 500 मोहरें भेंट करने के लिए बाबा बकाला पहुँचा। यहाँ वह 22 गुरु देखकर चकित रह गया। वास्तविक गुरु को ढूंढने के लिए उसने बारी-बारी प्रत्येक गुरु को दो-दो मोहरें भेंट की। नकली गुरु दो-दो मोहरें लेकर प्रसन्न हो गए। जब मक्खन शाह ने अंत में श्री तेग़ बहादुर जी को दो मोहरें भेंट की तो गुरु साहिब ने कहा, “जहाज़ डूबते समय तो तूने 500 मोहरें भेंट करने का वचन दिया था,परंतु अब केवल दो मोहरें ही भेंट कर रहा है।” यह सुनकर मक्खन शाह एक मकान की छत पर चढ़कर ज़ोर-ज़ोर से कहने लगा, “गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे।” अर्थात् गुरु मिल गया है। इस प्रकार सिख संगतों ने गुरु तेग़ बहादुर जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु तेग़ बहादुर जी 1664 ई० से 1675 ई० तक गुरुगद्दी पर विराजमान रहे।
6. धीरमल का विरोध (Opposition of Dhir Mal)-धीरमल गुरु हरराय जी का बड़ा भाई था। बकाला में स्थापित 22 मंजियों में से एक धीरमल की भी थी। जब धीरमल को यह समाचार मिला कि सिख संगतों ने तेग़ बहादुर जी को अपना गुरु मान लिया है तो उसने कुछ गुंडों के साथ गुरु जी पर आक्रमण कर दिया। इस घटना से सिख रोष से भर उठे। वे धीरमल को पकड़कर गुरु जी के पास लाए। धीरमल द्वारा क्षमा याचना करने पर गुरु साहिब ने उसे क्षमा कर दिया।
2. “Guru Tegh Bahadur’s tours left the country in ferment. It was not the same country again, nor the same people. A new awakening had spread.” Harbans Singh, Guru Tegh Bahadur (New Delhi : 1982) p. 92.

GURDWARA SIS GANJ : DELHI
गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान एवं महत्त्व (Martyrdom and Importance of Guru Tegh Bahadur Ji)
प्रश्न 4.
नौवें गुरु साहिब जी की शहीदी के कारणों का आलोचनात्मक अध्ययन करें। इसके परिणामों की भी चर्चा करें।
(Critically examine the circumstances leading to the martyrdom of 9th Guru. Also discuss its results.)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के कारणों और परिणामों का वर्णन करें।
(Discuss the causes and results of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के कारणों तथा महत्त्व का वर्णन करें। (Describe the causes and significance of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के क्या कारण थे? इस शहीदी का क्या महत्त्व है?
(What were the main causes of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji ? What is its importance ?)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के लिए उत्तरदायी कारणों का संक्षिप्त विवरण दें। उनके बलिदान का देश एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ?
(Give a brief account of the circumstances leading to the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji. Also explain the effects of his martyrdom on the country and the society.)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी किन कारणों से हुई ? इन्हें कब, कहाँ और कैसे शहीद किया गया ?
(What were the causes responsible for the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji ? When, where and how was he executed ?)
अथवा
गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के लिए जिम्मेवार हालात का वर्णन करें। (P.S.E.B. Sept. 2000) (Explain the circumstances which led to the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के क्या कारण थे ? उनके शहीदी का क्या प्रभाव पड़ा ?
(Describe the causes of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji. What were the effects of his martyrdom ?)
उत्तर-
गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान इतिहास की एक अति महत्त्वपूर्ण घटना है। धर्म तथा मानवता के लिए अपना बलिदान देकर गुरु साहिब ने अपना नाम चिरकाल के लिए अमर कर लिया। गुरु जी के बलिदान से जुड़े तथ्यों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—
I. बलिदान के कारण (Causes of Martyrdom)
गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार है—
1. मुग़लों और सिखों में शत्रुता (Enmity between the Mughals and the Sikhs)-1605 ई० तक सिखों और मुग़लों में मैत्रीपूर्ण संबंध चले आ रहे थे, परंतु जब 1606 ई० में मुग़ल सम्राट् जहाँगीर ने गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया तो ये संबंध शत्रुता में बदल गए। गुरु हरगोबिंद जी द्वारा अपनाई गई नई नीति के कारण उन्हें जहाँगीर द्वारा दो वर्ष के लिए ग्वालियर के दुर्ग में नज़रबंद कर दिया गया। शाहजहाँ के काल में गुरु हरगोबिंद साहिब को चार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं। औरंगजेब के शासनकाल में सिखों और मुग़लों के बीच शत्रुता में और वृद्धि हो गई। यही शत्रुता गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान का एक प्रमुख कारण बनी।
2. औरंगज़ेब की कट्टरता (Fanaticism of Aurangzeb)–औरंगज़ेब की धार्मिक कट्टरता भी गुरु साहिब के बलिदान का प्रमुख कारण बनी। औरंगज़ेब 1658 ई० में मुग़लों का नया बादशाह बना था। वह भारत में चारों ओर इस्लाम धर्म का बोलबाला देखना चाहता था। इसलिए उसने हिंदुओं के कई प्रसिद्ध मंदिरों को गिरवा कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनवा दी थीं तथा उनके त्योहारों और रीति-रिवाजों पर प्रतिबंध लगा दिए। उसके शासनकाल में तलवार के बल पर गैर-मुसलमानों को बलपूर्वक इस्लाम धर्म में सम्मिलित किया जाने लगा। औरंगज़ेब ने यह भी आदेश दिया कि सिखों के सभी गुरुद्वारों को गिरा दिया जाए। डॉक्टर आई० बी० बैनर्जी के अनुसार,
“निस्संदेह औरंगजेब के सिंहासन पर बैठने के साथ ही साम्राज्य की सारी नीति को उलट दिया गया और एक नए युग का सूत्रपात हुआ।”3
3. नक्शबंदियों का औरंगज़ेब पर प्रभाव (Impact of Naqshbandis on Aurangzeb)-कट्टर सुन्नी मुसलमानों के नक्शबंदी संप्रदाय का औरंगज़ेब पर बहुत प्रभाव था। इस संप्रदाय के लिए गुरु साहिब की बढ़ रही ख्याति असहनीय थी। नक्शबंदियों को यह खतरा हो गया कि कहीं सिख धर्म का विकास इस्लाम के लिए कोई गंभीर चुनौती न बन जाए। इसलिए उन्होंने सिखों के विरुद्ध औरंगज़ेब को भडकाना आरंभ कर दिया।
4. सिख धर्म का प्रचार (Spread of Sikhism)-गुरु तेग़ बहादुर जी की सिख धर्म के प्रचार के लिए की गई यात्राओं से प्रभावित होकर हज़ारों लोग सिख मत में सम्मिलित हो गए थे। गुरु साहिब जी ने सिख मत के प्रचार में तीव्रता और योग्यता लाने के लिए सिख प्रचारक नियुक्त किए तथा उन्हें संगठित किया। सिख धर्म का हो रहा विकास तथा उसका संगठन औरंगज़ेब की सहन शक्ति से बाहर था।
5. राम राय की शत्रुता (Enmity of Ram Rai)-राम राय गुरु हर कृष्ण जी का बड़ा भाई था। गुरु हर कृष्ण जी के पश्चात् जब गुरुगद्दी तेग़ बहादुर जी को मिल गई तो वह यह सहन न कर पाया। उसने गुरुगद्दी प्राप्त करने के लिए कई हथकंडे अपनाने आरंभ किए। जब उसके सभी प्रयास असफल रहे तो उसने गुरु साहिब के विरुद्ध औरंगजेब के कान भरने आरंभ कर दिए।
6. कश्मीरी पंडितों की पुकार (Call of Kashmiri Pandits)-कश्मीरी ब्राह्मण अपने धर्म और प्राचीन संस्कृति के संबंधों में बहुत दृढ़ थे तथा समस्त भारत में उनका आदर होता था। औरंगज़ेब ने सोचा कि यदि ब्राह्मणों को किसी प्रकार मुसलमान बना लिया जाए तो भारत के शेष हिंदू स्वयंमेव ही इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। उसने शेर अफ़गान को कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया। शेर अफ़गान ने इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए ब्राह्मणों पर घोर अत्याचार किए। जब उन्हें अपने धर्म के बचाव का कोई मार्ग दिखाई न दिया तो पंडित कृपा राम के नेतृत्व में उनका एक दल 25 मई, 1675 ई० में श्री आनंदपुर साहिब गुरु तेग़ बहादुर जी के पास अपनी करुण याचना लेकर पहुँचा। गुरु साहिब के मुख पर गंभीरता देख बालक गोबिंद राय ने पिता जी से इसका कारण पूछा। गुरु साहिब ने बताया कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। बालक गोबिंद राय ने झट से कहा, “पिता जी आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है ?” बालक के मुख से यह उत्तर सुनकर गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि वे जाकर मुग़ल अधिकारियों को यह बता दें कि यदि वे गुरु तेग़ बहादुर को मुसलमान बना लें तो वे बिना किसी विरोध के इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे।
3. “Necessarily, on the accession of Aurangzeb the entire policy of the Empire was reversed and a new era commenced.” Dr. I.B. Banerjee, Evolution of the Khalsa (Calcutta : 1972) Vol 2, p. 68.
II. बलिदान किस प्रकार हुआ ? (How was Guru Martyred ?)
औरंगज़ेब ने गुरु साहिब को दिल्ली बुलाने का निश्चय किया। गुरु तेग़ बहादुर जी अपने तीन साथियों-भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी तथा भाई दयाला जी को लेकर 11 जुलाई, 1675 ई० को चक्क नानकी (श्री आनंदपुर साहिब) से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुग़ल अधिकारियों ने उन्हें रोपड़ के निकट गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 4 महीने तक सरहिंद के कारावास में रखा गया तथा औरंगजेब के आदेश पर 6 नवंबर, 1675 ई० को दिल्ली दरबार में पेश किया गया। औरंगज़ेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अथवा मृत्यु में से एक स्वीकार करने को कहा। गुरु साहिब तथा उनके तीनों साथियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। मुग़लों ने गुरु जी को हतोत्साहित करने के लिए उनके तीनों साथियों भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी तथा भाई दयाला जी को उनके सम्मुख शहीद कर दिया। इसके पश्चात् गुरु जी को कोई चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया, परंतु गुरु साहिब ने इंकार कर दिया। परिणामस्वरूप 11 नवंबर,1675 ई० को दिल्ली के चाँदनी चौक में गुरु जी का शीश धड़ से अलग कर दिया गया। हरबंस सिंह तथा एल० एम० जोशी का यह कथन पूर्णत: ठीक है,
“यह भारतीय इतिहास की सर्वाधिक दिल दहला देने वाली एवं कंपाने वाली घटना थी।”4
जिस स्थान पर गुरु तेग़ बहादुर जी को शहीद किया गया उस स्थान पर गुरुद्वारा शीश गंज का निर्माण किया गया। भाई लक्खी शाह गुरु जी के धड़ को अपनी बैलगाड़ी में छुपा कर अपने घर ले आया। यहाँ उसने गुरु जी के धड़ का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने घर को आग लगा दी। इस स्थान पर आजकल गुरुद्वारा रकाब गंज बना हुआ है।
III. बलिदान का महत्त्व (Significance of the Martyrdom)
गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान की घटना न केवल सिख इतिहास अपितु समूचे विश्व इतिहास की एक अतुलनीय घटना है। इस बलिदान से न केवल पंजाब, अपितु भारत के इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पड़े। गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के साथ ही महान् मुग़ल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह के शब्दों में,
“गुरु तेग़ बहादुर जी के महान् बलिदान के सिखों पर प्रभावशाली एवं दूरगामी प्रभाव पड़े।”5
4. “This was a most moving and earthshaking event in the history of India.” Harbans Singh and L.M. Joshi, An Introduction to Indian Religions (Patiala : 1973) p. 248.
5. “The impact of the great sacrifice of Guru Tegh Bahadur was extremely powerful and farreaching in its consequences on the Sikh people.” Dr. Trilochan Singh, Guru Tegh Bahadur : Prophet and Martyr (New Delhi : 1978) p. 179.
1. इतिहास की एक अद्वितीय घटना (A Unique Event of History)—संसार का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। ये बलिदान अधिकतर अपने धर्म की रक्षा अथवा देश के लिए दिए गए। परंतु गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता तथा सत्य के लिए अपना शीश दिया। निस्संदेह संसार के इतिहास में यह एक अतुलनीय उदाहरण थी। इसी कारण गुरु तेग़ बहादुर जी को ‘हिंद की चादर’ कहा जाता है।
2 सिखों में प्रतिशोध की भावना (Feeling of revenge among the Sikhs)—गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के फलस्वरूप समूचे पंजाब में मुग़ल साम्राज्य के प्रति रोष की लहर दौड़ गई। अतः सिखों ने मुग़लों के अत्याचारी शासन का अंत करने का निर्णय किया।
3. हिंदू धर्म की रक्षा (Protection of Hinduism)-औरंगजेब के दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे अत्याचारों से तंग आकर बहुत-से हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करना आरंभ कर दिया था। हिंदू धर्म के अस्तित्व के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो चुका था। ऐसे समय में गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देकर हिंदू धर्म को लुप्त होने से बचा लिया। इस बलिदान ने हिंदू कौम में एक नई जागृति उत्पन्न की। अतः वे औरंगज़ेब के अत्याचारों का सामना करने के लिए तैयार हो गए।
4. खालसा का सृजन (Creation of the Khalsa)—गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान ने सिखों को यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब धर्म की रक्षा के लिए उनका संगठित होना अत्यावश्यक है। इस उद्देश्य से गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ई० में बैसाखी के दिन खालसा पंथ का सृजन किया। खालसा पंथ के सृजन ने ऐसी बहादुर जाति को जन्म दिया जिसने मुग़लों और अफ़गानों का पंजाब से नामो-निशान मिटा दिया।
5. बलिदानों की परंपरा का आरंभ होना (Beginning of the tradition of Sacrifice)-गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान ने सिखों में धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने की, एक परंपरा आरंभ कर दी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस मार्ग का अनुसरण करते हुए अनेक कष्ट सहन किए। आपके छोटे साहिबजादों को जीवित नींवों में चिनवा दिया गया। बड़े साहिबजादे युद्धों में शहीद हो गए। गुरु साहिब के पश्चात् बंदा सिंह बहादुर तथा उनके साथ सैंकड़ों सिखों ने बलिदान दिए। सिखों ने मुग़ल अत्याचारों के आगे हँस-हँस कर बलिदान दिए। इस प्रकार गुरु तेग़ बहादुर जी का बलिदान आने वाली नस्लों के लिए एक प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ।
6. सिखों और मुग़लों में लड़ाइयाँ (Battles between the Sikhs and the Mughals)-गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के पश्चात् सिखों एवं मुग़लों के बीच लड़ाइयों का एक लंबा दौर आरंभ हुआ। इन लड़ाइयों के दौरान सिख चट्टान की तरह अडिग रहे। अपने सीमित साधनों के बावजूद सिखों ने अपनी वीरता के कारण महान् मुग़ल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। अंत में, हम प्रसिद्ध इतिहासकार एस० एस० जौहर के इन शब्दों से सहमत हैं,
“गुरु तेग़ बहादुर जी का बलिदान भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना है। इसके बहुत गहरे परिणाम निकले। “6
6. “The Martyrdom of Guru Tegh Bahadur was an event of great significance in the history of India. It had far-reaching consequences.” S.S. Johar, Guru Tegh Bahadur (New Delhi : 1975) p. 231.

प्रश्न 5.
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के सिख इतिहास पर बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। वर्णन करें।
(The martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji had far-reaching consequences on Sikh History. Discuss.)
उत्तर-
गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान की घटना न केवल सिख इतिहास अपितु समूचे विश्व इतिहास की एक अतुलनीय घटना है। इस बलिदान से न केवल पंजाब, अपितु भारत के इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पड़े। गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के साथ ही महान् मुग़ल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। डॉक्टर त्रिलोचन सिंह के शब्दों में,
“गुरु तेग़ बहादुर जी के महान् बलिदान के सिखों पर प्रभावशाली एवं दूरगामी प्रभाव पड़े।”5
5. “The impact of the great sacrifice of Guru Tegh Bahadur was extremely powerful and farreaching in its consequences on the Sikh people.” Dr. Trilochan Singh, Guru Tegh Bahadur : Prophet and Martyr (New Delhi : 1978) p. 179.
1. इतिहास की एक अद्वितीय घटना (A Unique Event of History)—संसार का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। ये बलिदान अधिकतर अपने धर्म की रक्षा अथवा देश के लिए दिए गए। परंतु गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता तथा सत्य के लिए अपना शीश दिया। निस्संदेह संसार के इतिहास में यह एक अतुलनीय उदाहरण थी। इसी कारण गुरु तेग़ बहादुर जी को ‘हिंद की चादर’ कहा जाता है।
2. सिखों में प्रतिशोध की भावना (Feeling of revenge among the Sikhs)—गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के फलस्वरूप समूचे पंजाब में मुग़ल साम्राज्य के प्रति रोष की लहर दौड़ गई। अतः सिखों ने मुग़लों के अत्याचारी शासन का अंत करने का निर्णय किया।
3. हिंदू धर्म की रक्षा (Protection of Hinduism)-औरंगजेब के दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे अत्याचारों से तंग आकर बहुत-से हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करना आरंभ कर दिया था। हिंदू धर्म के अस्तित्व के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो चुका था। ऐसे समय में गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देकर हिंदू धर्म को लुप्त होने से बचा लिया। इस बलिदान ने हिंदू कौम में एक नई जागृति उत्पन्न की। अतः वे औरंगज़ेब के अत्याचारों का सामना करने के लिए तैयार हो गए।
4. खालसा का सृजन (Creation of the Khalsa)—गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान ने सिखों को यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब धर्म की रक्षा के लिए उनका संगठित होना अत्यावश्यक है। इस उद्देश्य से गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ई० में बैसाखी के दिन खालसा पंथ का सृजन किया। खालसा पंथ के सृजन ने ऐसी बहादुर जाति को जन्म दिया जिसने मुग़लों और अफ़गानों का पंजाब से नामो-निशान मिटा दिया।
5. बलिदानों की परंपरा का आरंभ होना (Beginning of the tradition of Sacrifice)-गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान ने सिखों में धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने की, एक परंपरा आरंभ कर दी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस मार्ग का अनुसरण करते हुए अनेक कष्ट सहन किए। आपके छोटे साहिबजादों को जीवित नींवों में चिनवा दिया गया। बड़े साहिबजादे युद्धों में शहीद हो गए। गुरु साहिब के पश्चात् बंदा सिंह बहादुर तथा उनके साथ सैंकड़ों सिखों ने बलिदान दिए। सिखों ने मुग़ल अत्याचारों के आगे हँस-हँस कर बलिदान दिए। इस प्रकार गुरु तेग़ बहादुर जी का बलिदान आने वाली नस्लों के लिए एक प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ।
6. सिखों और मुग़लों में लड़ाइयाँ (Battles between the Sikhs and the Mughals)-गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के पश्चात् सिखों एवं मुग़लों के बीच लड़ाइयों का एक लंबा दौर आरंभ हुआ। इन लड़ाइयों के दौरान सिख चट्टान की तरह अडिग रहे। अपने सीमित साधनों के बावजूद सिखों ने अपनी वीरता के कारण महान् मुग़ल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। अंत में, हम प्रसिद्ध इतिहासकार एस० एस० जौहर के इन शब्दों से सहमत हैं,
“गुरु तेग़ बहादुर जी का बलिदान भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना है। इसके बहुत गहरे परिणाम निकले। “6
6. “The Martyrdom of Guru Tegh Bahadur was an event of great significance in the history of India. It had far-reaching consequences.” S.S. Johar, Guru Tegh Bahadur (New Delhi : 1975) p. 231.

संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न (Short Answer Type Questions)
प्रश्न 1.
किस श्रद्धालु सिख ने नवम् गुरु की तलाश की और क्यों ? (Name the devotee Sikh who searched for the Ninth Guru and why ?)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की तलाश किसने की ओर क्यों ? (Who found Guru Tegh Bahadur Ji and why ?)
उत्तर-
गुरु हर कृष्ण जी ने अपने ज्योति-जोत समाने से पूर्व सिख संगतों को यह संकेत दिया कि उनका अगला गुरु बाबा बकाला में है। इसलिए 22 सोढियों ने वहाँ अपनी 22 मंजियाँ स्थापित कर लीं। हर कोई स्वयं को गुरु कहलवाने लगा। ऐसे समय में मक्खन शाह लुबाणा ने इसका हल ढूँढ़ा। एक बार जब उसका जहाज़ समुद्री तूफान में डूबने लगा था तो उसने अरदास की कि यदि उसका जहाज़ किनारे पर पहुँच जाए तो वह गुरु साहिब के चरणों में सोने की 500 मोहरें भेंट करेगा। गुरु कृपा से उसका जहाज़ बच गया। वह बकाला पहुँचा। जब मक्खन शाह ने तेग़ बहादुर जी के पास जाकर दो मोहरें भेंट की तो गुरु साहिब ने कहा, “जहाज डूबते समय तो तूने 500 मोहरें भेंट करने का वचन दिया था।” यह सुनकर मक्खन शाह एक मकान की छत पर चढ़ कर ज़ोर-ज़ोर से कहने लगा “गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे” अर्थात्- गुरु मिल गया है।
प्रश्न 2.
गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की यात्राओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। (Give a brief account of the travels of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग बहादुर जी की यात्राओं के संबंध में आप क्या जानते हैं ? (What do you know about the travels of Guru Tegh Bahadur Ji ?)
उत्तर-
सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग़ बहादुर जी ने अपनी गुरुगद्दी के दौरान (1664-75 ई०) पंजाब और बाहर के प्रदेशों की अनेकं यात्राएँ कीं। गुरु साहिब की यात्राओं का उद्देश्य लोगों में फैली अज्ञानता को दूर करना और सिख सिद्धांतों का प्रचार करना था। गुरु साहिब ने अपनी यात्राएँ 1664 ई० में अमृतसर से आरंभ की। तत्पश्चात् । गुरु साहिब ने पंजाब तथा पंजाब के बाहर अनेक स्थानों की यात्राएं की। गुरु साहिब की इन यात्राओं ने सिख पंथ । के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इससे गुरु साहिब की ख्याति चारों ओर फैल गई।
प्रश्न 3.
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें।
(Highlight the causes of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के क्या कारण थे ?
(What were the causes of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji ?)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करें।
(Study the causes responsible for the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के कोई तीन कारण बताएँ। (List any three causes of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के क्या कारण थे? (What were the causes of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
उत्तर-
- गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी में सबसे प्रमुख योगदान औरंगज़ेब की धार्मिक कट्टरता का था।
- औरंगज़ेब सिख धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को सहन करने को तैयार नहीं थे।
- राम राय ने गुरुगद्दी प्राप्त करने के लिए औरंगज़ेब को गुरु तेग़ बहादुर जी के विरुद्ध भड़काया।
- कश्मीरी पंडितों की पुकार गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान का तत्कालीन कारण बनी।

प्रश्न 4.
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी में नक्शबंदियों की भूमिका की समीक्षा कीजिए।
(Discuss the role played by Naqshbandis in the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
उत्तर-
नक्शबंदी कट्टर सुन्नी मुसलमानों का एक संप्रदाय था। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र सरहिंद था। इस संप्रदाय के लिए गुरु साहिब की बढ़ रही ख्याति और सिख मत का बढ़ रहा प्रचार असहनीय था। इसलिए उन्होंने सिखों के विरुद्ध कार्यवाई करने के लिए औरंगज़ेब के कान भरने आरंभ कर दिए। उनकी कार्यवाई ने जलती पर तेल डालने का काम किया। अत: औरंगजेब ने गुरु जी के विरुद्ध कदम उठाने का निर्णय किया।
प्रश्न 5.
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी का तात्कालिक कारण क्या था ?
(What was the immediate cause of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji ?)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी ने कश्मीरी ब्राह्मणों की सहायता क्यों की ? (Why did Guru Tegh Bahadur Ji help the Kashmiri Brahmans ?)
उत्तर-
औरंगज़ेब चाहता था कि कश्मीर के ब्राह्मणों को किसी प्रकार मुसलमान बना लिया जाए तो भारत के शेष हिंदू स्वयंमेव ही इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। इसी उद्देश्य से उसने ब्राह्मणों को तलवार की नोक पर इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए विवश किया। पंडित कृपा राम के नेतृत्व में उनका एक दल 1675 ई० में श्री आनंदपुर साहिब गुरु तेग़ बहादुर जी के पास पहुँचा। जब गुरु जी ने उनकी रौंगटे खड़े कर देने वाली अत्याचारों की कहानी सुनी तो उन्होंने अपना बलिदान देने का निर्णय कर लिया।
प्रश्न 6.
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के ऐतिहासिक महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए।
(Evaluate the historical importance of martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी की ऐतिहासिक महत्ता का वर्णन करो। (Explain the historical importance of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का क्या महत्त्व है ?
(What is the significance of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji ?)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी की महत्ता बताओ।
(Explain the importance of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
उत्तर-
गुरु तेग बहादुर जी की इस शहीदी के कारण समूचा पंजाब क्रोध और रोष की भावना से भड़क उठा। गुरु साहिब ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक भारत में मुग़ल साम्राज्य रहेगा, तब तक अत्याचार भी बने रहेंगे। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुग़लों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए 1699 ई० में खालसा पंथ की स्थापना की। तत्पश्चात् सिखों और मुग़लों के बीच एक लंबा संघर्ष आरंभ हुआ। इस संघर्ष ने मुग़ल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)
(i) एक शब्द से एक पंक्ति तक के उत्तर (Answer in One Word to One Sentence)
प्रश्न 1.
सिखों के नौवें गुरु कौन थे ?
उत्तर-
गुरु तेग़ बहादुर जी।
प्रश्न 2.
गुरु तेग़ बहादुर जी का जन्म कहाँ हुआ ?
उत्तर-
अमृतसर।
प्रश्न 3.
गुरु तेग़ बहादुर जी का जन्म कब हुआ ?
उत्तर-
1 अप्रैल, 1621 ई० ।
प्रश्न 4.
गुरु तेग़ बहादुर जी की माता जी का नाम बताएँ।
उत्तर-
नानकी।

प्रश्न 5.
गुरु तेग बहादुर जी के पिता जी का नाम बताएँ।
उत्तर-गुरु हरगोबिंद जी।
प्रश्न 6.
गुरु तेग़ बहादुर जी का बचपन का नाम बताएँ।
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी का पहला नाम क्या था?
उत्तर-
त्याग मल।
प्रश्न 7.
‘तेग़ बहादुर’ से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
तलवार का धनी।
प्रश्न 8.
गुरु तेग़ बहादुर जी का विवाह किससे हुआ ?
उत्तर-
गुजरी जी।

प्रश्न 9.
गुरु तेग़ बहादुर जी के पुत्र का नाम क्या था ?
उत्तर-
गोबिंद राय अथवा गोबिंद दास।
प्रश्न 10.
बाबा बकाला में सच्चे गुरु तेग़ बहादुर जी को किसने ढूँढा?
उत्तर-
मक्खन शाह लुबाणा।
प्रश्न 11.
“गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे” नामक शब्द किसने कहे थे ?
उत्तर-
मक्खन शाह लुबाणा।
प्रश्न 12.
गुरु तेग़ बहादुर जी का गुरुगद्दी काल बताएँ।
उत्तर-
1664 ई० से 1675 ई०

प्रश्न 13.
पंजाब से बाहर किसी एक स्थान का नाम बताएँ जहाँ गुरु तेग़ बहादुर जी ने यात्रा की ?
उत्तर-
दिल्ली।
प्रश्न 14.
पंजाब के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम बताएँ जिसकी यात्रा गुरु तेग बहादुर जी ने की थी ?
उत्तर-
अमृसतर।
प्रश्न 15.
श्री आनंदपुर साहिब का पहला (प्रारंभिक) नाम क्या था ?
उत्तर-
माखोवाल अथवा चक नानकी।
प्रश्न 16.
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी का एक मुख्य कारण क्या था ?
उत्तर-
औरंगजेब सिखों के बढ़ते हुए प्रभाव को सहन करने को तैयार नहीं था।

प्रश्न 17.
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी का तात्कालिक कारण क्या था ?
उत्तर-
कश्मीरी पंडितों की पुकार।
प्रश्न 18.
उस मुग़ल सूबेदार का नाम बताएँ जिसने कश्मीर के पंडितों पर भारी अत्याचार किए थे।
उत्तर-
शेर अफ़गान।
प्रश्न 19.
किस के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक दल गुरु तेग बहादुर जी को श्री आनंदपुर साहिब में 1675 ई० में मिला था ?
उत्तर-
पंडित कृपा राम।
प्रश्न 20.
किस गुरु साहिब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया ?
उत्तर-
गुरु तेग़ बहादुर जी ने।

प्रश्न 21.
गुरु तेग़ बहादुर जी को कहाँ शहीद किया गया था ?
उत्तर-
दिल्ली।
प्रश्न 22.
गुरु तेग बहादुर जी को कौन-से मग़ल बादशाह ने शहीद करवाया था ?
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी किस मुग़ल बादशाह के समय हुई ?
अथवा
नौवें गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के समय किस मुग़ल बादशाह का शासन था ?
उत्तर-
औरंगज़ेब।
प्रश्न 23.
गुरु तेग़ बहादुर जी को कब शहीद किया गया था ?
उत्तर-
11 नवंबर, 1675 ई०
प्रश्न 24.
गुरु तेग़ बहादुर जी के साथ उनके किन तीन श्रद्धालु सिखों को शहीद किया गया?
उत्तर-
भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी।

प्रश्न 25.
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के स्थान पर किस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया ?
उत्तर-
गुरुद्वारा शीश गंज।
प्रश्न 26.
गुरुद्वारा शीश गंज का निर्माण कहाँ किया गया था ?
उत्तर-
दिल्ली।
प्रश्न 27.
गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान का कोई एक महत्त्वपूर्ण परिणाम बताएँ।
उत्तर-
सिखों और मुग़लों में संघर्ष का एक लंबा अध्याय आरंभ हुआ।
प्रश्न 28.
गुरु गोबिंद सिंह जी ने ‘रंगरेटे गुरु के बेटे’ शब्द किसके लिए प्रयोग किए थे ?
उत्तर-
भाई जैता जी।

प्रश्न 29.
‘हिंद की चादर’ नामक शब्द किस गुरु के लिए प्रयोग किए जाते हैं ?
अथवा
“हिंद की चादर’ किस गुरु साहिब को कहा जाता है ? .
उत्तर-
गुरु तेग़ बहादुर जी।
(ii) रिक्त स्थान भरें (Fill in the Blanks)
प्रश्न 1.
……………….. सिखों के नवम् गुरु थे।
उत्तर-
(गुरु तेग बहादुर जी)
प्रश्न 2.
गुरु तेग़ बहादुर जी का जन्म ……………. में हुआ था।
उत्तर-
(अमृतसर)
प्रश्न 3.
गुरु तेग़ बहादुर जी के पिता जी का नाम ……………. था। ”
उत्तर-
(गुरु हरगोबिंद जी)

प्रश्न 4.
गुरु तेग़ बहादुर जी की माता जी का नाम ……………..था।
उत्तर-
(नानकी)
प्रश्न 5.
गुरु तेग़ बहादुर जी का आरंभिक नाम ………… था।
उत्तर-
(त्याग मल)
प्रश्न 6.
गुरु तेग़ बहादुर जी के पुत्र का नाम ………… था।
उत्तर-
(गोबिंद राय)
प्रश्न 7.
गुरु तेग़ बहादुर जी की खोज ………….. ने की थी।
उत्तर-
(मक्खन शाह लुबाणा)

प्रश्न 8.
गुरु तेग़ बहादुर जी …………… में गुरुगद्दी पर विराजमान हुए।
उत्तर-
(1664 ई०)
प्रश्न 9.
गुरु तेग़ बहादुर जी ने अपनी यात्राओं का आरंभ ……………… से किया।
उत्तर-
(अमृतसर)
प्रश्न 10.
चक्क नानकी नगर की स्थापना ……….. ने की थी।
उत्तर-
(गुरु तेग बहादुर जी)
प्रश्न 11.
औरंगजेब ने ………….में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया।
उत्तर-
(1679 ई०)

प्रश्न 12.
राम राय गुरु हर राय जी का बड़ा ……..था।
उत्तर-
(पुत्र)
प्रश्न 13.
गुरु तेग़ बहादुर जी को…….. के आदेश पर शहीद किया गया था।
उत्तर-
(औरंगज़ेब)
प्रश्न 14.
गुरु तेग़ बहादुर जी को ……..में दिल्ली में शहीद किया गया।
उत्तर-
(11 नंवबर, 1675 ई०)
प्रश्न 15.
जिस स्थान पर गुरु तेग़ बहादुर जी को शहीद किया गया वहाँ…….. का निर्माण करवाया गया है।
उत्तर-
(गुरुद्वारा शीश गंज)

प्रश्न 16.
‘रंगरेटे गुरु के बेटे’ कह कर ………….. को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने गले से लगाया।
उत्तर-
(भाई जैता जी)
प्रश्न 17.
गुरु तेग़ बहादुर जी को शहीद करने वाले जल्लाद का नाम …………. था।
उत्तर-
(जलालुद्दीन)
प्रश्न 18.
…….को ‘हिंद की चादर’ के नाम से जाना जाता है।
उत्तर-
(गुरु तेग़ बहादुर जी)
(iii) ठीक अथवा गलत (True or False)
नोट-निम्नलिखित में से ठीक अथवा गलत चुनें
प्रश्न 1.
गुरु तेग़ बहादुर जी सिखों के नौवें गुरु थे।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 2.
गुरु तेग बहादुर जी का जन्म अमृतसर में हुआ।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 3.
गुरु तेग़ बहादुर जी का जन्म 1621 ई० में हुआ।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 4.
गुरु तेग़ बहादुर जी के पिता जी का नाम हरकृष्ण था।
उत्तर-
गलत
प्रश्न 5.
गुरु तेग़ बहादुर जी की माता जी का नाम गुजरी था।
उत्तर-
गलत

प्रश्न 6.
गुरु तेग़ बहादुर जी का आरंभिक नाम त्याग मल था।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 7.
गुरु तेग़ बहादुर जी के पुत्र का नाम गोबिंद राय था।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 8.
मक्खन शाह लुबाणा ने गुरु तेग़ बहादुर जी की खोज की थी।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 9.
गुरु तेग़ बहादुर जी 1664 ई० में गुरुगद्दी पर बिराजमान हुए।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 10.
गुरु तेग़ बहादुर जी अपनी यात्राओं के दौरान सर्वप्रथम अमृतसरं पहुँचे।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 11.
गुरु तेग़ बहादुर जी ने अपनी यात्राओं का आरंभ 1666 ई० में किया था।
उत्तर-
गलत
प्रश्न 12.
गुरु तेग़ बहादुर जी ने चक्क नानकी नगर की स्थापना की।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 13.
औरंगजेब ने 1664 ई० में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया।
उत्तर-
गलत

प्रश्न 14.
गुरु तेग बहादुर जी के समय शेर अफ़गान कश्मीर का गवर्नर था।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 15.
औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग़ बहादुर जी को दिल्ली में शहीद किया गया था।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 16.
गुरु तेग़ बहादुर जी को 11 नवंबर, 1675 ई० को शहीद किया गया था।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 17.
गुरु तेग़ बहादुर जी को जिस स्थान पर शहीद किया गया था उस स्थान पर गुरुद्वारा रकाब गंज का निर्माण करवाया गया है।
उत्तर-
गलत

(iv) बहु-विकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)
नोट-निम्नलिखित में से ठीक उत्तर का चयन कीजिए—
प्रश्न 1.
सिखों के नवम् गुरु कौन थे ?
(i) गुरु अमरदास जी
(ii) गुरु हर राय जी
(iii) गुरु हर कृष्ण जी
(iv) गुरु तेग़ बहादुर जी।
उत्तर-
(iv)
प्रश्न 2.
गुरु तेग़ बहादुर जी का जन्म कब हुआ ?
(i) 1601 ई० में
(ii) 1621 ई० में
(iii) 1631 ई० में
(iv) 1656 ई० में।
उत्तर-
(ii)
प्रश्न 3.
गुरु तेग़ बहादुर जी के बचपन का क्या नाम था ?
(i) हरी मल जी
(ii) त्याग मल जी
(iii) भाई लहणा जी
(iv) भाई जेठा जी।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 4.
गुरु तेग़ बहादुर जी के पिता जी का क्या नाम था ?
(i) गुरु हरगोबिंद जी
(ii) गुरु हर राय जी
(iii) गुरु हर कृष्ण जी
(iv) बाबा गुरदित्ता जी।
उत्तर-
(i)

प्रश्न 5.
गुरु तेग़ बहादुर जी की माता जी का क्या नाम था ?
(i) गुजरी जी
(ii) सुलक्खनी जी
(iii) नानकी जी
(iv) गंगा देवी जी।
उत्तर-
(iii)
प्रश्न 6.
गुरु तेग़ बहादुर जी का विवाह किसके साथ हुआ ?
(i) निहाल कौर के साथ
(ii) गुजरी के साथ
(iii) सुलक्खनी के साथ
(iv) सभराई देवी के साथ।
उत्तर-
(ii)
प्रश्न 7.
गुरु तेग़ बहादुर जी के पुत्र का क्या नाम था ?
(i) महादेव
(ii) अर्जन देव
(iii) राम राय
(iv) गोबिंद राय।
उत्तर-
(iv)
प्रश्न 8.
उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने यह प्रमाणित किया कि गुरु तेग़ बहादुर जी सिखों के वास्तविक गुरु हैं ?
(i) मक्खन शाह मसतूआना
(ii) मक्खन शाह लुबाणा
(iii) बाबा बुड्डा जी
(iv) भाई गुरदास जी।
उत्तर-
(i)

प्रश्न 9.
गुरु तेग़ बहादुर जी गुरुगद्दी पर कब विराजमान हुए ?
(i) 1661 ई० में
(ii) 1664 ई० में
(iii) 1665 ई० में
(iv) 1666 ई० में।
उत्तर-
(ii)
प्रश्न 10.
गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रा के समय सबसे पहले कहाँ पहुँचे. ?
(i) गोइंदवाल साहिब
(ii) खडूर साहिब
(iii) अमृतसर
(iv) कीरतपुर साहिब।
उत्तर-
(iii)
प्रश्न 11.
1665 ई० में गुरु तेग़ बहादुर जी ने किस नए नगर की स्थापना की थी ?
(i) चक्क नानकी
(ii) बिलासपुर
(iii) साहनेवाल
(iv) कीरतपुर साहिब।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 12.
चक्क नानकी बाद में किस नाम के साथ प्रसिद्ध हुआ ?
(i) श्री आनंदपुर साहिब
(ii) कीरतपुर साहिब
(iii) चमकौर साहिब
(iv) गोइंदवाल साहिब।
उत्तर-
(i)

प्रश्न 13.
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी का मुख्य कारण क्या था ?
(i) औरंगजेब की कट्टरता
(ii) कश्मीरी पंडितों की पुकार
(iii) नक्शबंदियों का विरोध
(iv) राम राय की शत्रुता।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 14.
किस मुगल बादशाह के आदेशानुसार गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया ?
(i) जहाँगीर
(ii) शाहजहाँ
(iii) औरंगजेब
(iv) बहादुरशाह प्रथम।
उत्तर-
(iii)
प्रश्न 15.
गुरु तेग बहादुर जी को कहाँ शहीद किया गया ?
(i) लाहौर में
(ii) दिल्ली में
(iii) अमृतसर में
(iv) पटना में।
उत्तर-
(ii)
प्रश्न 16.
गुरु तेग़ बहादुर जी को कब शहीद किया गया ?
(i) 1661 ई० में
(ii) 1664 ई० में
(iii) 1665 ई० में
(iv) 1675 ई० में।
उत्तर-
(iv)

प्रश्न 17.
गुरु तेग़ बहादुर जी को जिस स्थान पर शहीद किया गया वहाँ पर कौन-सा गुरुद्वारा स्थित है ? ”
(i) शीश गंज
(ii) रकाब गंज
(iii) बाला साहिब
(iv) दरबार साहिब।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 18.
‘हिंद की चादर’ नामक शब्द किस गुरु के लिए प्रयोग किए जाते हैं ?
(i) गुरु अर्जन देव जी
(ii) गुरु हरगोबिंद जी
(iii) गुरु तेग़ बहादुर जी
(iv) गुरु गोबिंद सिंह जी।
उत्तर-
(iii)
Long Answer Type Question
प्रश्न 1.
किस श्रद्धालु सिख ने नवम् गुरु की तलाश की और क्यों ? (Name the sincere Sikh, who searched for the Ninth Guru and why ?)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी को किसने ढूँढ़ा और क्यों ?
(Who found Guru Tegh Bahadur Ji and why ?)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की तलाश किसने और क्यों की ? (Who discovered the ninth Guru Tegh Bahadur Ji and how ?)
उत्तर-
1664 ई० में दिल्ली में ज्योति-जोत समाने से पूर्व गुरु हर कृष्ण जी ने सिख संगतों को यह संकेत दिया कि उनका अगला गुरु बाबा बकाला में है। जब यह समाचार बाबा बकाला पहुँचा कि गुरु साहिब आगामी गुरु का नाम बताए बिना ज्योति-जोत समा गए हैं तो 22. सोढियों ने वहाँ अपनी 22 मंजियाँ स्थापित कर लीं। हर कोई स्वयं को गुरु कहलवाने लगा। ऐसे समय में मक्खन शाह लुबाणा नामक एक सिख ने इसका समाधान ढूंढा। वह एक व्यापारी था। एक बार जब उसका जहाज समुद्री तूफान में घिर कर डूबने लंगा तो उसने अरदास की कि यदि उसका जहाज़ किनारे पर पहुँच जाए तो वह गुरु साहिब के चरणों में सोने की 500 मोहरें भेट करेगा। गुरु साहिब की कृपा से उसका जहाज़ बच गया। वह गुरु साहिब को 500 मोहरें भेट करने के लिए सपरिवार बाबा बकाला पहुँचा। यहाँ वह 22 गुरु देख कर चकित रह गया। उसने वास्तविक गुरु को ढूंढने की एक योजना बनाई। वह बारी-बारी प्रत्येक गुरु के पास गया तथा उन्हें दो-दो मोहरें भेट करता गया। झूठे गुरु दो-दो मोहरें लेकर प्रसन्न हो गए। जब मक्खन शाह ने अंत में तेग़ बहादुर जी के पास जाकर दो मोहरें भेट की तो गुरु साहिब ने कहा, “जहाज़ डूबते समय तो तूने 500 मोहरें भेट करने का वचन दिया था, परंतु अब केवल दो मोहरें ही भेट कर रहा है।” यह सुनकर मक्खन शाह बहुत प्रसन्न हुआ और वह एक मकान की छत पर चढ़ कर ज़ोर-ज़ोर से कहने लगा “गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे।” अर्थात् गुरु मिल गया है। इस प्रकार सिख संगतों ने गुरु तेग़ बहादुर को अपना गुरु स्वीकार कर लिया।

प्रश्न 2.
गुरु तेग बहादुर जी की यात्राओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। (Give a brief account of the travels of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग बहादुर जी की यात्राओं के संबंध में आप क्या जानते हैं ? ‘ (What do you know about the travels of Guru Tegh Bahadur Ji ?)
उत्तर-
गुरु तेग़ बहादुर साहिब ने अपनी गुरुगद्दी के समय (1664-75 ई०) के दौरान पंजाब और पंजाब से बाहर के प्रदेशों की यात्राएँ कीं। इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों में फैली अज्ञानता को दूर करना और सिख धर्म का प्रचार करना था। गुरु साहिब ने अपनी यात्राएँ 1664 ई० में अमृतसर से आरंभ की। तत्पश्चात् गुरु साहिब ने वल्ला, घुक्केवाली, खडूर साहिब, गोइंदवाल साहिब, तरनतारन, खेमकरन, कीरतपुर साहिब और बिलासपुर इत्यादि पंजाब के प्रदेशों की यात्राएँ कीं। पंजाब की यात्राओं के पश्चात् गुरु तेग़ बहादुर साहिब पूर्वी भारत की यात्राओं पर निकल पड़े। अपनी इस यात्रा के दौरान गुरु साहिब सैफाबाद, धमधान, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, कानपुर, प्रयाग, बनारस, गया, पटना, ढाका और असम इत्यादि स्थानों पर गए। इन यात्राओं के पश्चात् गुरु तेग़ बहादुर साहिब अपने परिवार सहित पंजाब आ गए। यहाँ पर आकर गुरु साहिब ने एक बार फिर पंजाब के विख्यात स्थानों की यात्राएँ की। गुरु साहिब की ये यात्राएँ सिख-पंथ के विकास के लिए बहुत लाभप्रद प्रमाणित हुईं। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग सिख मत में सम्मिलित हुए।
प्रश्न 3.
गुरु तेग़ बहादुर जी की किन्हीं छः यात्राओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। (Give a brief account of any six travels of Guru Tegh Bahadur Ji.)
उत्तर-
1664 ई० में गुरुगद्दी पर विराजमान होने के शीघ्र पश्चात् गुरु तेग़ बहादुर जी ने सिख धर्म के प्रचार के लिए पंजाब तथा पंजाब से बाहर की यात्राएँ आरंभ कर दीं। इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों को सत्य तथा प्रेम का संदेश देना था।—
1. अमृतसर-गुरु तेग़ बहादुर जी ने अपनी यात्राओं का आरंभ 1664 ई० में अमृतसर से किया। उस समय हरिमंदिर साहिब में पृथी चंद का पौत्र हरजी मीणा कुछ भ्रष्टाचारी मसंदों के साथ मिलकर स्वयं गुरु बना बैठा था। गुरु साहिब के आने की सूचना मिलते ही उसने हरिमंदिर साहिब के सभी द्वार बंद करवा दिए। जब गुरु साहिब वहाँ पहुँचे तो द्वार बंद देखकर उन्हें दुःख हुआ। अतः वह अकाल तख्त के निकट एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। यहाँ पर अब एक छोटा-सा गुरुद्वारा बना हुआ है जिसे ‘थम्म साहिब’ कहते हैं।
2. वल्ला तथा घुक्केवाली-अमृतसर से गुरु तेग़ बहादुर जी वल्ला नामक गाँव गए। यहाँ लंगर में महिलाओं की अथक सेवा से प्रसन्न होकर गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा कहा “माईयाँ रब्ब रजाईयां”। वल्ला के पश्चात् गुरु जी घुक्केवाली गाँव गए। इस गाँव में अनगिनत वृक्षों के कारण गुरु जी ने इसका नाम ‘गुरु का बाग’ रख दिया।
3. बनारस-प्रयाग की यात्रा के पश्चात् गुरु तेग़ बहादुर जी बनारस पहुँचे यहाँ सिख संगतें प्रतिदिन बड़ी संख्या में गुरु साहिब के दर्शन और उनके उपदेश सुनने के लिए उपस्थित होतीं। यहाँ के लोगों का विश्वास था कि कर्मनाशा नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति के सभी अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। गुरु साहिब ने स्वयं इस नदी में स्नान किया और कहा कि नदी में स्नान करने से कुछ नहीं होता मनुष्य जैसे कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है।
4. पटना-गुरु तेग़ बहादुर जी 1666 ई० में पटना पहुंचे। यहाँ पर सिख संगतों (श्रद्धालुओं) ने गुरु साहिब का भव्य स्वागत किया। गुरु साहिब ने सिख सिद्धांतों पर प्रकाश डाला तथा पटना को ‘गुरु का घर’ कहकर सम्मानित किया। गुरु साहिब ने अपनी पत्नी और माता जी को यहाँ छोड़कर स्वयं मुंघेर के लिए प्रस्थान किया।
5. मथुरा-गुरु तेग़ बहादुर जी दिल्ली के पश्चात् मथुरा पहुंचे। यहाँ गुरु जी ने धर्म प्रचार किया तथा संगतों को उपदेश दिए। गुरु जी के उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उनके श्रद्धालु बन गए।
6. ढाका-ढाका पूर्वी भारत में सिख धर्म का एक प्रमुख प्रचार केंद्र था। गुरु तेग़ बहादुर जी के आगमन के कारण बड़ी संख्या में लोग सिख-धर्म में शामिल हुए। गुरु साहिब ने यहाँ संगतों को जाति-पाति के बंधनों से ऊपर उठने और नाम सिमरिन से जुड़ने का संदेश दिया।

प्रश्न 4.
गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के कारणों के बारे में आप क्या जानते हैं ?
(What do you know about the causes of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur ji ?)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के क्या कारण थे ?
(What were the causes of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji ?)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करें। (Study the causes responsible for the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
उत्तर-
गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त विवरण अग्रलिखित अनुसार है—
1. मुग़लों और सिखों में शत्रुता-1605 ई० तक सिखों और मुग़लों में मैत्रीपूर्ण संबंध चले आ रहे थे, परंतु जब 1606 ई० में मुगल सम्राट् जहाँगीर ने गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया तो ये संबंध शत्रुता में बदल गए। औरंगज़ेब के शासनकाल में सिखों और मुग़लों के बीच शत्रुता में और वृद्धि हो गई। यही शत्रुता गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान का एक प्रमुख कारण बनी।
2. औरंगजेब की कट्टरता-औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता भी गुरु साहिब के बलिदान का प्रमुख कारण बनी। औरंगज़ेब 1658 ई० में मुग़लों का नया बादशाह बना था। वह भारत में चारों ओर इस्लाम धर्म का बोलबाला देखना चाहता था। अतः तलवार के बल पर लोगों को बलपूर्वक इस्लाम धर्म में सम्मिलित किया जाने लगा।
3. नक्शबंदियों का औरंगजेब पर प्रभाव-कट्टर सुन्नी मुसलमानों के नक्शबंदी संप्रदाय का औरंगज़ेब पर बहुत प्रभाव था। इस संप्रदाय के लिए गुरु साहिब की बढ़ रही ख्याति असहनीय थी। नक्शबंदियों को यह ख़तरा हो गया कि कहीं सिख धर्म का विकास इस्लाम के लिए कोई गंभीर चुनौती न बन जाए। इसलिए उन्होंने सिखों के विरुद्ध औरंगज़ेब को भड़काना आरंभ कर दिया।
4. सिख धर्म का प्रचार—गुरु तेग बहादुर साहिब की सिख धर्म के प्रचार के लिए की गई यात्राओं से प्रभावित होकर हज़ारों लोग सिख मत में सम्मिलित हो गए थे। गुरु साहिब जी ने सिख मत के प्रचार में तीव्रता और योग्यता लाने के लिए सिख प्रचारक नियुक्त किए तथा उन्हें संगठित किया। सिख धर्म का हो रहा विकास तथा उसका संगठन औरंगज़ेब की सहन शक्ति से बाहर था।
5. राम राय की शत्रुता-राम राय गुरु हर राय जी का बड़ा पुत्र था। वह स्वयं को गुरुगद्दी का अधिकारी समझता था। परंतु जब गुरुगद्दी पहले गुरु हरकृष्ण जी को तथा इसके पश्चात् गुरु तेग़ बहादुर जी को मिली तो वह यह सहन न कर पाया। फलस्वरूप उसने औरंगजेब के गुरु तेग़ बहादुर जी के विरुद्ध कान भरने आरंभ कर दिए।
6. कश्मीरी पंडितों की पुकार-कश्मीर के गवर्नर शेर अफ़गान ने इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए ब्राह्मणों पर घोर अत्याचार किए। जब उन्हें अपने धर्म के बचाव का कोई मार्ग दिखाई न दिया तो पंडित कृपा राम के नेतृत्व में उनका एक दल मई, 1675 ई० में श्री आनंदपुर साहिब गुरु तेग़ बहादुर जी के पास अपनी करुण याचना लेकर पहुँचा। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि वे जाकर मुग़ल अधिकारियों को यह बता दें कि यदि वे गुरु तेग़ बहादुर को मुसलमान बना लें तो वे बिना किसी विरोध के इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे।
प्रश्न 5.
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी में नक्शबंदियों की भूमिका की समीक्षा कीजिए।
(Discuss the role played by Naqshbandis in the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
उत्तर-
नक्शबंदी कट्टर सुन्नी मुसलमानों का एक संप्रदाय था। इस संप्रदाय का औरंगजेब पर बहुत प्रभाव था। इस संप्रदाय के लिए गुरु साहिब की बढ़ रही ख्याति, सिख मत का बढ़ रहा प्रचार और मुसलमानों की गुरु घर के प्रति बढ़ रही प्रवृत्ति असहनीय थी। नक्शबंदियों को यह ख़तरा हो गया कि कहीं लोगों में आ रही जागृति और सिख धर्म का विकास इस्लाम के लिए कोई गंभीर चुनौती ही न बन जाए। ऐसा होने की दशा में भारत में मुस्लिम समाज की जड़ें हिल सकती थीं। इसलिए उन्होंने सिखों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए औरंगज़ेब को भड़काना आरंभ किया। उनकी इस कार्यवाही ने जलती पर तेल डालने का कार्य किया। उस समय शेख़ मासूम नक्शबंदियों का नेता था। वह अपने पिता शेख़ अहमद सरहिंदी से भी अधिक कट्टर था। उसका विचार था कि यदि पंजाब में सिखों का शीघ्र दमन नहीं किया गया तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डगमगा सकती है। परिणामस्वरूप औरंगज़ेब ने गुरु जी के विरुद्ध कदम उठाने का निर्णय किया। निस्संदेह हम कह सकते हैं कि गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी में नक्शबंदियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

प्रश्न 6.
गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का तात्कालिक कारण क्या था ? (What was the immediate cause of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji ?)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी ने कश्मीरी ब्राह्मणों की सहायता क्यों की ? (Why did Guru Tegh Bahadur Ji help the Kashmiri Brahmins ?)
उत्तर-
कश्मीर में रहने वाले ब्राह्मणों का सारे भारत के हिंदू बहुत आदर करते थे। औरंगज़ेब ने सोचा कि यदि ब्राह्मणों को किसी प्रकार मुसलमान बना लिया जाए तो भारत के शेष हिंदू स्वयंमेव ही इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। इसी उद्देश्य से उसने शेर अफ़गान को कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया। शेर अफ़गान ने ब्राह्मणों को तलवार की नोक पर इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए विवश किया। जब उन्हें अपने धर्म के बचाव का कोई मार्ग दिखाई न दिया तो पंडित कृपा राम के नेतृत्व में उनका एक दल मई, 1675 ई० में श्री आनंदपुर साहिब गुरु तेग़ बहादुर जी के पास अपनी करुण याचना लेकर पहुँचा। जब गुरु जी ने उनकी रौंगटे खड़े कर देने वाली अत्याचारों की कहानी सुनी तो वह सोच में पड़ गए। गुरु साहिब के मुख पर गंभीरता देख बालक गोबिंद राय जो उस समय 9 वर्ष के थे, ने पिता जी से इसका कारण पूछा। गुरु साहिब ने बताया कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। बालक गोबिंद राय ने झट से कहा, “पिता जी आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है ?” बालक के मुख से यह उत्तर सुन कर गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना बलिदान देने का निर्णय कर लिया। गुरु जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि वे जाकर मुग़ल अधिकारियों को बता दें कि यदि वे गुरु तेग़ बहादुर को मुसलमान बना लें तो वे इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे। जब औरंगज़ेब को इस बात का पता चला तो उसने गुरु जी को दिल्ली बुलाकर मुसलमान बनाने का निश्चय किया।
प्रश्न 7.
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के ऐतिहासिक महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए। (Evaluate the historical importance of martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के छः महत्त्वपूर्ण नतीजों का वर्णन करो। (Explain six significant results of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji.)
अथवा
गुरु तेग़ बहादुर जी की शहीदी के छः परिणाम बताएँ। (What were the six results of the martyrdom of Guru Tegh Bahadur ?)
उत्तर-
गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान की घटना न केवल सिख इतिहास अपितु समूचे विश्व इतिहास की एक अतुलनीय घटना है। इस बलिदान से न केवल पंजाब, अपितु भारत के इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पड़े। गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के साथ ही महान् मुग़ल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया।—
1. इतिहास की एक अद्वितीय घटना–संसार का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। ये बलिदान अधिकतर अपने धर्म की रक्षा अथवा देश के लिए दिए गए। परंतु गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता तथा सत्य के लिए अपना शीश दिया। निस्संदेह संसार के इतिहास में यह एक अतुलनीय उदाहरण थी। इसी कारण गुरु तेग़ बहादुर जी को ‘हिंद की चादर’ कहा जाता है।
2. सिखों में प्रतिशोध की भावना-गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के फलस्वरूप समूचे पंजाब में मुग़ल साम्राज्य के प्रति रोष की लहर दौड़ गई। अतः सिखों ने मुग़लों के अत्याचारी शासन का अंत करने का निर्णय किया।
3. हिंदू धर्म की रक्षा औरंगज़ेब के दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे अत्याचारों से तंग आकर बहत-से हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करना आरंभ कर दिया था। हिंदू धर्म के अस्तित्व के लिए भारी ख़तरा उत्पन्न हो चुका था। ऐसे समय में गुरु तेग़ बहादुर जी ने अपना बलिदान देकर हिंदू धर्म को लुप्त होने से बचा लिया।
4. खालसा का सृजन-गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने सिखों को यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब धर्म की रक्षा के लिए उनका संगठित होना अत्यावश्यक है। इस उद्देश्य से गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ई० में बैसाखी के दिन खालसा पंथ का सृजन किया। खालसा पंथ के सृजन ने ऐसी बहादुर जाति को जन्म दिया जिसने मुग़लों और अफ़गानों का पंजाब से नामो-निशान मिटा दिया।
5. सिखों और मुग़लों में लड़ाइयाँ—गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के पश्चात् सिखों एवं मुग़लों के बीच लड़ाइयों का एक लंबा दौर आरंभ हुआ। इन लड़ाइयों के दौरान सिख चट्टान की तरह अडिग रहे। अपने सीमित साधनों के बावजूद सिखों ने अपनी वीरता के कारण महान् मुग़ल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया।
6. बलिदानों की परंपरा का आरंभ होना-गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान के पश्चात् सिखों में धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने की परंपरा आरंभ हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी चार साहिबजादे, बंदा सिंह बहादुर तथा अनेक श्रद्धालु सिखों ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए। गुरु तेग़ बहादुर जी का बलिदान आने वाली नस्लों के लिए अद्धितीय उदाहरण सिद्ध हुआ।

प्रश्न 8.
भाई मती दास जी और भाई सती दास जी पर संक्षिप्त नोट लिखें। (Write a comprehensive note on Bhai Mati Das Ji and Bhai Sati Das Ji.)
उत्तर-
सिख इतिहास शहीदियों से भरा पड़ा है। परंतु जो अद्वितीय शहीदी भाई मती दास जी तथा भाई सती दास जी ने दी उसकी कोई अन्य उदाहरण मिलना कठिन है। भाई मती दास जी तथा भाई सती दास जी दोनों भाई थे। भाई मती दास जी गुरु तेग बहादुर जी के दीवान थे जबकि भाई सती दास जी फ़ारसी के लेखक थे। जब गुरु तेग़ बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने का निर्णय किया तो भाई मती दास जी और भाई सती दास जी भी उनके साथ हो लिए। जब शासकों ने दिल्ली में गुरु तेग़ बहादुर जी से अपमानजनक व्यवहार किया तो भाई मती दास जी इसे सहन न कर सके। उन्होंने गुरु जी से यह प्रार्थना की कि यदि वह आज्ञा दें तो मुग़ल शासन को तहस-नहस कर दिया जाए। गुरु जी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। उनका कथन था कि सब कुछ उस परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हो रहा है। आप चिन्ता न करें परमात्मा उन्हें अवश्य मज़ा चखाएगा। अत्याचारी काज़ी ने भाई मती दास जी तथा भाई सती दास जी को इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत-से प्रलोभन दिए परंतु वे अपने धर्म पर पक्के रहे। अंत में भाई मती दास जी को आरों के साथ, दो भाग कर दिया गया था तथा भाई सती दास जी को रूई में लिपटा कर आग लगा कर शहीद कर दिया गया। इनकी शहीदी ने सिख इतिहास में नए कार्तिमान स्थापित किए।
Source Based Questions
नोट-निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके अंत में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
1
गुरु तेग़ बहादुर जी सिखों के नवम् गुरु थे। वे 1664 ई० से लेकर 1675 ई० तक गुरुगद्दी पर आसीन रहे। सिख धर्म का प्रचार एवं लोगों में फैले अंधविश्वासों को दूर करने के लिए गुरु साहिब ने पंजाब एवं पंजाब से बाहर अनेक स्थानों की यात्राएँ की। उस समय भारत में मुग़ल सम्राट् औरंगजेब का शासन था। वह बड़ा कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदुओं को इस्लाम धर्म में सम्मिलित करने के उद्देश्य से समस्त भारत में आतंक फैला रखा था। कश्मीरी पंडित उसके अत्याचारों का सर्वाधिक शिकार हुए। गुरु तेग़ बहादुर जी ने हिंदुओं के धर्म की रक्षा के लिए 11 नवंबर, 1675 ई० को दिल्ली में अपना बलिदान दिया। गुरु साहिब के इस अद्वितीय बलिदान के बहुत दूरगामी परिणाम निकले। इसने न केवल पंजाब, बल्कि भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान ने पंजाब में एक ऐसी चिंगारी सुलगाई जिसने शीघ्र ही ज्वाला का रूप धारण कर लिया और जिसमें शक्तिशाली मुग़ल साम्राज्य जलकर भस्म हो गया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी द्वारा अपना बलिदान देने के कारण उन्हें इतिहास में ‘हिंद की चादर’ के नाम से भी स्मरण किया जाता है।
- गुरु तेग़ बहादुर जी गुरुगद्दी पर कब बैठे ?
- गुरु तेग़ बहादुर जी की यात्राओं का उद्देश्य क्या था ?
- गुरु तेग बहादुर जी को किस मुगल बादशाह ने शहीद करने का आदेश दिया था ?
- गुरु तेग बहादुर जी को कहाँ शहीद किया गया था ?
- लाहौर
- दिल्ली
- अमृतसर
- उपरोक्त में से कोई नहीं।
- गुरु तेग़ बहादुर जी को हिंद की चादर क्यों कहा जाता है ?
उत्तर-
- गुरु तेग़ बहादुर जी 1664 ई० में गुरुगद्दी पर बैठे।
- सिख धर्म का प्रचार करना।
- मुग़ल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग़ बहादुर जी को शहीद किया गया था।
- दिल्ली।
- गुरु तेग़ बहादुर जी को हिंद की चादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी थी।
2
कश्मीर में रहने वाले ब्राह्मण अपने धर्म और प्राचीन संस्कृति के संबंध में बहुत दृढ़ थे। सारे भारत के हिंदू उनका बहुत आदर करते थे। औरंगज़ेब ने सोचा कि यदि ब्राह्मणों को किसी प्रकार मुसलमान बना लिया जाए तो भारत के शेष हिंदू स्वयंमेव ही इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। इसी उद्देश्य से उसने शेर अफ़गान को कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया। शेर अफ़गान ने ब्राह्मणों को इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए विवश किया। इंकार करने वाले ब्राह्मणों पर घोर अत्याचार किए जाते और प्रतिदिन बड़ी संख्या में उनका वध किया जाने लगा। जब उन्हें अपने धर्म के बचाव का कोई मार्ग दिखाई न दिया तो पंडित कृपा राम के नेतृत्व में उनका 16 सदस्यों का एक दल 25 मई, 1675 ई० में चक्क नानकी (श्री आनंदपुर साहिब) में गुरु तेग़ बहादुर जी के पास अपनी करुण याचना लेकर पहुंचा।
- शेर अफ़गान कौन था ?
- शेर अफ़गान क्यों बदनाम था ?
- किसके नेतृत्त्व अधीन कश्मीरी पंडितों का एक गुट गुरु तेग़ बहादुर जी के पास अपनी दुख भरी फरियाद लेकर पहुंचा था ?
- कश्मीर के ब्राह्मण गुरु तेग़ बहादुर जी को कहाँ मिले ?
- लाहौर
- अमृतसर
- चक्क नानकी
- जालंधर।
- चक्क नानकी का आधुनिक नाम क्या है ?
उत्तर-
- शेर अफ़गान कश्मीर का गवर्नर था।
- उसने कश्मीरी पंडितों पर भारी अत्याचार किए।
- पंडित कृपा राम के नेतृत्व के अधीन कश्मीरी पंडितों का एक गुट गुरु तेग़ बहादुर जी के पास अपनी दुख भरी फरियाद लेकर आया था।
- चक्क नानकी।
- चक्क नानकी का आधुनिक नाम श्री आनंदपुर साहिब है।

गुरु तेग़ बहादुर जी और उनका बलिदान PSEB 12th Class History Notes
- प्रारंभिक जीवन (Early Career)—गुरु तेग़ बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल, 1621 ई० को अमृतसर में हुआ–आपके पिता जी का नाम गुरु हरगोबिंद जी तथा माता जी का नाम नानकी थागुरु तेग़ बहादुर जी ने बाबा बुड्डा जी और भाई गुरदास जी से शिक्षा प्राप्त की-गुरु जी का विवाह करतारपुर. वासी लाल चंद की सुपुत्री गुजरी से हुआ-अपने पिता जी के आदेश पर गुरु जी 20 वर्ष तक बकाला में रहे-मक्खन शाह लुबाणा द्वारा उन्हें ढूंह निकालने पर सिखों ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया-वे 1664 ई० में गुरुगद्दी पर विराजमान हुए।
- गुरु तेग़ बहादुर जी की यात्राएँ (Travels of Guru Tegh Bahadur Ji)-गुरु पद संभालने के पश्चात् गुरु तेग़ बहादुर जी ने पंजाब तथा बाहर के प्रदेशों के अनेक स्थानों की यात्राएँ की-इन यात्राओं का उद्देश्य सिख धर्म का प्रचार करना तथा सत्य और प्रेम का संदेश देना था-गुरु जी ने सर्वप्रथम 1664 ई० में पंजाब के अमृतसर, वल्ला, घुक्केवाली, खडूर साहिब, गोइंदवाल साहिब, तरनतारन, कीरतपुर साहिब और बिलासपुर आदि प्रदेशों की यात्रा की-इसके उपरांत गुरु जी पूर्वी भारत के सैफाबाद, धमधान, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, कानपुर, बनारस, गया, पटना, ढाका तथा असम की यात्रा पर गए-1673 ई० में गुरु तेग़ बहादुर ने पंजाब के मालवा और बांगर प्रदेश की दूसरी बार यात्रा की-इन यात्राओं से गुरु साहिब तथा सिख धर्म की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई।
- गुरु तेग़ बहादुर जी का बलिदान (Martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji)-गुरु तेग़ बहादुर जी के बलिदान से संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं—
- कारण (Causes)-सिखों तथा मुग़लों में शत्रुता बढ़ती जा रही थी-औरंगज़ेब बड़ा कट्टर सुन्नी मुसलमान था-नक्शबंदियों ने सिखों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए औरंगजेब को खूब भड़कायारामराय गुरुगद्दी की प्राप्ति के लिए कई हथकंडे अपना रहा था-कश्मीरी पंडितों ने गुरु साहिब से अपने धर्म की रक्षा के लिए सहायता माँगी।
- बलिदान (Martyrdom)-गुरु तेग़ बहादुर जी को अपने तीन साथियों-भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी के साथ 6 नवंबर, 1675 ई० को दिल्ली दरबार में पेश किया गया-उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा गया जिसका उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इंकार कर दियागुरु जी के तीनों साथियों को शहीद करने के बाद 11 नवंबर, 1675 ई० को दिल्ली के चाँदनी चौक में गुरु साहिब को शहीद कर दिया गया।
- महत्त्व (Importance)—समूचे पंजाब में मुग़ल साम्राज्य के प्रति घृणा और प्रतिशोध की लहर दौड़ गई–हिंदू धर्म को लुप्त होने से बचा लिया गया-गुरु गोबिंद सिंह जी को खालसा पंथ की स्थापना की प्रेरणा मिली-सिखों में धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने की एक परंपरा आरंभ हो गई-मुग़ल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया।
![]()
![]()
![]()
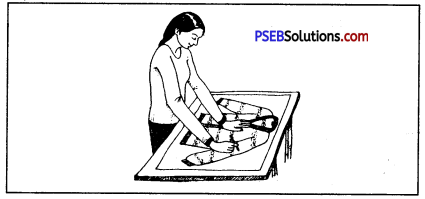
![]()
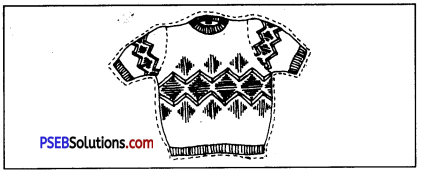
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
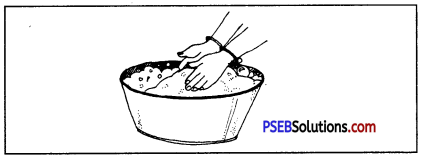
![]()
![]()
![]()