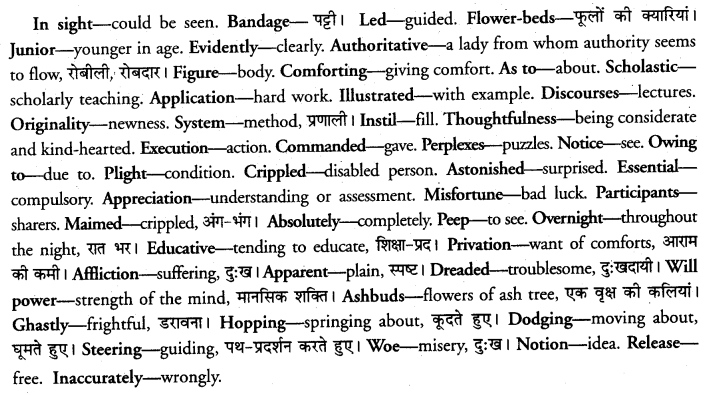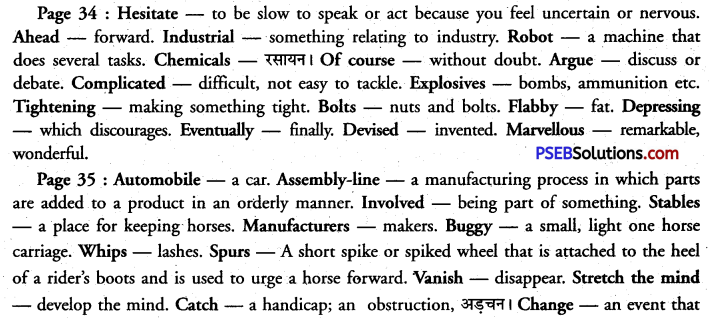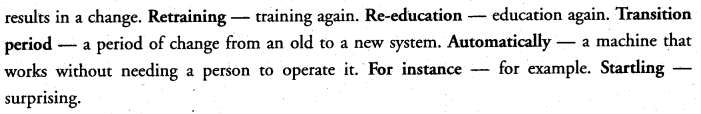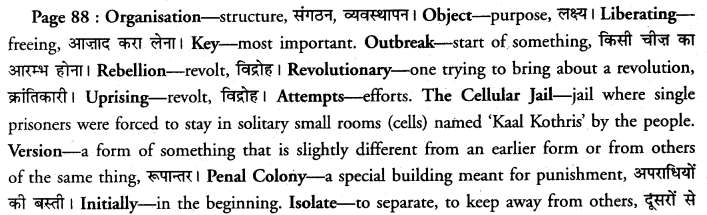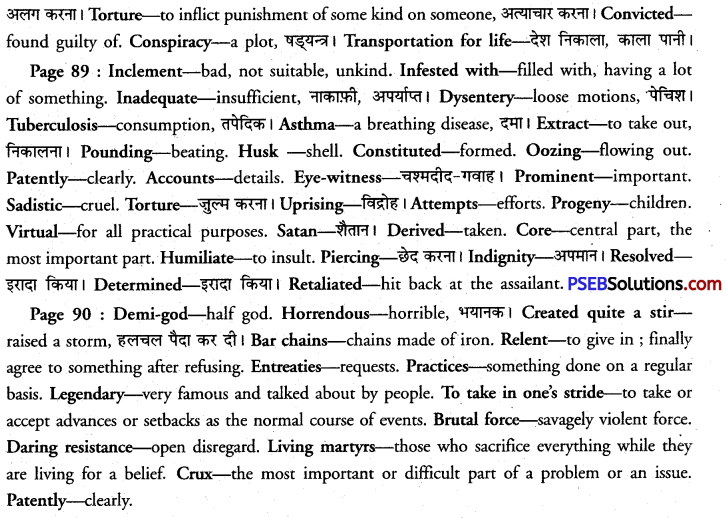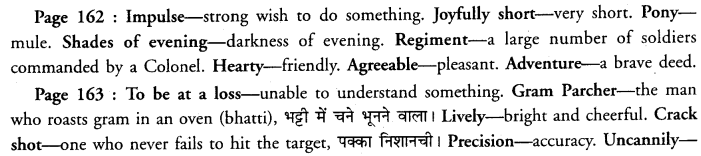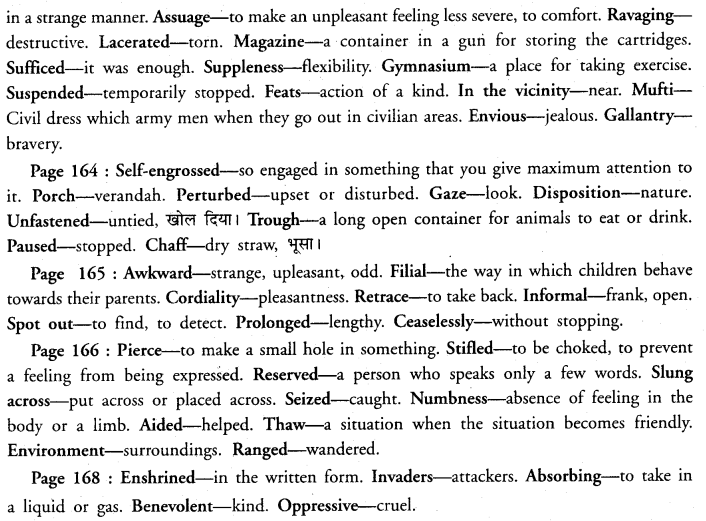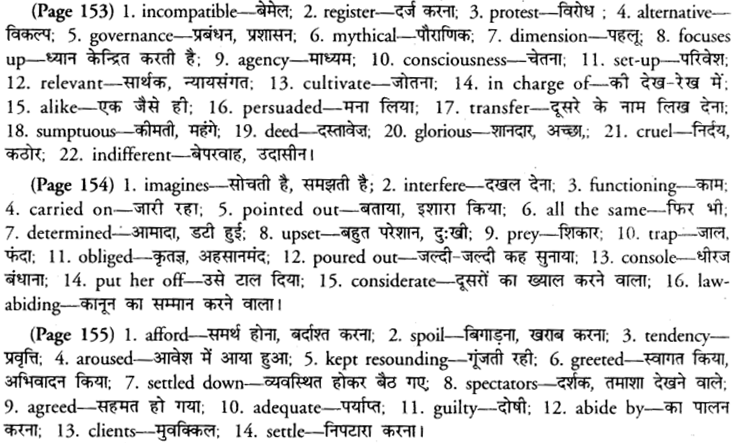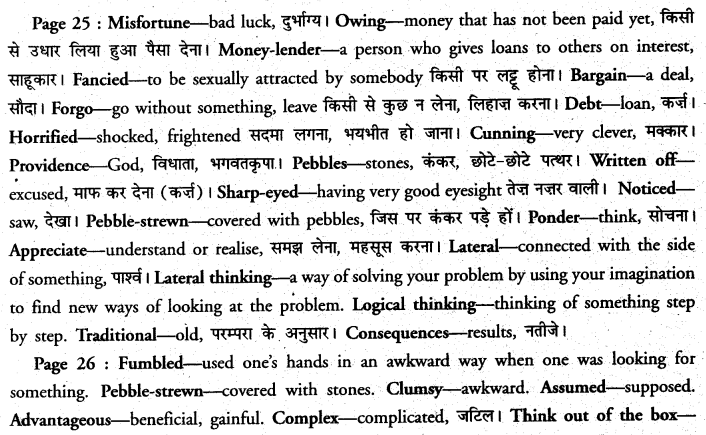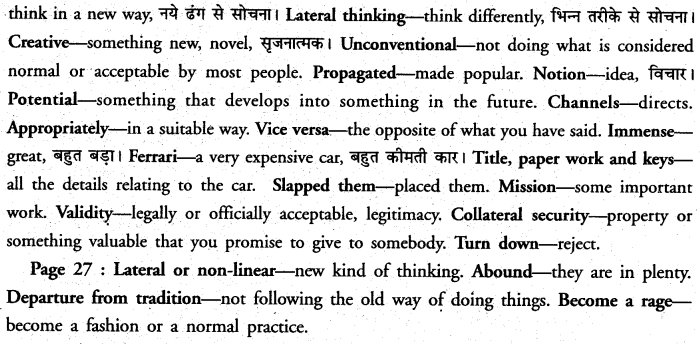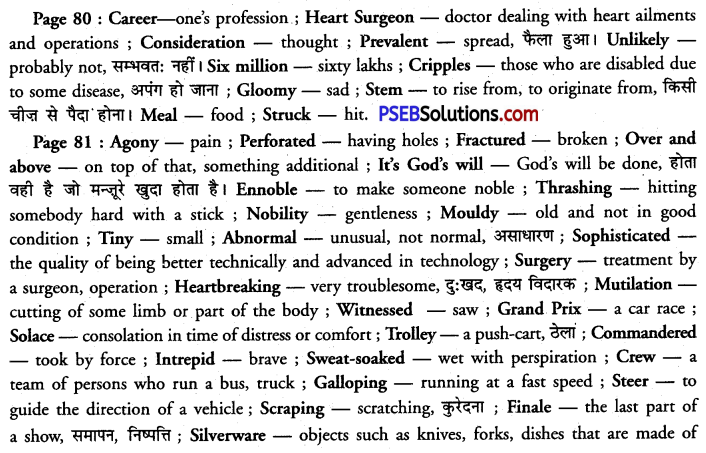Punjab State Board PSEB 11th Class English Book Solutions Chapter 4 Liberty and Discipline Textbook Exercise Questions and Answers.
Class 11th English Book Chapter 4 Liberty and Discipline Question Answers
Liberty and Discipline Class 11 Questions and Answers
Short Answer Type Questions
Question 1.
How does the author define liberty’ ?
Answer:
‘Liberty’ is the freedom to think what we like, say what we like, work at what we like and go where we like. Liberty is the birthright of each and every person. But even then, it is not a personal affair. It is a compromise or social contract.
‘लिबर्टी’ आज़ादी है – वह सोचने की जो हम सोचना चाहते हैं, वह कहने की जो हम कहना चाहते हैं, वह काम करने की जो हम करना चाहते हैं और वहां जाने की जहां हम जाना चाहते हैं। स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होती है। परन्तु फिर भी यह कोई निजी विषय नहीं होता। यह एक समझौता अथवा एक सामाजिक इकरारनामा होता है।

Question 2.
What is discipline ?
Answer:
Discipline is restraint on liberty. It trains people to obey rules and orders and punishes them if they don’t do. Discipline is very necessary in every field of society. It is only discipline that enables men to live in a society and yet retain individual liberty.
अनुशासन स्वतन्त्रता पर लगाई गई एक पाबन्दी है। यह लोगों को नियमों तथा आदेशों का पालन करने में प्रशिक्षित करता है और यदि वे ऐसा न करें तो उन्हें दण्ड देता है। समाज के हर क्षेत्र में अनुशासन बहुत जरूरी है। यह केवल अनुशासन ही है जो व्यक्ति को समाज में रहने और फिर भी अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कायम रखने के योग्य बनाता है।
Question 3.
Why should one keep to the left ?
Answer:
Keeping to the left while going on a road is the rule of the road. We should obey this rule of the road not only for our own advantage, but also for the rights of others. If we don’t do so, we will not only endanger others, but ourselves also.
सड़क पर जाते समय बाएं तरफ चलना सड़क का नियम है। हमें सड़क के इस नियम का पालन सिर्फ अपने फायदे के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के अधिकारों के लिहाज से भी करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी खतरे में डालते हैं।
Question 4.
How does pure discipline differ from enforced discipline ?
Answer:
The discipline that comes from our inside is pure discipline. And the discipline that is enforced on us from outside is enforced discipline. Since discipline is a restraint on liberty, it is quite natural that man has an inclination to avoid this restraint.
वह अनुशासन जो हमारे अन्दर से उठता है, वह शुद्ध अनुशासन होता है। और वह अनुशासन जो बाहर से हम पर थोपा जाता है, वह बाध्यकारी (जबरदस्ती लागू किया गया) अनुशासन होता है। क्योंकि अनुशासन स्वतन्त्रता पर लगा एक प्रतिबन्ध होता है, इसलिए यह बहुत स्वाभाविक है कि मनुष्य के अन्दर इस प्रतिबन्ध को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति होती है ।

Question 5.
What types of liberty do the British believe in ?
Answer:
The British believe in four types of liberty. They want the liberty to think what they like. They want the liberty to say what they like. They want to have liberty to work at what they like. They want to have the liberty to go where they like.
अंग्रेज चार किस्मों की स्वतन्त्रता में विश्वास रखते हैं। वह सोचने की आजादी चाहते हैं जो वे सोचना चाहें। वह कहने की आजादी चाहते हैं जो वे कहना चाहें। वह काम करने की आजादी चाहते हैं जो वे करना चाहें। वे वहां जाने की आजादी चाहते हैं जहां वे जाना चाहें।
Question 6.
Why does one have a natural inclination to avoid discipline ?
Answer:
Discipline trains people to obey rules and orders and punishes them if they don’t do so. It is a restraint on liberty. So it is quite natural that man has an inclination to avoid this restraint.
अनुशासन लोगों को नियमों और आदेशों का पालन करने की शिक्षा देता है और यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह उन्हें दण्ड देता है। यह स्वतन्त्रता पर लगा एक प्रतिबन्ध होता है। इसलिए यह बहुत स्वाभाविक है कि मनुष्य के अन्दर इस प्रतिबन्ध को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति होती है ।
Question 7.
Why is discipline unavoidable for a modern man ?
Answer:
Modern man lives in complex communities in which every person is dependent on others. So discipline is unavoidable for a modern man. If every man were free to do what he liked, there
would be chaos everywhere. So discipline is very necessary for modern man in every field of society.
आधुनिक मनुष्य मिश्रित समुदायों में रहता है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरों पर निर्भर करता है। इसलिए आधुनिक मनुष्य के लिए अनुशासन बहुत अनिवार्य है। यदि प्रत्येक व्यक्ति वही करने को आजाद हो जो वह करना चाहता है, तो सभी जगह अराजकता फैल जाएगी। इसलिए आधुनिक मनुष्य के लिए समाज के हर क्षेत्र में अनुशासन बहुत जरुरी हैं।
Question 8.
How did the author acknowledge the salute of a private soldier ?
Answer:
The author was a brand new second lieutenant at that time. Once he was walking on to parade. A private soldier passed him and saluted him. The author acknowledged the salute of that soldier with an airy wave of his hand.
उस समय लेखक नया-नया भर्ती हुआ सैकण्ड लेफ्टिनेंट था। एक दिन वह परेड के लिए जा रहा था। एक निचले दर्जे का सैनिक उसके पास से गुजरा और उसने उसे सलामी दी। लेखक ने उस सैनिक की सलामी का जवाब हवा में अपना हाथ लहराते हुए दिया ।

Question 9.
How did the Colonel punish the author for not returning a salute properly ?
Answer:
The Colonel rebuked the author for not returning a salute properly. He punished the author for this. He made the author march in front of the whole battalion and practise before the Sergeant Major’s cane how to return a salute. “Discipline begins with the officers,” he said to the author.
कर्नल ने सलामी का जवाब उचित ढंग से न देने के लिए लेखक को डांटा। उसने इसके लिए लेखक को दंडित किया। उसने लेखक से पूरी बटालियन के सामने मार्च करवाया और सार्जेंट मेजर के बेंत के आगे अभ्यास करवाया कि सलामी का जवाब कैसे दिया जाता है। “अनुशासन की शुरुआत अफसरों से होती है,” उसने लेखक से कहा।
Question 10.
What did the Colonel tell the author about discipline ?
Answer:
The author had not returned the salute of a private soldier properly. The Colonel rebuked him for this and also punished him. He made the author practise before the Sergeant Major’s cane how to return a salute. The Colonel told the author that discipline begins with the officers.
लेखक ने एक निजी सैनिक की सलामी का जवाब उचित ढंग से नहीं दिया था। कर्नल ने उसे इस बात के लिए डांटा और उसे सजा भी दी। उसने सार्जेन्ट मेजर के बेंत के आगे उससे अभ्यास भी करवाया कि सलामी का जवाब कैसे दिया जाता है। कर्नल ने लेखक को बताया कि अनुशासन की शुरुआत अफसरों से होती है ।
Question 11.
How can the leader build up the leadership of his team ?
Answer:
The leader can build up the leadership of his team on the discipline of understanding. In order to inculcate a sense of discipline in his team, he must first realize his own responsibility. He must display high standards of discipline in his own life. Only then he can succeed in building up the leadership of his team.
नेता अपने दल के नायकत्त्व का निर्माण आपसी समझ के अनुशासन के आधार पर कर सकता है। अपने दल में अनुशासन की भावना भरने के लिए एक नेता को सबसे पहले अपनी स्वयं की जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। उसे स्वयं के जीवन में अनुशासन के उच्च मापदण्डों का प्रदर्शन करना चाहिए। सिर्फ तभी वह अपने दल के नायकत्व का निर्माण करने में सफल हो सकता है।
Question 12.
What, according to the author, was not a new technique invented in the last war ?
Answer:
According to the author, taking men into one’s confidence was not a new technique invented in the last war. He says that leaders have always followed this technique to lead the people by winning their confidence. This art is a must in a successful leader. It helps in building a good rapport between the leader and his followers.
लेखक के अनुसार लोगों को अपने विश्वास में ले लेना पिछले युद्ध में खोजी गई कोई नई तकनीक नहीं थी। वह कहता है कि नेताओं ने लोगों का विश्वास जीत कर उनका नेतृत्व करने के लिए हमेशा ही इस तकनीक का अनुसरण किया है। एक सफल नेता में यह कला होना अनिवार्य है। यह नेता तथा उसके अनुचरों के बीच अच्छे संबंध पैदा करने में मदद करती है।
Question 13.
How can you say that discipline is not derogatory?
Answer:
It is only discipline that enables people to live in a community and yet retain individual liberty. It does put some check on our freedom, but it does not cut down our individual freedom. It makes man truly free. Totalitarian discipline with its slogan-shouting masses is deliberately designed to submerge the individual.
यह केवल अनुशासन ही है जो लोगों को समाज में रहने और फिर भी अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बनाए रखने के योग्य बनाता है। यह हमारी स्वतन्त्रता पर कुछ रोक अवश्य लगाता है, परन्तु यह हमारी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में कोई कटौती नहीं करता। यह व्यक्ति को सही अर्थों में स्वतन्त्र बनाता है। सर्वसत्तावादी अनुशासन, जिसमें नारेबाजी करती जनता शामिल होती है, का निर्माण पूर्ण विचार-विमर्श के साथ किया गया है, व्यक्ति को पूरी तरह से गायब कर देने के लिए।

Question 14.
What type of discipline is deliberately designed to submerge the individual ?
Answer:
Totalitarian discipline with its slogan-shouting masses is deliberately designed to submerge the individual. Totalitarian discipline means a system of government in which there is only one political party that has complete power and control over the people.
सर्वसत्तावादी अनुशासन, जिसमें नारेबाजी करती जनता शामिल होती है, का निर्माण पूर्ण विचार-विमर्श के साथ किया गया है, व्यक्ति को पूरी तरह से गायब कर देने के लिए। सर्वसत्तावादी अनुशासन का अर्थ है, सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिससे केवल एक राजनीतिक दल होता है जिसका लोगों के ऊपर सम्पूर्ण अधिकार एवं नियंत्रण होता है।
Question 15.
How does the author commend the role of British railway signalmen in the last war?
Answer:
The author says that in the blitz of the last war, not even a single British Railway signalman left his post. They stood in the heart of the target area. They didn’t leave their place. They put
their job before themselves. They knew the importance of their work for their country.
लेखक कहता है कि पिछले युद्ध में हुए हमलों के दौरान बरतानवी रेलवे सिग्नलमैनों में से एक भी व्यक्ति ने अपनी नियुक्त की गई जगह नहीं छोड़ी। वे लक्ष्य बनाई गई जगहों के बीचो-बीच पर डटे रहे। उन्होंने अपनी जगह न छोड़ी। उन्होंने अपने काम को अपने से पहले रखा। वे जानते थे कि उनके देश के लिए उनके काम का क्या महत्त्व था।
Question 16.
How can a nation overcome an economic or military crisis ?
Answer:
A nation can overcome an economic or military crisis with the help of discipline only. Any nation without discipline surely goes to the dogs. And no work or progress is possible without a disciplined living. Rather there is bound to be confusion, disorder and chaos.
सिर्फ अनुशासन की सहायता से ही एक राष्ट्र किसी आर्थिक अथवा सैन्य संकट से उभर सकता है। किसी भी ऐसे राष्ट्र की दुर्दशा होना निश्चित है जिसमें अनुशासन न हो। और अनुशासित जीवन के बिना कोई भी कार्य अथवा प्रगति संभव नहीं है। बल्कि वहां अफरा-तफरी, अव्यवस्था तथा अशांति होना निश्चित है।
Question 17.
What, according to the author, is meant by democracy ?
Answer:
According to the author, democracy means that responsibility is decentralised. And no one can avoid doing something he should do. He says that a nation can overcome an economic or military crisis with the help of discipline only.
लेखक के अनुसार, प्रजातन्त्र का अर्थ है कि ज़िम्मेदारी विकेन्द्रित होती है। और कोई भी उस काम को नज़रअंदाज नहीं कर सकता जो उसे करना चाहिए। वह कहता है कि सिर्फ अनुशासन की सहायता से ही एक राष्ट्र किसी आर्थिक अथवा सैन्य-संकट से उभर सकता है।
Question 18.
Why did the Colonel punish the author ?
Answer:
The author had acknowledged the salute of a private soldier with an airy wave of his hand. At this, his Colonel punished him for not returning a salute properly. He made the author march in front of the whole battalion and practise before the Sergeant Major’s cane how to return a salute.
लेखक ने एक निजी सैनिक की सलामी का जवाब हवा में अपना हाथ लहराते हुए दिया था। इस बात पर उसके कर्नल ने उसे सलामी का जवाब उचित प्रकार से न देने के लिए दंड दिया। उसने लेखक से पूरी बटालियन के सामने मार्च करवाया और सार्जेंट मेजर के बेंत के सामने अभ्यास करवाया कि सलामी का जवाब कैसे दिया जाता है।
Question 19.
What are the advantages of discipline ?
Answer:
Discipline is, in fact, the foundation of all freedom. It makes man truly free. It enables man to live in the society and yet retain individual liberty. It brings order in the society. It is only discipline which enables a nation to march on the way to progress.
वास्तव में, अनुशासन ही संपूर्ण स्वतन्त्रता की नींव होता है। यह मनुष्य को सही अर्थों में स्वतन्त्र बनाता है। यह मनुष्य को समाज में रहने और फिर भी अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कायम रखने के योग्य बनाता है। यह समाज में व्यवस्था लाता है। यह सिर्फ अनुशासन ही है जो किसी राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाता है।

Question 20.
What does indiscipline lead to ?
Answer:
Indiscipline leads to confusion and chaos in a society. It creates corruption, lawlessness and disorder all around. The evil elements in the society look for excuses to create violence. Security for the poor and the weak vanishes. In short, indiscipline eats into the roots of our moral, social and national life.
अनुशासनहीनता समाज में अफरा-तफरी तथा अशांति फैलाती है। यह हर तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता तथा अव्यवस्था फैलाती है। समाज में फैले बुरे तत्त्व हिंसात्मक कार्य करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। गरीब लोगों तथा कमज़ोरों के प्रति सुरक्षा गायब हो जाती है। संक्षेप में, अनुशासनहीनता हमारे नैतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन की जड़ों तक को खा जाती है।
Question 21.
What do you mean by totalitarian discipline?
Answer:
Totalitarian discipline means a system of government in which there is only one political party that has complete power and control over the people. Totalitarian discipline with its slogan-shouting masses is deliberately designed to submerge the individual.
सर्वसत्तावादी अनुशासन का अर्थ है, सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें सिर्फ एक राजनीतिक दल होता है जिसका लोगों के ऊपर सम्पूर्ण अधिकार तथा नियंत्रण होता है। सर्वसत्तावादी अनुशासन, जिसमें नारेबाजी करती जनता शामिल होती है, का निर्माण पूर्ण विचार-विमर्श के साथ किया गया है, व्यक्ति को पूरी तरह से गायब कर देने के लिए।
Question 22.
What great job did the British Railway signalmen do during the last war ?
Answer:
They never left their post during the war. They stood often in the heart of target areas where the bombs were dropped. They always put their job before themselves.
युद्ध के दौरान उन्होंने अपना स्थान बिल्कुल न छोड़ा। वे अक्सर उन लक्ष्य क्षेत्रों के मध्य में खड़े रहते थे जहां बम गिराए जाते थे। उन्होंने अपने काम को सदैव स्वयं से पहले रखा।
Long Answer Type Questions
Question 1.
How does history teach us the need of a disciplined living ? Explain.
Answer:
From history, we have learnt that whenever the sense of order or discipline fades in a nation, its economic life declines completely. Its standard of living falls and its security vanishes. Then the nation goes into the hands of either some more powerful militant power or a dictator.
In short, any nation without discipline surely goes to the dogs. And no work or progress is possible without a disciplined living. Rather there is bound to be confusion, disorder and chaos. Modern man lives in complex communities in which every person is dependent on others. So discipline is indispensable for a modern man.
इतिहास से हमने सीखा है कि जब भी किसी राष्ट्र में व्यवस्था अथवा अनुशासन की भावना लुप्त हो जाती है, तब इसके आर्थिक जीवन का पूरी तरह पतन हो जाता है। इसका जीवन-स्तर गिर जाता है तथा इसकी सुरक्षा गायब हो जाती है। फिर वह राष्ट्र या तो किसी अधिक ताकतवर लड़ाकू शक्ति के हाथों में चला जाता है या फिर किसी तानाशाह के हाथों में चला जाता है। संक्षेप में कहें तो किसी भी ऐसे राष्ट्र की दुर्दशा होना निश्चित है जिसमें अनुशासन न हो।
और अनुशासित जीवन के बिना कोई भी कार्य अथवा प्रगति संभव नहीं है। बल्कि वहां अफरा-तफरी, अव्यवस्था तथ अशांति होना निश्चित है। आधुनिक मनुष्य जटिल समुदायों में रहता है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर करता है। इसलिए आधुनिक मनुष्य के लिए अनुशासन बहुत अनिवार्य है।

Question 2.
What is the relationship between liberty and discipline ?
Answer:
“Liberty’ is the freedom to think what we like, say what we like, work at what we like and go where we like. Discipline is a restraint on liberty. It trains people to obey rules and orders and punishes them if they don’t do. Liberty is the birthright of each and every person. But even then, it is not a personal affair. It is a compromise or social contract.
If every man were free to do what he liked, there would be chaos everywhere. So discipline is very necessary in every field of society. It is only discipline that enables men to live in a society and yet retain individual liberty. We can have discipline without liberty, but we cannot have liberty without discipline.
‘लिबर्टी’ आज़ादी है वह सोचने की जो हम सोचना चाहते हैं, वह कहने की जो हम कहना चाहते हैं, वह काम करने की जो हम करना चाहते हैं और वहां जाने की जहां हम जाना चाहते हैं। अनुशासन स्वतन्त्रता पर लगाई गई एक पाबन्दी है। यह लोगों को नियमों तथा आदेशों का पालन करने में प्रशिक्षित करता है और यदि वे ऐसा न करें, तो उन्हें दण्ड देता है। स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होती है।
परन्तु फिर भी यह कोई निजी विषय नहीं होता। यह एक समझौता अथवा एक सामाजिक इकरारनामा होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति वही करने के लिए आज़ाद हो जो वह करना चाहता है, तो सभी जगह अराजकता फैल जाएगी। इसलिए समाज के हर क्षेत्र में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। यह केवल अनुशासन ही है जो व्यक्ति को समाज में रहने और फिर भी अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कायम रखने के योग्य बनाता है। हम स्वतन्त्रता के बिना अनुशासन तो प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु अनुशासन के बिना स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकते।
Question 3.
What does indiscipline lead to ?
Answer:
Indiscipline leads to confusion and chaos in a society. It creates corruption, lawlessness and disorder all around. It creates violence also among the people. The evil elements in the society look for excuses to create violence. Security for the poor and the weak vanishes. Indiscipline eats into the roots of our moral, social and national life.
Whenever the sense of order or discipline fades in a nation, its economic life declines completely. Its standard of living falls and its security vanishes. Then the nation goes into the hands of either some more powerful militant power or a dictator. And an indisciplined nation surely goes to the dogs.
अनुशासनहीनता समाज में अफरा-तफरी तथा अशांति फैलाती है। यह हर तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता तथा अव्यवस्था फैलाती है। यह लोगों के बीच हिंसा की भावना पैदा करती है। समाज में फैले बुरे तत्त्व हिंसात्मक कार्य करने के बहाने ढूंढते हैं। गरीब लोगों तथा कमज़ोरों के प्रति सुरक्षा गायब हो जाती है। अनुशासनहीनता हमारे नैतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन की जड़ों तक को खा जाती है।
जब भी किसी राष्ट्र में व्यवस्था अथवा अनुशासन की भावना लुप्त हो जाती है, तब इसके आर्थिक जीवन का पूरी तरह पतन हो जाता है। इसका जीवन-स्तर गिर जाता है तथा इसकी सुरक्षा गायब हो जाती है। फिर वह राष्ट्र या तो किसी अधिक ताकतवर लड़ाकू शक्ति के हाथों में चला जाता है या फिर किसी तानाशाह के हाथों में चला जाता है। और एक अनुशासनहीन राष्ट्र को अवश्य ही दुर्दशा का शिकार होना पड़ता है।
Question 4.
How can an officer inculcate a sense of discipline in his subordinates ?
Answer:
In order to inculcate a sense of discipline in his subordinates, an officer must first realize his own responsibility. He must display high standards of discipline in his own life. Only then can his teaching or his instructions have an effect on his subordinates.
In this chapter, the writer tells us that once he acknowledged the salute of a private soldier with an airy wave of his hand. And his Colonel punished him for not returning the salute properly. He made the writer march in front of the whole battalion and practise before the Sergeant Major’s cane how to return a salute. He said to the writer, “Discipline begins with the officers.”
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुशासन की भावना जगाने के लिए एक अधिकारी को पहले अपनी खुद की ज़िम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। उसे स्वयं अपने जीवन में अनुशासन के उच्च मानदण्डों का प्रदर्शन करना चाहिए। सिर्फ तब ही उसकी शिक्षा अथवा उसके दिशा-निर्देश उसके अधीनस्थ कर्मचारियों पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं।
इस पाठ में लेखक हमें बताता है कि एक बार उसने निचले दर्जे के एक सैनिक की सलामी का जवाब हवा में अपना हाथ लहराते हुए दिया। और उसके कर्नल ने उसे सलामी का जवाब उचित प्रकार से न देने के लिए दण्ड दिया। उसने लेखक से पूरी बटालियन के सामने मार्च करवाया और सार्जेंट मेजर के बेंत के सामने इस बात का अभ्यास करवाया कि सलामी का जवाब कैसे दिया जाता है। उसने लेखक से कहा, “अनुशासन की शुरुआत अफ़सरों से होती है।”

Question 5.
What are the advantages of discipline ?
Answer:
Discipline is very necessary in every field of society. It means training of the mind and character. It trains people to obey rules and orders. It does put some checks on our freedom. But it does not cut down our individual freedom. In fact, it is the foundation of all freedom.
It makes man truly free. It enables man to live in the society and yet retain individual liberty. It helps in maintaining law and order in the society. It is only discipline which enables a nation to march on the way to progress.
समाज के हर क्षेत्र में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है, मन तथा चरित्र का प्रशिक्षण। यह लोगों को नियमों तथा आदेशों का पालन करने में प्रशिक्षित करता है। यह हमारी स्वतन्त्रता पर कुछ रोक अवश्य लगाता है। परन्तु यह हमारी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में कोई कटौती नहीं करता है। वास्तव में यह सारी स्वतन्त्रता की नींव है।
यह मनुष्य को सही अर्थों में स्वतन्त्र बनाता है। यह मनुष्य को समाज में रहने और फिर भी अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कायम रखने के योग्य बनाता है। यह समाज में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। यह सिर्फ अनुशासन ही है जो किसी राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाता है।
Question 6.
In the chapter, Liberty and Discipline’, the writer describes an incident which took place when he was a brand new second lieutenant. What was that incident ?
Answer:
Once he was walking to to parade. A private soldier passed him and saluted him. The writer acknowledged his salute with an airy wave of the hand. Just then, his Colonel came there along with the Regimental Sergeant Major.
He rebuked the writer for not returning the salute properly. He punished the writer for this. He said to the Major, “Plant your staff in the ground and let Mr Slim practise until he does know how to return a salute !” After about ten minutes, he called the writer up to him and said, “Now remember, discipline begins with the officers.”
एक दिन वह परेड के लिए जा रहा था। एक निचले दर्जे का सैनिक उसके पास से गुजरा और उसने उसे सलामी दी। लेखक ने उसकी सलामी का जवाब अपना हाथ हवा में लहराते हुए दिया। तभी उसका कर्नल, रेजिमेण्टल सार्जेंट मेजर के साथ वहां आ गया। उसने सलामी का जवाब उचित तरीके से न देने के लिए लेखक को डांटा।
उसने इसके लिए लेखक को दण्ड दिया। उसने मेजर से कहा, “अपना डंडा जमीन में गाड़ दो और मिस्टर स्लिम को तब तक अभ्यास करने दो जब तक उसे यह न पता चल जाए कि सलामी का जवाब कैसे दिया जाता है !” लगभग दस मिनट के पश्चात् उसने लेखक को अपने पास बुलाया और कहा, “अब याद रखना, अनुशासन की शुरुआत अफसरों से होती है।”
Question 7.
What should a person do when he / she holds a position of authority ?
Answer:
If a man holds a position of authority, he must impose discipline on himself first. It is true that if he gives orders, they will be obeyed. But he should keep in mind that he can build up the leadership of his team on the discipline based on understanding only.
In order to inculcate a sense of discipline in his subordinates, an officer must first realize his own responsibility. He must display high standards of discipline in his own life. Only then can his teaching or his instructions have an effect on his subordinates.
यदि किसी व्यक्ति के पास प्रभावशाली पद हो तो उसे सबसे पहले खुद के ऊपर अनुशासन लागू करना चाहिए। यह सच है कि अगर वह आदेश देगा तो उसका पालन होगा। लेकिन उसे यह बात दिमाग़ में रखनी चाहिए कि वह अपने दल के नेतृत्व का निर्माण केवल आपसी समझ के अनुशासन की नींव पर ही कर सकता है।
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुशासन की भावना भरने के लिए एक अधिकारी को सबसे पहले अपनी स्वयं की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उसे स्वयं के जीवन में अनुशासन के उच्च मापदण्डों का प्रदर्शन करना चाहिए। केवल.तभी उसके अधीनस्थ कर्मचारियों पर उसकी शिक्षा या उसके दिशा-निर्देशों का कोई प्रभाव हो सकता है।
Question 8.
We can have discipline without liberty. But we can’t have liberty without discipline. Explain.
Answer:
Without discipline, no nation can overcome any economic or military crisis. Democracy means that responsibility is decentralised. And no one can avoid doing something he should do. But it is very sad that many of us shirk our share of work. If everyone of us really works, we can overcome any sort of crisis.
But all that takes discipline pure discipline that comes from inside. We think more of liberty than of responsibility. We should always keep in mind that we can never get anything without paying something for it. And in this case, liberty is no exception. We can have discipline without liberty, but we cannot have liberty without discipline.

अनुशासन के बिना कोई भी राष्ट्र किसी आर्थिक अथवा सैनिक संकट पर काबू नहीं पा सकता है। प्रजातन्त्र का अर्थ होता है, जिम्मेदारी का विकेन्द्रीकृत होना। और कोई भी उस काम की अनदेखी नहीं कर सकता जो काम करने की उससे आशा की जाती है। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि हम में से बहुत से लोग अपने हिस्से के काम से जी चुराते हैं। यदि हम में से हर कोई काम करे, तो हम किसी भी प्रकार के संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन इस सब के लिए अनुशासन – बल्कि शुद्ध अनुशासन -की आवश्यकता होती है जो कि हमारे अन्दर से पैदा होता है। हम अपनी ज़िम्मेदारी से ज़्यादा अपनी आज़ादी के बारे में सोचते हैं। हमें यह बात हमेशा दिमाग़ में रखनी चाहिए कि हम किसी भी चीज़ की कीमत अदा किए बगैर उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस संबंध में आज़ादी भी कोई अपवाद नहीं है। हम आज़ादी के बिना अनुशासन तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन के बिना हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
Objective Type Questions
Question 1.
Who wrote the chapter, ‘Liberty and Discipline’ ?
Answer:
William Slim.
Question 2.
What is discipline’ ?
Answer:
It is the training of mind and character.
Question 3.
What is considered as a restraint on liberty ?
Answer:
Discipline
Question 4.
What would happen if everybody did what he wanted ?
Answer:
There would be complete disorder in the world.
Question 5.
What happens when the sense of order or discipline fades in a nation ?
Answer:
Its economic life declines.
Question 6.
What would you call the discipline imposed forcibly’ ?
Answer:
It is nothing but dictatorship.
Question 7.
Who saluted the narrator when he was walking on to a parade ?
Answer:
A private soldier.
Question 8.
What did the Colonel rebuke the writer for ?
Answer:
For not returning a salute properly.
Question 9.
For what purpose is totalitarian discipline designed ?
Answer:
To submerge the individual.

Question 10.
How can a nation overcome an economic or military crisis?
Answer:
With the help of discipline only.
Question 11.
How can an officer build up the leadership of his team ?
Answer:
He can build up the leadership of his team on the discipline of understanding only.
Question 12.
What should an officer do to inculcate a sense of discipline in his subordinates ?
Answer:
He must display high standards of discipline in his own life.
Vocabulary And Grammar
1. Tick mark (✓) the correct meaning of each of the following words :
1. choose
a. select
b. reject
c. accept
2. sermon
a. rebuke
b. a holy lecture
c. a political practice
3. inclination
a. dislike
b. hatred
c. bent of mind
4. unavoidable
a. impossible
b. simultaneous
c. inevitable
5. acknowledge
a. admire
b. dislike
c. know to be correct
6. grin
a. burst out
b. smile widely
c. praise
7. technique
a. desire
b. method
c. description
8. derogatory
a. ennobling
b. insulting
c. praiseworthy
9. initiative
a. fear
b. helplessness
c. courage to start

10. crisis a.
a walkover
b. a difficult situation
c. a challene.
Answer:
1. choose = select
2. sermon = a holy lecture
3. inclination = bent of mind;
4. unavoidable = inevitable
5. acknowledge = know to be correct
6. grin = smile widely
7. technique = method
8. derogatory = insulting
9. initiative = courage to start
10. crisis = a difficult situation.
2. Form adjectives from the following words :
Word — Adjective
1. ornament — ornamental
2. delight — delightful
3. business — businesslike
4. use — useful / useless
5. craft — crafty
6. taste — tasty
7. curiosity — curious
8. memory — memorable
9. wit — witty
10. defect — defective.
3. Fill in each blank with a suitable determiner :
1. We felt …………… indefinable sense of discomfort. (a / an)
2. …………… fugitives had fled from Hiroshima. (many / much)
3. ………….. living thing was petrified in an attitude of indescribable suffering. (many / every)
4. Children begin learning by imitating …………… elders. (his/ their)
5. Each unhappy family is unhappy in ………….. own way. (his / its)
Answer:
1. an
2. Many
3. Every
4. their
5. its.

4. Change the form of narration :
1. The teacher will say, “Gita is performing on the stage.”
2. She said, “If I were rich, I would help him.”
3. “Oh, Tom,” she said, “I am so ashamed of you !”
4. The lawyer asked Bob, “Do you still deny the charges ?”
5. The principal said, “Virtue is its own reward.”
Answer:
1. The teacher will say that Gita is performing on the stage.
2. She said that if she had been rich, she would have helped him.
3. She rebuked Tom saying she was very ashamed of him.
4. The lawyer asked Bob if he still denied the charges.
5. The principal said that virtue is its own reward.
5. Use each of the following words as a noun and a verb :
face, lock, delight, water, consent.
Answer:
1. Face (noun) – Her face is very pretty.
(verb) – I had to face several difficulties.
2. Lock (noun) – I have lost the key to this lock.
(verb) – Lock the room.
3. Delight (noun) – He takes great delight in teasing others.
(verb) – His victory delighted his fans all over the world.
4. Water (noun) — Please give me a glass of water.
(verb) – The gardener is watering the plants.
5. Consent (noun) – Our parents finally gave their consent to our marriage.
(verb) – At last, Mr Raman had to consent to answer our questions.
Liberty and Discipline Summary & Translation in English
Liberty and Discipline Summary in English:
Liberty is the freedom to think what we like, say what we like, work at what we like and go where we like. Discipline is the training of mind and character. It trains people to obey rules and orders and punishes them if they don’t. In short, discipline is a restraint on liberty.
So man has a very natural inclination to avoid it. But since ancient times, man has no option but to accept it. If everybody did what he wanted, there would be complete disorder in the world. There would be the law of the jungle.
From all history we have learnt that whenever the sense of order or discipline fades in a nation, its economic life declines. Its standard of living falls and its security vanishes. Then the nation goes into the hands of either some more virile militant power or a dictator.

Then both of them impose their own brand of discipline. Somehow, eventually, discipline is again enforced. Now the question is not “Shall we accept discipline ?” Sooner or later we have to accept it. So the question is “How shall we accept it ?” Shall it be imposed by physical violence and fear or accepted by consent and understanding. However, the discipline imposed forcibly is not discipline. That is dictatorship. The discipline that comes from our inside is pure discipline.
Here the writer describes an incident which took place when he was a brand new second lieutenant. Once he was walking on to parade. A private soldier passed him and saluted him. The writer acknowledged his salute with an airy wave of the hand. Just then, his Colonel came there along with the Regimental Sergeant Major.
He rebuked the writer for not returning a salute properly. He punished the writer for this. He said to the Major, “Plant your staff in the ground and let Mr Slim practise until he does know how to return a salute !” After about ten minutes, he called the writer up to him and said, “Now remember, discipline begins with the officers.”
If a man holds a position of authority, he must impose discipline on himself first. It is true that if he gives orders, they will be obeyed. But he should keep in mind that he can build up the leadership of his team on the discipline based on understanding only.
In order to inculcate a sense of discipline in his subordinates, an officer must first realize his own responsibility. He must display high standards of discipline in his own life. Only then can his teaching or his instructions have an effect on his subordinates.
No doubt, discipline puts some checks on our freedom. But it does not cut down individual freedom. In fact, it is the foundation of all freedom. It makes man truly free. It enables man to live in a community and yet retain individual liberty.
So it is not at all derogatory for any man or woman. Rather it is ennobling. Without discipline, no nation can overcome any economic or military crisis. Democracy means that responsibility is decentralised. And no one can avoid doing something he should do. But it is very sad that many of us shirk our share of work. If everyone of us really works,
we can overcome any sort of crisis. But all that takes discipline pure discipline that comes from inside. We think more of liberty than of responsibility. We should always keep in mind that we can never get anything without paying something for it. And in this case, liberty is no exception. We can have discipline without liberty. But we cannot have liberty without discipline.
Liberty and Discipline Translation in English:
Field Marshal Sir William Slim, the Chief of the Imperial General Staff, held the highest office in the British Army. He is well qualified to speak on the subject of discipline and the relation it bears to liberty?. This chapter has been condensed from an article contributed by Sir William Slim to The Fortnightly, London. This will be of special interest to all those who are rightly worried about the general disquiet for lack of discipline both at the personal and the national level.

When you get into your car or on your bicycle, you can choose where you want to go. That is liberty. But, as you drive or ride through the streets, you will keep to the left of the road. That is discipline.
There are four reasons why you will keep to the left :
- Your own advantage
- Consideration for others
- Confidence in your fellows; and
- Fear of punishment.
It is the relative weight which we give to each of these reasons that decides what sort of discipline we have. And that can vary from the pure self-discipline of the Sermon on the Mount to the discipline of the concentration camp, the enforced discipline of fear. In spite of all our squabbles, the British are united when it comes to the most of the things that matter and liberty is one of them.
We believe in freedom to think what we like, say what we like, work at what we like, and go where we like. Discipline is a restraint on liberty, so many of us have a very natural inclination to avoid it. But we cannot. Man, ever since the dim prehistoric past, has had no option but to accept the discipline of some kind. For a modern man, living in complex communities, in which every individual is dependent on others, discipline is more than ever unavoidable.
All history teaches that when through either idleness, weakness or faction, the sense of order fades in a nation, its economic life sinks into decay, then, as its standard of living falls and security vanishes, one of two things happens.
Either some more virile militant power steps in to impose its own brand of discipline or a dictator arises and clamps down the iron control of the police state. Somehow, eventually, discipline is again enforced. The problem is not; “Shall we accept discipline ?”
sooner or later we have to; it is “How shall we accept it ?” Shall it be imposed by physical violence and fear, by grim economic necessity, or accepted by consent and understanding ? Shall it come from without or from within ? The word “discipline” for some flashes on the screen of the mind a jackbooted commissar bawling commands across the barrack square at tramping squads. But that is dictatorship, not discipline. The voluntary, reasoned discipline accepted by free, intelligent men and women is another thing. It is binding on all, from top to bottom.
One morning, long ago, as a brand new second lieutenant, I was walking on to parade. A private soldier passed me and saluted. I acknowledged his salute with an airy wave of the hand. Suddenly behind me, a voice rasped out my name.
I spun round and there was my Colonel, for whom I had a most wholesome respect, and with him the Regimental Sergeant Major, of whom also I stood in some awe . “I see,” said the Colonel, “you don’t know how to return a salute. Sergeant Major, plant your staff in the ground, and let Mr Slim practise saluting it until he does know how to return a salute !”
So to and fro I marched in sight of the whole battalion, saluting the Sergeant Major’s cane. (I could cheerfully have murdered the Colonel, the Sergeant Major, and my grinning9 fellow-subalterns.) At the end of ten minutes, the Colonel called me up to him. All he said was : “Now remember, discipline begins with the officers !”
And so it does. The leader must be ready, not only to accept a higher degree of responsibility but a severer standard of self – discipline than those he leads. If you hold a position of authority, whether you are the managing director or the charge-head, you must impose discipline on yourself first. Then forget the easy way of trying to enforce
it on others by just giving orders and expecting them to be obeyed’. You will give orders and you will see they are obeyed, but you will only build up the leadership of your team on the discipline of understanding. There is more to a soldier’s discipline than blind obedience and to take men into your confidence is not a new technique invented in the last war.

Oliver Cromwell demanded that every man in his new model army should “know what he fights for, and love what he knows. Substitute work for fight and you have the essence of industrial discipline too to know what you work for and to love what you know. it is only discipline that enables men to live in a community and yet retain individual liberty.
Sweep away or under mine discipline, and security for the weak and the poor vanishes. That is why, far from it being derogatory” for any man or woman voluntarily to accept discipline, it is ennobling.
Totalitarian discipline with its slogan shouting masses is deliberately designed to submerge the individual. The discipline a man imposes on himself because he believes intelligently that it helps him to get a worthwhile job done to his own and his country’s benefit, fosters character and initiative’.
It makes a man do his work, without being watched, because it is worth doing. in the blitzt of the last war not a man of the thousands of British railway signalmen even left his post. They stood, often in the heart of the target areas, cooked up in flimsy buildings, surrounded by glass, while the bombs screamed down. They knew what they worked for, they knew its importance to others and to their country and they put their job before themselves.
That was discipline. No nation even got out of a difficult position, economic or military, without discipline. Democracy means that responsibility is decentralized and that no one can shirk his share of the strain. And some of us, a lot of us, in all walks of life, do not. If everyone not only the other fellows we are always pointing at really worked when we were supposed to be working, we should beat our economic crisis hollow.
That takes discipline based not only on ourselves, but backed by a healthy public opinion. We are apt these days to think more of liberty than of responsibility but, in the long run, we never get anything worth having without paying something for it. Liberty is no exception. You can have discipline without liberty, but you cannot have liberty without discipline.
Liberty and Discipline Summary & Translation in Hindi
Liberty and Discipline Summary in Hindi:
लेख का विस्तृत सार । आजादी वह सोचने की स्वतंत्रता होती है जो हम सोचना चाहते हैं, वह कहने की स्वतंत्रता जो हम कहना चाहते हैं, वह काम करने की स्वतंत्रता जो हम करना चाहते हैं, वहां जाने की स्वतंत्रता जहां हम जाना चाहते हैं। अनुशासन दिमाग तथा चरित्र का प्रशिक्षण होता है। यह लोगों को नियमों तथा आदेशों का पालन करना सिखाता है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह उन्हें दण्ड देता है।
संक्षेप में, अनुशासन आजादी पर लगाई गई पाबन्दी होता है। इसलिए मनुष्य के अन्दर इसे अनदेखा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लेकिन प्राचीन समय से ही मनुष्य के पास इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहा है। अगर हर कोई वही करता जो उसे पसन्द था, तो दुनिया में पूर्ण अव्यवस्था होती।
तब वहां जंगल का कानून चलता। पूरे इतिहास से हमने सीखा है कि जब भी किसी राष्ट्र में व्यवस्था तथा अनुशासन की भावना लुप्त हो जाती है, तो इसके आर्थिक जीवन का पतन हो जाता है। उसका जीवन-स्तर गिर जाता है तथा उसकी सुरक्षा गायब हो जाती है। फिर राष्ट्र या तो किसी अधिक ताकतवर लड़ाकू शक्ति के हाथों में चला जाता है या किसी तानाशाह के हाथ में। फिर वे दोनों अपने-अपने किस्म के अनुशासन को जबरदस्ती लागू कर देते हैं।
अब प्रश्न यह नहीं है -“क्या हम इसे स्वीकार करें ?” देर-सवेर हमें इसे स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिए प्रश्न यह है – “हम इसे कैसे स्वीकार करें ?” क्या इसे शारीरिक हिंसा तथा भय के द्वारा थोपा जाएगा अथवा सहमति और आपसी समझ के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा ? परंतु जबरदस्ती थोपा गया अनुशासन, अनुशासन नहीं होता है। वह तानाशाही होता है। वह अनुशासन जो हमारे अन्दर से उत्पन्न होता है, वही शुद्ध अनुशासन होता है।

यहां लेखक उस समय की एक घटना का वर्णन करता है जब वह बिल्कुल नया-नया भर्ती हुआ सैकण्ड लेफ्टिनेंट था। एक दिन वह परेड के लिए जा रहा था। एक निचले दर्जे का सैनिक उसके पास से गुजरा और उसने उसे सलामी दी। लेखक ने उसकी सलामी का जवाब अपना हाथ हवा में लहराते हुए दिया। तभी उसका कर्नल, रेजीमेण्टल सारजैंट मेजर के साथ वहां आ गया।
उसने सलाम का जवाब उचित तरीके से न देने के लिए लेखक को डांटा। उसने इसके लिए लेखक को दण्ड दिया। उसने मेजर से कहा, “अपना डंडा जमीन में गाड़ दो और मिस्टर स्लिम को तब तक अभ्यास करने दो जब तक उसे यह न पता चल जाए कि सलामी का जवाब कैसे दिया जाता है !” लगभग दस मिनट के पश्चात् उसने लेखक को अपने पास बुलाया और कहा, “अब याद रखना, अनुशासन की शुरुआत अफसरों से होती है।”
यदि किसी व्यक्ति के पास प्रभावशाली पद हो तो उसे सबसे पहले खुद के ऊपर अनुशासन लागू करना चाहिए। यह सच है कि अगर वह आदेश देगा तो उसका पालन होगा, लेकिन उसे यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि वह अपने दल के नेतृत्व का निर्माण केवल आपसी समझ के अनुशासन की नींव पर ही कर सकता है।
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में अनुशासन की भावना भरने के लिए एक अधिकारी को सबसे पहले अपनी स्वयं की जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। उसे स्वयं के जीवन में अनुशासन के उच्च मापदण्डों का प्रदर्शन करना चाहिए। केवल तभी उसके अधीनस्थ कर्मचारियों पर उसकी शिक्षा या उसके दिशा-निर्देशों का कोई प्रभाव हो सकता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुशासन हमारी स्वतंत्रता पर कुछ पाबन्दियां लगाता है। लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कटौती नहीं करता है। वास्तव में यह सारी स्वतंत्रता की नींव है। यह मनुष्य को वास्तव में स्वतंत्र बनाती है। यह मनुष्य को समाज में रहने और फिर भी अपनी निजी आज़ादी बनाए रखने के योग्य बनाती है। यह किसी पुरुष या स्त्री के लिए अपमानजनक नहीं होता है। अपितु यह तो महान् बनाने वाला होता है। अनुशासन के बिना कोई भी राष्ट्र किसी आर्थिक अथवा सैनिक संकट पर काबू नहीं पा सकता है।
प्रजातन्त्र का अर्थ होता है-जिम्मेवारी का विकेन्द्रीकृत होना। और कोई भी उस काम की अनदेखी नहीं कर सकता जो काम करने की उससे आशा की जाती है। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि हम में से बहुत से लोग अपने 53 हिस्से के काम से जी चुराते हैं। यदि हम में से हर कोई काम करे, तो हम किसी भी प्रकार के संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए अनुशासन – बल्कि शुद्ध अनुशासन – की आवश्यकता होती है जो कि हमारे अन्दर से पैदा होता है।
हम अपनी जिम्मेवारी से ज़्यादा अपनी आज़ादी के बारे में सोचते हैं। हमें यह बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि हम किसी भी चीज़ की कीमत अदा किए बगैर उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस संबंध में आजादी भी कोई अपवाद नहीं है। हम आज़ादी के बिना अनुशासन तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन के बिना हम आजादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
Liberty and Discipline Translation in Hindi:
फील्ड मार्शल सर विलियम स्लिम, जो कि इंपीरियल जनरल स्टाफ का मुखिया था, बरतानवी सेना में सबसे ऊँचे ओहदे पर था। वह अनुशासन तथा स्वतंत्रता के साथ इसके सम्बन्ध के विषय में बोलने के लिए सुयोग्य है। यह अध्याय सर विलियम स्लिम के दि फोर्टनाईटली, लन्दन, के लिए लिखे गए लेख में से संक्षिप्त किया गया है। यह उन सभी लोगों के लिए विशेष दिलचस्पी वाला साबित होगा जो उचित रूप से व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अनुशासन की कमी के कारण फैली अशांति के बारे में चिंतित हैं।

आप जब अपनी कार में बैठते हैं या अपनी साइकिल पर बैठते हैं तो आप फैसला कर सकते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं। इसे स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन जब आप कार में या साइकिल पर सवार होकर गलियों में से निकलेंगे तो आप सड़क की बाईं तरफ रहेंगे। इसे अनुशासन कहते हैं।
इसके चार कारण हैं कि आप बाईं तरफ ही क्यों चलेंगे :
- आपका अपना फायदा
- दूसरों का लिहाज़
- अपने साथियों में आपका विश्वास; और
- सज़ा का भय।
यह तुलनात्मक महत्त्व है जो कि हम इन कारणों मेंसे प्रत्येक को देते हैं जो यह निश्चित करता है कि हम किस प्रकार का अनुशासन रखते हैं। और यह सरमन ऑन दि माउन्ट (ईसा मसीह द्वारा पहाड़ी पर खड़े होकर दिया गया पहला उपदेश) वाले शुद्ध आत्म-अनुशासन से लेकर बंदी शिविर, जो कि भय पैदा करने का जबरदस्ती लागू किया हुआ अनुशासन था, तक भिन्न हो सकता है। हमारे सभी महत्त्वहीन झगड़ों के बावजूद, बरतानवी लोग एक हैं जब बात उन ज्यादातर चीज़ों पर आ जाती है जो महत्त्व की हैं और स्वतंत्रता इनमें से एक है।
हम इन बातों की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं की जो हम चाहते हैं, वह कहने की जो हम चाहते हैं, वह काम करने की जो हम चाहते हैं, तथा वहां जाने की जहां हम जाना चाहते हैं। अनुशासन स्वतंत्रता पर लगाई गई पाबन्दी है, इसलिए हम में से बहुतेरों का स्वाभाविक झुकाव इसे नज़रअंदाज़ करने की तरफ ही रहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते।
धुंधले अति पुरातन काल से ही मनुष्य के पास किसी न किसी प्रकार के अनुशासन को स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा है। उस आधुनिक मनुष्य के लिए, जो कि जटिल समुदायों में रहता है, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरों पर निर्भर है, अनुशासन पहले से भी कहीं अधिक अनिवार्य है।
सारे इतिहास ने हमें सिखाया है कि जब आलस्य, कमज़ोरी अथवा गुटबन्दी के कारण किसी राष्ट्र में व्यवस्था की भावना लुप्त हो जाती है, तो इसके आर्थिक जीवन का पतन हो जाता है, फिर, जब इसका जीवन-स्तर गिर जाता है तथा सुरक्षा गायब हो जाती है, तो दो में से एक बात घटित होती है। या तो कोई अधिक ताकतवर लड़ाकू
शक्ति अपनी ही किस्म का अनुशासन थोपने के लिए आ जाती है अथवा एक तानाशाह का उदय होता है और वह पुलिस राज्य (शासन) का सख़्त नियंत्रण (लोगों के ऊपर) लागू कर देता है। किसी न किसी तरह अन्ततः अनुशासन को दोबारा लागू कर दिया जाता है। समस्या यह नहीं है; “क्या हम अनुशासन को स्वीकार करें?” आज नहीं तो कल हमें करना ही पड़ना है-; समस्या तो यह है “हम इसे कैसे स्वीकार करें?”

क्या इसे शारीरिक हिंसा या भय के द्वारा, गंभीर आर्थिक आवश्यकता के द्वारा लागू किया जाएगा अथवा सहमति तथा (आपसी) समझ के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा? क्या यह कहीं बाहर से आएगा या हमारे भीतर से? शब्द ‘अनुशासन’ कुछ लोगों के लिए मन के पर्दे पर एक ऊँचे जूते पहने हुए अधिकारी, जो कि बैरकों के
चौराहे के उस तरफ मार्च कर रहे फौजियों के दस्ते को जोर-जोर से आदेश दे रहा हो, की तस्वीर बिजली की चमक की भांति ले आता है। लेकिन यह तानाशाही है, अनुशासन नहीं। बुद्धिमान पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा स्वीकार किया गया स्वैच्छिक तथा तर्कसंगत अनुशासन एक दूसरी चीज़ है।
यह ऊपर से नीचे तक सभी के ऊपर लागू होता है। बहुत समय पहले, एक सुबह नए-नए भर्ती हुए सेकण्ड लेफ्टिनेंट के रूप में, मैं परेड के लिए जा रहा था। एक निचले दर्जे का सैनिक मेरे पास से गुज़रा और उसने सलामी दी। मैंने उसकी सलामी का जवाब हवा में हाथ लहराते हुए दिया। अचानक मेरे पीछे से एक रूखी-सी आवाज़ ने मेरा नाम पुकारा। मैं तुरंत घूमा और यह मेरा कर्नल था, जिसके लिए मेरे अंदर बहुत आदर था, तथा |
उसके साथ रेजीमेण्टल सारजैंट मेजर था, जिसका मैं आदर भी करता था और जिससे मैं डरता भी था। “मैंने देखा है,” कर्नल ने कहा, “तुम्हें नहीं मालूम कि सलामी का जवाब कैसे दिया जाता है। सारजैंट मेजर, अपना डंडा मैदान में गाड़ दो, और मिस्टर स्लिम को तब तक अभ्यास करने दो जब तक उसे पता न चल जाए कि सलामी का जवाब कैसे दिया जाता है!”
इसलिए आगे-पीछे मैं पूरी बटालियन की आंखों के सामने मार्च करने लगा, सारजैंट मेजर के बेंत को सलामी देते हुए। (मैंने प्रसन्नतापूर्वक कर्नल, सारजैंट मेजर तथा दांत निकालकर हँसते हुए अपने साथी अफसरों को मार दिया होता।) दस मिनट समाप्त होने के बाद कर्नल ने मुझे अपने पास बुलाया।
उसने जो भी कहा वह था “अब याद रखना, अनुशासन की शुरुआत अफसरों से |होती है!” और होता भी ऐसे ही है। नेता को तैयार रहना चाहिए, न सिर्फ उत्तरदायित्व के ऊँचे दर्जे को स्वीकार करने के लिए, बल्कि जिनकी अगुवाई वह करता है उनसे भी अधिक सख़्त आत्म-अनुशासन के दर्जे के लिए। अगर आप किसी प्रभावशाली ओहदे पर हैं, चाहे आप प्रबंध निदेशक हैं या किसी कार्यभार के मुखिया हैं, सबसे पहले आपको अनुशासन अपने स्वयं के ऊपर लागू करना चाहिए। फिर इसे दूसरों के ऊपर लागू करने की कोशिश
करने के आसान तरीके को भूल जाइए – केवल आदेश दे देना और आशा करना कि उनका पालन किया जाएगा। आप आदेश देंगे और आप देखेंगे कि उनका पालन किया जाएगा, लेकिन आप केवल (आपसी) समझ के अनुशासन के ऊपर अपनी टीम के नेतृत्व का निर्माण करेंगे। एक फौजी के अनुशासन में अंधाधुंध आज्ञापालन से बढ़कर भी कुछ होता है और लोगों को अपने विश्वास में लेना कोई पिछले युद्ध में खोजी गई नई तकनीक नहीं है।
ओलिवर क्रॉमवैल यह अपेक्षा करता था कि उसकी should नई आदर्श सेना में प्रत्येक व्यक्ति को “यह मालूम होना चाहिए कि वह किस के लिए लड़ रहा है तथा वह जो जानता है, उससे उसे प्यार होना चाहिए।” शब्द ‘लड़ाई’ की जगह ‘काम’ कर दीजिए और आपको औद्योगिक अनुशासन का सार भी मिल जाएगा – यह जानना कि आप किस के लिए काम करते हैं तथा जो आप जानते हैं उससे प्यार करना।
यह केवल अनुशासन ही है जो लोगों को समाज में रहने तथा फिर भी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने के योग्य बनाता है। अनुशासन से छुटकारा पा लीजिए या इसे अंदर ही अंदर खोखला कर लीजिए, और कमज़ोर लोगों तथा गरीबों की सुरक्षा गायब हो जाएगी। इसलिए, किसी पुरुष या स्त्री के द्वारा अनुशासन को स्वेच्छा से स्वीकार करना अपमानजनक होना तो दूर की बात है, बल्कि यह तो श्रेष्ठ बना देने वाला होता है।

सर्वसत्तावादी अनुशासन, जिसमें नारेबाजी करती जनता शामिल होती है, का निर्माण व्यक्ति को पूरी तरह से छिपा देने के लिए किया गया है। वह अनुशासन, जिसे व्यक्ति अपने ऊपर इसलिए लागू करता है क्योंकि उसका समझदारीपूर्वक मानना होता है कि इससे उसकी अपनी तथा देश की भलाई के लिए किए जाने वाले लाभदायक काम को करने में उसे सहायता मिलेगी, चरित्र तथा पहलकदमी का विकास करता है।
यह व्यक्ति को उसका काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, किसी के जाने या देखे बगैर, क्योंकि यह काम करने लायक होता है। पिछले युद्ध के हमलों के दौरान हज़ारों बरतानवी रेलवे सिग्नलमैनों में से एक भी व्यक्ति ने अपनी नियुक्त की गई जगह नहीं छोड़ी। जब बम शोर करते हुए नीचे गिर रहे थे तो वे चारों तरफ शीशे लगी हुई कमज़ोर इमारतों में गर्मी से झुलसे हुए लक्ष्य-क्षेत्रों के बीचों-बीच डटे रहे।
वे जानते थे कि वे किस लिए काम कर रहे थे, वे जानते थे कि इसका दूसरों के लिए तथा उनके देश के लिए क्या महत्त्व था और उन्होंने स्वयं से पहले अपने काम को रखा। यह था अनुशासन। कोई भी देश कभी भी अनुशासन के बिना बुरी स्थिति, चाहे वह आर्थिक हो या सैन्य, से बाहर नहीं निकला।
प्रजातन्त्र का अर्थ है कि जिम्मेवारी विकेन्द्रीकृत होती है और कोई भी परिश्रम के अपने हिस्स स जा नहा चुरा सकता। और हम में से कुछ (बल्कि ) हम में से बहुतेरे, जिंदगी के सभी क्षेत्रों में, जी नहीं चुराते हैं। यदि हर किसी – सिर्फ वही अन्य लोग नहीं जिनकी तरफ हम हमेशा इशारा करते रहते हैं ने उस समय काम किया होता जब उससे काम करने की उम्मीद की जाती थी, तो हम अपने आर्थिक संकट से छुटकारा पा चुके होते।
उसके लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ हम पर ही आधारित न हो, बल्कि जिसको एक स्वस्थ जनमत का समर्थन भी प्राप्त हो। आजकल हम जिम्मेवारी से ज्यादा स्वतन्त्रता के बारे में सोचते हैं, लेकिन अन्ततः हमें कोई भी अच्छी चीज़ उसकी कीमत अदा किए बगैर नहीं मिलती। स्वतन्त्रता भी कोई अपवाद नहीं है। आप स्वतन्त्रता के बिना अनुशासन तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप अनुशासन के बिना स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकते।
A Panorama of Life PSEB Solutions Class 11
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()