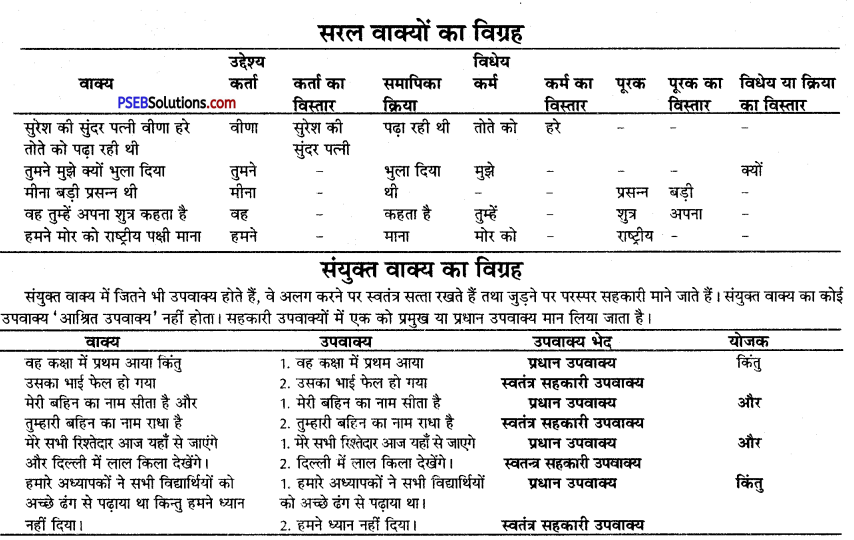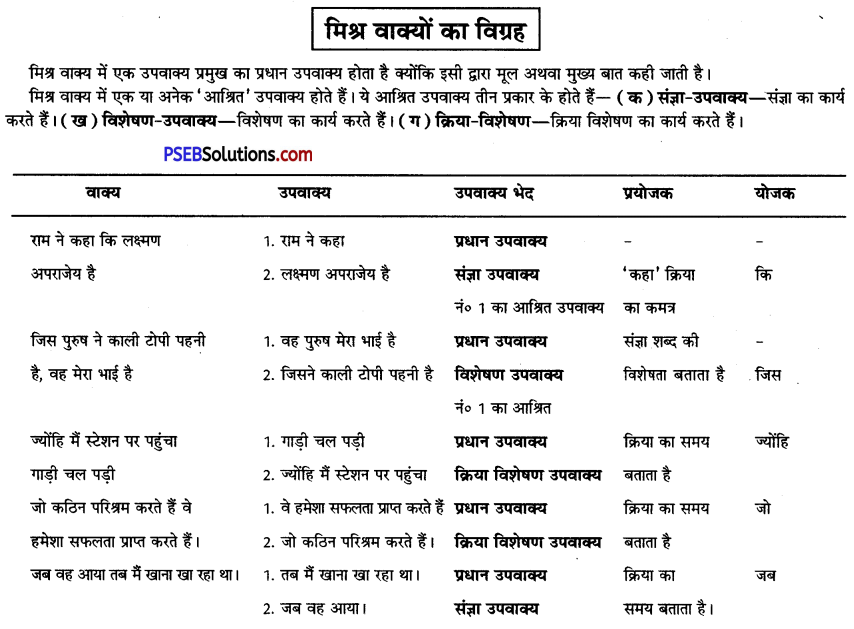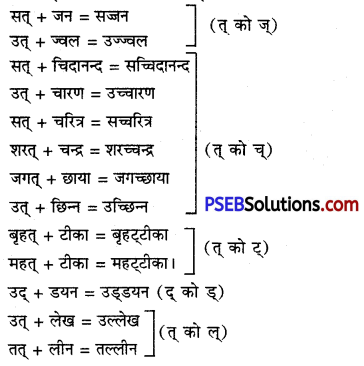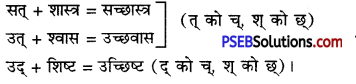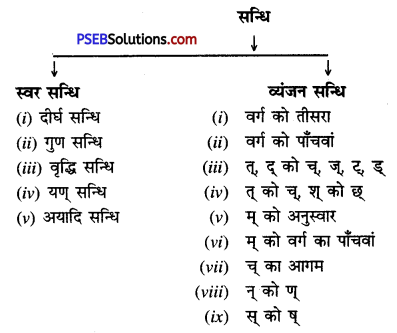Punjab State Board PSEB 11th Class Hindi Book Solutions Hindi संप्रेषण कौशल संक्षेपिका लेखन / संक्षेपीकरण Questions and Answers, Notes.
PSEB 11th Class Hindi संप्रेषण कौशल संक्षेपिका लेखन / संक्षेपीकरण
(ग) संक्षेपिका लेखन/संक्षेपीकरण
(ABRIDGEMENT)
आज के यान्त्रिक युग में लोगों के पास समय की बड़ी कमी है और काम उसे बहुत-से करने होते हैं, इसलिए संक्षेपीकरण का महत्त्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। आज लम्बी-लम्बी, हातिमताई जैसी कहानियां सुनने का समय किसके पास है। आज रात-रात भर पण्डाल में बैठकर नाटक कोई नहीं देख सकता। हर कोई चाहता है कि बस काम फटाफट हो जाए। संक्षेपीकरण हमारी इसी प्रवृत्ति का समाधान करता है।
संक्षेपीकरण का अर्थ विषय को संक्षिप्त करने से है। उसकी जटिलताओं को दूर कर सरल बनाना ही संक्षेपीकरण का मूल उद्देश्य है। संक्षेपीकरण के द्वारा विषय के मूलभूत तत्त्वों का विश्लेषण करके उसका भावार्थ सरलतापूर्वक समझा जा सकता है।
संक्षेपीकरण की परिभाषा-संक्षेपीकरण की परिभाषा हम इन शब्दों में कर सकते हैं
“विभिन्न लेखों, कहानियों, संवादों, व्यावसायिक एवं कार्यालयों पत्रों आदि में वर्णित विषयों का भावार्थ संक्षेप में, सरल शब्दों में स्पष्ट करना ही संक्षेपीकरण है।”
संक्षेपीकरण द्वारा विषय का जो रूप प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही संक्षेपिका कहते हैं। वर्तमान युग में हमें संक्षेपीकरण की कदम-कदम पर आवश्यकता पड़ती है। व्यापार एवं वाणिज्य के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं कार्यालयीन पत्र-व्यवहार में तो इसका विशेष महत्त्व है। सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालयों में, व्यापारिक संस्थानो में प्रतिदिन सैकड़ों पत्र आते हैं। उन पत्रों को निपटाने और उन पर अन्तिम निर्णय अधिकारियों को ही लेना होता है और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे प्राप्त होने वाले सभी पत्रों को पढ़ सकें। अतः उनके सामने इन पत्रों की संक्षेपिका तैयार करके प्रस्तुत की जाती है। इसके लिए कार्यालयों में, व्यापारिक संस्थानों में अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है जो आने वाले पत्रों को पढ़कर उनका संक्षेपीकरण करके उच्चाधिकारी के सामने प्रस्तुत करते हैं।
संक्षेपीकरण केवल पत्रों का ही नहीं होता, समाचारों का भी होता है अथवा किया जाता है। सरकारी और गैरसरकारी कार्यालयों में इस उद्देश्य से लोक सम्पर्क विभाग का गठन किया गया है। प्रायः बड़े-बड़े व्यापारिक संस्थान भी अपने यहां लोक सम्पर्क अधिकारी (P.R. O.) नियुक्त करते हैं। इन अधिकारियों का काम समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की संक्षेपिका तैयार करके सम्बन्धित अधिकारी को भेजना होता है क्योंकि उच्चाधिकारी के पास सारे समाचार पढ़ने का समय नहीं होता। वह उस संक्षेपिका के ही आधार पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों अथवा कार्यालयों को आवश्यक कारवाई हेतु निर्देश जारी कर देता है।
संक्षेपीकरण भी एक कला है जो निरन्तर अभ्यास से आती है। इसका मूलभूत उद्देश्य विषय की जटिलता को समाप्त कर उसे अधिक सरल, स्पष्ट एवं ग्राह्य बनाकर समय एवं श्रम की बचत करना तथा एक शिल्पी की भान्ति उसे आकर्षक बनाना है। संक्षेपीकरण से विषय की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है।
संक्षेपीकरण का महत्त्व एवं व्यवहारक्षेत्र
यदि यह कहा जाये कि आज का युग संक्षेपीकरण का युग है तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। आप ने प्रायः बड़ेबड़े अफसरों की मेज़ पर यह तख्ती अवश्य रखी देखी होगी- ‘Be Brief’ । इसका कारण समय की कमी और काम की ज़्यादती के अतिरिक्त यह भी है कि हम आज हर काम Short cut से करना चाहते हैं। संक्षेपीकरण का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है, व्यापारियों, अफसरों, वकीलों, न्यायाधीशों, डॉक्टरों, प्राध्यापकों, संवाददाताओं, नेताओं और छात्रों इत्यादि सभी के लिए संक्षेपीकरण का ज्ञान आवश्यक है। इससे श्रम और समय की बचत तो होती ही है, व्यक्ति को जीवन की निरन्तर बढ़ती हुई व्यस्तता के कारण विषय की पूरी जानकारी भी हो जाती है।
विद्यार्थी वर्ग के लिए इसका विशेष महत्त्व है। पुस्तकालय में किसी पुस्तक को पढ़ते समय जो विद्यार्थी पठित पुस्तक अथवा अध्याय की संक्षेपिका तैयार कर लेता है, उसके ज्ञान में काफी वृद्धि होती है, जो परीक्षा में उसकी सहायक होती है। इसी प्रकार जो विद्यार्थी कक्षा में प्राध्यापक के भाषण की नित्य संक्षेपिका तैयार कर लेता है, उसे बहुत-सी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्राध्यापक का भाषण भी तो एक तरह से बहुत-सी पुस्तकों को पढ़कर एक संक्षेपिका का ही रूप होता है। कुछ विद्यार्थी तो परीक्षा से पहले मूल पाठ के स्थान पर अपनी तैयार की गयी संक्षेपिका को ही पढ़ते हैं। किन्तु याद रहे कि वह संक्षेपिका विद्यार्थी की अपनी तैयार की हुई होनी चाहिए, किसी गाइड से नकल की हुई नहीं।
संक्षेपीकरण से मस्तिष्क में विचार-शक्ति का विकास होता है। व्यक्ति को थोड़े में बहुत कह जाने का अभ्यास हो जाता है। इससे तर्क-शक्ति तथा भावों को प्रकट करने की शक्ति का भी विकास होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, डॉक्टर या प्राध्यापक को इसमें दक्षता प्राप्त करना ज़रूरी है। यह आधुनिक युग का श्रमसंचक यन्त्र है।

संक्षेपिका लेखन के प्रकार
अध्ययन की दृष्टि से संक्षेपिका लेखन तीन प्रकार का हो सकता है
1. संवादों का संक्षेपीकरण-संक्षेपिका लेखन का अभ्यास करने के लिए उसका पहला चरण संवादों का संक्षेपीकरण करना है। संवादों की संक्षेपिका प्रायः हर विद्यार्थी तैयार कर सकता है। संवादों की संक्षेपिका तैयार करने में दक्ष होने पर हर व्यक्ति अन्य विषयों का संक्षेपीकरण सरलता से कर सकता है।
2. समाचारों, विशेष लेख, भाषण या अवतरण की संक्षेपिका लिखना-समाचारों की संक्षेपिका दो तरह के व्यक्ति तैयार करते हैं एक पत्रकार या संवाददाता, दूसरे लोक सम्पर्क अधिकारी (Public Relation Officer)। पत्रकार अथवा संवाददाता किसी समाचार के महत्त्वपूर्ण तथ्यों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठक सरलतापूर्वक उसके विचारों को समझ जाएं। समाचार पत्रों के संवाददाता के लिए तो संक्षेपीकरण विशेष महत्त्व रखता है। वह किसी घटना को देखता है, किसी नेता का भाषण सुनता है और उसे जब तार द्वारा, टेलिफोन पर या पत्र द्वारा समाचार पत्र को उसका प्रतिवेदन (Report) भेजता है, तो वह एक प्रकार की संक्षेपिका ही होती है। आजकल इसी कारण समचारपत्रों में संवाददाता का नाम भी प्रकाशित किया जाने लगा है ताकि लोगों को पता चल जाये कि इस समाचार की संक्षेपिका किस ने तैयार की है। अपनी संक्षेपिका लेखन के कौशल के कारण ही बहुत-से संवाददाता पाठकों में अपनी एक अलग पहचान बना लेने में सफल होते हैं। कुछ ऐसा ही कार्य समाचार-पत्रों के सह-सम्पादक या उप-सम्पादक करते हैं। वे प्राप्त समाचारों को, अपने पत्र की पॉलिसी अथवा स्थान को देखते हुए संक्षेपिका करके ही प्रकाशित करते हैं।
ठीक ऐसा ही कार्य समाचारों की संक्षेपिका तैयार करने में लोक सम्पर्क अधिकारी अथवा उस कार्यालय के अन्य सम्बन्धित अधिकारी करते हैं। जो अधिकारी कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक सरल और स्पष्ट भाषा में समाचार-पत्रों की संक्षेपिका तैयार कर अपने अधिकारियों अथवा मन्त्रियों को भेजता है वही विभाग में नाम कमाता है और ऐसे लोक सम्पर्क अधिकारी को हर अफसर, हर मन्त्री अपने साथ रखना चाहता है।
एक प्रकार की संक्षेपिका विद्यार्थी भी लिखते हैं। परीक्षा में उन्हें किसी विशेष लेख, किसी विद्वान् के भाषण या किसी अवतरण, कविता अथवा निबन्ध की संक्षेपिका लिखने को कहा जाता है। यह अध्ययन किये हुए विषय की संक्षेपिका लिखना है। इस प्रकार की संक्षेपिका में विद्यार्थी को चाहिए कि वह लेख, भाषण, अवतरण, कविता या निबन्ध में प्रस्तुत किये गये विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत करें। भाषा उसकी अपनी हो किन्तु मूल प्रतिपाद्य वही हों।।
3. पत्रों अथवा टिप्पणियों की संक्षेपिका-सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में तथा व्यापारिक संस्थानों में नित्य प्रति हज़ारों पत्रों का आदान-प्रदान होता रहता है। सभी मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए कार्यालय में आने वाले पत्रों अथवा इन पर लिखी गयी टिप्पणियों की संक्षेपिका तैयार करनी पड़ती है। कार्यालयों में प्रायः अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानान्तरण होता रहता है। ऐसी दशा में कार्य को निपटाने में संक्षेपिका ही सहायक होती है। हर मामले में सम्बन्धित फाइल में उसकी संक्षेपिका रहने से नये व्यक्ति को कोई मामला समझने में देर नहीं लगती।
सार लेखन और संक्षेपिका लेखन में अन्तर
सार लेखन और संक्षेपिका लेखन में महत्त्वपूर्ण अन्तर है। सारांश लिखते समय मूल अवतरण अथवा पत्र में लेखक के द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों को, जो कि बिखरे हुए होते हैं, एक सूत्र में बांध कर अधिक स्पष्ट एवं सरल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है जबकि संक्षेपिका तैयार करते समय लेखक के भावों को महत्त्व दिया जाता है और उसे अपने शब्दों में प्रस्तुत कर दिया जाता है। सारांश लिखते समय मूल अवतरण या पत्र में लेखक द्वारा प्रस्तुत सभी तर्कों को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि संक्षेपिका लिखते समय केवल आवश्यक तथ्यों एवं तर्कों को ही प्रस्तुत किया जाता है। अनावश्यक बातों को संक्षेपिका में कोई स्थान नहीं दिया जाता। संक्षेपिका सारांश की अपेक्षा अधिक सरल और स्पष्ट होती है।
संक्षेपिका में कौन-से गुण होने चाहिएँ
संक्षेपिका लेखन एक कला है। इसलिए संक्षेपिका लिखते समय एक कलाकार की भान्ति अत्यन्त कुशलता से उसे लिखना चाहिए। वर्तमान युग की मांग और परिस्थितियों को देखते हुए हमें संक्षेपिका के महत्त्व एवं आदर्श स्वरूप को समझकर उसे लिखने का अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं कि एक आदर्श संक्षेपिका वही होती है जिसमें विचारों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि आम आदमी भी उसे आसानी से समझ जाए। समाचार पत्रों के संवाददाताओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि समाचार-पत्र हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ता है।
आदर्श संक्षेपिका के गुण-एक आदर्श संक्षेपिका में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है
1. संक्षिप्तता-संक्षेपिका का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण उसकी संक्षिप्तता है। किन्तु संक्षेपीकरण इतना भी संक्षिप्त नहीं होना चाहिए कि उसका अर्थ ही स्पष्ट न हो सके तथा उसमें सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों का समावेश न हो। संक्षेपिका कितनी संक्षिप्त होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है (जैसे कि सार लेखन में अवतरण के तृतीयांश का नियम है)। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों का समावेश हो जाए।
2. स्पष्टता-संक्षेपिका तैयार ही इसलिए की जाती है कि समय और श्रम की बचत हो अत: उसमें स्पष्टता का गुण अनिवार्य माना गया है। यदि संक्षेपिका पढ़ने वाले को अर्थ समझने में कठिनाई हो अथवा देरी लगे तो उसका मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। संक्षेपिका इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ते ही सारी बातें पाठक के सामने स्पष्ट हो जाएं।
3. क्रमबद्धता-संक्षेपिका में सभी तथ्यों का वर्णन श्रृंखलाबद्ध रूप में किया जाना चाहिए। मूल अवतरण में यदि वैचारिक क्रम न भी हो तो भी संक्षेपिका में उन विचारों को क्रम से लिखना चाहिए इस तरह संक्षेपिका पढ़ने वाले को सारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी।
4. भाषा की सरलता और प्रवाहमयता-संक्षेपिका की भाषा शैली इतनी सरल एवं सुबोध होनी चाहिए कि आम आदमी भी उसे आसानी से समझ सके। संक्षेपिका तैयार करते समय लेखक को चाहिए कि वह क्लिष्ट और समासबहुल भाषा का प्रयोग न करे और न ही अलंकृत भाषा का प्रयोग करें।
5. भाषा की शुद्धता-भाषा की शुद्धता से दो अभिप्राय हैं
- संक्षेपिका में वे ही तथ्य या तर्क लिखे जाएं जो मूल सन्दर्भ में हों, जिनसे उनके सही-सही वे ही अर्थ लगाये जाएं जो मूल अवतरण या पत्र में दिये गए हों। अपनी तरफ से उसमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं।
- संक्षेपिका की भाषा व्याकरण सम्मत और विषयानुकूल हो। मूल अवतरण के शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेपिका में पूर्ण शुद्धता बनी रहेगी। ध्यान रहे कि संक्षेपिका, जहां तक सम्भव हो सके, भूतकाल और अन्य पुरुष में ही लिखी जानी चाहिए।
6. अपनी भाषा शैली-संक्षेपिका लिखते समय लेखक को स्वयं अपनी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। अपनी भाषा और शैली में भावों को संक्षिप्त रूप में सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है।
7. स्वतः पूर्णतः-संक्षेपिका का लेखन एक कला है और कोई भी कलाकृति अपने में पूर्ण होती है। अत: संक्षेपिका लेखक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संक्षेपिका संक्षिप्त भी हो, स्पष्ट भी हो और साथ ही साथ पूर्ण भी हो, तभी उसे आदर्श संक्षेपिका कहा जाएगा। अत: संक्षेपिका में मूल अवतरण के सभी आवश्यक तथ्यों का समावेश करना ज़रूरी है जिससे पढ़ने वाले को इस संदर्भ में अपूर्णता की अनुभूति न हो। यदि संक्षेपिका लेखक उपर्युक्त सभी गुणों को अपनी संक्षेपिका में ले आए तो उसमें पूर्णतः अपने आप आ जाएगी।
संक्षेपिका लेखन की विधि
जिस प्रकार एक कुशल चित्रकार अपने चित्र का पहले अच्छा प्रारूप तैयार करता है जो उसकी कल्पना और भावनाओं के अनुरूप होता है, उसी प्रकार एक कुशल संक्षेपिका लेखक को भी पहले संक्षेपिका अथवा संक्षेपीकरण का अच्छा प्रारूप तैयार करना चाहिए। इसके लिए उसे पहले दो-तीन बार संक्षेपिका तैयार करने लिए कहे जाने वाले मसौदे को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और कच्चा प्रारूप तैयार हो जाने पर यह चैक कर लेना चाहिए कि मूल अवतरण या पत्र का कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छूट तो नहीं गया है, जिसके बिना संक्षेपिका पूर्ण नहीं होगी। साथ ही वह अपनी भाषा अथवा व्याकरण की रह गई अशुद्धियों को भी ठीक कर सकेगा।
संक्षेपिका तैयार करने से पूर्व अवतरण का भली-प्रकार अध्ययन करके उस में निहित भावों, विचारों, तथ्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए और हो सके तो उस रेखा के नीचे 1, 2, 3 इत्यादि भी लिख देना चाहिए ताकि संक्षेपिका का प्रारूप तैयार करते समय आप अवतरण के विचारों, तथ्यों आदि को क्रमपूर्वक लिख सकें।
जब मूल अवतरण का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त उसका भावार्थ मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाए तब उसका कच्चा प्रारूप लिख देना चाहिए।
जब आपको सन्तोष हो जाए कि कच्चा प्रारूप मूल अवतरण के भावों, विचारों और तथ्यों को भली-भान्ति स्पष्ट करने में सक्षम है तो उसे सरल और स्पष्ट भाषा में लिख देना चाहिए।
संक्षेपिका लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें
(1) मूल अवतरण को सावधानीपूर्वक दो तीन बार पढ़ना चाहिए।
(2) महत्त्वपूर्ण विचारों, भावों अथवा तथ्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए।
(3) संक्षेपिका का पहले एक कच्चा प्रारूप तैयार करना चाहिए।
(4) संक्षेपिका यदि किसी समाचार की तैयार की जानी है तो उसका उचित शीर्षक भी दे दिया जाना चाहिए (वैसे समाचारों का शीर्षक समाचार-पत्र का सम्पादक ही दिया करता है।)
(5) संक्षेपिका की भाषा-शैली सरल, सुबोध और ग्राह्य होनी चाहिए।
(6) संक्षेपिका अपने शब्दों या भाषा में लिखनी चाहिए।
(7) संक्षेपिका जहां तक सम्भव हो सके, भूतकाल और अन्य पुरुष में लिखनी चाहिए।
(8) संक्षेपिका में मूल अवतरण के विचारों, तथ्यों आदि को श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(9) संक्षेपिका ऐसी होनी चाहिए कि पाठक उसे तुरन्त समझ जाए। उसकी भाषा-शैली ऐसी होनी चाहिए कि सामान्य ज्ञान रखने वाला आम आदमी भी उसे समझ जाए।
(10) संक्षेपिका अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए।
संक्षेपिका लेखक को इन बातों से बचना चाहिए
(1) मूल अवतरण में प्रस्तुत किसी कथन को ज्यों-का-त्यों नहीं लिखना चाहिए।
(2) अपनी ओर से कोई विवरण या आलोचना नहीं करनी चाहिए।
(3) संक्षेपिका में द्वि-अर्थी या अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
(4) संक्षेपिका का रूप किसी भी हालत में मूल अवतरण से बड़ा नहीं होना चाहिए वह जितना संक्षिप्त और सारगर्भित होगा, उतना ही अच्छा है।
(5) संक्षेपिका में शब्दों या विचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
(क) संवादों का संक्षेपीकरण
‘संवाद’ कथोपकथन या वार्तालाप को कहते हैं। वार्तालाप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। ऐसे संवादों या कथोपकथन का संक्षेपीकरण प्रस्तुत करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है जैसे
(1) संवादों में ऐसी बहुत-सी बातें होती हैं जिन्हें संक्षेपीकरण करते समय त्याग देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वाक्य का भाव या सार संक्षेपीकरण में अवश्य शामिल किया जाए।
(2) संवादों में कभी-कभी किसी पात्र का संवाद बहुत लम्बा हो जाता है ऐसी दशा में उस संवाद का सारपूर्ण मुख्य भाव ही ग्रहण करना चाहिए।
(3) महत्त्वपूर्ण भावों वाले संवादों को रेखांकित कर लेना चाहिए।
(4) प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में बदल देना चाहिए। इसका भाव यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्त किये गए विचारों को ज्यों का त्यों उद्धृत नहीं करना चाहिए। संक्षेपीकरण में सभी उद्धरण चिह्नों को हटा देना चाहिए तथा प्रथम पुरुष तथा मध्यम पुरुष सर्वनाम मैं और तुम को अन्य पुरुष वह आदि में बदल देना चाहिए। क्रियापद भी अन्य पुरुष सर्वनाम वह के अनुसार रखे जाने चाहिएं।
(5) संवादों की संक्षेपिका प्रस्तुत करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि वक्ता या पात्रों की मनोदशा और भाव-भंगिमा स्पष्ट हो जाए।
संवादों का संक्षेपीकरण करने का सरल उपाय : एक उदाहरण
टेलिफोन की घण्टी बजती है। रमन कुमार के भाई को उसके मित्र सुभाष का टेलिफोन आया है जो उस समय घर पर नहीं है। रमन कुमार उस टेलिफोन को सुनता है। रमन कुमार और सुभाष में टेलिफोन पर इस प्रकार बातचीत होती है।
रमन-हैलो?
सुभाष-हैलो, क्या मैं कमल से बात कर सकता हूं?
रमन-जी, वे तो बाहर गये हैं, क्या आप उनके लिए कोई सन्देश छोड़ना चाहेंगे?
सुभाष-ओह, हां क्यों नहीं। मैं सुभाष बोल रहा हूं। क्या कमल आज संध्या के समय खाली होगा? मैं संध्या को ज्योति सिनेमा में फिल्म देखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वह भी मेरे साथ फिल्म देखने चले। वह कब तक लौट आयेगा?
रमन-वे बड़ी देर तक बाहर नहीं रहेंगे। बस डाकघर तक कुछ पत्र पोस्ट करने गये हैं। मुझे विश्वास है कि आज संध्या के समय वे बिलकुल खाली हैं।
सुभाष-बहुत अच्छे। तो फिर आप उससे कह दें कि मैं उसकी पांच रुपए के टिकट वाली खिड़की के पास 600 बजे तक प्रतीक्षा करूंगा। यदि वह 6-30 तक नहीं पहुंचा तो मैं टिकट लेकर सिनेमा हाल के भीतर चला जाऊंगा। रमन-हां हां, निश्चय रखिए, मैं उनसे बोल दूंगा।
सुभाष-धन्यवाद।
जब कमल बाहर से लौटकर घर आया तो रमन ने उसे सुभाष के टेलिफोन के बारे में इन शब्दों में बात की भैया जब तुम बाहर गए थे तो सुभाष का फोन आया था। वह यह जानना चाहता था कि इस संध्या को तुम खाली हो। वह ज्योति सिनेमा में फिल्म देखने जा रहा है और चाहता है कि तुम भी उसके साथ फिल्म देखो। मैंने उसे कह दिया है कि तुम शीघ्र लौट आओगे और संध्या को भी तुम्हें कोई काम नहीं है। वह तुम्हारी 6-00 और 6-30 के बीच पांच रुपये की टिकट-खिड़की के पास प्रतीक्षा करेगा।
इस उदाहरण में रमन ने जो कमल को कहा वह उसके और कमल के मित्र सुभाष के बीच हुई वार्तालाप का संक्षेपीकरण था।
उदाहरण-1 मूल संवाद
द्रोणाचार्य-युधिष्ठिर तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है?
युधिष्ठिर-गुरु जी मुझे पेड़ पर चिड़िया, पत्ते आदि सभी कुछ दिखाई दे रहा है।
द्रोणाचार्य-अच्छा भीम तुम बताओ, तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है?
भीम-गुरुदेव मुझे तो चिड़िया दिखाई दे रही है।
द्रोणाचार्य-अच्छा अर्जुन तुम्हें क्या-क्या दिखाई दे रहा है?
अर्जुन-गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
द्रोणाचार्य-बहुत अच्छे, तीर चलाओ।

संक्षेपीकरण (कच्चा प्रारूप)
जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से बारी-बारी पूछा कि उन्हें पेड़ पर क्या-क्या दिखाई दे रहा है तो युधिष्ठिर ने कहा उसे चिड़िया, पत्ते आदि सभी कुछ दिखाई दे रहा है। भीम न कहा उसे केवल चिड़िया दिखाई दे रही है और अर्जुन ने कहा उसे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु जी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को तीर चलाने की आज्ञा दी।
आदर्श संक्षेपीकरण
जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से पूछा कि उन्हें पेड़ पर क्या-क्या नज़र आ रहा है तो युधिष्ठिर ने चिड़िया और पत्ते, भीम ने चिड़िया और अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख दिखाई देने की बात कही। गुरु द्रोण ने प्रसन्न होकर अर्जुन को तीर चलाने का आदेश दिया।
उदाहरण-2 मूल संवाद
चन्द्रगुप्त-कुमारी आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।
कार्नेलिया-किस बात की?
चन्द्रगुप्त-कि मैं विस्मृत नहीं हुआ।
कार्नेलिया-स्मृति कोई अच्छी वस्तु है क्या?
चन्द्रगुप्त-स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुन्दरी।
कार्नेलिया-परन्तु मैं कितने दूर देश की हूं। स्मृति ऐसे अवसर पर दण्ड हो जाती है। अतीत के कारागृह में बंदिनी। स्मृतियां अपने करुण विश्वास की श्रृंखलाओं को झनझना कर सूची भेद्य अंधकार में खो जाती हैं। __ चन्द्रगुप्त-ऐसा हो तो भूल जाओ मुझे। इस केन्द्रच्युत जलते हुए उल्कापिण्ड की कोई कक्षा नहीं। निर्वासित, अपमानित प्राणों की चिन्ता क्या?
कार्नेलिया-नहीं चन्द्रगुप्त, मुझे इस देश से, जन्म भूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहां के श्याम कुञ्ज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैली-श्रेणी, हरी-भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमायें हैं। यह स्वप्नों का देश, वह त्याग और ज्ञान का पालन, यह प्रेम की रंग भूमि-भारतभूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्य की जन्म भूमि हैं, भारत मानवता की जन्म भूमि है।
-‘चन्द्रगुप्त’ नाटक, जयशंकर प्रसाद से ‘उपर्युक्त संवादों में दो मुख्य बातें देखने को मिलती है। सिल्योकस की पुत्री कार्नेलिया के चन्द्रगुप्त के प्रति प्रेम और भारत देश के प्रति अनुराग और श्रद्धा।
संक्षेपिका का कच्चा प्रारूप
चन्द्रगुप्त ने स्मृति को जीवन का पुरस्कार बताया और कार्नेलिया ने उसे प्रवास में हृदय को झकझोर देने वाला दण्ड। चन्द्रगुप्त ने कहा कि वह स्मृति को दण्ड मानती है तो वह उसे भी भूल जाए। इस जलते हुए उल्कापिण्ड की कोई कक्षा नहीं। कार्नेलिया ने उत्तर दिया कि ऐसी बात नहीं है। उसे इस देश के वन, पर्वत, नदियां, गर्मी-सर्दी, वर्षा चांदनी और धूप, बचपन में सुनी कहानियों को साकार करने वाले और प्रिय लगते हैं। यह भारत भूमि, जो प्रेम की रंग भूमि है, कभी भुलाई नहीं जा सकती। यह तो मनुष्य की नहीं, मानवता की जन्म-भूमि है।
आदर्श संक्षेपीकरण
जब चन्द्रगुप्त ने स्मृति को जीवन का पुरस्कार बताया तो कार्नेलिया ने उसे प्रवास का दण्ड कहा। इस पर चन्द्रगुप्त . ने कहा कि यदि ऐसा है तो वह उसे भूल जाए। कार्नेलिया ने अस्वीकृति के स्वर में कहा वह इस देश को कैसे भूल सकती है ? भारत के वन, पर्वत, नदियां, ऋतुएं बचपन में सुनी कहानियों को साकार कर देते हैं। यह देश प्रेम की रंगभूमि है। मनुष्य की नहीं, मानवता की जन्म भूमि है।
उदाहरण-3 मूल संवाद
सिपाही-महाराज का आदेश है कि जो हट्टा-कट्टा हो, उसे पकड़ कर फांसी पर चढ़ा दो।
गुरु ने शिष्य से धीरे से कहा-‘खा लिए लड्डू’ परन्तु गुरु घबराया नहीं। वह बड़ा समझदार था, उसने शिष्य के कान में कोई बात कह दी।
जब वे राजा के सामने फांसी के तख्ते के पास लाये गये तो गुरु ने कहा-“पहले मैं फांसी पर चढंगा।” शिष्य ने धक्का देकर कहा-“मेरा अधिकार पहले है।” वह आगे बढ़ा।
फांसी पर चढ़ने के लिए इस होड़ को देखकर राजा अचम्भे में था। उसने पूछा-‘भाई बात क्या है कि तुम दोनों फांसी पर चढ़ना चाहते हो?”
गुरु बोला-‘अरे महाराज मुझे चढ़ने भी दो, मेरा समय क्यों बरबाद करते हो?’ राजा ने कहा-आखिर कोई बात तो होगी ही।
गुरु ने कहा-अच्छा तुम बहुत हठ करते हो तो सुनो। इस समय स्वर्ग लोक में इन्द्र का आसन खाली पड़ा है। जो फांसी पर पहले चढ़ेगा, वही स्वर्ग का राजा होगा। राजा-अच्छा, यह बात है! तब तो मैं ही सबसे पहले फांसी पर चढुंगा।
संक्षेपीकरण
गुरु-शिष्य के पूछने पर कि उन्हें क्यों पकड़ा है, सिपाही ने राजा की आज्ञा बताई कि किसी हट्टे-कट्टे आदमी को फांसी पर चढ़ाना है। गुरु समझदार था, घबराया नहीं। उसने शिष्य के कान में कुछ कहा। फांसी के तख्ते के निकट लाये जाने पर दोनों गुरु-शिष्य पहले फांसी चढ़ने के लिए जिद्द करने लगे। राजा ने हैरान होकर इसका कारण पूछा तो गुरु ने कहा, इस समय स्वर्ग में इन्द्रासन खाली पड़ा है जो पहले फांसी चढ़ेगा वही उस आसन को पायेगा। राजा ने कहा तब तो वह ही सबसे पहले फांसी पर चढ़ेगा।
उदाहरण-4 मूल संवाद
यश-आप अंग्रेज़ी भी जानते हैं ?
कामरेड जगत हँसे–हाँ हाँ, क्यों? तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है?
यश-इसलिए कि इधर के जितने नेता हैं, वे दर्जा चार से आगे नहीं पढ़ सके। आप भी तो नेता ही हैं न।
कामरेड जगत बहुत ज़ोर से हँसे–’बहुत मज़ेदार हो दोस्त। हां कहो, तुम कौन हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं।’
यश-मैं इसी कस्बे का रहने वाला हूँ। विद्यार्थी हूँ। दर्जा सात का इम्तिहान दिया है। आप के बारे में बहुत सुना था। आप से मिलने की इच्छा बहुत दिनों से थी।
कामरेड जगत-क्यों, मुझ में ऐसी क्या खास बात है कि तुम मुझसे मिलना चाहते रहे? वे मुस्कराये। यश-मुझे हमेशा से लगता रहा है कि सेठ चोकर दास को आप मार सकते हैं। ‘क्या कहा?’ कामरेड चौंक गये थे। “क्या मेरे हाथ में बन्दूक है, क्या मैं हत्यारा हूँ?” यश थोड़ा डर गया और सोचने लगा कि क्या कह बैठा। फिर सम्भल कर बोला
“कामरेड, मेरे कहने का अर्थ दूसरा था। वह यह कि सेठ ग़रीबों का खून चूसता है और आप ग़रीबों की भलाई के लिए इतना सारा काम करते हैं। आप ही हैं जो ग़रीबों को सेठ या उन जैसे लोगों से छुड़ा सकते हैं। सेठ को मारने का मतलब उसके छल-कपट की ताकत को मारने का है।”
संक्षेपीकरण
यश ने जब कामरेड जगत को अंग्रेजी बोलते सुना तो हैरान हुआ। कामरेड के पूछने पर उसने बताया कि और नेता तो दर्जा चार तक पढ़े होते हैं। यश ने कामरेड को अपना परिचय दिया कि वह इसी गांव का है, दर्जा सात का इम्तिहान दिया है। उसने यह भी बताया कि वह उसको बहुत दिनों से मिलना चाहता था। कामरेड ने कारण पूछा तो यश ने कहा कि वह सेठ चोकर दास को मार सकता है। कामरेड ने कहा क्या उसके हाथ में कोई बन्दूक है? क्या वह हत्यारा है? इस पर यश डर गया कि क्या कह बैठा। उसने सम्भल कर कहा कि उसका अर्थ यह नहीं था। सेठ ग़रीबों का खून चूसता है और वह उनकी भलाई करता है। वह ही ग़रीबों को सेठ या उस जैसे लोगों से छुड़ा सकता है। सेठ को मारने से उसका भाव उसके छल-कपट को समाप्त करने से था।
संक्षेपीकरण के अभ्यासार्थ कुछ संवाद
-बाल सुलझाते-सुलझाते रूपमति ने उसकी नज़रों को पकड़ लिया और मुस्कराने लगी।
-“अब तुम जवान हो गये जस बाबू! ओह कितने दिन बीत गये तुम्हें यहां से गये हुए।” वह मुस्कराती रही लेकिन यश संकुचित हो गया।
– “मुझे प्यास लगी है रूपमति। पानी नहीं पिलाओगी।” -“पानी मैं कैसे पिलाऊं, बामण के लड़के को?” -“क्यों बामन का लड़का होना कोई गुनाह है, रूपमति? क्या उसे प्यास लगी हो तो पानी नहीं मांग सकता?”
-गुनाह तुम्हारा बामन होना नहीं, गुनाह है एक अछूत जाति की औरत से पानी मांगना। वह पानी तो पिला देगी लेकिन सोचो, तुम्हारी जाति वाले तुम्हें कहां रखेंगे और फिर तुम्हें तो दोष कम देंगे, मुझे ज्यादा गाली देंगे। खैर मुझे अपनी चिन्ता नहीं, तुम्हारी है।” वह मुस्कराती रही।
__-रूपमति, मुझे तुम पानी पिलाओ, अपनी जाति वालों से क्या, अपने घर वालों से भी कब का निष्कासित हो चुका हूं। अब मेरा कोई घर-द्वार, जाति-पाति नहीं है। जहां चाहूं जाऊंगा, जहां चाहूं रहूंगा, जहां चाहूं जिऊंगा, जहां चाहूं मरूंगा।
2.
मेरी आँख लगने को थी कि वह बोल उठा-“छुट्टी कब दोगी?”
– “पांच बजे” कह मैंने फिर आंख मूंद ली। वह बोला
– “स्कूल में भी चार बजे छुट्टी हो जाती है और नौकरी में पांच बजे ! मैंने स्कूल ही इसलिए छोड़ दिया था।” कुछ क्षण वह चुप रहा फिर बोला।
-“मां कहती थी स्कूल जाने से बाबू बनते हैं–पर नौकरी करने से क्या बनते हैं।”
मैं उसका प्रश्न सुन चौंक उठी और चुप रह गयी। कहती भी क्या-यही न कि नौकरी करने से पंखा कुली कहलाते
धीरे से बोली
– “तुम स्कूल जाया करो!”
-“स्कूल? स्कूल कैसे जाया करूं? मास्टर जी का गोल-गोल काला-काला मोटा रूल नहीं देखा तुम ने, तभी कहती हो! एक दिन मास्टर जी के मकान के पास से क्या निकले कि वो कहने लगे, तुम ने मेरे खेत की ककड़ियां तोड़ ली हैं। दूसरे दिन स्कूल में उन्होंने खूब पीटा। मैं नहीं गया स्कूल उसके बाद-और फिर स्कूल में चार बजे तक बैठना जो पड़ता है।”
3.
युवती-“मगर हमारा विवाह हो कैसे सकेगा?” युवती ने पूछा, “सुना है शीघ्र ही फिर उन भयानक विदेशी और विजातियों की चढ़ाई मेवाड़ पर होने वाली है। ऐसे अवसर पर तुम युद्ध करोगे या व्याह?”
युवक-“तुम्हारी क्या इच्छा है?”
युवती-(गर्व से) मैं यदि पुरुष होता तो ऐसे अवसर पर विदेशियों से युद्ध करती और जन्मभूमि मेवाड़ की उद्धार चिन्ता में प्राण दे देती।”
युवक-मगर पद्मा बुरा न मानना, मैं तो पहले तुम्हें चाहता हूं, फिर किसी और को। यदि युद्ध हुआ भी तो मैं पहले तुमसे व्याह करूंगा और फिर रण प्रस्थान।
युवती-(भंवों पर अनेक बल देकर) क्यों?
युवक-इसलिए कि तुम सी युवती सुन्दरियों का पता विदेशी सूंघते फिरते हैं। उन्हें यदि मालूम हो गया कि इस देवपुर रूपी गुदड़ी में पद्मा रूपी कोई मणि रहती है तो मुश्किल ही समझो।
युवती-(बगल से कटार निकाल कर दिखाती हुई) हि:! तुम भी कैसी बातें करते हो! जब तक यह मां दुर्गा हमारे साथ है तब तक विदेशी हमारी ओर क्या आंखें उठाएंगे। पिछले दो युद्धों में मेरी दो बड़ी विवाहिता बहनें जौहर कर चुकी है।
युवक-और मेरे तीन भाई वीरगति पा चुके हैं।
युवती—फिर क्या जब तक हम राजपूत स्त्री-पुरुषों को स्वतन्त्रता, स्वधर्म और स्वदेश के लिए प्राण देना आता है, तब तक एक विदेशी तो क्या, लाख विदेशी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
4.
बाज ने मनुष्य की आवाज़ में कहा:
“आप न्याय को जानने वाले राजा हैं। आप को किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। यह कबूतर मेरा भोजन है। आप इसे मुझे दे दीजिए।”
महाराज शिवि ने कहा:”
“तुम मनुष्य की भाषा में बोलते हो। तुम साधारण पक्षी नहीं हो सकते। तुम चाहे कोई भी हो, यह कबूतर मेरी शरण में आया है; मैं शरणागत को त्याग नहीं सकता।”
बाज बोला:
“मैं बहुत भूखा हूं। आप मेरा भोजन छीन कर मेरे प्राण क्यों लेते हैं ?”
राजा शिवि बोले:
“तुम्हारा काम तो किसी भी मांस से चल सकता है। तुम्हारे लिए यह कबूतर ही मारा जाये, इसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हें कितना मांस चाहिए?”
बाज कहने लगा:

“महाराज! कबूतर मरे या कोई दूसरा प्राणी मरे, मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। सभी प्राणी आप की प्रजा हैं, सब आपकी शरण में हैं। उनमें से जब किसी को मरना ही है, तो इस कबूतर को ही मारने में क्या दोष है। मैं तो ताज़ा मांस खाने वाला प्राणी हूं और अपवित्र मांस नहीं खाता। मुझे कोई लोभ भी नहीं है। इस कबूतर के बराबर तोल कर किसी पवित्र प्राणी का ताज़ा मांस मुझे दे दीजिए। उतने से ही मेरा पेट भर जाएगा।”
राजा ने विचार किया और बोले-“मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, अपना मांस ही मैं तुम को दूंगा।”
बाज बोला:
“एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर अपना शरीर क्यों काटते हैं ? आप फिर से सोच लीजिए।”
राजा ने कहा:
“बाज तुम्हें तो अपना पेट भरने से काम है। तुम मांस लो और अपना पेट भरो। मैंने सोच-समझ लिया है। मेरा शरीर कुछ अजर–अमर नहीं है। शरण में आए हुए एक प्राणी की रक्षा में शरीर लग जाए, इससे अच्छा इसका दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता।”
5.
-“तेरे घर कहां हैं?”
-“मगरे में; और तेरे?”
-“माझे में, यहां कहां रहती है?”
-‘अतर सिंह की बैठक में; वह मेरे मामा होते हैं।’
-‘मैं भी मामा के यहां आया हूं, उनका घर गुरु बाज़ार में है।’
इतने में दुकानदार निबटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ-साथ चले। कुछ दूर जा कर लड़के ने मुस्करा कर पूछा
‘तेरी कुड़माई हो गई।’
इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर ‘धत्त’ कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया।
(ख) समाचारों का संक्षेपीकरण
समाचार-पत्रों के कार्यालयों में संक्षेपीकरण अथवा संक्षेपिका लेखन का अत्यन्त महत्त्व है। यह कार्य प्रायः समाचारपत्र के सहायक या उपसंपादकों द्वारा किया जाता है। इसलिए इस कला में उन्हें पूर्ण दक्ष होना चाहिए। यह उनका दैनिक कार्य है। वैसे तो संक्षेपीकरण का कार्य पत्रों को समाचार भेजने वाले संवाददाता भी करते हैं किन्तु किसी घटना का, किसी नेता के भाषण का अथवा किसी महत्त्वपूर्ण सम्मेलन का ब्योरा समाचार-पत्र को भेजते समय वे तनिक विस्तार से उसका प्रतिवेदन भेजते हैं।
अब यह काम समाचार-पत्र के सह-सम्पादक, उप-संपादक का होता है कि संवाददाता द्वारा भेजे गए समाचार का इस तरह संक्षेपीकरण करे कि समाचार के महत्त्व के अनुसार उसका समाचार-पत्र में प्रकाशन हो सके और पाठक उस समाचार अथवा घटना इत्यादि के विवरण से अवगत भी हो सके। समाचार-पत्रों में स्थान की कमी के कारण कभी-कभी कुछ समाचार अत्यन्त संक्षिप्त रूप में प्रकाशित किये जाते हैं। ये संक्षिप्त समाचार समाचारपत्र के कार्यालय में संक्षेपीकरण के पश्चात् प्रकाशित किये जाते हैं। अतः समाचार-पत्र के सह-सम्पादक, उपसंपादक तथा संवाददाता के लिए संक्षेपीकरण की कला में प्रवीण होना अनिवार्य है।
समाचारों का संक्षेपीकरण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है
(1) नेताओं के भाषणों का संक्षेपीकरण करते समय नेता के नाम का उल्लेख अवश्य करना चाहिए।
(2) घटनाओं के विवरण का संक्षेपीकरण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस घटना के मुख्यमुख्य तथ्यों का उल्लेख अवश्य हो जाए। जैसे घटनास्थल, उससे प्रभावित लोगों के नाम अथवा संख्या तथा उस पर सरकार अथवा जनता की प्रतिक्रिया आदि।
(3) किसी समिति की बैठक अथवा किसी महत्त्वपूर्ण सम्मेलन के समाचार का संक्षेपीकरण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि संक्षेपिका में उस बैठक अथवा सम्मेलन के सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों का समावेश हो जाए। जैसे बैठक कहां, कब और किस की अध्यक्षता में हुई, उसका उद्देश्य क्या था तथा उसमें पारित कुछ महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव कौन-से थे।
ऐसे समाचारों का शीर्षक सभा या बैठक के अध्यक्ष या मुख्य मेहमान के भाषण के किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य को आधार बनाकर दिया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप किसी कॉलेज के दीक्षान्त समारोह के समाचार का शीर्षक लिखा जा सकता
“विद्यार्थी देश का भविष्य हैं-उपकुलपति……………
अथवा
“विद्यार्थी समाज सेवा के कामों में रुचि लें” इत्यादि।
(4) प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में बदल लेना चाहिए।
(5) आवश्यकतानुसार अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए ‘एक शब्द’ का प्रयोग करना चाहिए। समस्त पदों के प्रयोग की विधि अपनानी चाहिए।
(6) समाचार किसी भी प्रकार का हो उसमें तिथि, स्थान और सम्बद्ध व्यक्तियों के नाम अवश्य रहने चाहिएं।
(7) स्थानीय समाचारों में अधिक-से-अधिक स्थानीय व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से समाचार-पत्र की बिक्री बढ़ती है और उससे अधिक-से-अधिक लोग जुड़ते हैं।
(8) स्थानीय सभा-सोसाइटियों, गोष्ठियों, बैठकों आदि के समाचारों का संक्षेपीकरण करते समय यह न समझना चाहिए कि यह समाचार तो एक कोने में छपेगा, इसलिए जैसा चाहो छाप दो, ध्यान रहे जो लोग उस सभा सोसाइटी के सदस्य हैं वे तो उस समाचार को ढूंढ़ ही लेंगे। ऐसे समाचारों की भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए।
(9) जब कोई समाचार अनेक स्रोतों से प्राप्त हो तो सभी स्रोतों का नामोल्लेख समाचार से पूर्व अवश्य देना चाहिए जैसे प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया, यू० एन० आई० और हिन्दुस्तान समाचार से प्राप्त होने वाले समाचारों को मिलाकर उनका संक्षेपीकरण करना चाहिए। हो सकता है कि किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करना कोई समाचार एजेंसी भूल गयी हो।
(10) संक्षेपीकरण का यदि कच्चा प्रारूप पहले तैयार कर लिया जाए तो अच्छा रहता है।
समाचारों का संक्षेपीकरण : कुछ उदाहरण
उदाहरण 1
मूल समाचार
नई दिल्ली 5 जुलाई, …….., आज यहां शब्दावली आयोग की एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से सरकार को सुझाव दिया गया कि प्राध्यापकों की सीमित भाषागत सामर्थ्य को देखते हुए तथा उनको अध्यापन कार्य में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्राध्यापकों के लिए ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं, जिनसे उन्हें व्यावहारिक हिन्दी और परिभाषिक और तकनीकी शब्दावली के उचित प्रयोग के विषय में उनकी दक्षता में वृद्धि हो और अपने विषय को पढ़ाने की भाषा-सामर्थ्य भी बढ़े। ये कार्यशालाएं विश्वविद्यालयों और प्रमुख महाविद्यालयों में आयोजित की जाएंगी, जिनमें विशिष्ट भाषण देने के लिए ऐसे वरिष्ठ अध्यापक आमन्त्रित किये जाएंगे जो सफलतापूर्वक व्यावहारिक हिन्दी की कक्षाएं ले रहे हैं।
संक्षेपीकरण (कच्चा प्रारूप)
नई दिल्ली 5 जुलाई, ………..-शब्दावली आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह प्राध्यापकों को व्यावहारिक हिन्दी और पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली के प्रयोग और अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करे जो प्राध्यापकों की इस विषय सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर कर उनकी भाषा सामर्थ्य और दक्षता में वृद्धि कर सकें। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं जिनमें कुछ वरिष्ठ प्राध्यापकों को भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया जाए।
आदर्श संक्षेपीकरण
नई दिल्ली-5 जुलाई। शब्दावली आयोग ने व्यावहारिक हिन्दी एवं पारिभाषिक शब्दावली के पठन-पाठन की कठिनाइयों को दूर करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य की कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश दें।
उदाहरण-2
मूल समाचार
नई दिल्ली 26 मार्च, ……. – भारतीय लेखक संगठन के तत्वाधान में आज यहां के कांस्टीट्यूशन क्लब में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें जीवन के पैंसठ वर्ष पूरा करने पर हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार रामदरश मिश्र को सम्मानित किया गया। इस गोष्ठी में डॉ० नित्यानन्द तिवारी और डॉ० ज्ञानचन्द्र गुप्त के संपादन में प्रकाशित पुस्तक ‘रचनाकार रामदरश मिश्र’ पर भी चर्चा की गई जिसमें दिल्ली और बाहर के अनेक गण्यमान्य और नये रचनाकारों ने भाग लिया। चर्चा में भाग लेते हुए कन्हैयालाल नन्दन में मिश्रजी से शिकायत की कि वे अब गीत क्यों नहीं लिखते। महीप सिंह ने कहा कि मिश्र जी ने अंतरंग मानवीय सम्बन्ध की गरिमा हमेशा बनाये रखी। लेखन के प्रति समर्पित व प्रतिबद्ध मिश्र जी ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया।
नरेन्द्र मोहन ने कहा कि मिश्रजी के साहित्य में अपनी जमीन से जुड़े रहने का संवेदन और उसकी अनुभूति के दर्शन होते हैं। डॉ० रमाकान्त शुक्ल ने कहा कि मिश्र जी ने बड़ी-बड़ी बातें नहीं की बल्कि छोटी-छोटी बातों को संवेदनशील ढंग से सामने रखा और विशिष्ट शैली अर्जित की।
मुख्य अतिथि कमलेश्वर ने कहा कि मिश्र जी में आक्रोश है किन्तु उत्तेजना नहीं। मिश्र जी को आक्रोश की शक्ति का प्रयोग और अधिक करना चाहिए। मिश्र जी में अहम् नहीं है, ठोस स्वाभिमान है। स्वयं मिश्र जी ने अपने सम्बन्ध में कहा कि मैं बहुत मामूली इन्सान हूं मुझे इस बात का बोध हमेशा रहा, नहीं तो मैं आज महत्त्वाकांक्षा के जंगल में खो गया होता। संगठन सचिव डॉ० रत्न लाल शर्मा ने गोष्ठी का संचालन किया तथा महासचिव डॉ० विनय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
संक्षेपीकरण
नई दिल्ली 26 मार्च,………..- भारतीय लेखक संगठन ने प्रसिद्ध उपन्यासकार रामदरश मिश्र के जीवन के पैंसठ वर्ष पूरा करने पर उन्हें सम्मानित करने हेतु एक गोष्ठी आयोजन किया गोष्ठी में डॉ० नित्यानन्द तिवारी और डॉ० ज्ञान चन्द गुप्त द्वारा संपादित पुस्तक ‘रचनाकार रामदरथ मिश्र’ पर भी चर्चा की गयी। चर्चा में भाग लेने वालों में मुख्य विद्वान् थे-कन्हैया लाल नन्दन, महीपसिंह, नरेन्द्र मोहन तथा गोष्ठी के मुख्य मेहमान कमलेश्वर। मिश्र जी ने अपने सम्बन्ध में कही गयी बातों का उत्तर देते हुए कहा कि वे बहुत मामूली इंसान हैं और उन्हें सदा इस बात का बोध रहा है, नहीं तो वे आज महत्त्वाकांक्षा के जंगल में खो गये होते। गोष्ठी का संचालन संगठन के साहित्य सचिव डॉ० रत्नलाल शर्मा ने किया तथा महासचिव डॉ० विनय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
उदाहरण-3
मूल समाचार
पेरिस, 25 नवम्बर (ए० पी०) विश्व प्रसिद्ध धावक बेन जानसन ने कल फ्रांसीसी टैलीविजन के एक कार्यक्रम में भी स्वीकार किया कि उसने 1988 के सियोल ओलम्पिक में नशीले पदार्थ का सेवन किया था। इस कार्यक्रम में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के मेडिकल कमीशन के प्रमुख प्रिंस एलेक्जेंडर डी-मेरोड भो शामिल थे। उन्होंने कहा कि–“बेन जानसन की धोखा–धड़ी से उन्हें काफ़ी गहरा दुःख हुआ था लेकिन इस घटना से नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ हमारी लड़ाई और तेज़ हो गई।”
बेन जानसन की मेडिकल जांच के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन की पुष्टि होने के समय श्री मेरोड भी उस समय मंच पर थे। इस घटना के बाद पहली बार दोनों का इस कार्यक्रम में आमना-सामना हुआ। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ फ्रांसीसी एथलीट, प्रशिक्षक और खेल संगठनों के अधिकारी भी शामिल थे।
जानसन ने न केवल 1992 ओलम्पिक में भाग लेने की बल्कि 1991 में टोक्यो में विश्व इंडोर चैम्पियनशिप में भाग लेने की इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि वह कड़ी मेहनत कर रहा है और अगले ओलम्पिक में तेज़ दौड़ेगा तथा टोक्यो में वह सबको पीछे छोड़ देगा।

संक्षेपीकरण
टोक्यो में सबको पीछे छोड़ दूँगा : जॉनसन
पेरिस, 25 नवम्बर (ए० पी०) विश्व प्रसिद्ध धावक बेन जॉनसन ने कल यहां फ्रांसीसी टेलीविज़न से प्रसारित एक कार्यक्रम में 1988 के सियोल ओलम्पिक में नशीले पदार्थों के सेवन को स्वीकार किया। इसी कार्यक्रम के अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के मैडिकल कमीशन के प्रमुख श्री मेरोड ने कहा कि जॉनसन की धोखाधड़ी से उन्हें गहरा दुःख हुआ था। वे नशीले पदार्थों के सेवन के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
जॉनसन की डॉक्टरी जांच के दौरान श्री मेरोड भी वहीं मौजूद थे। इस घटना के पश्चात् पहली बार दोनों इस कार्यक्रम में आमने-सामने हुए थे। इस कार्यक्रम में फ्रांस के वरिष्ठ एथलीट, प्रशिक्षक और खेल संगठनों के अधिकारी भी मौजूद थे। बेन जॉनसन ने कहा कि उसकी इच्छा है कि वह 1991 के टोक्यो में होने वाली इन्डोर चैम्पियनशिप तथा 1992 के ओलम्पिक में भाग ले। उसके लिए वह अभी से कड़ी मेहनत कर रहा है और उसे पूरी आशा है कि इन दोनों प्रतियोगिताओं में सबको पीछे छोड़ देगा।
उदाहरण-4
मूल समाचार
चण्डीगढ़ 20 जनवरी (संघी); मध्यम आय वर्ग के ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने दो नई योजनाएं ‘स्कूम’ तथा ‘ट्रैवल कैश’ शुरू की हैं। इस पहली योजना के तहत नए दोपहिया वाहन जैसे स्कूटर, मोटर साइकिल तथा मोपेड खरीदने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है। बैंक के चीफ जनरल मैनेजर श्री जी० एच० देवलालकर ने यहां पत्रकारों को बताया है कि जो कर्मचारी न्यूनतम 1000 रु० मासिक शुद्ध वेतन लेते हैं, वे इस वेतन का 12 गुणा या खरीदे जाने वाले वाहन की कीमत का 90% जो भी कम होगा, ऋण रूप में ले सकते हैं। इस ऋण पर 16.5% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा और इस ऋण की वसूली 36 बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी।
उन्होंने बताया कि ‘ट्रैवल कैश’ के तहत विभिन्न संस्थानों (सरकारी, सार्वजनिक और निजी) के कर्मचारी देश भर में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए ऋण ले सकते हैं बशर्ते कि पिछले छः मास के दौरान बैंक के चालू खाते में उनकी पर्याप्त बचत हो। यह ऋण मासिक आय की चार गुना राशि या परिवार के बस/रेल/हवाई टिकट का खर्च या 30000 रु० जो भी कम हो, लिया जा सकता है। 17.5% वार्षिक ब्याज दर वाले इस ऋण की वसूली 12 मासिक बराबर किस्तों में की जाएगी।
संक्षेपीकरण
स्टेट बैंक की मध्यम वर्ग के लोगों के लिए दो नई योजनाएँ
चण्डीगढ़ 20 जनवरी-भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महा प्रबन्धक श्री जी० एच देवलालकर ने यहां पत्रकारों को बताया कि उनके बैंक ने मध्यम आय वर्ग के ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए दो नई योजनाएं स्कूम’ तथा ‘ट्रैवल कैश’ शुरू की है। पहली योजना के अन्तर्गत दोपहिया नये वाहन खरीदने के लिए ऋण दिया जाएगा। यह ऋण, 1000 रु० मासिक शुद्ध वेतन पाने वालों को उनके वेतन के बारह गुणा अथवा वाहन का 90% जो भी कम होगा, के बराबर होगा। इस ऋण की ब्याज-दर 16.5% होगी और इसकी वसूली 36 बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी।
उन्होंने दूसरी योजना का ब्यौरा देते हुए बताया कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वह किसी भी संस्थान, सरकारी या गैरसरकारी में कार्यरत हो, देशभर में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए ऋण ले सकता है किन्तु उतनी राशि उसके बचत स्रोत में पिछले छः मास से होनी ज़रूरी है। यह ऋण, मासिक आय का चार गुना अथवा वास्तविक यात्रा टिकट का खर्चा अथवा वह राशि जो 30000 रु० से कम हो, लिया जा सकता है। इस ऋण की ब्याज दर 17.5% होगी और वसूली 12 बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी।
उदाहरण-5
मूल समाचार
वेलिंगटन, 24 मार्च (ए०पी०) इस महीने के शुरू में क्रिकेट जीवन से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले न्यूज़ीलैण्ड के हरफनमौला रिचर्ड हैडली ने आज कहा कि इंग्लैण्ड जाने वाली अपने देश की भ्रमणकारी क्रिकेट टीम में वह भी शामिल होंगे। न्यूज़ीलैण्ड की टीम के चयनकर्ताओं ने 16 खिलाड़ियों की जिस टीम की घोषणा की है, उसमें हैडली तथा कप्तान जान राइट भी शामिल हैं। इससे पूर्व उन्होंने इंग्लैण्ड के दौरे पर जाने अथवा न जाने के बारे में कुछ नहीं बताया था। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट मैचों में रिकार्ड विकेट लेने वाले हैडली ने इस महीने के शुरू में वेलिंगटन में ऑस्ट्रेलियाई टीम के विरुद्ध नौ विकेट की जीत के बाद कहा था कि यह उसके जीवन का अन्तिम टेस्ट मैच होगा, लेकिन बाद में उसने अपना विचार बदल कर कहा कि वह भ्रमणकारी टीम में शामिल होगा।
संक्षेपीकरण
हैडली द्वारा संन्यास का इरादा फिलहाल स्थगित!
वेलिंगटन, 25 मार्च (ए०पी०)-टैस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले न्यूज़ीलैण्ड के गेंदबाज़ रिचर्ड हैडली ने इस महीने के शुरू में वेलिंगटन में ऑस्ट्रेलियाई टीम के विरुद्ध नौ विकेट लेने के पश्चात् क्रिकेट जगत् से संन्यास लेने की जो बात कही थी, लगता है उन्होंने अपना यह निर्णय अभी स्थगित कर दिया है। इंग्लैण्ड के दौरे पर जाने वाली न्यूज़ीलैण्ड की टीम में उनका नाम भी शामिल है।
गद्यांशों का सार
उदाहरण-1
अनुशासनहीनता एक प्रचंडतम संक्रामक बीमारी है। आग की तरह यह फैलती है और आग की ही तरह जो कुछ इसके अधीन आता जाता है, उसे ध्वस्त करती जाती है। अत: हर स्तर पर जो भी संचालक अथवा प्रभारी है, उसका यह प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि अनुशासनहीनता के पहले लक्षणों को देखते ही उसका प्रभावी उपचार कर दें अन्यथा यह बीमारी सम्पूर्ण राष्ट्र का ही पतन कर सकती है। वस्तुतः अनुशासन शिथिल होने का अर्थ है, मूल्यों और मान्यताओं का अवमूल्यन होना और जब ऐसा होता है तो कोई भी राष्ट्र अथवा सभ्यता कितनी ही दिव्य क्यों न हो, नष्ट हो जाएगी। अनुशासित हुए बिना कोई समाज, कोई विभाग या कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। इतना ही नहीं अनुशासन के बिना किसी देश से दरिद्रता, अन्याय आपसी फूट और वैमनस्थ कभी दूर नहीं हो सकते।
संक्षेपीकरण शीर्षक : अनुशासनहीनता
अनुशासनहीनता का अर्थ है-मूल्यों और मान्यताओं का अवमूल्यन होना और ऐसी स्थिति में कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र भी नष्ट हो सकता है। अनुशासनहीनता के कारण कोई समाज, विभाग या राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता न ही इससे अन्याय और पारस्परिक भेदभाव मिट सकते हैं।
उदाहरण-2
गुरु गोबिन्द सिंह जी का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति के जीवन-दर्शन के ताने बाने से बुना गया था। यही व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हुआ है। उनका ‘दशमग्रंथ’ अन्याय के प्रतिकार के लिए सत्य के लिए, आत्म बलिदान हेतु और अन्तरम को परिकृत और सरस बनाने के लिए नियोजित काव्य और देश और काल की सीमाओं के माध्यम से सीमातीत को हृदयंगम कराने का आध्यात्मिक प्रतीक है। वह महान भारतीय संस्कृति का कवच है और शुष्क वैयक्तिक साधना के स्थान पर सरस धार्मिक जीवन का संदेशवाहक है। वह कायरता, भीरूता और निष्कर्म पर कस के कुशाघात है। वह छुपी हुई जाति का प्राणप्रद संजीवन-रस है और मोहनग्रस्त समाज का मूर्छा-मोचन रसायन है।
संक्षेपीकरण शीर्षक : दशमग्रंथ
गरु गोबिन्द सिंह जी द्वारा रचित ‘दशमग्रंथ’ गुरु जी के व्यक्तित्व यथा अन्याय के विरुद्ध लड़ना, सत्य के लिए आत्मबलिदान तक को तत्पर रहने जैसे गुणों का द्योतक है। यह भारतीय संस्कृति का कवच है जो वैयक्तिक साधन के स्थान पर धार्मिक जीवन का सन्देश देता है।
उदाहरण-3
‘मध्यकालीन ब्रज संस्कृति के दो पक्ष हो सकते हैं। पहला, नगर-सभ्यता, दूसरा कृषक-समाज। पहले का प्रतिनिधित्व मथुरा करती है और गोपियां उसे अपनी पीड़ा का कारण मानते हुए कोसती हैं। उनके लिए तो मथुरा काजल की कोठरी है इसीलिए वे मथुरा की नागरिकाओं को कोसती हैं, कुब्जा पर व्यंग्य करती हैं। सूरदास की रचनाओं में जो ब्रज मंडल उपस्थित है, वह ग्राम-जन, कृषक-समाज और चरवाहों की ज़िन्दगी का समाज है-सीधा-सादा, सरल, निश्छल। सूरदास की सृजनशीलता यह है कि ब्रजमंडल का लगभग समूचा सांस्कृतिक जगत् अपने संस्कारों, त्योहारों, जीवन-चर्चा की कुछ झांकियों और शब्दावली के साथ यहां प्रवेश कर जाता है।
संक्षेपीकरण शीर्षक : मध्यकालीन ब्रज संस्कृति
सर के काव्य में ब्रजमण्डल की कृषक संस्कृति अपनी सम्पूर्ण उत्सवशीलता के साथ झूम रही है। वहां मथुरा के रूप में नागर संस्कृति भी है तो सही, परन्तु गोपियों के माध्यम से उसे निन्दा और उपहास का पात्र ही बनाया गया है। वस्तुतः सूरदास ग्राम्य-संस्कृति के चितेरे कवि हैं।
उदाहरण-4
किसी नेता द्वारा रामपुर में 14 अक्तूबर को दिए गए भाषण का अंश-
हमने अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में इस इलाके के विकास के लिए जो कुछ किया है, उसे यदि अपने मुँह से कहूँ तो कोई कह सकता है, अपने मुँह मियाँ मिठू। लेकिन भाइयो, यदि मैं वह सब आपको नहीं बताऊँगा तो आप ही कहिए, किस हक से मैं आपसे फिर से वोट मांगूंगा। मैंने पाँच सालों से इस इलाके के लिए अपना खून-पसीना बहाया है। कोई भी अपनी समस्या लेकर आया, मैंने उसका समाधान करने की भरसक कोशिश की। आज जब मेरी जीप इस रैली-स्थल की ओर आ रही थी तो सड़क की बढ़िया हालत देख मुझे विश्वास हो गया जो पैसा मैंने इस इलाके के विकास के लिए आबंटित किया था, उसका सही उपयोग हुआ है। भाइयो, मैं गलत तो नहीं कह रहा न ? आपने भी तो आज उस सड़क को देखा ही होगा !
याद करो पाँच साल पहले उस सड़क की हालत कैसी थी ? जगह-जगह गड्ढे, उनमें भरा हुआ पानी और वो गड्ढे तो होने ही थे। किया क्या था हमारे प्रतिपक्षियों ने ? भाइयो, अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ ? और अपने बारे में ही क्या बोलूँ ? हमारा तो काम बोलता है। हमारा तो धर्म ही आपकी सेवा करना है। यदि मेरी जान भी चली जाए तो भी परवाह नहीं। भाइयो, देश-सेवा का, आप सबकी सेवा का व्रत मैंने तो तब ही ले लिया था जब मैं राजनीति में आया था।………….’ (संवाददाता द्वारा उपर्युक्त भाषण के आधार पर बनाया गया संक्षिप्त समाचार)
संक्षेपीकरण शीर्षक : ‘देश के लिए कुर्बान मेरी जान’……. (नाम)
रामपुर, 14 अक्तूबर
एक स्थानीय चुनाव-सभा को सम्बोधित करते हुए………… पार्टी के नेता श्री …………. ने अपनी पार्टी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सड़क-निर्माण के क्षेत्र में उनकी पार्टी द्वारा किए गए कार्य का बार-बार उल्लेख किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने विरोधी दलों पर कई बार चुटीला व्यंग्य भी कसा।
उदाहरण-5
सोमा बुआ बोली, “अरे मैं कहीं चली जाऊं तो इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोली लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्यौता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गरूर है कि मुण्डन पर भी सारी बिरादरी का न्यौता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से सम्भलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही,” और सरककर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। “एक काम गत से नहीं हो रहा था। भट्टी पर देखो तो अजब तमाशासमोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि दो बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम किए कि एक पंगत में भी पूरे न पड़ें। उसी समय मैदा बनाकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊँ।”
सार:
सोमा बुआ को काम का बहुत अनुभव है। उनके बिना कहीं भी कोई काम अच्छी प्रकार से नहीं होता है। इसीलिए वे सभी जगह काम को अपने काम तरह करती है। इसलिए सभी जगह उनका मान होता है।
शीर्षक:
सोमा बुआ।
उदाहरण-6
सुख की तरह सफलता भी ऐसी चीज़ है जिसकी चाह प्रत्येक मनुष्य के दिल में बसी मिलती है। इन्सान की तो बात ही क्या है, हर जीव अपने अस्तित्व के उद्देश्य को निरन्तर पूरा करने में लगा ही रहता है और अपने जीवन को सफल बना जाता है। यही हाल पदार्थों तक का है, उनकी भी कीमत तभी है जब तक वे अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। एक छोटी-सी माचिस भी जब कभी बहुत सील जाती है और जलने में असफल हो जाती है, तो उसे कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाता है। टॉर्च से सेल बल्ब जलाने में असमर्थ हो जाते हैं तो बिना किसी मोह के उन्हें निकाल कर फेंक दिया जाता है। जाहिर है, किसी वस्तु की कीमत तभी तक है, जब तक वह सफल है। इसी तरह हर इन्सान की कीमत भी तभी तक है, जब तक वह सफल है। शायद इसीलिए इन्सान सफलता का उतना ही प्यासा रहता है, जितना सुख का, या जितना जिन्दा रहने का। सफलता ही किसी के जीवन को मूल्यवान बनाती है। मगर सफलता है क्या ?
सार:
सफलता मनुष्य जीवन को मूल्यवान् बना देती है। सफल मनुष्य जीवन में सुख का अनुभव करता है इसीलिए वह सफलता के लिए प्रयत्नशील रहता है। परन्तु सफलता क्या है इसका आज तक पता नहीं चला है। सफल मनुष्य भी सफलता के पीछे दौड़ रहा है।
शीर्षक:
सफलता की चाह।

उदाहरण-7
सम्पूर्ण सृष्टि में, सूक्ष्मतम जीवाणु से लेकर समस्त जीव-जन्तु ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण वनस्पति तथा सृष्टि के समस्त तत्व, बिना किसी आलस्य के, प्रकृति द्वारा निर्धारित, अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति में निरन्तर लगे हुए देखे जाते हैं। कहीं भी, किसी भी स्तर पर इस नियम का अपवाद देखने को नहीं मिलता। यदि लघुतम एन्जाइम भी अपने कर्त्तव्य में किंचित् भी शिथिलता ले आए, तो मानव खाए हुए भोजन को पचा भी न सकेगा। कैसी विडम्बना है कि अपने को प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना कहने वाला मनुष्य ही इस सम्पूर्ण विधान में अपवाद बनते देखा जाता है। कितने ही मनुष्य नितान्त निरुद्देश्य जीवन-जीते रहते हैं। जो प्रकृति उनका पोषण करती है, जिन असंख्य मानव-रत्नों के श्रम से प्राप्त सुख-सामग्री की असंख्य वस्तुओं का वे नित्य उपभोग करते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिन माता-पिता से उन्होंने जन्म पाया, उन सभी के प्रति मानो उनका कोई दायित्व ही न हो।
सार:
ईश्वर की बनाई सृष्टि में सभी जीव-जन्तु, वनस्पति तथा अन्य तत्त्व अपने कर्त्तव्य और उद्देश्य की पूर्ति निरन्तर करते हैं परन्तु ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना अर्थात् मनुष्य अपने दायित्व के प्रति उदासीन है। वह सबसे लेना जानता है परन्तु अपने कर्तव्यों को पूरा करना नहीं जानता।
शीर्षक:
मनुष्य : अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीन।
उदाहरण-8
‘मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे अन्य लोगों से मेल या सम्पर्क करना होता है। घर से बाहर निकलते ही उसे किसी मित्र या साथी की आवश्यकता पड़ती है। मित्र ही व्यक्ति के सुख-दुख में सहायक होता है पर किसी को मित्र बनाने से पहले मित्रता की परख कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति घोड़े को खरीदते समय उसकी अच्छी प्रकार जाँच-पड़ताल करता है, उसी प्रकार मित्र को भी जांच-परख लेना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है, जो किसी भी प्रकार की विपत्ति में हमारे काम आता है या हमारी सहायता करता है। सच्चा मित्र हमें बुराई के रास्ते पर जाने से रोकता है तथा सन्मार्ग की ओर ले जाता है। वह हमारी अमीरी-गरीबी को नहीं देखता, जात-पात को महत्ता नहीं देता। वह निःस्वार्थ भाव से मित्र की सहायता करता है। सच्चे मित्र को औषधि, वैद्य और खजाना कहा गया है क्योंकि वह औषधि की तरह हमारे विचारों खो शुद्ध बनाता है, वैद्य की तरह हमारा इलाज करता है, खज़ाने की तरह मुसीबत में हमारी सहायता करता है। आज के जीवन में सच्चा मित्र प्राप्त करना बहुत कठिन है। स्वार्थी मित्रों की आज भरमार है। ऐसे स्वार्थी मित्रों से मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। सच्चा मित्र जीवनभर मित्रता के पवित्र सम्बन्ध को निभाता है-कृष्ण और सुदामा की तरह।’
सार:
सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को मित्र की आवश्यकता पड़ती ही है। यदि भली-भांति जांच-परख कर मित्र बनाया जाए तो ऐसा मित्र सुख-दुख में हमारा सहायक तो होता है, वह हमारा मार्गदर्शक तथा हितैषी भी होता है। आज के स्वार्थ-लोलुप युग में सच्चा मित्र मिलना दुर्लभ है। जिसे वह मिल जाएगा, उसे उस मित्री की मैत्री जीवनभर सम्भालने और निभाने का प्रयास करना चाहिए।
शीषर्क:
सच्ची मित्रता।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()