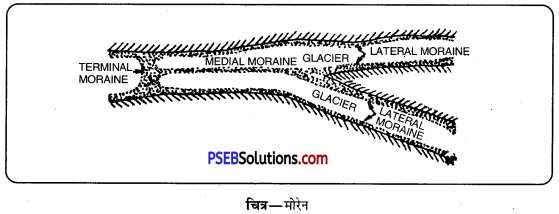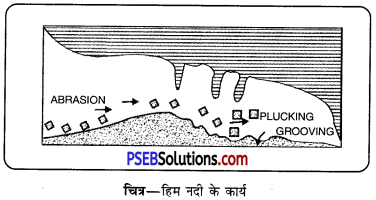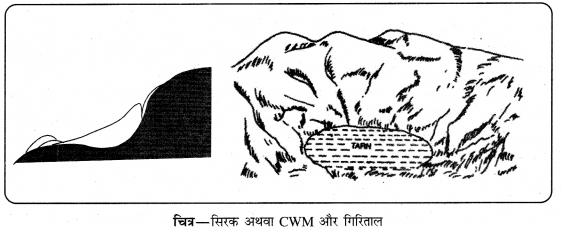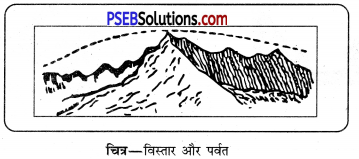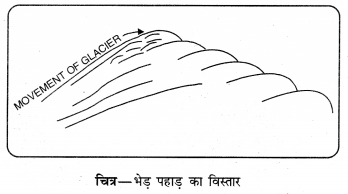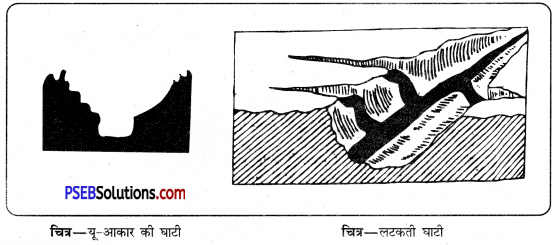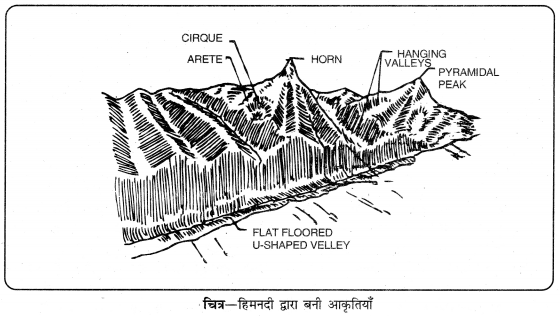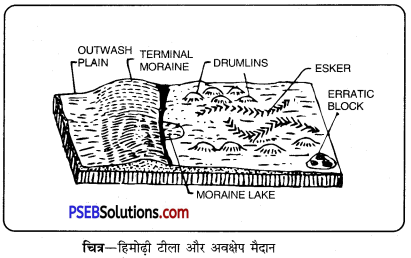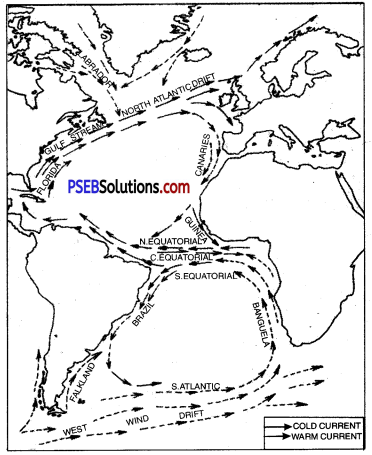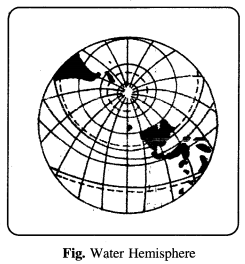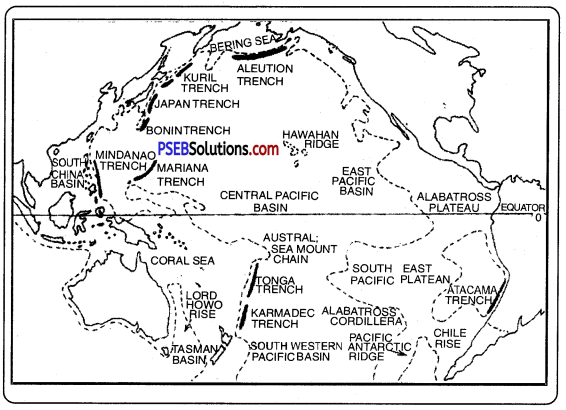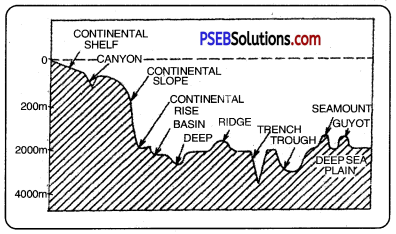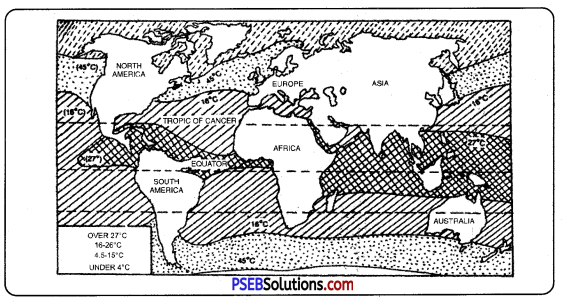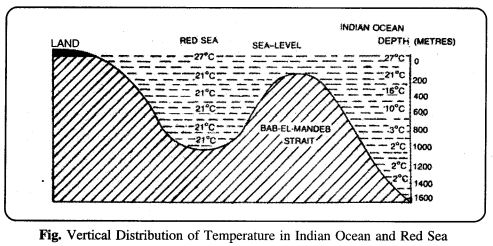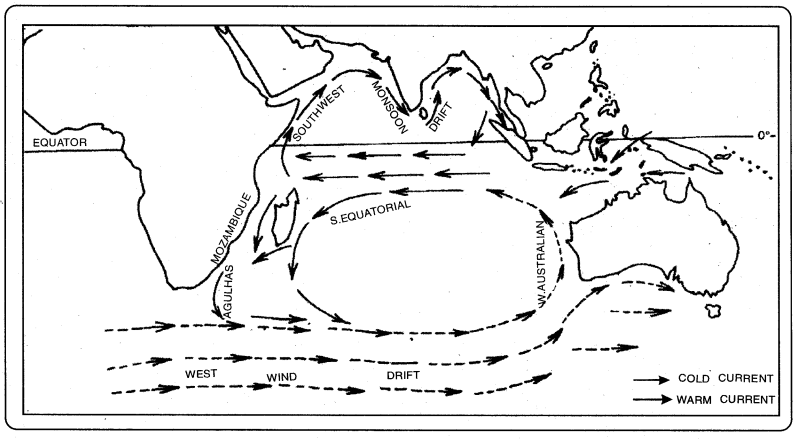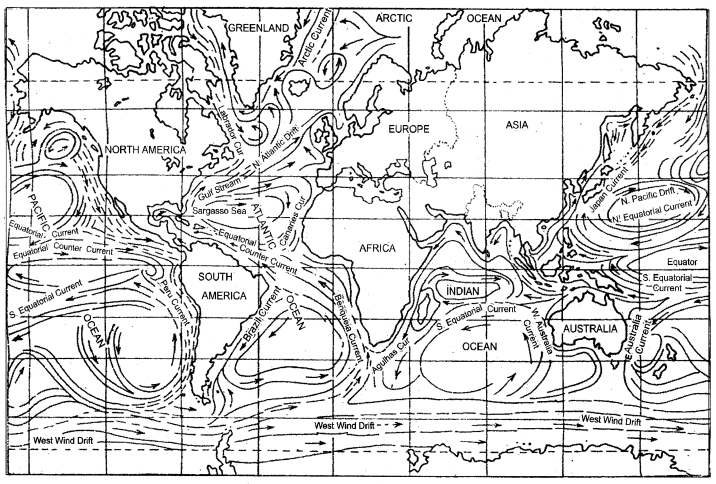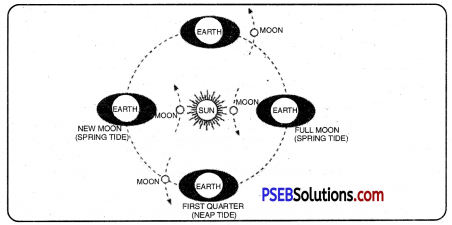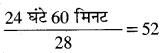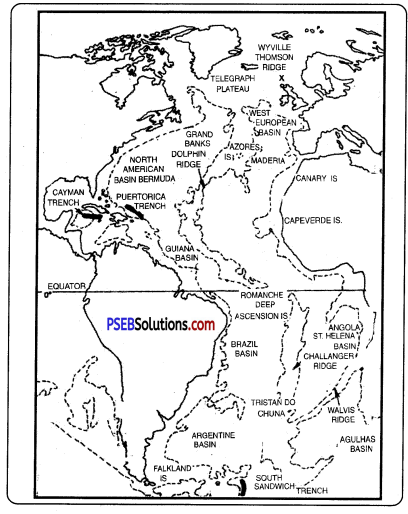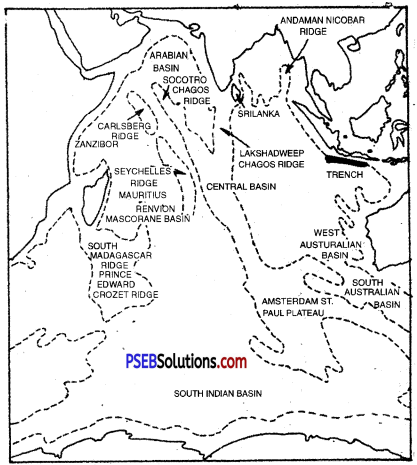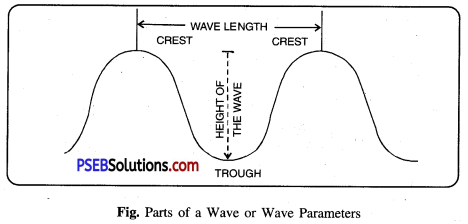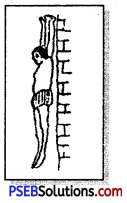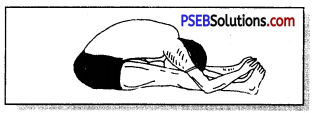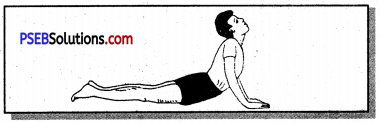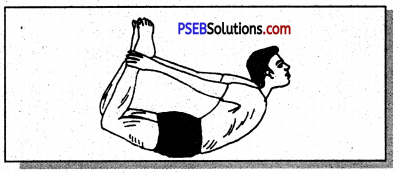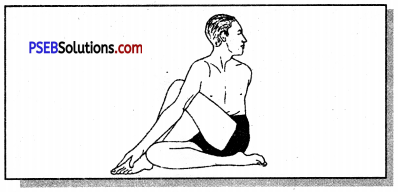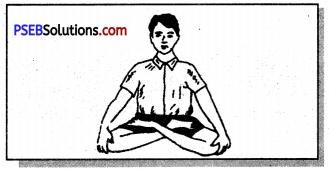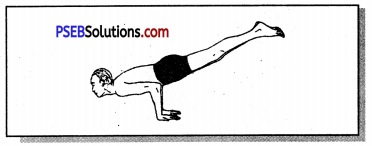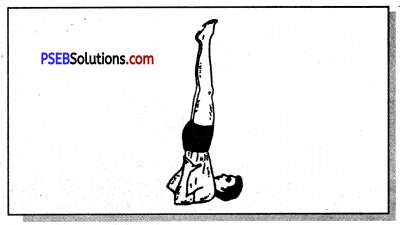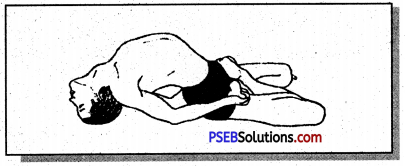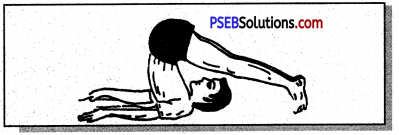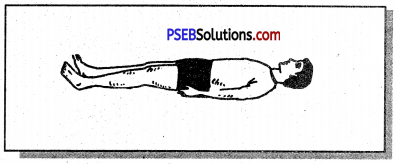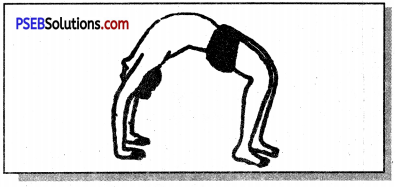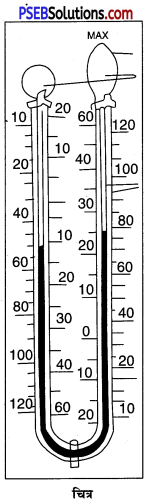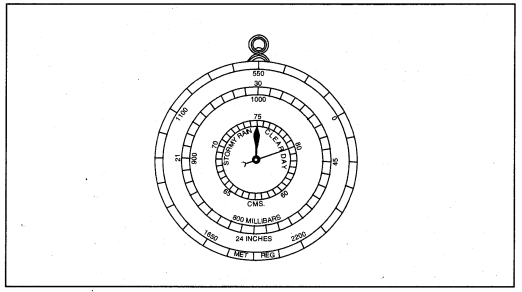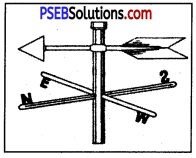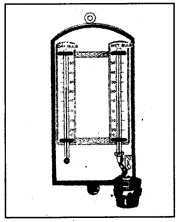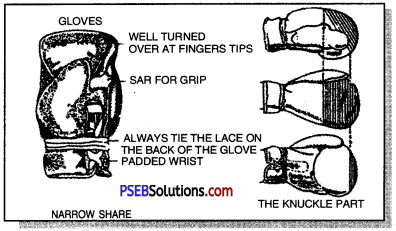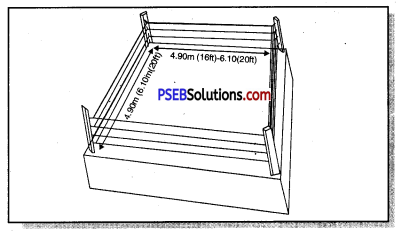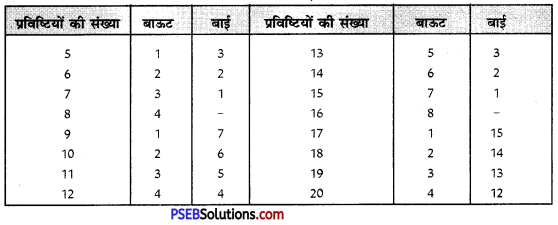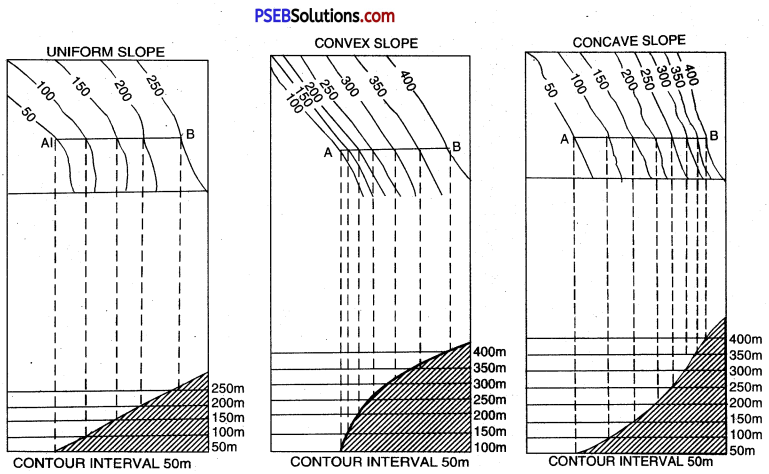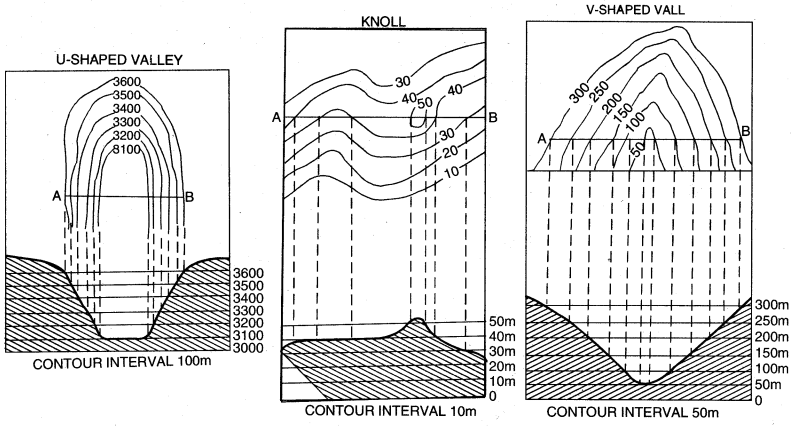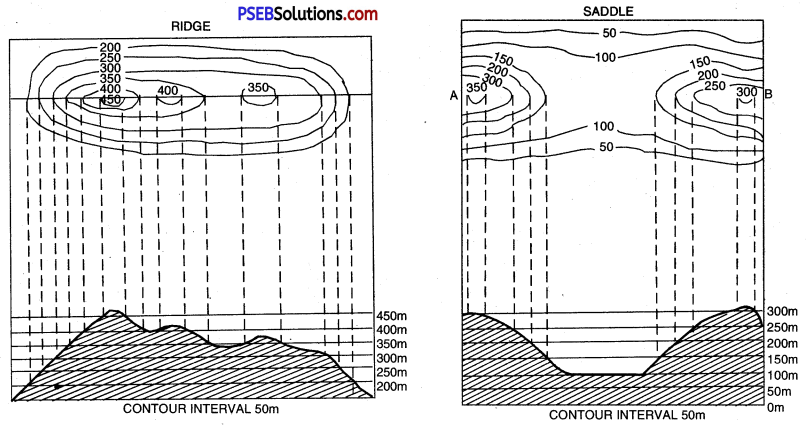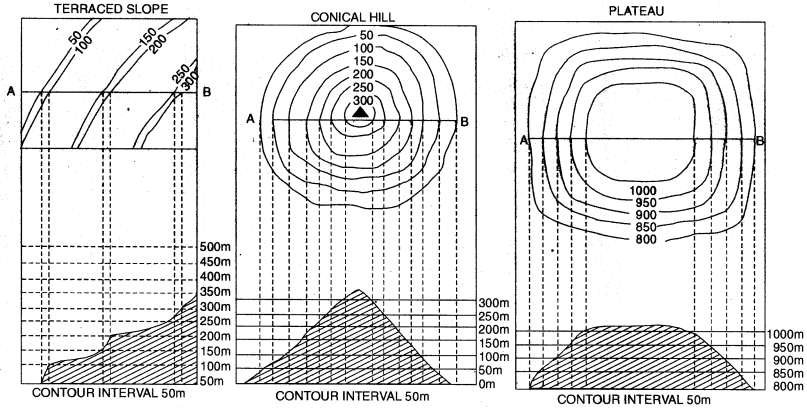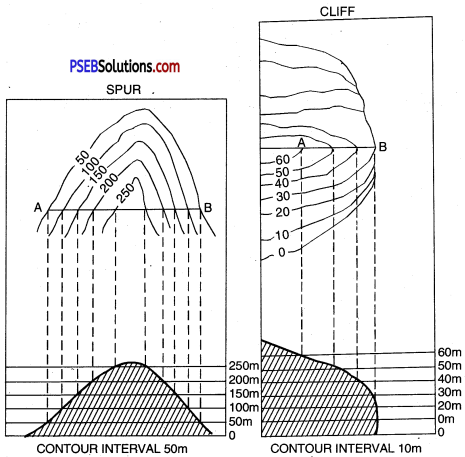Punjab State Board PSEB 11th Class Sociology Book Solutions Chapter 7 विवाह, परिवार तथा नातेदारी Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 11 Sociology Chapter 7 विवाह, परिवार तथा नातेदारी
पाठ्य-पुस्तक के प्रश्न (Textual Questions)
I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-15 शब्दों में दीजिए :
प्रश्न 1.
अन्तर्विवाह से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर-
वह विवाह जिसमें व्यक्ति को एक निश्चित समूह, जाति या उपजाति के अंदर ही विवाह करवाना पड़े, अन्तर्विवाह होता है।
प्रश्न 2.
विवाह संस्था की उत्पत्ति के कोई दो महत्त्वपूर्ण आधार बताइये।
उत्तर-
शारीरिक आवश्यकता, भावात्मक आवश्यकता, समाज को आगे बढ़ाना तथा बच्चों का पालन-पोषण करके विवाह की संस्था सामने आयी।
प्रश्न 3.
एक विवाह किसे कहते हैं ?
उत्तर-
जब एक पुरुष का एक समय में एक स्त्री के साथ विवाह होता है तो इसे एक विवाह का नाम दिया जाता है।
प्रश्न 4.
साली विवाह किसे कहते हैं ?
उत्तर-
जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् उसकी बहन से विवाह कर लेता है तो उसे साली विवाह कहते हैं।

प्रश्न 5.
बहुपति विवाह के प्रकार बताइये।
उत्तर-
यह दो प्रकार का होता है-भातृ बहुपति विवाह जिसमें स्त्री के सभी पति भाई होते हैं तथा अभ्रातृ बहुपति विवाह जिसमें स्त्री के सभी पति भाई नहीं होते।
प्रश्न 6.
बहुपत्नी विवाह के प्रकार बताइये।
उत्तर-
यह दो प्रकार का होता है-द्वि-पत्नी विवाह जिसमें एक व्यक्ति की दो पत्नियाँ होती हैं तथा बहुपत्नी विवाह जिसमें व्यक्ति की कई पत्नियाँ होती हैं।
प्रश्न 7.
अन्तर्विवाह के कुछ उदाहरण दीजिए।
उत्तर-
मुसलमानों में शिया तथा सुन्नी अन्तर्वैवाहिक समूह हैं। ईसाइयों में रोमन कैथोलिक तथा प्रोटैस्टैंट अन्तर्वैवाहिक समूह है।
प्रश्न 8.
विवाह को परिभाषित कीजिए।
उत्तर-
लुण्डबर्ग के अनुसार, “विवाह के नियम तथा तौर-तरीके होते हैं जो पति पत्नी के एक-दूसरे के प्रति अधिकारों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों का वर्णन करते हैं।”

प्रश्न 9.
परिवार के दो प्रकार्य बताइये।
उत्तर-
- परिवार बच्चों का समाजीकरण करता है।
- परिवार बच्चे को सम्पत्ति प्रदान करता है।
प्रश्न 10.
आकार के आधार पर परिवार के स्वरूपों के नाम लिखिए।
उत्तर-
आकार के आधार पर परिवार के तीन प्रकार होते हैं-केन्द्रीय परिवार, संयुक्त परिवार तथा विस्तृत परिवार।
प्रश्न 11.
सत्ता के आधार पर परिवार के स्वरूपों के नाम लिखिए।
उत्तर-
सत्ता के आधार पर परिवार के दो प्रकार होते हैं-पितृसत्तात्मक व मातृसत्तात्मक।

प्रश्न 12.
वैवाहिक सम्बन्ध किसे कहते हैं ?
उत्तर-
वह नातेदारी जो विवाह के पश्चात् बनती है, उसे वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। उदाहरण के लिए सास, ससुर, जमाई, बहू इत्यादि।
प्रश्न 13.
संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर-
वह परिवार जिसमें दो से अधिक पीढ़ियों के लोग रहते हैं तथा एक रसोई में खाना खाते हैं, संयुक्त परिवार होता है।
प्रश्न 14.
नातेदारी से आप क्या समझते हैं ? .
उत्तर-
नातेदारी में वह संबंध शामिल होते हैं जो काल्पनिक या वास्तविक वंश परम्परागत बन्धनों पर आधारित तथा समाज द्वारा प्रभावित होते हों।
प्रश्न 15.
नातेदारी के प्रकार बताइये।
उत्तर-
नातेदारी दो प्रकार की होती है :- वैवाहिक तथा रक्त संबंधी।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-35 शब्दों में दीजिए :
प्रश्न 1.
संस्था शब्द से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर-
संस्था न तो लोगों का समूह है तथा न ही संगठन है। संस्था तो किसी कार्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिमापों की व्यवस्था है। संस्था तो किसी विशेष महत्त्वपूर्ण मानवीय क्रियाओं के इर्द-गिर्द केन्द्रित रूढ़ियों तथा लोक रीतियों का गुच्छा है। संस्थाएं तो संरचित प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कार्य करता है।
प्रश्न 2.
अधिमान्य नियम किसे कहते हैं ?
उत्तर-
प्रत्येक संस्था के कुछ अधिमान्य नियम होते हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। उदाहरण के लिए विवाह एक ऐसी संस्था है जो पति-पत्नी के बीच संबंधों को नियमित करती है। इस प्रकार शैक्षिक संस्थाओं के रूप में स्कूल तथा कॉलेज के अपने-अपने नियम तथा कार्य करने के तौर-तरीके होते हैं।
प्रश्न 3.
अनुलोम तथा प्रतिलोम क्या है ?
उत्तर-
- अनुलोम-यह एक प्रकार का सामाजिक नियम है जिसके अनुसार उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है।
- प्रतिलोम-यह एक प्रकार का विवाह है जिसमें निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है। इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं मिलती है।
प्रश्न 4.
बहुविवाह के दो प्रकारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
- बहपति विवाह-इस प्रकार के विवाह में एक स्त्री के कई पति होते हैं तथा इसके दो प्रकार होते हैं। भ्रातृ बहुपति विवाह जिसमें सभी पति भाई होते हैं तथा गैर-भ्रातृ बहुपति विवाह जिसमें सभी पति भाई नहीं होते।
- बहुपत्नी विवाह-इस प्रकार के विवाह में एक पति की एक समय में कई पत्नियाँ होती हैं।

प्रश्न 5.
भ्रातृत्व बहपति विवाह किसे कहते हैं ?
उत्तर-
इस प्रकार के विवाह में एक पत्नी के कई पति होते हैं तथा वह सभी आपस में भाई होते हैं। बच्चों का पिता बड़े भाई को माना जाता है तथा पत्नी से संबंध बनाने से पहले बड़े भाई की आज्ञा लेनी पड़ती है।
प्रश्न 6.
निकटाभिगमन निषेध की चर्चा कीजिए।
उत्तर-
निकटाभिगमन निषेध का अर्थ है शारीरिक अथवा वैवाहिक संबंध उन दो व्यक्तियों के बीच एक-दूसरे के साथ रक्त संबंधित हैं अथवा एक परिवार से संबंध रखते हैं। इस प्रकार के संबंध सभी मानवीय समाजों में वर्जित हैं। किसी भी संस्कृति में रक्त संबंधियों के बीच किसी प्रकार के लैंगिक संबंधों की आज्ञा नहीं होती है।
प्रश्न 7.
गोत्र किसे कहते हैं ?
उत्तर-
गोत्र रिश्तेदारों का समूह होता है जो किसी साझे पूर्वज की एक रेखीय संतान होते हैं। पूर्वज साधारणतया कल्पित ही होते हैं क्योंकि उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। यह बहिर्वैवाहिक समूह होते हैं। यह वंश समूह का ही विस्तृत रूप है जोकि माता या पिता के अनुरेखित रक्त संबंधियों से बनता है।
प्रश्न 8.
सलिंग तथा विलिंग सहोदर विवाह के मध्य अन्तर कीजिए।
उत्तर-
- सलिंग विवाह एक प्रकार का विवाह है जिसमें दो भाइयों या दो बहनों के बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। मुसलमानों में यह विवाह प्रचलित है।
- विलिंग सहोदर विवाह में व्यक्ति के मामा की बेटी या बुआ की लड़की के साथ विवाह हो जाता है। इस प्रकार के विवाह गोंड, उराओं तथा खड़िया जनजातियों में प्रचलित हैं।

प्रश्न 9.
निकटता तथा दूरी के आधार पर नातेदारी को परिभाषित कीजिए।
उत्तर-
निकटता तथा दूरी के आधार पर तीन प्रकार की नातेदारी होती है-
- प्राथमिक रिश्तेदार-वह रिश्तेदार जिनके साथ हमारा सीधा तथा नज़दीक का रक्त संबंध होता है जैसे कि माता-पिता, भाई-बहन।
- द्वितीय रिश्तेदार-यह हमारे प्राथमिक रिश्तेदारों के प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं जैसे कि पिता के पितादादा।
- तृतीय रिश्तेदार-वह रिश्तेदार जो हमारे द्वितीय संबंधियों के प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं जैसे कि चाचा की पत्नी-चाची।
III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 75-85 शब्दों में दीजिए :
प्रश्न 1.
महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।
उत्तर-
1. विवाह-विवाह सबसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिसकी सहायता से व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने तथा बच्चे पैदा करने की आज्ञा होती है। विवाह के बाद ही परिवार का निर्माण होता है।
2. परिवार-जब व्यक्ति विवाह करता है तथा बच्चे पैदा करता है तो परिवार का निर्माण होता है। परिवार ही व्यक्ति को जीवन जीने के तरीके सिखाता है तथा उसे समाज में रहने के तरीके सिखाता है।
3. नातेदारी-नातेदारी रिश्तेदारों की व्यवस्था है जिसमें रक्त संबंधी व वैवाहिक संबंधी रिश्तेदार शामिल होते हैं। रिश्तेदारी के बिना व्यक्ति जीवन जी नहीं सकता है।
प्रश्न 2.
विवाह की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं कौन-सी हैं ?
उत्तर-
- विवाह एक सर्वव्यापक संस्था है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है।
- विवाह लैंगिक संबंधों को सीमित तथा नियन्त्रित करता है।
- विवाह से व्यक्ति के लैंगिक संबंधों को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है।
- विवाह से स्त्री व पुरुष को सामाजिक स्थिति प्राप्त हो जाती है।
- अलग-अलग समाजों में अलग-अलग प्रकार के विवाह होते हैं।
- इसकी सहायता से धार्मिक रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखा जाता है।

प्रश्न 3.
विवाह के स्वरूपों के रूप में एक विवाह तथा बहविवाह के बीच विवाह के मध्य अंतर कीजिए।
उत्तर-
1. एक विवाह-आजकल के समय में एक विवाह का प्रचलन सबसे अधिक है। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करवा सकता है। इसमें एक पति या पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह ग़ैर-कानूनी है। पति-पत्नी के संबंध गहरे, स्थायी तथा प्यार से भरपूर होते हैं।
2. बहुविवाह-बहुविवाह का अर्थ है एक से अधिक विवाह करवाना। अगर एक स्त्री या पुरुष एक से अधिक विवाह करवाए तो इसे बहुविवाह कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है-बहुपत्नी विवाह तथा बहुपति विवाह । बहुपति विवाह दो प्रकार का होता है-भ्रातृ बहुपति विवाह तथा गैर-भ्रातृ बहुपति विवाह।
प्रश्न 4.
परिवार के प्रकार्यों को समझाइये।
उत्तर-
- परिवार में बच्चे का समाजीकरण होता है। परिवार में व्यक्ति समाज में रहने के तौर-तरीके सीख़ता है तथा अच्छा नागरिक बनता है।
- परिवार हमारी संस्कृति को संभालता है। प्रत्येक परिवार अपने बच्चों को संस्कृति देता है जिससे संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी संचार होता रहता है।
- परिवार में व्यक्ति की संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है तथा इससे व्यक्ति के जीवन भर की कमाई सुरक्षित रह जाती है।
- पैसे की आवश्यकता व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए होती हैं तथा इस कारण ही परिवार पैसे का भी प्रबन्ध करता है।
- परिवार व्यक्ति के ऊपर नियन्त्रण रखता है ताकि वह गलत रास्ते पर न जाए।
प्रश्न 5.
(अ) अनुलोम (ब) प्रतिलोम (स) लेवीरेट/ देवर विवाह (द) सोरोरेट/साली विवाह जैसी अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
(अ) अनुलोम-यह एक प्रकार का सामाजिक नियम है जिसके अनुसार उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है।
प्रतिलोम-यह एक प्रकार का विवाह है जिसमें निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है। इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं मिलती है।
(ब) अनुलोम-यह एक प्रकार का सामाजिक नियम है जिसके अनुसार उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है।
प्रतिलोम-यह एक प्रकार का विवाह है जिसमें निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करता है। इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं मिलती है।
(स) देवर विवाह-विवाह की इस प्रथा में पति की मृत्यु के पश्चात् पत्नी पति के छोटे भाई से विवाह कर लेती है। इससे परिवार की जायदाद सुरक्षित रह जाती है तथा परिवार टूटने से बच जाता है। बच्चों का पालन-पोषण ठीक ढंग से हो जाता है।
(द) साली विवाह-इस विवाह में पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् अपनी साली से विवाह करवा लेता है। यह दो प्रकार का होता है-सीमित साली विवाह तथा समकालीन साली विवाह।

IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250-300 शब्दों में दें :
प्रश्न 1.
संस्था से आप क्या समझते हैं ? इसकी विशेषताएं बताइये।
उत्तर-
संस्था का अर्थ (Meaning of Institution)-हम अपने जीवन में हजारों बार इस संस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। एक आम इन्सान की नज़र में संस्था का अर्थ किसी इमारत (Building) तक ही सीमित रहता है जबकि एक समाज शास्त्री की नज़र में इसका अर्थ किसी इमारत या लोगों के समूह से नहीं लिया जाता। समाज शास्त्री तो संस्था का अर्थ विस्तृत शब्दों में तथा समाज के अनुसार करते हैं। इनके अनुसार एक संस्था नियमों तथा परिमापों की व्यवस्था है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में मदद करती हैं। इस तरह संस्था तो व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूढ़ियों तथा लोक रीतियों का समूह है। यह तो वह प्रक्रिया है जिनकी मदद से व्यक्ति अपने कार्य करता है। संस्था तो सम्बन्धों की वह संगठित व्यवस्था है जिसमें समाज की कीमतें शामिल होती हैं तथा जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसका कार्य मनुष्य की आवश्यताओं को पूरा करना होता है तथा मनुष्य के कार्य तथा व्यवहारों को पूरा करना होता है। इसमें पदों तथा भूमिकाओं का भी जाल होता है तथा इन्हें विभाजित किया जाता है।
इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्था मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार्यविधियां, व्यवस्थाओं तथा नियमों का संगठन है। मनुष्य को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अनेक समूहों का सदस्य बनना पड़ता है। हर समूह में अपने सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिशें होती रहती हैं। बहुत-सी सफल तथा असफल कोशिशों के बाद समूह अपने सदस्य की ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके ढूंढ लेता है तथा समूह के सभी सदस्य इन तरीकों को मान लेते हैं। इस तरह समूह के सभी नहीं तो ज्यादातर सदस्य इनको मान लेते हैं। इस तरह समाज में कुछ विशेष हालातों के लिए कुछ विशेष प्रकार के तरीके निर्धारित हो जाते हैं तथा इन तरीकों के विरुद्ध काम करना ठीक नहीं समझा जाता। इस तरह मनुष्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना तथा सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यविधियों को संस्था कहते हैं।
परिभाषाएं (Definitions) –
- मैरिल तथा एलडरिज़ (Meril and Eldridge) के अनुसार, “सामाजिक संस्थाएं सामाजिक प्रतिमान हैं जोकि मनुष्य प्राणियों के अपने मौलिक कार्यों को करने में व्यवस्थित व्यवहार को स्थापित करती है।”
- एलवुड (Elwood) के अनुसार, “संस्था इकट्ठे मिलकर रहने के प्रतिमानित तरीके हैं जो समुदाय की सत्ता द्वारा स्वीकृत, व्यवस्थित तथा स्थापित किए गए हों।”
- सुदरलैंड (Sutherland) के अनुसार, “समाजशास्त्रीय भाषा में संस्था उन लोक रीतों तथा रूढ़ियों का समूह है जो मनुष्यों के उद्देश्यों या लक्षणों को प्राप्ति में केन्द्रित हो जाता है।”
इस तरह उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्था का विकास किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। इसलिए यह रीति-रिवाजों, परिमापों, नियमों, कीमतों आदि का भी समूह है। समनर (sumner) ने अपनी पुस्तक “Folkways” में, सामाजिक संरचना को भी संस्था में शामिल कर लिया है। संस्था व्यक्ति को व्यक्तिगत व्यवहार के तरीके पेश करती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि संस्था क्रियाओं का वह संगठन होता है, जिसे समाज किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वीकार कर लेता है। समाज में अलगअलग सभाएं पाई जाती हैं तथा हर एक सभा की अपनी ही संस्था होती है, जिसके द्वारा वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेती है। उदाहरण के लिए राज्य की संस्था सरकार होती है। यह संस्थाएं व्यक्तियों को आपस में बाँध कर रखती हैं।
संस्था की विशेषताएं (Characteristics of Institution) –
1. यह सांस्कृतिक तत्त्वों से बनती है (It is made up of cultural things)-समाज में संस्कृति के जो तत्त्व मौजूद होते हैं जैसे रूढ़ियों, लोकरीतियों, परिमाप, प्रतीमान के संगठन को संस्था कहते हैं। एक समाज शास्त्री ने तो इसे प्रथाओं का गुच्छा कहा है। जब समाज में मिलने वाली प्रथाएं रीति-रिवाज, लोकरीतियां, रूढियां संगठित हो जाती हैं तथा एक व्यवस्था का रूप धारण कर लेती हैं तो यह संस्था है। इस तरह व्यवस्था संस्कृति में मिलने वाले तत्त्वों से बनती है तथा यह फिर मनुष्य की अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करती है।
2. यह स्थायी होती है (It is Permanent) एक संस्था तब तक उपयोगी नहीं हो सकती जब तक वह ज्यादा समय तक लोगों की ज़रूरतों को पूरा न करे। अगर वह कम समय तक लोगों की आवश्यकता को पूरा करती है तो वह संस्था नहीं बल्कि सभा कहलाएगी। इस तरह संस्था अधिक समय तक लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि संस्था कभी भी अलोप हो सकती है। किसी भी संस्था मांग समय के अनुसार होती है। किसी विशेष समय में किसी संस्था की मांग कम भी हो सकती है तथा अधिक भी। अगर किसी समय में किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होती या कोई संस्था अगर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती तो वह धीरे-धीरे अलोप हो जाती है।
3. इसके कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं (It has some special motives or objectives)-जब भी संस्था का निर्माण होता है तो उसका कोई विशेष उद्देश्य होता है। संस्था को यह ज्ञान होता है कि अगर वह बन रही है तो उसके क्या उद्देश्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की विशेष प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करना है। इस तरह लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना ही इनका विशेष उद्देश्य होता है परन्तु फिर भी यह हो सकता है कि समय बदलने के साथ-साथ संस्था लोगों की आवश्यकताओं को पूरा न कर सके तो फिर इन स्थितियों में उसकी जगह कोई और संस्था उत्पन्न हो जाती है।
4. संस्कृति के उपकरण (Cultural Equipments)-संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्कृति के भौतिक पक्ष का सहारा लिया जाता है, जैसे फर्नीचर, ईमारत इत्यादि। इनका रूप तथा व्यवहार दोनों ही निश्चित किए जाते हैं। इस तरह अगर संस्था को अपने उद्देश्य पूरे करने हैं तो उसे भौतिक संस्कृति से बहुत कुछ लेना पड़ता है। अभौतिक संस्कृति जैसे विचार, लोक रीतियां, रूढ़ियां इत्यादि तो पहले ही संस्था में रहते हैं।
5. अमूर्तता (Abstractness)—जैसे कि ऊपर बताया गया है कि संस्था का विकास लोक रीतियों, रूढ़ियों, रिवाजों के साथ होता है। ये सभी अभौतिक संस्कृति का ही भाग हैं तथा अभौतिक संस्कृति के इन पक्षों को हम देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं। इस तरह संस्था में अमूर्त्तता का पक्ष शामिल होता है। इसे स्पर्श नहीं सकते केवल महसूस किया जा सकता है। संस्था किसी स्पर्श करने वाली वस्तुओं का संगठन नहीं बल्कि नियमों, कार्य प्रणालियों, लोक रीतों का संगठन है जोकि मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करने के लिए विकसित होती है।

प्रश्न 2.
एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
विवाह स्त्री व पुरुष का समाज की ओर से स्वीकृत मेल है जो नए गृहस्थ का निर्माण करता है। विवाह न केवल आदमी व औरत के सम्बन्धों को ही मान्यता प्रदान करता है बल्कि इससे अन्य सम्बन्धों को भी मान्यता मिलती है। विवाह का अर्थ केवल सम्भोग नहीं है बल्कि विवाह परिवार की नींव है। विवाह की सहायता से व्यक्ति लैंगिक सम्बन्धों में प्रवेश करता है, घर बसाता है व सन्तान पैदा करके उसका पालन-पोषण करता है।
विवाह का अर्थ (Meaning of Marriage)-साधारण शब्दों में विवाह से अर्थ केवल लिंग सम्बन्धों की पूर्ति तक ही लिया जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह अर्थ बिल्कुल ही अधूरा है। विवाह का अर्थ है कि उस संस्था में विरोधी लिंगों के मेल जिसके द्वारा परिवार का निर्माण हो व समाज के द्वारा स्वीकारा जाए अर्थात् विवाह की संस्था का अर्थ केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकृति से भी जोड़ते हैं।
विवाह की परिभाषाएं (Definitions of Marriage) –
1. मजूमदार (Majumdar) के अनुसार, “विवाह पुरुष व स्त्री का सामाजिक तौर से स्वीकार किया हुआ मेल होता है या पुरुष व स्त्री के मेल और सम्भोग को मान्यता प्रदान करने के लिए समाज द्वारा निकाली एक प्रतिनिधि या गौण संस्था है जिसका उद्देश्य है-(1) घर की स्थापना (2) लैंगिक सम्बन्धों में प्रवेश (3) बच्चे पैदा करना (4) बच्चों का पालन-पोषण करना ।”
2. वैस्टर मार्क (Western Mark) के अनुसार, “विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों से होने वाला वह सम्बन्ध है, जो प्रथा या कानून द्वारा स्वीकार किया गया है जिसमें विवाह के दोनों पक्षों के और उनसे पैदा होने वाले बच्चों के अधिकार व कर्त्तव्य भी शामिल होते हैं।”
3. एण्डर्सन व पार्कर (Anderson and Parker) के अनुसार, “विवाह एक या ज्यादा पुरुषों व एक या अधिक स्त्रियों के बीच समाज द्वारा स्वीकारा स्थायी सम्बन्ध है, जिसमें पितृत्व हेतु सम्भोग की आज्ञा होती है।”
उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विवाह की संस्था एक ऐसी संस्था है, जिसके ऊपर हमारे समाज की संरचना भी निर्भर करती है। आदमी व औरत के लैंगिक सम्बन्धों को नियमित करके ही हम बच्चों के पालन-पोषण पर ध्यान दे सकते हैं। इसी कारण इस संस्था को सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त होती है। जब यह लिंग सम्बन्ध समाज के द्वारा स्वीकारे बिना ही स्थापित हो जाएं तो हम उस विवाह को या उन सम्बन्धों को गैर-कानूनी करार दे देते हैं व पैदा हुए बच्चों के लिए भी ‘नाजायज़ बच्चा’ (illegal child) शब्द का प्रयोग करते हैं। इस कारण विवाह का अर्थ केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बन कर कई और तरह के काम करता है, जो समाज के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं।
प्रश्न 3.
विवाह के विभिन्न प्रकारों अथवा स्वरूपों को विस्तार से समझाइये।
उत्तर-
प्रत्येक समाज अपने आप में दूसरे समाज से अलग है। प्रत्येक समाज के अपने-अपने नियम, परम्पराएं व संस्थाएं होती हैं व प्रत्येक समाज में अलग-अलग संस्थाओं के भिन्न-भिन्न प्रकार होते हैं। क्योंकि प्रत्येक समाज में इन प्रकारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाता है। इस तरह विवाह नामक संस्था की अलगअलग समाजों में उनकी आवश्यकताओं के मुताबिक प्रकार किस्में या रूप हैं। इन रूपों का वर्णन निम्नलिखित है-
1. एक विवाह (Monogamy)-आजकल के आधुनिक युग में एक विवाह का प्रचलन अधिक है। इस तरह से विवाह में एक आदमी एक समय में एक ही औरत से विवाह करवा सकता है। एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह ग़ैर-कानूनी है। इसमें पति-पत्नी के सम्बन्ध अधिक स्थाई, गहरे, प्यार व हमदर्दी पूर्ण होते हैं। इसमें बच्चों का पालन-पोषण सही ढंग से हो सकता है और उन्हें माता-पिता का भरपूर प्यार मिलता है। इस तरह के विवाह में पति-पत्नी में पूरा तालमेल होता है जिससे परिवार में झगड़े होने की सम्भावना काफ़ी कम रहती है। किन्तु इस तरह के विवाह में कई समस्याएं भी हैं। पत्नी अथवा पति के अस्वस्थ होने पर सारे काम रुक जाते हैं व बच्चों की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता।
2. बहु पति विवाह (Polyandry)- इसमें एक स्त्री के कई पति होते हैं। यह आगे दो प्रकार का होता है।
(i) भ्रातृ बहुपति विवाह (Fraternal Polyandry)-इस विवाह के अनुसार स्त्री के सारे पति आपस में भाई होते हैं पर कभी-कभी ये सगे भाई न होकर एक ही जाति के व्यक्ति भी होते हैं। इस विवाह की प्रथा में सबसे बड़ा भाई एक स्त्री से विवाह करता है और उसके सब भाई उस पर पत्नी के रूप में अधिकार मानते हैं व सारे उससे लैंगिक सम्बन्ध रखते हैं। यदि कोई छोटा भाई विवाह करता है तो उसकी पत्नी भी सब भाइयों की पत्नी होती है जितने बच्चे होते हैं वह सब बड़े भाई के माने जाते हैं व सम्पत्ति में अधिकार भी सबसे अधिक बड़े भाई या सबसे पहले पति का होता है। भारत में ये प्रथा मालाबार, पंजाब, नीलगिरि, लद्दाख, सिक्किम व आसाम में पाई जाती है।
(ii) गैर-भ्रातृ बहुपति विवाह (Non Fraternal Polyandry) बहुपति विवाह के इस प्रकार में एक स्त्री के पति आपस में भाई नहीं होते। यह सब पति भिन्न-भिन्न स्थान के रहने वाले होते हैं। ऐसे हालात में स्त्री निश्चित समय के लिए एक पति के पास रहती है व फिर दूसरे के पास व फिर तीसरे के पास। इस तरह सम्पूर्ण वर्ष वह अलग-अलग पतियों के पास जीवन व्यतीत करती है। जिस समय में एक स्त्री एक पति के पास रहती है उस समय दौरान दूसरे पतियों को उससे सम्बन्ध बनाने का अधिकार नहीं होता। बच्चा होने के पश्चात् कोई एक पति एक विशेष संस्कार से उसका पिता बन जाता है। वह गर्भावस्था में स्त्री को तीर कमान भेंट करता है व उसे बच्चे का पिता मान लिया जाता है। बारी-बारी सभी पतियों को ऐसा करने दिया जाता है।
3. बहु-पत्नी विवाह (Polygyny)-बहु-पत्नी विवाह की प्रथा भारतवर्ष में पुराने समय में प्रचलित थी। राजा और उसके बड़े-बड़े मन्त्री बहुत सी पत्नियों को रखा करते थे। उस समय राजा के स्तर का अनुमान उसके द्वारा रखी गयी पत्नियों से होता था। मध्यकाल में भी मुग़ल वंशों में बहुत-सी पत्नियां रखने की प्रथा प्रचलित थी और अब भी मुसलमानों में चार विवाहों की प्रथा प्रचलित है। पुरुष की लैंगिक इच्छा को पूरा करने और परिवार की इच्छा को पूरा करने के कारण विवाह की इस प्रथा को अपनाया गया। इस प्रथा से समाज में बहुत सी समस्याएं पैदा हो गयी हैं और समाज में स्त्री को निम्न स्तर प्राप्त होता है।
4. साली विवाह (Sarorate-Marriage)—इस विवाह में पुरुष अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह करता है। साली के साथ विवाह दो तरह का होता है। साली विवाह में पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन के साथ विवाह करता है। समकाली साली विवाह में पति अपनी पत्नी की सभी छोटी बहनों को अपनी पत्नी जैसा समझ लेता है। विवाह की इस पहली प्रथा का प्रचलन दूसरी प्रथा से अधिक प्रचलित है। इस प्रथा में परिवार के टूटने की शंका नहीं रहती और बच्चों का पालन-पोषण अच्छी तरह से हो जाता है।
5. देवर विवाह (Levirate Marriage)-विवाह की इस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति की मौत के बाद पति के छोटे भाई से विवाह करती है। इस प्रथा के कारण ही एक तो घर की जायदाद सुरक्षित रहती है और दूसरा परिवार भी टूटने से बच जाता है, तीसरा बच्चों का पालन-पोषण ठीक ढंग से हो जाता है। इस प्रथा के अनुसार लड़के के माता-पिता को लड़की के माता-पिता का मूल्य वापिस नहीं करना पड़ता।
6. प्रेम विवाह (Love Marriage)-आधुनिक समाज में प्रेम विवाह का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। इस विवाह में लड़का और लड़की में कॉलेज में पढ़ते हुए या इकट्ठे दफ्तर में नौकरी करते हुए पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। उनमें आपस की मुलाकातों का सिलसिला आरम्भ हो जाता है। वह दोनों होटल, सिनेमा, पार्क आदि में मिलते रहते हैं। वह सच्चे प्यार और आपस में जीने मरने की कसमें खाते हैं। समाज उनको विवाह करने से रोकता है और उनके रास्ते में कई तरह की समस्याएं खड़ी करने की कोशिश की जाती है पर वह दोनों अपने फैसले पर अटल रहते हैं। यदि लड़का और लड़की के माता-पिता उनके विवाह को इजाजत नहीं देते हैं। वह दोनों अदालत में जाकर कानूनी तौर पर विवाह कर लेते हैं। इस तरह इस विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है।
7. अन्तर्विवाह (Endogamy)—अन्तर्विवाह के अन्तर्गत व्यक्ति को अपनी ही जाति की स्त्री से विवाह करवाना पड़ता था। अन्तर्विवाह के गुणों का वर्णन इस प्रकार है। इसके साथ रक्त की शुद्धता को सम्भाल कर रखा जाता है। इसके साथ समाज में एकता को बनाये रखा जाता है। इसके साथ सामूहिक जाति की सम्पत्ति सुरक्षित रहती है। इस विवाह में स्त्रियां काफ़ी खुश रहती हैं क्योंकि अपनी ही संस्कृति मिलने से उनका आपस में तालमेल अच्छा बैठता है। परन्तु दूसरी तरफ इस तरह का विवाह देश की एकता में रुकावट पैदा करता है। इस तरह जातिवाद को बढ़ावा मिलता है जिससे सामाजिक प्रगति में रुकावट पैदा होती है।
8. बहिर्विवाह (Exogemy)-बहिर्विवाह का अर्थ अपने गोत्र अपने गांव के बाहर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना है। एक ही गोत्र और गांव के आदमी और औरत आपस में भाई-बहन माने जाते हैं। वैस्टमार्क के अनुसार ऐसे विवाह का उद्देश्य नज़दीकी रिश्तेदारी में यौन सम्बन्धों को स्थापित न करना। यह विवाह प्रगतिवाद का सूचक है। इस विवाह से अलग-अलग समूहों में सम्बन्ध बढ़ता है। जैविक दृष्टिकोण से भी इस विवाह को उचित माना गया है। इस विवाह का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसमें लड़का और लड़की को एक-दूसरे के विचारों को समझने में मुश्किल होती है। बर्हिविवाह करने से अलग-अलग समूहों में प्यार बढ़ता है। इस तरह राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है।
9. अनुलोम विवाह (Anulom Marriage)-अनुलोम हिन्दू विवाह का एक नियम है जिसमें उच्च जाति या पुरुष अपने से नीची जाति की लड़कियों से विवाह कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक ब्राह्मण व्यक्ति क्षत्रिय, वैश्य और निम्न जाति की लड़की के साथ विवाह कर सकता था। इसका मुख्य कारण निम्न जाति के लोग उच्च जाति में विवाह करना अपनी इज्जत समझते थे क्योंकि इस तरह के विवाह से उनको भी समाज में उच्च स्थान मिल जाता था।
10. प्रतिलोम विवाह (Pratilom Marriage)–इस तरह के विवाह में निम्न जाति के पुरुष उच्च जाति की स्त्रियों के साथ विवाह करते थे। मनु ने इस तरह के विवाह का सख्त विरोध किया है। मनु के अनुसार इस तरह के विवाह से पैदा हुई सन्तान को अस्पृश्य माना जाता है। मनु ने ब्राह्मण स्त्री और निम्न जाति पुरुष से पैदा हुई सन्तान को चंडाल की संज्ञा दी थी। इसलिए इस तरह का विवाह हमेशा संकीर्णता के साथ देखा गया है। इस तरह से पैदा हुई सन्तान को किसी भी वंश के नाम को धारण नहीं कर सकती थी।

प्रश्न 4.
विवाह को परिभाषित कीजिए। जीवन साथी चुनने के नियमों को विस्तार से लिखिए।
उत्तर-
विवाह स्त्री व पुरुष का समाज की ओर से स्वीकृत मेल है जो नए गृहस्थ का निर्माण करता है। विवाह न केवल आदमी व औरत के सम्बन्धों को ही मान्यता प्रदान करता है बल्कि इससे अन्य सम्बन्धों को भी मान्यता मिलती है। विवाह का अर्थ केवल सम्भोग नहीं है बल्कि विवाह परिवार की नींव है। विवाह की सहायता से व्यक्ति लैंगिक सम्बन्धों में प्रवेश करता है, घर बसाता है व सन्तान पैदा करके उसका पालन-पोषण करता है।
विवाह का अर्थ (Meaning of Marriage)-साधारण शब्दों में विवाह से अर्थ केवल लिंग सम्बन्धों की पूर्ति तक ही लिया जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह अर्थ बिल्कुल ही अधूरा है। विवाह का अर्थ है कि उस संस्था में विरोधी लिंगों के मेल जिसके द्वारा परिवार का निर्माण हो व समाज के द्वारा स्वीकारा जाए अर्थात् विवाह की संस्था का अर्थ केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक स्वीकृति से भी जोड़ते हैं।
विवाह की परिभाषाएं (Definitions of Marriage) –
1. मजूमदार (Majumdar) के अनुसार, “विवाह पुरुष व स्त्री का सामाजिक तौर से स्वीकार किया हुआ मेल होता है या पुरुष व स्त्री के मेल और सम्भोग को मान्यता प्रदान करने के लिए समाज द्वारा निकाली एक प्रतिनिधि या गौण संस्था है जिसका उद्देश्य है-(1) घर की स्थापना (2) लैंगिक सम्बन्धों में प्रवेश (3) बच्चे पैदा करना (4) बच्चों का पालन-पोषण करना ।”
2. वैस्टर मार्क (Western Mark) के अनुसार, “विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों से होने वाला वह सम्बन्ध है, जो प्रथा या कानून द्वारा स्वीकार किया गया है जिसमें विवाह के दोनों पक्षों के और उनसे पैदा होने वाले बच्चों के अधिकार व कर्त्तव्य भी शामिल होते हैं।”
3. एण्डर्सन व पार्कर (Anderson and Parker) के अनुसार, “विवाह एक या ज्यादा पुरुषों व एक या अधिक स्त्रियों के बीच समाज द्वारा स्वीकारा स्थायी सम्बन्ध है, जिसमें पितृत्व हेतु सम्भोग की आज्ञा होती है।”
उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विवाह की संस्था एक ऐसी संस्था है, जिसके ऊपर हमारे समाज की संरचना भी निर्भर करती है। आदमी व औरत के लैंगिक सम्बन्धों को नियमित करके ही हम बच्चों के पालन-पोषण पर ध्यान दे सकते हैं। इसी कारण इस संस्था को सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त होती है। जब यह लिंग सम्बन्ध समाज के द्वारा स्वीकारे बिना ही स्थापित हो जाएं तो हम उस विवाह को या उन सम्बन्धों को गैर-कानूनी करार दे देते हैं व पैदा हुए बच्चों के लिए भी ‘नाजायज़ बच्चा’ (illegal child) शब्द का प्रयोग करते हैं। इस कारण विवाह का अर्थ केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं बल्कि व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बन कर कई और तरह के काम करता है, जो समाज के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं।
साथी के चुनाव के नियम (Rules of Mate Selection)—प्रत्येक समाज में जीवन साथी के चुनाव के नियम पाए जाते हैं, जो व्यक्ति को यह बताते हैं कि वह किस लड़की या लड़के से विवाह करवा सकता है व किससे नहीं करवा सकता यह नियम निम्नलिखित है-
- अन्तर्विवाह (Endogamy)
- बहिर्विवाह (Exogamy) –
- अनुलोम (Hyperpamy)
- प्रतिलोम (Hypogamy)
अन्तर्विवाह (Endogamy)-अन्तर्विवाह के नियम के द्वारा व्यक्ति को अपनी जाति में ही विवाह करवाना पड़ता था। जाति आगे उप-जातियों में (Sub-caste) बंटी हुई थी। इस प्रकार व्यक्ति को उपजाति में ही विवाह करवाना पड़ता था। जाति प्रथा के समय अन्तः विवाह के इस नियम को बहुत सख्ती से लागू किया गया था। यदि कोई व्यक्ति इस नियम की उल्लंघना करता था तो उसको जाति में से बाहर निकाल दिया जाता था व उससे हर तरह के सम्बन्ध भी तोड़ लिए जाते थे। धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार समाज को चार जातियों में बांटा हुआ था।
यह जातियां आगे उप-जातियों में बंटी हुई थीं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उप-जाति में ही विवाह करवाता था। वर्तमान भारतीय समाज में विवाह के इस रूप में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है।
होईबल (Hoebal) के अनुसार, “अन्तर्विवाह एक सामाजिक नियम है जो यह मांग करता है कि व्यक्ति अपने सामाजिक समूह में जिसका वह सदस्य है विवाह करवाए।”
(“Endogamy is a social rule which demands that a person should marry with in a group at in which he is a member.”)
बहिर्विवाह (Exogamy) – विवाह की संस्था एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। कोई भी समाज किसी जोडे को बिना विवाह के पति-पत्नी के सम्बन्धों को स्थापित करने की स्वीकृति नहीं देता। इसी कारण प्रत्येक समाज विवाह स्थापित करने के लिए कुछ नियम बना लेता है। सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य साथी का चुनाव करना होता है। बहिर्विवाह में भी साथी के चुनाव करने का नियम होता है।
कई समाज में जिन व्यक्तियों में रक्त के सम्बन्ध होते हैं या अन्य किसी किस्म से वह एक-दूसरे से सम्बन्धित हों तो ऐसी अवस्था में उन्हें विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती।
इस प्रकार बहिर्विवाह का अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपने समूह में विवाह करवाने की मनाही होती है। एक ही माता-पिता के बच्चों को आपस में विवाह करने से रोका जाता है।
मुसलमानों में माता-पिता के रिश्तेदारों में विवाह करने की इजाजत दी जाती है। इंग्लैण्ड के रोमन कैथोलिक चर्च में व्यक्ति को अपनी पत्नी की मौत के पश्चात अपनी साली से विवाह करने की इजाजत नहीं दी जाती।
ऑस्ट्रेलिया में लड़का अपने पिता की पत्नी से विवाह कर सकता है यदि वह उसकी सगी मां नहीं है।
बर्हिविवाह के नियम अनुसार व्यक्ति को अपनी जाति, गोत्र, स्पर्वर, सपिंड आदि में विवाह करवाने की आज्ञा नहीं दी जाती इसके कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं
1. गोत्र बहिर्विवाह-गोत्र बहिर्विवाह का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को अपने गोत्र में विवाह करवाने की इजाजत नहीं दी जाती। अर्थात् एक ही गोत्र के व्यक्तियों में विवाहित सम्बन्ध स्थापित नहीं किए जा सकते। गोत्र का अर्थ गायों को पालने वाला समूह होता है। मैक्स मूलर के अनुसार जो लोग अपनी गायों को एक ही स्थान पर बाँधते थे, उनमें नैतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाते थे जिस कारण वह आपस में विवाह नहीं करवा सकते थे। इस प्रकार गोत्र में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनमें नैतिक सम्बन्ध या रक्त सम्बन्ध पाए जाएं। इसी कारण एक गोत्र के व्यक्ति को दूसरे गोत्र के व्यक्ति से विवाह करवाने की इजाजत नहीं दी जाती।
2. स्पर्वर बहिर्विवाह-स्पर्वर बहिर्विवाह के नियम अनुसार एक ही पर्वर (Pravara) के लड़के व लड़की को विवाह करवाने की इजाजत नहीं होती। पर्वर में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनमें साझे ऋषि-पूर्वज होते हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने पर्वर के पूर्वजों से सम्बन्धित औरत से विवाह नहीं करवा सकता।
3. सपिंडा बहिर्विवाह-सपिण्ड बहिर्विवाह के नियम अनुसार उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी एक ही होते हैं। पुत्र के शरीर में माता-पिता दोनों के रक्त कण होते हैं। वैज्ञानिकों ने रक्त से सम्बन्धित रिश्तेदारों में माता द्वारा पांच पीढ़ियों व पिता द्वारा सात पीढ़ियों के व्यक्तियों को शामिल किया है। इस तरह से सम्बन्धित लोगों में पुरुष व स्त्री विवाह नहीं करवा सकते। माता व पिता की तरफ से पीढ़ियों को निश्चित करना समाज के अपने ऊपर निर्भर करता है।
गांव बहिर्विवाह-इस नियम के अनुसार एक गांव के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं करवा सकते। उत्तरी भारत में विवाह का यह नियम काफ़ी प्रचलित है। एक ही गांव के व्यक्तियों को आपस में सगे-सम्बन्धियों से भी अधिक माना जाता है। जैसे पंजाब में आमतौर से यह शब्द कहे जाते हैं कि गांव की बहन बेटी सबकी ही होती इसके अतिरिक्त गांव में लोग एक-दूसरे को रिश्तेदारियों के नाम से ही बुलाना शुरू कर देते हैं।
5. टोटम बहिर्विवाह-इस विवाह के नियम के अनुसार एक टोटम की पूजा करने वाले व्यक्ति आपस में विवाह नहीं करवा सकते। टोटम का अर्थ किसी पौधे या जानवर आदि को अपना देवता मान लेते हैं। इस प्रकार का नियम भारत के कबाईली लोगों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति अपने टोटम से बर्हिविवाह करवाता है।
अनुलोम विवाह (Hypergamy)-अनुलोम विवाह का वह नियम होता है जिसमें लड़की का विवाह उसके बराबर या उससे ऊंची जाति वाले लड़के के साथ किया जाता है। दूसरे अर्थ अनुसार उच्च जाति का पुरुष, निम्न जाति की स्त्री से जब विवाह करवाता था तो उसे अनुलोम विवाह का नाम दिया जाता था। इस प्रकार के विवाह को कुलीन विवाह का नाम भी दिया जाता है। इस प्रकार के विवाह में ब्राह्मण लड़की, केवल ब्राह्मण लड़के से ही विवाह करवा सकती है। क्षत्रिय लड़की क्षत्रिय लड़के या ब्राह्मण लड़के से विवाह करवा सकती है। वैश्य लड़की वैश्य लड़के या क्षत्रिय लड़के या ब्राह्मण लड़के से विवाह करवा सकती है।
इसके अतिरिक्त ब्राह्मण लड़का किसी भी जाति की लड़की से विवाह करवा सकता है। क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण लड़की के अलावा बाकी किसी भी लड़की से विवाह करवा सकता है। वैश्य लड़का ब्राह्मण व क्षत्रिय लड़की के अलावा किसी भी लड़की से व निम्न जाति का लड़का केवल निम्न जाति की लड़की से ही विवाह करवा सकता है। जब अन्तः विवाह के द्वारा समाज में समस्याएं पैदा होनी आरम्भ हो गईं तो अनुलोम विवाह को प्रोत्साहन मिला।
कुलीन विवाह भी अनुलोम विवाह की भान्ति थे। इस नियम अनुसार एक ही जाति का व्यक्ति, उसी जाति या निम्न जाति की लड़की से विवाह करवा सकता था। कुलीन विवाह के पाए जाने के कुछ कारण भी थे। एक तो यह कि प्रत्येक कोई अपनी लड़की का विवाह उच्च जाति के लड़के से करना चाहता था। उच्च जाति में लड़कियों की कमी होनी शुरू हो जाती थी। इस कारण कई लड़कों को बिना विवाह के ही ज़िन्दगी गुजारनी पड़ जाती थी। लड़की की कीमत बढ़ जाती थी। कई बार उच्च जाति का वर ढूंढ़ते समय उन्हें बड़ी उम्र के व्यक्ति से अपनी लड़की का विवाह करना पड़ जाता था। बहु विवाह की प्रथा भी इसी नियम के कारण ही पाई जाती थी। इसके अतिरिक्त अनैतिकता में भी बढ़ोत्तरी हुई व औरत की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। इस प्रकार कुलीन विवाह की प्रथा ने भी हमारे भारतीय समाज में कई सामाजिक बुराइयां पैदा की जिन्हें समाप्त करने के लिए सरकार को कई कानून बनाने पड़े।
प्रतिलोम विवाह (Hypogamy)-अन्तर्जातीय विवाह का दूसरा नियम प्रतिलोम है। यह नियम अनुलोम के बिल्कुल विपरीत है। इस नियम के अनुसार निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करवाता था। जैसे ब्राह्मण जाति की लड़की क्षत्रिय जाति के लड़के से विवाह करवाए या फिर क्षत्रिय जाति का लड़का ब्राह्मण लड़की से। प्रतिलोम विवाह के नियम में यदि निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से विवाह करवाता था तो उससे पैदा सन्तान किसी भी जाति में नहीं रखी जाती थी व उसको चाण्डाल कहा जाता था।
अन्तर्जातीय विवाह के दोनों रूप हमारे भारतीय समाज में विकसित रहे हैं। वर्तमान समाज में अन्तर्जातीय विवाह की पाबन्दी नहीं है। जाति प्रथा का भेद-भाव भी हमारे भारतीय समाज में समाप्त हो गया है। अन्तर्जातीय विवाह की मदद से हम भारतीय समाज में पाई जा रही कई सामाजिक बुराइयों का खात्मा कर सकेंगे।

प्रश्न 5.
परिवार किसे कहते हैं ? परिवार की मूलभूत विशेषताएं कौन-सी हैं ?
उत्तर-
यदि हम मानवीय समाज का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहला समूह परिवार ही है। प्राचीन समय में तो श्रम-विभाजन परिवारों के आधार पर ही होता था। हमें कोई भी समाज ऐसा नहीं मिलेगा जहां कि परिवार नाम की संस्था न हो। आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक प्रत्येक स्थान पर यह संस्था मौजूद रही है। चाहे और बहुत सारी संस्थाएं विकसित हैं या समाप्त हो गईं पर परिवार की संस्था वहीं पर ही खड़ी है। चाहे आजकल के विकसित समाज में परिवार का महत्त्व कुछ कम हो गया है, परिवार के बहुत सारे कार्य अन्य संस्थाओं ने ले लिए हैं, परन्तु आजकल भी मानव की अधिकतर क्रियाएं परिवार को केन्द्र मानकर ही होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिस तरह का परिवार बच्चे को प्राप्त होता है, उसी प्रकार का चरित्र बच्चे का बनता है व वह उसी अनुसार आगे चलकर कार्य करता है। सामाजिक विघटन व समाज की बहुत सारी समस्याओं के कारण ही परिवार में विघटन होता है।
परिवार सामाजिक संगठन के लिए एक महत्त्वपूर्ण समूह है, अंग्रेजी शब्द ‘Family’ रोमन भाषा के शब्द ‘Famulous’ से लिया गया है, जिसका अर्थ है ‘नौकर’। रोमन कानून के अनुसार इस शब्द का अर्थ ऐसे समूह से है, जिसमें नौकर, दास या मालिक वह सभी सदस्य शामिल होते हैं जो रक्त सम्बन्धों या विवाह सम्बन्धों पर आधारित होते हैं। यह एक ऐसा समूह है, जो आदमी व औरत की लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा बनाया जाता है। बच्चा परिवार में पल कर बड़ा होता है व समाज का एक नागरिक बनता है।
साधारण शब्दों में परिवार का अर्थ पति-पत्नी व उनके बच्चों से है, पर समाज शास्त्र में इसका अर्थ केवल लोगों का संग्रह ही नहीं बल्कि उनके आपसी सम्बन्धों की व्यवस्था है व इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे पैदा करना, उनका पालन-पोषण करना, समाजीकरण करना व लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति करना है।
परिभाषाएं (Definitions) –
1. मैकाइवर (Maclver) के अनुसार, “परिवार बच्चों की उत्पत्ति व पालन-पोषण की व्यवस्था करने के लिए काफ़ी रूप से निश्चित व स्थायी यौन सम्बन्धों से परिभाषित एक समूह है।”
2. जी० पी० मर्डोक (G. P. Murdock) के अनुसार, “परिवार एक ऐसा समूह है, जिसकी विशेषताएं साझी रिहायश, आर्थिक सहयोग व सन्तान की उत्पत्ति या प्रजनन हैं। इसमें दोनों लिंगों के बालिग शामिल होते हैं, जिनमें कम-से-कम दो में समाज द्वारा स्वीकृत लैंगिक सम्बन्ध होता है व लैंगिक सम्बन्धों में बने इन बालिगों में अपने या स्वीकृत एक या अधिक बच्चे होते हैं।”
3. एच० एम० जॉनसन (H. M. Johnson) के अनुसार, “परिवार रक्त, विवाह या गोद लेने के आधार पर सम्बद्ध दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है। इन सभी व्यक्तियों को एक परिवार का सदस्य समझा जाता है।”
इस प्रकार परिवार वह समूह है जिसमें आदमी व औरत के लैंगिक सम्बन्धों को समाज के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यह एक सर्व व्यापक समूह है। इसके अर्थ के बारे में अन्त में हम यह कह सकते हैं कि परिवार एक जैविक इकाई है जिसको लैंगिक सम्बन्धों के लिए एक संस्था के तौर पर स्वीकृत किया जाता है। इसमें सदस्य एक दूसरे से निजी रूप से प्रजनन की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि परिवार में मातापिता व बच्चों को शामिल किया जाता है, जो प्रत्येक समाज में विकसित हैं।
विशेषताएं (Characteristics)-
1. सर्वव्यापकता (Universality)-परिवार एक सामाजिक समूह है। यह मानवीय इतिहास में पहली संस्था के रूप में जाना जाता है क्योंकि प्रत्येक समय पर प्रत्येक समाज में यह किसी-न-किसी किस्म में विकसित रहा है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी परिवार का सदस्य ज़रूर होता है।
2. भावात्मक आधार (Emotional Basis)-परिवार मानवीय समाज की नींव होता है जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है जैसे-सन्तान उत्पत्ति, पति-पत्नी सम्बन्ध, वंश परम्परा कायम रखना, जायदाद की सुरक्षा आदि जैसी भावनाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं व इसके साथ ही सहयोग, प्यार, त्याग इत्यादि की भावना का भी विकास होता है जो समाज की प्रगति व विकास के लिए भी आवश्यक होता है।
3. रचनात्मक प्रभाव (Formative Influence) सामाजिक संरचना में परिवार को एक महत्त्वपूर्ण इकाई माना जाता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी रचनात्मक प्रभाव डालता है। परिवार ही पहली ऐसी संस्था होती है जिसमें रहकर बच्चा सामाजिक व्यवहार के बारे में जानकारी लेता है। व्यक्ति का बहुपक्षीय विकास परिवार की संस्था में ही हो सकता है।
4. लघु आकार (Small Size)-परिवार का आकार सीमित होता है क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया होता है या जिनमें विवाह के सम्बन्ध होते हैं उसे ही परिवार में शामिल किया जाता है। प्राचीन समय में जब कृषि प्रधान समाज होता था तो संयुक्त परिवार पाया जाता था जिसमें माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची, ताया-ताई इकट्ठे मिलकर रहते थे। जैसे-जैसे समाज में शिक्षा का विकास हुआ, स्त्रियों का नौकरी करना आरम्भ हुआ इत्यादि के साथ मूल परिवार अस्तित्व में आया जिसमें माता-पिता व बच्चे ही केवल शामिल किए जाते हैं। छोटे आकार का अर्थ होता है कि परिवार में व्यक्ति की सदस्यता केवल जन्म पर आधारित होती है व इसमें रक्त सम्बन्ध भी पाए जाते हैं।
5. सामाजिक संरचना में केन्द्रीय स्थान (Central position in the Social Structure)-परिवार पर हमारा सारा समाज आधारित होता है व अलग-अलग सभाओं का निर्माण भी परिवार से ही होता है। इसी कारण सामाजिक संरचना में इसको केन्द्रीय स्थान प्राप्त होता है। आरम्भिक समाज में संगठन परिवार पर ही आधारित होता था। सामाजिक प्रगति भी इस पर आधारित होती थी। चाहे आजकल के समय में अन्य संस्थाओं ने परिवार के कई काम ले लिए हैं परन्तु फिर भी कुछ काम समाज के लिए परिवार जो कर सकता है, वह दूसरी संस्थाएं नहीं कर सकती।
6. सदस्यों की ज़िम्मेदारी (Responsibility of the members)—परिवार का प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे से जुड़ा होता है व परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को भी संभालते हैं। इसमें किसी भी सदस्य में स्वार्थ की भावना नहीं होती बल्कि वह जो कुछ भी करता है अपने परिवार के विकास के लिए ही करता है। यहां तक कि उसमें त्याग की भावना का विकास भी परिवार में रहकर ही होता है। जिस तरह के निजी सम्बन्ध परिवार के सदस्यों में पाए जाते हैं उस प्रकार के सम्बन्ध किसी दूसरी संस्था में नहीं पाए जाते। परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो दूसरे सदस्य अपना फर्ज़ समझने लगते हैं कि उस व्यक्ति की सेवा करें। इस प्रकार उनमें सहयोग की भावना का भी विकास हो जाता है।
7. यौन सम्बन्ध (Sexual relation)-परिवार के द्वारा ही आदमी व औरत में यौन सम्बन्धों की स्थापना होती है क्योंकि समाज के द्वारा स्वीकृति भी विवाह के पश्चात् ही परिवार का निर्माण करने की होती है। आरम्भिक समाज में यौन सम्बन्धों की उत्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार के कोई नियम नहीं होते थे तो परिवार का वास्तविक रूप भी नहीं था। हमारे सामने समाज भी विघटन की दिशा की ओर अग्रसर था।
प्रश्न 6.
परिवार के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाइये ।
उत्तर-
अलग-अलग समाजों में अलग-अलग आधारों पर कई प्रकार के परिवार पाए जाते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है-
(A) सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार (Types of Family on the Basis of Authority)-सत्ता के आधार पर परिवार के निम्नलिखित प्रकार हैं
- पित प्रधान परिवार (Patriarchal Family)
- मातृ प्रधान परिवार (Matriarchal Family)
1. पितृ प्रधान परिवार (Patriarchal Family)-इस प्रकार के परिवार की किस्म में सम्पूर्ण शक्ति आदमी के हाथ में होती है। परिवार का मुखिया भी आदमी को बनाया जाता है। वंश परम्परा भी पिता पर ही निर्भर होती है। विवाह के पश्चात् औरत, आदमी के घर रहने लग जाती है व जायदाद भी केवल लडकों के बीच बांटी जाती है। घर में सबसे बड़े लड़के को सबसे अधिक आदर व सम्मान मिलता है। उसकी घर में इज्ज़त पिता के बराबर ही होती है। घर के हर तरह के ज़रूरी मामलों में भी आदमियों की ही दखलअंदाजी को ठीक समझा जाता है। यदि हम प्राचीन हिन्दू समाज की तरफ देखें तो भी वैदिक ग्रन्थों के अनुसार आदमी को ही औरत के लिए परमात्मा समझा जाता था। पिता के मरने के पश्चात् उसके सारे अधिकार उनके पुत्र को मिल जाते हैं।
2. मातृ प्रधान परिवार (Matriarchal Family)-इस प्रकार के परिवार में स्त्री जाति की ही समाज में प्रधानता होती थी। घर की सारी जायदाद की मलकीयत भी उसके हाथ में होती थी। परिवार की स्त्रियों का ही सम्पत्ति पर अधिकार होता है। विवाह के पश्चात् लड़का-लड़की के घर रहने चला जाता था। पुरोहितों का काम भी स्त्रियां ही करती थीं। परिवार की जायदाद का विभाजन भी स्त्रियों के बीच ही होता था। स्त्री की वंश- परम्परा ही आगे चलती थी। मैकाइवर ने मात प्रधान परिवार की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया जो निम्नानुसार है –
- इन बच्चों का वंश परिवार में मां के वंश के साथ निर्धारित होता है। इसलिए बच्चे पिता के कुल के नहीं बल्कि मां के कुल से सम्बन्धित समझे जाते हैं।
- स्त्री व उसकी मां, भाई-बहन व बहनों के बच्चे शामिल होते हैं।
- इन परिवारों के बीच पुत्र को पिता से कोई सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती क्योंकि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार माता द्वारा निश्चित किए जाते हैं।
- सामाजिक सम्मान के पद पुत्र की बजाए भांजे को मिलते हैं।
- इन परिवारों का अर्थ यह नहीं कि समाज में सभी अधिकार औरतों के होते हैं, आदमियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। कई क्षेत्रों में पुरुषों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, परन्तु मिलते औरतों के द्वारा ही हैं।
(B) विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार (Types of Family On the Basis of Marriage)विवाह के आधार पर परिवार के निम्नलिखित प्रकार हैं
- एक विवाही परिवार (Monogamous Family)
- बहु-पत्नी विवाह (Polygamous Family)
- बहु-पति परिवार (Polyandrous Family)
1. एक विवाही परिवार (Monogamous Family)-जब एक पुरुष एक स्त्री से या एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करवाती है तो इस विवाह के आधार पर जो परिवार पाया जाता है उसको एक विवाह परिवार का नाम दिया जाता है। आधुनिक समय में इस परिवार को अधिक महत्ता प्राप्त है। इस परिवार की किस्म में सदस्यों का रहन-सहन का दर्जा ऊंचा होता है। बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से होती है। पुरुष व स्त्री के सम्बन्धों में भी बराबरी पाई जाती है। इसमें बच्चों की संख्या भी बहुत कम होती है। जिस कारण परिवार का आकार छोटा होता है।
2. बहु-पत्नी परिवार (Polygamous Family)-परिवार की इस प्रकार में एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करवाता है। आरम्भ के राजा-महाराजाओं के समय इस प्रकार के विवाह द्वारा पाए गए परिवार को महत्ता प्राप्त थी। राजा-महाराजा कितने-कितने विवाह करवा लेते थे व पैदा हुए बच्चों का सम्मान भी काफ़ी होता था। फर्क कई बार यह होता था कि पहली पत्नी से पैदा हुए बच्चे को राजगद्दी दी जाती थी। आधुनिक समय में भारत में कानून द्वारा इस प्रकार के विवाह की पाबन्दी लगा दी है।
3. बहु-पति परिवार (Polyandrous Family)-इस प्रकार के परिवार में एक स्त्री के कितने ही पति होते थे। इसमें दो प्रकार पाए जाते हैं। इस प्रकार के परिवार को भ्रातृ विवाही परिवार का नाम दिया जाता है व दूसरे प्रकार के परिवार में स्त्री के सभी पतियों का भाई होना ज़रूरी नहीं होता। इस कारण इसको गैर भ्रातृ विवाही परिवार का नाम दिया जाता है। इस प्रकार के परिवार में स्त्री बारी-बारी सभी पतियों के पास रहती है। कुछ कबायली समाज में अभी भी इस प्रकार के विवाह की प्रथा के आधार पर परिवार पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देहरादून के ‘ख़स’ कबीले व आस्ट्रेलिया के कुछ कबीलों में भी इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं।
(C) वंश के आधार पर परिवार के प्रकार (Types of Family On the Basis of Nomenclature)-
- पितृ वंशी परिवार (Patrilineal)
- मातृ वंशी परिवार (Matrilineal)
- दो वंश-नामी परिवार (Bilinear)
- अरेखकी परिवार (Nonunilineal)
पितृ वंशी परिवार में व्यक्ति का वंश अपने पिता वाला होता है। इस प्रकार का परिवार आजकल भी पाया जा रहा है। मात वंशी परिवार में मां के वंश नाम ही बच्चों को प्राप्त होता है। दो वंश नामी परिवार में माता व पिता दोनों का वंश साथ-साथ चलता है व अरेखकी परिवार में वंश के रिश्तेदार जो माता द्वारा या पिता द्वारा होते हों, इसके आधार पर पाया जाता है।
(D) रहने के स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार (Types of Family On the Basis of Residence)—इस आधार पर परिवार के तीन प्रकार हैं-
- पितृ स्थानीय परिवार (Patrilocal Family)
- मातृ स्थानीय परिवार (Matrilocal Family)
- नव-स्थानीय परिवार (Neolocal Family)
पितृ स्थानीय परिवार में विवाह के बाद लड़की पति के घर जाकर रहने लग जाती है व मातृ स्थानीय परिवार में पति विवाह के पश्चात् पत्नी के घर रहने लग जाता है व नव स्थानीय परिवार में विवाह के पश्चात् पति-पत्नी दोनों अपना अलग किस्म का घर बनाकर रहने लग जाते हैं।
(E) रिश्तेदारी के आधार पर परिवार के प्रकार (Types of Family On the Basis of Relatives)- लिंटन ने इस प्रकार के परिवारों को दो भागों में बांटा है-
- रक्त सम्बन्धी परिवार (Consanguine family)
- विवाह सम्बन्धी परिवार (Conjugal family)
रक्त सम्बन्धी परिवार में केवल लिंग सम्बन्ध नहीं बल्कि दूसरे ही शामिल होते हैं। इस प्रकार के परिवार में सम्बन्ध व्यक्ति के जन्म पर आधारित होते हैं। यह तलाक होने पर भी टूटता नहीं। विवाह सम्बन्धी परिवार में पतिपत्नी व उनके अविवाहित बच्चे पाए जाते हैं।
इस प्रकार का परिवार पति-पत्नी के तलाक होने के पश्चात् टूट जाता है।

प्रश्न 7.
समकालीन समय में परिवार संस्था में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर-
आधुनिक समय में परिवार नामक संस्था में हर पक्ष से परिवर्तन आ गए हैं क्योंकि जैसे-जैसे हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आ रहे हैं, उसी तरह से पारिवारिक व्यवस्था भी बदल रही है। परिवार की बनावट और कामों पर नए हालातों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अब हम देखेंगे कि परिवार के ढांचे और कामों में किस तरह के परिवर्तन आए हैं-
1. स्थिति में परिवर्तन-पुराने समय में लडकी के जन्म को शाप माना जाता था। उसको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। धीरे-धीरे समाज में जैसे-जैसे परिवर्तन आए, औरत ने भी शिक्षा लेनी प्रारम्भ कर दी। पहले विवाह के बाद औरत सिर्फ़ पति पर ही निर्भर होती थी पर आजकल के समय में काफ़ी औरतें आर्थिक पक्ष से आज़ाद हैं और वह पति पर कम निर्भर हैं। कई स्थानों पर तो पत्नी की तनख्वाह पति से ज़्यादा है। इन हालातों में पारिवारिक विघटन की स्थिति पैदा होने का खतरा हो जाता है। इसके अलावा पति-पत्नी की स्थिति आजकल बराबर होती है जिसके कारण दोनों का अहं एक-दूसरे से नीचा नहीं होता। इस कारण दोनों में लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है और इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। इस तरह ऐसे कई और कारण हैं जिनके कारण परिवार के टूटने के खतरे काफ़ी बढ़ जाते हैं और बच्चे तथा परिवार दोनों मुश्किल में आ जाते हैं।
शैक्षिक कार्यों में परिवर्तन-समाज में परिवर्तन आने के साथ इसकी सारी संस्थाओं में भी परिवर्तन आ रहे हैं। परिवार जो भी काम पहले अपने सदस्यों के लिए करता था। उनमें भी ख़ासा परिवर्तन आया है। प्राचीन समाजों में बच्चा शिक्षा परिवार में ही लेता था और शिक्षा भी परिवार के परम्परागत काम से सम्बन्धित होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली होती थी और जो काम पिता करता था वही काम पुत्र भी करता था और पिता के अधीन पुत्र भी उस काम में माहिर हो जाता था। धीरे-धीरे आधुनिकता के अधीन बच्चा पढ़ाई करने के लिए शिक्षण संस्थाओं में जाने लग गया और इसके कारण वह अब परिवार के परम्परागत कामों से दूर होकर कोई अन्य कार्य अपनाने लग गया है। इस तरह परिवार का शिक्षा का परम्परागत काम उससे कट कर शिक्षण संस्थाओं के पास चला गया है।
2. आर्थिक कार्यों में परिवर्तन-पहले समय में परिवार आर्थिक क्रियाओं का केन्द्र होता था। रोटी कमाने का सारा काम परिवार ही करता था जैसे-आटा पीसने का काम, कपड़ा बनाने का काम, आदि। इस तरह जीने के सारे साधन परिवार में ही उपलब्ध थे। पर जैसे-जैसे औद्योगीकरण शुरू हुआ और आगे बढ़ा, उसके साथ-साथ परिवार के यह सारे काम बड़े-बड़े उद्योगों ने ले लिए हैं, जैसे कपड़ा बनाने का काम कपड़े की मिलें कर रही हैं, आटा चक्की पर पीसा जाता है। इस तरह परिवार के आर्थिक कार्य कारखानों में चले गए हैं। इस तरह आर्थिक उत्पादन की ज़िम्मेदारी परिवार से दूसरी संस्थाओं ने ले ली है।
3. धार्मिक कार्यों में परिवर्तन-पुराने समय में परिवार का एक मुख्य काम परिवार के सदस्यों को धार्मिक शिक्षा देना होता है। परिवार में ही बच्चे को नैतिकता और धार्मिकता के पाठ पढ़ाए जाते हैं। पर जैसे-जैसे नई वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार सामने आएं, वैसे-वैसे लोगों का दृष्टिकोण बदलकर धार्मिक से वैज्ञानिक हो गया। पहले ज़माने में धर्म की बहुत महत्ता थी, परन्तु विज्ञान ने धार्मिक क्रियाओं की महत्ता कम कर दी है। इस प्रकार परिवार के धार्मिक काम भी अब पहले से कम हो गए हैं।
4. सामाजिक कार्यों में परिवर्तन-परिवार के सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। पराने ज़माने में पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती थी। पति का यह फर्ज़ होता था कि वह अपनी पत्नी को खुश रखे। इसके अलावा परिवार अपने सदस्यों पर सामाजिक नियन्त्रण रखने का भी काम करता था, पर अब सामाजिक नियन्त्रण का कार्य अन्य एजेंसियां, जैसे पुलिस, सेना, कचहरी आदि, के पास चला गया है। इसके अलावा बच्चों के पालनपोषण का काम भी परिवार का होता था। बच्चा घर में ही पलता था और बड़ा हो जाता था और घर के सारे सदस्य उसको प्यार करते थे। पर धीरे-धीरे आधुनिकीकरण के कारण औरतों ने घर से निकलकर बाहर काम करना शुरू कर दिया और बच्चों की परवरिश के लिए क्रैच खुल गए जहां बच्चों को दूसरी औरतों द्वारा पाला जाने लग गया। इस तरह परिवार के इस काम में भी कमी आ गई है।
5. पारिवारिक एकता में कमी-पुराने जमाने में विस्तृत परिवार हुआ करते थे, पर आजकल परिवारों में यह एकता और विस्तृत परिवार खत्म हो गए हैं। हर किसी के अपने-अपने आदर्श हैं। कोई एक-दूसरे की दखलअंदाजी पसंद नहीं करता। इस तरह वह इकट्ठे रहते हैं, खाते-पीते हैं पर एक-दूसरे के साथ कोई वास्ता नहीं रखते। उनमें एकता का अभाव होता है।
प्रश्न 8.
नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों को विस्तार से समझाइये।
उत्तर-
नातेदारी का अर्थ (Meaning of Kinship)-Kin शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जोकि शब्द Cynn से निकला है जिसका अर्थ केवल ‘रिश्तेदार’ होता है और समाज शास्त्रियों और मानव वैज्ञानियों ने अपने अध्ययन के वक्त इस ‘रिश्तेदार’ शब्द को मुख्य रखा है। नातेदारी शब्द में रिश्तेदार होते हैं ; जैसे रक्त सम्बन्धी, सगे और रिश्तेदार।
आम शब्दों में समाज शास्त्र में नातेदारी व्यवस्था से मतलब उन नियमों के संकूल से है जो वंश क्रम, उत्तराधिकार, विरासत, विवाह, विवाह के बाहर लैंगिक सम्बन्धों, निवास आदि का नियमन करते हुए समाज विशेष में मनुष्य या उसके समूह की स्थिति उसके रक्त के सम्बन्धों या विवाहिक सम्बन्धों के पक्ष से निर्धारित करते हों। इसका यह अर्थ हुआ कि असली या रक्त और विवाह द्वारा बनाए और विकसित सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। इसका साफ़ एवं स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि वह सम्बन्ध जो खून द्वारा बनाए होते हैं और विवाह द्वारा बन जाते हैं वह सभी नातेदारी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। इसमें वह सारे रिश्तेदार शामिल होते हैं जोकि खून और विवाह द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची, मामा-मामी, ताया-ताई, भाई-बहन, सास-ससुर, साला-साली आदि। यह सभी हमारे रिश्तेदार होते हैं और नातेदारी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं।
परिभाषाएं (Definitions) –
- लूसी मेयर (Lucy Mayor) के अनुसार, “बंधुत्व या नातेदारी में, सामाजिक सम्बन्धों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है।”
- चार्ल्स विनिक (Charles Winick) के अनुसार, “नातेदारी व्यवस्था में वह सम्बन्ध शामिल किए जाते हैं जो कल्पित या वास्तविक वंश परम्परागत बन्धनों पर आधारित और समाज द्वारा प्रभावित होते हैं।”
- लैवी टास (Levi Strauss) के अनुसार, “नातेदारी व्यवस्था एक निरंकुश व्यवस्था है।”
- रैडक्लिफ ब्राऊन (Redcliff Brown) के अनुसार, “परिवार और विवाह के अस्तित्व से पैदा हुए या इसके परिणामस्वरूप पैदा हुए सारे सम्बन्ध नातेदारी व्यवस्था में होते हैं।”
- डॉ० मजूमदार (Dr. Majumdar) के अनुसार, “सारे समाजों में मनुष्य भिन्न प्रकार के बन्धनों में समूह में बंधे हुए हैं। इन बन्धनों में सबसे सर्वव्यापक और सबसे ज़्यादा मौलिक वह बन्धन है जोकि सन्तान पैदा करने पर आधारित है जोकि आन्तरिक मानव प्रेरणा है। यही नातेदारी कहलाती है।”
उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो व्यक्ति रिश्तेदार होते हैं यदि उनके पूर्वज एक ही हों तो वह एक व्यक्ति की संतान होते हैं। नातेदारी व्यवस्था रिश्तेदारों की व्यवस्था है जोकि रक्त सम्बन्धों या विवाह सम्बन्धों पर आधारित होता है। नातेदारी व्यवस्था सांस्कृतिक है और इसकी बनावट सारे संसार में अलगअलग है। नातेदारी व्यवस्था में उन सभी असली या नकली रक्त-सम्बन्धों को शामिल किया जाता है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। एक नाजायज़ बच्चे को नातेदारी में ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, पर एक गोद लिए बच्चे को नातेदारी व्यवस्था में ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है। यह एक विशेष नातेदारी समूह की व्यवस्था है जिसमें सारे रिश्तेदार शामिल होते हैं और जो एक-दूसरे के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियां समझते हैं। इस तरह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त असली या नकली रक्त के और विवाह द्वारा स्थापित और गहरे सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था को नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है।
नातेदारी के प्रकार (Types of Kinship)-व्यक्ति की नज़दीकी और दूरी के आधार पर नातेदारी को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। नातेदारी में सभी रिश्तेदारों में एक जैसे सम्बन्ध नहीं पाए जाते हैं। जो सम्बन्ध हमारे अपने माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चों के साथ होंगे वह हमारे अपने चाचे-भतीजे, मामा-मामी के साथ नहीं हो सकते क्योंकि हमारा अपने माता-पिता, पति-पत्नी के साथ जो सम्बन्ध है वह चाचा, भतीजे, मामा आदि के साथ नहीं हो सकता। उनमें बहुत ज्यादा गहरे सम्बन्ध नहीं पाए जाते। इस नज़दीकी और दूरी के आधार पर नातेदारी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है जिनका वर्णन इस प्रकार है-
1. प्राथमिक रिश्तेदार (Primary relatives)-पहली श्रेणी की नातेदारी में प्राथमिक रिश्तेदार जैसे, पतिपत्नी, पिता-पुत्र, माता-पुत्र, माता-पुत्री, पिता-पुत्री, बहन-बहन, भाई-बहन, बहन-भाई, भाई-भाई आदि आते हैं। मरडोक के अनुसार, यह आठ प्रकार के होते हैं। यह प्राथमिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें सम्बन्ध प्रत्यक्ष और गहरे होते हैं।
2. गौण सम्बन्धी (Secondary relations)-हमारे कुछ रिश्तेदार प्राथमिक होते हैं जैसे, माता, पिता, बहन, भाई आदि। इनके साथ हमारा प्रत्यक्ष रिश्ता होता है। पर कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं होता बल्कि, हम उनके साथ प्राथमिक रिश्तेदार के माध्यम के साथ जुड़े होते हैं जैसे-माता का भाई, पिता का भाई, माता की बहन, पिता की बहन, बहन का पति, भाई की पत्नी आदि। इन सब के साथ हमारा गहरा रिश्ता नहीं होता बल्कि यह गौण सम्बन्धी होते हैं। मर्डोक के अनुसार, यह सम्बन्ध 33 प्रकार के होते हैं।
3. तीसरे दर्जे के सम्बन्धी (Tertiary Kins) सबसे पहले रिश्तेदार प्राथमिक होते हैं और फिर गौण सम्बन्धी अर्थात् प्राथमिक सम्बन्धों की मदद के साथ रिश्ते बनते हैं। तीसरी प्रकार के सम्बन्धी वह होते हैं जो गौण सम्बन्धियों के प्राथमिक रिश्तेदार हैं। जैसे पिता के भाई का पुत्र, माता के भाई की पत्नी-(मामी), पत्नी के भाई की पत्नी अर्थात् साले की पत्नी, माता की बहन का पति अर्थात् मौसा जी इत्यादि। मर्डोक ने इनकी संख्या 151 दी है।
इस प्रकार यह तीन श्रेणियों की नातेदारी होती है पर यदि हम चाहें तो हम चौथी और पांचवीं श्रेणी के बारे में ज्ञान सकते हैं।

प्रश्न 9.
सामाजिक जीवन में नातेदारी के महत्त्व को समझाइये।
उत्तर-
नातेदारी व्यवस्था का सामाजिक संरचना में एक विशेष स्थान है। इसके साथ ही समाज की बनावट बनती है। यदि नातेदारी व्यवस्था ही न हो तो समाज एक संगठन की तरह नहीं बन सकेगा और सही तरीके से काम नहीं कर सकेगा। इसलिए इसका महत्त्व काफ़ी बढ़ गया है जिसका वर्णन अग्रलिखित है
1. नातेदारी सम्बन्धों के माध्यम से ही कबाइली और खेती वाले समाजों के बीच अधिकार और परिवार एवं विवाह, उत्पादन और उपभोग की पद्धति और राजनीतिक सत्ता के अधिकारों का निर्धारण होता है। शहरी समाजों में भी विवाह और पारिवारिक उत्सवों के समय नातेदारी सम्बन्धों का महत्त्व देखने को मिलता है।
2. नातेदारी, परिवार और विवाह में गहरा सम्बन्ध है। नातेदारी के माध्यम से ही इस बात का निर्धारण होता है कि कौन किसके साथ विवाह कर सकता है और कौन-कौन से सम्बन्धों की शब्दावली भी है। नातेदारी से ही वंश सम्बन्ध, गोत्र और खानदान का निर्धारण होता है और वंश, गोत्र और खानदान में बहिर्विवाह का सिद्धान्त पाया जाता है।
3. पारिवारिक जीवन, वंश सम्बन्ध, गोत्र और खानदान के सदस्यों के बीच नातेदारी के आधार पर ही जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों एवं कर्म-काण्डों में किसका क्या अधिकार और ज़िम्मेदारी है, इसका निर्धारण होता है, जैसे ; विवाह के संस्कार और इसके साथ जुड़े कर्म-काण्डों में बड़े भाई, मां और बुआ का विशेष महत्त्व है। मृत्यु के बाद आग कौन देगा, इसका सम्बन्ध भी नातेदारी पर निर्भर करता है। जिन लोगों को आग देने का अधिकार होता है, नातेदारी उनके उत्तराधिकार को निश्चित करती है। सामाजिक संगठन (जन्म, विवाह, मौत) और सामूहिक उत्सवों के मौकों और नातेदारी या रिश्तेदारों को बुलाया जाना जरूरी होता है, ऐसा करने के साथ सम्बन्धों में और मज़बूती बढ़ती है।
4. नातेदारी व्यवस्था के साथ समाज को मज़बूती मिलती है। नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन को बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि नातेदारी व्यवस्था ही न हो तो सामाजिक संगठन टूट जाएगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी।
5. नातेदारी व्यवस्था लैंगिक सम्बन्धों को निश्चित करती है। नातेदारी व्यवस्था में लैंगिक सम्बन्ध बनाने, हमारे समाज में वर्जित है। यदि नातेदारी व्यवस्था न हो तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और नाजायज़ लैंगिक सम्बन्ध और अवैध बच्चों की भरमार होगी जिसके साथ समाज छिन्न-भिन्न हो जाएगा।
6. नातेदारी व्यवस्था विवाह निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने गोत्र में विवाह नहीं करवाना, माता की तरफ से कितने रिश्तेदार छोड़ने हैं, पिता की तरफ से कितने रिश्तेदार छोड़ने हैं, यह सब कुछ नातेदारी व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। यदि यह व्यवस्था न हो तो विवाह करने में किसी भी नियम की पालना नहीं होगी जिसके कारण समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी।
7. नातेदारी व्यवस्था मनुष्य को मानसिक शान्ति प्रदान करती है। आजकल के औद्योगिक समाज में चाहे हमारे विचार Practical हो चुके हैं पर फिर भी मनुष्य नातेदारी के बन्धनों से मुक्त नहीं हो सका है। वह अपने बुजुर्गों की तस्वीरें घर में टांग कर रखता है, उनकी तस्वीरों का संग्रह करता है, मरने के बाद उनका श्राद्ध करता है। मनुष्य जाति नातेदारी पर आधारित समूहों में रही है। नातेदारी के बिना व्यक्ति एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। हमारे रिश्तेदार हमें सबसे ज्यादा जानते हैं, पहचानते हैं। वह अपने आपको अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। यदि हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारे रिश्तेदार हमें मानसिक तौर पर शान्त करते हैं। हम अपने रिश्तेदारों में ही रह कर सबसे ज्यादा प्रसन्नता और आनन्द महसूस करते हैं।
8. हमारी नातेदारी ही हमारे विवाह और परिवार का निर्धारण करती है कि किसके साथ विवाह करना है, किसके साथ नहीं करना है। सगोत्र, अन्तर्जातीय विवाह सब कुछ ही नातेदारी पर ही निर्भर करता है। परिवार में ही खून और विवाह के सम्बन्ध पाए जाते हैं। नातेदारी के कारण ही विवाह और नातेदारी में व्यवस्था पैदा होती है।
प्रश्न 10.
वैवाहिक तथा रक्त सम्बन्धों में अन्तर कीजिए।
उत्तर-
(i) रक्त संबंधी नातेदारी (Consanguinity) सगोत्र नातेदारी शुरुआती परिवार के आधार पर और इसमें पैदा हुए असली या नकली रक्त के वंश परम्परागत सम्बन्धों को सगोत्र नातेदारी कहते हैं। आम शब्दों में वह सभी रिश्तेदार या व्यक्ति जो रक्त के बन्धनों में बन्धे होते हैं उनको सगोत्र नातेदारी कहते हैं। रक्त का सम्बन्ध चाहे असली हो या नकली इसको नातेदारी व्यवस्था में तो ही ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। यदि इस सम्बन्ध को समाज की मान्यता प्राप्त हो। उदाहरण के तौर पर नाजायज़ बच्चे को, चाहे उसके साथ भी रक्त सम्बन्ध होता है, समाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती क्योंकि उसको समाज की मान्यता प्राप्त नहीं होती और गोद लिए बच्चे को, चाहे उसके साथ रक्त सम्बन्ध नहीं होता, समाज में मान्यता प्राप्त होती है और वह सगोत्र प्रणाली का हिस्सा होते हैं। रक्त सम्बन्धों को हर प्रकार के समाजों में मान्यता प्राप्त है।
इस तरह इस चर्चा से स्पष्ट है कि शुरुआती परिवार के आधार पर रक्त-वंश परम्परागत सम्बन्धों से पैदा हुए सारे रिश्तेदार इस सगोत्र नातेदारी प्रणाली में शामिल है। हम उदाहरण ले सकते हैं बहन-भाई, मामा, चाचा, ताया, नाना-नानी, दादा-दादी आदि। यहाँ यह बताने योग्य है कि रक्त सम्बन्ध सिर्फ़ पिता वाली तरफ से ही नहीं होता बल्कि माता वाली तरफ से भी होता है। इस तरह पिता वाली तरफ से रक्त सम्बन्धियों को पितृ पक्ष रिश्तेदार कहते हैं और माता वाली तरफ से रक्त सम्बन्धियों को मात पक्ष रिश्तेदार।
वर्गीकरण-खून के आधार पर आधारित रिश्तेदारों को अलग-अलग नामों के साथ जाना जाता है। एक ही मां-बाप के बच्चे, जो आपस में सगे भाई-बहन होते हैं, को सिबलिंग (Sibling) कहते हैं और सौतेले बहन-भाई को हॉफ़ सिबलिंग (Half sibling) कहते हैं। पिता वाली तरफ सिर्फ आदमियों के रक्त सम्बन्धियों जो सिर्फ आदमी होते हैं उनको सगा-सम्बन्धी (Agnates) कहते हैं और इसी तरह माता वाली तरफ सिर्फ औरतों के रक्त सम्बन्धियों जो सिर्फ औरतें होती हैं, उनको (Utrine) कहते हैं। इसी तरह वह लोग जो रक्त सम्बन्धों के कारण सम्बन्धित हों, उनको रक्त सम्बन्धी रिश्तेदार (Consanguined kin) कहा जाता है। इन रक्त सम्बन्धियों को दो हिस्सों में बांटा जाता है।
- एक रेखकी रिश्तेदार (Unilineal Kin)-इस प्रकार की रिश्तेदारी में वह व्यक्ति आते हैं जो वंश क्रम की सीधी रेखा द्वारा सम्बन्धित हों जैसे पिता, पिता का पिता, पुत्र और पुत्र का पुत्र ।
- कुलेटरल या समानान्तर रिश्तेदार (Collateral Kin)-इस प्रकार के रिश्तेदार वह व्यक्ति होते हैं, जो हर रिश्तेदारों के द्वारा असीधे तौर पर सम्बन्धित हों जैसे पिता का भाई चाचा, मां की बहन मौसी, मां का भाई मामा आदि।
(ii) विवाह संबंधी नातेदारी (Affinity)—इसको सामाजिक नातेदारी का नाम भी दिया जाता है। इस प्रकार की नातेदारी में उस तरह के रिश्तेदार शामिल होते हैं जो किसी आदमी या औरत के विवाह करने से पैदा होते हैं। जब किसी लड़के का लड़की से विवाह होता है तो उसका सिर्फ लड़की के साथ ही सम्बन्ध स्थापित नहीं होता बल्कि लड़की के माध्यम से उसके परिवार के बहुत सारे सदस्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इसी तरह जब लड़की का लड़के के साथ विवाह होता है तो लड़की का भी लड़के के परिवार के सारे सदस्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इस तरह सिर्फ विवाह करवाने के साथ ही लड़का-लड़की के कई प्रकार के नए रिश्ते अस्तित्व में आ जाते हैं। इस तरह विवाह पर आधारित नातेदारी को विवाहिक नातेदारी का नाम दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जीजा-साला, साढू-जमाई, ससुर, ननद, भाभी, बहु, सास आदि। इस तरह की नातेदारी की प्राणीशास्त्री महत्ता के साथ-साथ सामाजिक महत्ता भी होती है। प्राणीशास्त्रीय महत्त्व तो पति-पत्नी के लिए है पर सास-ससुर, देवर, ननद, भाभी, साढ़, साली, साला, जमाई आदि रिश्ते सामाजिक होते हैं। मॉर्गन ने दुनिया के कई भागों में प्रचलित साकेदारियों का अध्ययन किया और इनको वर्णनात्मक और व्यक्तिनिष्ठ नामकरण के साथ तो मनुष्य श्रेणियों में बांटा है। वर्णनात्मक प्रणाली में आम-तौर पर विवाहिक सम्बन्धियों के लिए एक ही नाम दिया जाता है। ऐसे नाम नातेदारी की तुलना में सम्बन्ध के बारे में ज्यादा बताते हैं। व्यक्तिनिष्ठ शब्द असली सम्बन्धों के बारे में बताते हैं। जैसे-अंकल को हम मामा, चाचा, फुफड़ और मौसा के लिए प्रयोग करते हैं। यह पहले प्रकार की उदाहरण है। परन्तु फादर या पिता के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं हो सकते।
इस तरह Nephew को भतीजे या भांजे के लिए, cousin को मामा, चाचा, ताया, मासी, बुआ के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह Sister-in-law को साली और ननद और Brother-in-law को देवर तथा साले के लिए प्रयोग किया जाता है।
इस तरह आधुनिक समाज में नए-नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। असल में यह सारे शब्द नातेदारी के सूचक हैं और विवाहिक नातेदारी पर आधारित होते हैं। जैसे व्यक्ति को जमाई का दर्जा, पति का दर्जा, औरत को बहू और पत्नी का दर्जा विवाह के कारण ही प्राप्त होता है। इस तरह हम बहुत सारी वैवाहिक रिश्तेदारियों को गिन सकते हैं।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न
I. बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) :
प्रश्न 1.
समाज की आधारभूत इकाई कौन-सी होती है ?
(A) परिवार
(B) विवाह
(C) नातेदारी
(D) सरकार।
उत्तर-
(A) परिवार।
प्रश्न 2.
यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज ने एक संस्था को मान्यता दी है जिसे ……. कहते हैं।
(A) विवाह
(B) परिवार
(C) सरकार
(D) नातेदारी।
उत्तर-
(A) विवाह।
प्रश्न 3.
बच्चे का समाजीकरण कौन शुरू करता है ?
(A) सरकार
(B) परिवार
(C) पड़ोस
(D) खेल समूह।
उत्तर-
(B) परिवार।

प्रश्न 4.
कौन अगली पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण करता है ?
(A) पड़ोस
(B) सरकार
(C) परिवार
(D) समाज।
उत्तर-
(C) परिवार।
प्रश्न 5.
यौन इच्छा ने किस संस्था को जन्म दिया ?
(A) परिवार
(B) समाज
(C) सरकार
(D) विवाह।
उत्तर-
(D) विवाह।
प्रश्न 6.
मातुलेय परिवारों में किन रिश्तेदारों में निकटता होती है ?
(A) मामा-भांजा
(B) माता-पुत्री
(C) पिता-पुत्र
(D) चाचा-भतीजा।
उत्तर
(A) मामा-भांजा।

प्रश्न 7.
रक्त सम्बन्धी या सीधे सम्बन्धी ……. सम्बन्धी होते हैं।
(A) प्राथमिक
(B) द्वितीय
(C) तृतीय
(D) चतुर्थ।
उत्तर-
(A) प्राथमिक।
प्रश्न 8.
जो सम्बन्ध हमारे माता पिता के लिए प्राथमिक होता है उसे क्या कहते हैं ?
(A) प्राथमिक सम्बन्ध
(B) द्वितीय सम्बन्ध
(C) तृतीय सम्बन्ध
(D) चतुर्थ सम्बन्ध।
उत्तर-
(B) द्वितीय सम्बन्ध।
प्रश्न 9.
जो सम्बन्धी द्वितीय सम्बन्धों से बनते हैं वह हमारे ……….. सम्बन्धी होते हैं।
(A) प्राथमिक
(B) द्वितीय
(C) तृतीय
(D) चतुर्थ।
उत्तर-
(C) तृतीय।

प्रश्न 10.
बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है ?
(A) सरकार
(B) परिवार
(C) खेल समूह
(D) पड़ोस।
उत्तर-
(B) परिवार।
प्रश्न 11.
उस परिवार को क्या कहते हैं जिसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं ?
(A) केंद्रीय परिवार
(B) संयुक्त परिवार ।
(C) विस्तृत परिवार
(D) नव स्थानीय परिवार।
उत्तर-
(A) केन्द्रीय परिवार।
प्रश्न 12.
इनमें से कौन सा परिवार का कार्य है ?
(A) बच्चे का समाजीकरण
(B) बच्चों पर नियंत्रण
(C) बच्चे का पालन-पोषण
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर-
(D) उपर्युक्त सभी।

प्रश्न 13.
विवाह के आधार पर परिवार का प्रकार बताएं।
(A) एक विवाह परिवार
(B) बहु विवाही परिवार
(C) समूह विवाही परिवार
(D) उपर्युक्त सभी।
उत्तर-
(D) उपर्युक्त सभी।
प्रश्न 14.
नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं ?
(A) एक
(B) दो
(C) तीन
(D) चार।
उत्तर-
(B) दो।
प्रश्न 15.
प्राथमिक रिश्तेदार कितने प्रकार के होते हैं ?
(A) पाँच
(B) छः
(C) आठ
(D) दस।
उत्तर-
(C) आठ।

प्रश्न 16.
द्वितीयक सम्बन्धी कितने प्रकार के होते हैं ?
(A) 30
(B) 33
(C) 36
(D) 39.
उत्तर-
(B) 33.
II. रिक्त स्थान भरें (Fill in the blanks) :
1. ……….. परिवार में पिता की सत्ता चलती है।
2. ………… परिवार में माता की सत्ता चलती है।
3. ………….. विवाह में अपने समूह में ही विवाह करवाया जाता है।
4. ……….. परिवार में दो या अधिक पीढ़ियों में परिवार इकट्ठे रहते हैं।
5. बहुपति विवाह …………….. प्रकार का होता है।
6. आकार के आधार पर परिवार ……….. प्रकार के होते हैं।
7. सत्ता के आधार पर परिवार …………… प्रकार के होते हैं।
उत्तर-
- पितृसत्तात्मक,
- मातृसत्तात्मक,
- अन्तः,
- संयुक्त,
- दो,
- तीन,
- दो।
III. सही/गलत (True/False) :
1. एकाकी परिवार में संपूर्ण नियंत्रण पिता के हाथों में होता है।
2. स्त्रियों की संख्या कम होने के कारण बहुपति विवाह होते हैं।
3. बहुविवाह संसार में सबसे अधिक प्रचलित हैं।
4. नातेदारी के दो प्रकार होते हैं।
5. परिवार संस्कृति के वाहक के रूप में कार्य करता है।
6. मातृवंशी परिवार में सम्पत्ति पुत्री को नहीं मिलती है।
7. परिवार के सदस्यों में रक्त संबंध होते हैं।
उत्तर-
- गलत,
- सही,
- गलत,
- सही,
- सही,
- गलत,
- सही।

IV. एक शब्द/पंक्ति वाले प्रश्न उत्तर (One Wordline Question Answers) :
प्रश्न 1.
एक विवाह का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो उसे एक विवाह कहते हैं।
प्रश्न 2.
बहुविवाह के कितने प्रकार हैं ?
उत्तर-
बहुविवाह के तीन प्रकार हैं।
प्रश्न 3.
द्विविवाह में एक पुरुष की कितनी पत्नियां होती हैं ?
उत्तर-
द्विविवाह में एक पुरुष की दो पत्नियां होती हैं।

प्रश्न 4.
बहुपति विवाह में एक स्त्री के कितने पति हो सकते हैं ?
उत्तर-
बहुपति विवाह में एक स्त्री के कई पति हो सकते हैं।
प्रश्न 5.
अन्तर्विवाह का अर्थ बताएं।
उत्तर-
जब व्यक्ति केवल अपनी ही जाति में विवाह करवा सकता हो उसे अंतर्विवाह कहा जाता है।
प्रश्न 6.
बर्हिविवाह का अर्थ बताएं।
उत्तर-
जब व्यक्ति को अपनी गोत्र के बाहर परंतु अपनी जाति के अंदर विवाह करवाना पड़े तो उसे बर्हिविवाह कहते हैं।

प्रश्न 7.
यह शब्द किसके हैं, “विवाह एक समझौता है जिसमें बच्चों की पैदाइश तथा देखभाल होती
उत्तर-
यह शब्द मैलीनोवस्की के हैं।
प्रश्न 8.
संसार में विवाह का कौन-सा प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है ?
उत्तर-
संसार में विवाह का सबसे अधिक प्रचलित प्रकार एक विवाह है।
प्रश्न 9.
बहु-पत्नी विवाह का अर्थ।
उत्तर-
जब एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ विवाह करवाए तो उसे बहु-पत्नी विवाह कहते हैं।

प्रश्न 10.
बहु-पति विवाह का अर्थ।
उत्तर-
जब कई पुरुष मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, तो उसे बहु-पति विवाह कहते हैं।
प्रश्न 11.
एफिनिटी क्या होता है ?
उत्तर-
सामाजिक सम्बन्ध जो विवाह पर आधारित होते हैं, उन्हें एफिनिटी कहते हैं।
प्रश्न 12.
यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्था कौन-सी है ?
उत्तर-
यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज ने एक संस्था को मान्यता दी हुई है, जिसे परिवार कहते हैं।

प्रश्न 13.
यौन इच्छा ने किस प्रथा को जन्म दिया ?
उत्तर-
यौन इच्छा ने विवाह नामक प्रथा को जन्म दिया।
प्रश्न 14.
विवाह क्या होता है ?
उत्तर-
यौन सम्बन्धों को समाज ने एक प्रथा के द्वारा मान्यता दी हुई है, जिसे विवाह कहते हैं।
प्रश्न 15.
कुलीन विवाह क्या होता है ?
उत्तर-
जब एक ही जाति में ऊंचे कुलों से सम्बन्धित लड़के-लड़की का विवाह होता है तो उसे कुलीन विवाह कहते हैं।

प्रश्न 16.
प्रेम विवाह का प्राचीन नाम क्या है ?
उत्तर-
प्रेम विवाह का प्राचीन नाम गंधर्व विवाह है।
प्रश्न 17.
भ्रातृक बहुपति विवाह का अर्थ बताएं।
उत्तर-
अगर सभी भाई एक स्त्री से इकट्ठे विवाह करें तो उसे भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं।
प्रश्न 18.
कौन-से पुरुष को पूर्ण पुरुष कहा जाता है ?
उत्तर-
जिस पुरुष के स्त्री तथा बच्चे हों, उसे पूर्ण पुरुष कहा जाता है।

प्रश्न 19.
अन्तर्विवाह का कोई कारण बताओ।
उत्तर-
रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए अन्तर्विवाह की आवश्यकताएं पड़ी।
प्रश्न 20.
प्राथमिक सम्बन्धी कौन-से होते हैं ? ।
उत्तर-
रक्त सम्बन्धी या सीधे सम्बन्ध प्राथमिक सम्बन्ध होते हैं, जैसे कि पिता, माता, भाई, बहन इत्यादि।
प्रश्न 21.
द्वितीय सम्बन्धी कौन-से होते हैं ?
उत्तर-
जो हमारे माता या पिता का प्राथमिक सम्बन्धी होता है वह हमारे लिए द्वितीय सम्बन्धी होता है, जैसे मामा, चाचा, ताया, बुआ इत्यादि।

प्रश्न 22.
तृतीय सम्बन्धी कौन-से होते हैं ? .
उत्तर-
जो सम्बन्धी द्वितीय सम्बन्धों से बनते हैं वह हमारे तृतीय सम्बन्धी होते हैं, जैसे पिता की बहन का पति, माता के भाई की पत्नी इत्यादि।
प्रश्न 23.
समूह विवाह क्या होता है ?
उत्तर-
जब बहुत सारी स्त्रियों का बहुत सारे पुरुषों के साथ इकट्ठे विवाह होता है, उसे समूह विवाह कहते
प्रश्न 24.
बहिर्विवाह में किससे बाहर विवाह करना पड़ता है ?
उत्तर-
बहिर्विवाह में अपने सपिण्ड, प्रवर तथा गोत्र से बाहर करना पड़ता है।

प्रश्न 25.
अन्तर्विवाह क्या होता है ?
उत्तर-
जब व्यक्ति को अपने समूह या जाति के अन्दर विवाह करना पड़े तो उसे अन्तर्विवाह कहते हैं।
प्रश्न 26.
प्रतिलोम विवाह क्या होता है ?
उत्तर-
जब निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं।
प्रश्न 27.
कौन-सी संस्था परिवार के निर्माण में सहायक होती है ?
उत्तर-
विवाह नामक संस्था परिवार के निर्माण में सहायक होती है।

प्रश्न 28.
किस संस्था से समाज विघटन से बचता है ?
उत्तर-
विवाह नामक संस्था के कारण समाज का विघटन नहीं होता।
प्रश्न 29.
बहु-पत्नी विवाह का अर्थ बताएं।
उत्तर-
जब एक व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करवाए तो उसे बहु-पत्नी विवाह कहते हैं।
प्रश्न 30.
बहु-पति विवाह का अर्थ बताएं।
उत्तर-
जब एक स्त्री के कई पति हों तो उस विवाह को बहुपति विवाह कहते हैं।

प्रश्न 31.
बहु-पति विवाह के कितने प्रकार होते हैं ?
उत्तर-
बहुपति विवाह के दो प्रकार-भ्रातृ बहुपति विवाह तथा गैर-भ्रात बहुपति विवाह होते हैं।
प्रश्न 32.
एक विवाह को आदर्श क्यों माना जाता है ?
उत्तर-
क्योंकि इससे परिवार अधिक स्थायी रहते हैं।
प्रश्न 33.
पितृ सत्तात्मक परिवार में ……….. शक्ति अधिक होती है।
उत्तर-
पितृ सत्तात्मक परिवार में पिता की शक्ति अधिक होती है।

प्रश्न 34.
मातृ सत्तात्मक परिवार में …………… की सत्ता चलती है।
उत्तर-
मातृ सत्तात्मक परिवार में माता की सत्ता चलती है।
प्रश्न 35.
रक्त सम्बन्धी परिवार में कौन-से सम्बन्ध पाए जाते हैं ?
उत्तर-
रक्त सम्बन्धी परिवार में रक्त सम्बन्ध पाए जाते हैं।
प्रश्न 36.
सदस्यों के आधार पर परिवार के कितने तथा कौन-से प्रकार होते हैं ?
उत्तर-
सदस्यों के आधार पर परिवार के तीन प्रकार केन्द्रीय परिवार, संयुक्त परिवार तथा विस्तृत परिवार होते हैं।

प्रश्न 37.
विवाह के आधार पर परिवार के कितने तथा कौन-से प्रकार होते हैं ?
उत्तर-
विवाह के आधार पर परिवार के दो प्रकार-एक विवाही परिवार तथा बहुविवाही परिवार होते हैं।
प्रश्न 38.
वंश के आधार पर कितने प्रकार के परिवार होते हैं ?
उत्तर-
चार प्रकार के परिवार ।
प्रश्न 39.
केन्द्रीय परिवार का अर्थ बताएं।
उत्तर-
वह परिवार जिसमें पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हों उसे केन्द्रीय परिवार कहा जाता है।

प्रश्न 40.
हिन्दू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था ?
उत्तर-
सन् 1856 में।
प्रश्न 41.
शब्द Family किस भाषा के शब्द का अंग्रेजी रूपान्तर है ?
उत्तर-
शब्द Family लातीनी भाषा के शब्द का अंग्रेज़ी रूपान्तर है।
प्रश्न 42.
शब्द Family लातीनी भाषा के किस शब्द से निकला है ?
उत्तर-
शब्द Family लातीनी भाषा के शब्द Famulus से निकला है।

प्रश्न 43.
परिवार के स्वरूप में परिवर्तन का एक कारण बताओ।
उत्तर-
आजकल स्त्रियां घर से जाकर दफ्तरों में काम करने लगी हैं जिससे उनकी परिवार तथा पति पर निर्भरता काफ़ी कम हो गई है।
प्रश्न 44.
परिवार एक सर्वव्यापक संस्था है। कैसे ?
उत्तर-
परिवार एक सर्वव्यापक संस्था है क्योंकि यह प्रत्येक समाज में किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है।
प्रश्न 45.
परिवार में सदस्यों के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध होते हैं ?
उत्तर-
परिवार में सदस्यों के बीच रक्त सम्बन्ध होते हैं।

प्रश्न 46.
समाज में परिवार का किस प्रकार का स्थान होता है ?
उत्तर-
समाज में परिवार का केन्द्रीय स्थान होता है।
प्रश्न 47.
परिवार के सदस्यों में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं ? ।
उत्तर-
परिवार के सदस्यों में हमदर्दी, त्याग, प्रेम जैसे गुण पाए जाते हैं।
प्रश्न 48.
परिवार के दो जैविक कार्य बताएं।
उत्तर-
- परिवार में ही व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सम्बन्ध बनाता है।
- परिवार में ही सन्तान उत्पन्न होती है।

प्रश्न 49.
परिवार के दो आर्थिक कार्य बताएं।
उत्तर-
- परिवार सदस्यों के खाने का प्रबन्ध करता है।
- परिवार एक उत्पादक इकाई के रूप में कार्य करता है।
प्रश्न 50.
परिवार में उत्तराधिकार का निर्धारण कैसे होता है ?
उत्तर-
बेटों में जायदाद का समान विभाजन कर दिया जाता है।
प्रश्न 51.
परिवार के दो सामाजिक कार्य बताएं।
उत्तर-
- परिवार व्यक्ति को सामाजिक स्थिति प्रदान करता है।
- परिवार संस्कृति को अगली पीढ़ी को सौंप देता है।

प्रश्न 52.
कौन-सी संस्था बच्चे का समाजीकरण करती है ?
उत्तर-
परिवार नामक संस्था बच्चे का समाजीकरण करती है।
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
विवाह से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निश्चित हो जाती है। स्पष्ट करें।
उत्तर-
विवाह के कारण व्यक्ति को समाज में कई सारे पद मिल जाते हैं, जैसे-पति, पिता, जीजा, दामाद इत्यादि। इन सभी पदों में ज़िम्मेदारी होती है। विवाह से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निश्चित हो जाती है।
प्रश्न 2.
मनु ने प्रतिलोम विवाह के बारे में कौन-से विचार व्यक्त किए हैं ?
उत्तर-
मनु के अनुसार निम्न जाति के पुरुष का उच्च जाति की स्त्री से विवाह करना पाप है। इसे उन्होंने निषेध करार दिया है। इस प्रकार के विवाह से पैदा होने वाली सन्तान को उन्होंने चण्डाल कहा है।

प्रश्न 3.
अनुलोम विवाह क्या होता है ?
उत्तर-
जब एक उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है तथा इस प्रकार के विवाह साधारणतया होते रहते थे।
प्रश्न 4.
विवाह पर प्रतिबन्ध।
उत्तर-
कई समाजों में विवाह करवाने के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबन्ध होते हैं कि किस समूह में विवाह करना है तथा किस में नहीं। साधारणतया रक्त सम्बन्धी, एक ही गोत्र वाले व्यक्ति आपस में विवाह नहीं करवा सकते।
प्रश्न 5.
गैर-भातृ बहुपति विवाह।
उत्तर-
बहुपति विवाह का वह प्रकार जिसमें पत्नी के सभी पति आपस में भाई नहीं होते गैर-भ्रातृ बहुपति विवाह होता है। विवाह के पश्चात् पत्नी निश्चित समय के लिए अलग-अलग पतियों के साथ रहती है।

प्रश्न 6.
बहुपत्नी विवाह का अर्थ।
उत्तर-
यह विवाह का वह प्रकार है जिसमें एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां होती हैं। यह दो प्रकार का होता है-प्रतिबन्धित तथा अप्रतिबन्धित बहु-पत्नी विवाह । इस प्रकार का विवाह आजकल वर्जित है।
प्रश्न 7.
बहु-पत्नी विवाह में स्त्रियों की स्थिति।
उत्तर-
बहु-पत्नी विवाह में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी निम्न होती है क्योंकि उसे कई पुरुषों से विवाह तथा संबंध रखने पड़ते हैं। इसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा उनकी सामाजिक स्थिति भी निम्न होती है।
प्रश्न 8.
एक विवाह पर संक्षेप नोट लिखें।
उत्तर-
जब एक ही स्त्री से एक ही पुरुष विवाह करवाता है तो विवाह को एक विवाह कहते हैं। जब तक दोनों जीवित हैं अथवा एक दूसरे से तलाक नहीं ले लेते, वह दूसरा विवाह नहीं करवा सकते।

प्रश्न 9.
बहु-पति विवाह के दो अवगुण।
उत्तर-
- इस प्रकार के विवाह में स्त्री का स्वास्थ्य खराब हो जाता है क्योंकि उसे कई पतियों की लैंगिक इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है।
- इस प्रकार के विवाह में स्त्री के लिए पतियों में झगडे होते रहते हैं।
प्रश्न 10.
एक विवाह के दो गुण।
उत्तर-
- एक विवाह में पति-पत्नी के संबंध अधिक गहरे होते हैं।
- इस विवाह में बच्चों का पालन-पोषण ठीक ढंग से हो जाता है।
- इस विवाह में पारिवारिक झगड़े कम होते हैं।
- इसमें पति-पत्नी में तालमेल रहता है।
प्रश्न 11.
बहुपत्नी विवाह के मुख्य कारण बताएं।
उत्तर-
- पुरुषों की अधिक यौन संबंधों की इच्छा के कारण बहुपत्नी विवाह सामने आए।
- लड़कियां पैदा होने के कारण तथा लड़का होने की इच्छा के कारण यह विवाह बढ़ गए।
- राजा-महाराजाओं के अधिक पत्नियां रखने के शौक के कारण यह विवाह सामने आए।

प्रश्न 12.
परिवार क्या होता है ?
उत्तर-
परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन सम्बन्धों पर आधारित है और जो इतना छोटा व स्थायी है कि उससे बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन-पोषण हो सके। इसमें सभी रक्त संबंधी शामिल होते हैं।
प्रश्न 13.
पितृ सत्तात्मक परिवार कौन-सा होता है ?
उत्तर-
वह परिवार जहां सारे अधिकार पिता के हाथ में होते हैं, परिवार पिता के नाम पर चलता है तथा परिवार पर पिता का पूरा नियन्त्रण होता है। घर के सभी सदस्यों को पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य करना पड़ता है।
प्रश्न 14.
मातृ-सत्तात्मक परिवार।
उत्तर-
वह परिवार जहां सारे अधिकार माता के हाथ में होते हैं, परिवार माता के नाम पर चलता है तथा परिवार पर माता का नियन्त्रण होता है। सम्पत्ति पर माता का अधिकार होता है तथा माता के पश्चात् सम्पत्ति पुत्री को प्राप्त होती है।

प्रश्न 15.
विवाह के आधार पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं ?
उत्तर-
विवाह के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं-
- एक विवाही परिवार
- बहु विवाही परिवार।
प्रश्न 16.
परिवार में शिक्षा संबंधी कार्यों में परिवर्तन।
उत्तर–
पहले परिवार बच्चों को शिक्षा देता था परन्तु अब इसमें परिवर्तन आ गया है। अब परिवार का यह कार्य स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों ने लिया है। पहले परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चों को शिक्षा देते थे परन्तु अब यह कार्य औपचारिक संस्थाओं के पास है।
प्रश्न 17.
परिवार की केंद्रीय स्थिति।
उत्तर-
परिवार की समाज में केन्द्रीय स्थिति है क्योंकि परिवार के बिना समाज अस्तित्व में नहीं आ सकता तथा प्रत्येक व्यक्ति समाज में ही रहना पसंद करता है। परिवार के कारण ही समाज अस्तित्व में आता है।
प्रश्न 18.
बच्चों का पालन-पोषण।
उत्तर-
बच्चों का पालन-पोषण परिवार का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है क्योंकि परिवार ही बच्चों की सभी आवश्यकताएं पूर्ण करता है। परिवार उसे अच्छा नागरिक बनाने के लिए सभी चीजें उपलब्ध करवाता है।

प्रश्न 19.
घर की व्यवस्था।
उत्तर-
परिवार अपने सदस्यों के लिए घर की व्यवस्था करता है। घर के बिना परिवार न तो बन सकता है तथा न ही प्रगति कर सकता है। इस प्रकार घर की व्यवस्था करके परिवार सदस्यों के व्यक्तित्व का विकास भी करता है।
प्रश्न 20.
परिवार में सहयोग।
उत्तर-
पति तथा पत्नी एक-दूसरे से सहयोग करते हैं ताकि परिवार का कल्याण हो सके। वह अपने बच्चों तथा परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए एक-दूसरे से सहयोग करते हैं। पति-पत्नी के सहयोग के कारण ही परिवार सामने आता है।
प्रश्न 21.
साझे परिवार पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव।
उत्तर-
साझे परिवार में रहने वाले व्यक्ति पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के अधीन आ रहे हैं। इस कारण वह अपने सांझे परिवारों को छोड़ रहे हैं तथा केंद्रीय परिवार बसा रहे हैं। इस तरह साझे परिवार खत्म हो रहे हैं।
प्रश्न 22.
परिवार के दो कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर-
- परिवार में व्यक्ति की सम्पत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँच जाती है तथा किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाती।
- बच्चों के पालन-पोषण तथा सुरक्षा का कार्य परिवार का ही होता है तथा उनका सही विकास परिवार में ही हो सकता है।

प्रश्न 23.
परिवार के कार्यों में कोई दो परिवर्तन।
उत्तर-
- आजकल के परिवार अधिक प्रगतिशील हो रहे हैं।
- स्त्रियां घरों से बाहर निकल कर कार्य कर रही हैं जिस कारण उनके कार्य बदल रहे हैं।
- परिवार के मुखिया का नियन्त्रण कम हो गया है तथा सभी अपनी इच्छा से कार्य करते हैं।
प्रश्न 24.
नवस्थानीय परिवार।
उत्तर-
इस प्रकार के परिवार में विवाह के पश्चात् पति-पत्नी अपने माता-पिता के घर जाकर नहीं रहते बल्कि अपना नया घर बसाते हैं तथा बिना रोक-टोक के रहते हैं। आजकल इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं।
लघु उत्तरात्मक प्रश्न
प्रश्न 1.
सामाजिक संस्था।
उत्तर-
संस्था न तो लोगों का समूह है और न ही संगठन है। सामाजिक संस्था तो किसी कार्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिमाप की व्यवस्था है। संस्था तो किसी विशेष महत्त्वपूर्ण क्रिया के आस-पास केन्द्रित रूढियों और लोक रीतों का जाल है। संस्थाएं तो संरचिंत प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने कार्य करता है।
प्रश्न 2.
संस्था के दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व बताइये।
उत्तर-
- निश्चित उद्देश्य-संस्था विशेष मानवीय आवश्यकता के लिए विकसित होती है। बिना उद्देश्य के संस्था नहीं होती है। इस प्रकार संस्था किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनती है।
- एक विचार-विचार ही संस्था का आवश्यक तत्त्व है। किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक विचार की शुरुआत होती है जिसको समूह अपने लिए आवश्यक समझता है। इस कारण इसकी रक्षा हेतु वह संस्था को विकसित करता है।

प्रश्न 3.
संस्था की चार विशेषताएं लिखो।
उत्तर-
- संस्था व्यवस्था एक इकाई है।
- संस्था के स्पष्ट तौर पर परिभाषित उद्देश्य हैं।
- संस्था अमूर्त होती है।
- संस्था की एक परम्परा व प्रतीक होता है।
प्रश्न 4.
संस्था के कोई चार कार्य बतायें।
उत्तर-
- संस्था समाज के ऊपर नियन्त्रण रखती है।
- संस्था व्यक्ति को पद एवं भूमिका प्रदान करती है।
- संस्था उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है।
- संस्था सांस्कृतिक एकसारता प्रदान करती है।
- संस्था संस्कृति की वाहक है।
प्रश्न 5.
संस्था कितने प्रकार की होती है ?
उत्तर-
वैसे तो संस्थाएं कई प्रकार की होती हैं, पर साधारणतया संस्थाएं चार प्रकार की होती हैं-
- सामाजिक संस्थाएं (Social Institutions)
- राजनैतिक संस्थाएं (Political Institutions)
- आर्थिक संस्थाएं (Economic Institutions)
- धार्मिक संस्थाएं (Religious Institutions)।
प्रश्न 6.
विवाह का अर्थ।
उत्तर–
प्रत्येक समाज में परिवार की स्थापना के लिए स्त्री व पुरुष के लिंगक सम्बन्धों को स्थापित करने की मान्यता विवाह द्वारा दी जाती है। इस प्रकार लिंग सम्बन्धों को निश्चित करने व संचालित करने के लिए बच्चों के पालनपोषण की ज़िम्मेदारी को निर्धारित करने व परिवार को स्थाई रूप देने के लिए बनाए गए नियमों को विवाह कहते हैं। परिवार बसाने के लिए दो या दो से अधिक स्त्रियों व पुरुषों के बीच ज़रूरी सम्बन्ध स्थापित करने व उन्हें स्थिर रखने के लिए संस्थात्मक व्यवस्था को विवाह कहते हैं। जिसका उद्देश्य घर की स्थापना, यौन सम्बन्धों में प्रवेश व बच्चों का पालन-पोषण है।

प्रश्न 7.
एक विवाह।
उत्तर-
आजकल के आधुनिक युग में एक विवाह का प्रचलन सबसे अधिक है। इस तरह के विवाह में एक पुरुष एक ही समय, एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता है। एक विवाह में पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करना गैरकानूनी माना जाता है। इसमें पति-पत्नी के सम्बन्ध गहरे, स्थायी और प्यार हमदर्दी वाले होते हैं। इसमें बच्चों का पालनपोषण अच्छे ढंग से हो जाता है। उनको माता-पिता का पूरा प्यार मिलता है। पति-पत्नी में प्यार और तालमेल होता है। इसमें पुरुष और स्त्री के सम्बन्धों में समान अधिकार पाये जाते हैं।
प्रश्न 8.
एक विवाह के गुण।
उत्तर-
- पति-पत्नी के सम्बन्ध अधिक गहरे होते हैं।
- इसमें बच्चों का पालन-पोषण अच्छी तरह होता है।
- पति-पत्नी में तालमेल अधिक रहता है।
- पारिवारिक झगड़े कम होते हैं।
- व्यक्ति मनोवैज्ञानिक और जैविक तनावों से मुक्त रहता है।
- लड़का और लड़की दोनों को समान अधिकार प्राप्त होता है।
प्रश्न 9.
एक विवाह के अवगुण।
उत्तर-
- बीमारी या गर्भावस्था में पति-पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध नहीं रख सकता इसलिए वह बाहर जाना आरम्भ कर देता है।
- बाहरी सम्बन्धों की वजह से अनैतिकता बढ़ती है।
- कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
- पति का पत्नी के बीमार होने से घरेलू काम रुक जाते हैं, जिससे बच्चों का पालन-पोषण सही नहीं हो पाता।
प्रश्न 10.
बहिर्विवाह से क्या अर्थ है ?
उत्तर-
बहिर्विवाह का अर्थ है कि अपनी गोत्र, अपने सपिण्ड और टोटम से बाहर वैवाहिक सम्बन्ध पैदा करने पड़ते हैं। एक ही गोत्र, सपिण्ड और टोटम के पुरुष और स्त्री आपस में भाई-बहन माने जाते हैं। वैस्ट मार्क के अनुसार इस विवाह का उद्देश्य नज़दीक के रिश्तेदारों में यौन सम्बन्ध स्थापित न होने देना है। ये विवाह प्रगतिवाद का सूचक है और ये विवाह भिन्न-भिन्न वर्गों में सम्पर्क बढ़ाता है। जैविक दृष्टिकोण से यह विवाह ठीक माना गया है। इस विवाह का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसमें वर-वधू को एक-दूसरे के विचारों को जानने में बड़ी मुश्किलें आती हैं।

प्रश्न 11.
अन्तर्विवाह।
उत्तर-
अन्तर्विवाह में व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता था। इसमें विवाह का एक बन्धन क्षेत्र होता है जिसके अनुसार आदमी औरत एक निश्चित सामाजिक समूह के अधीन ही विवाह कर सकते हैं। इसके साथ समूह की एकता रखी जा सकती है। यह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक प्रगति में रुकावट पैदा करती है। इसके साथ जातिवाद की भावना को भी बढ़ावा मिलता है।
प्रश्न 12.
दो पत्नी विवाह।
उत्तर-
इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष का विवाह दो स्त्रियों के साथ होता है। ये दोनों स्त्रियां उस पुरुष की पत्नियां होती हैं। इसलिये इस विवाह को दो पत्नी विवाह कहा जाता है। इसमें पुरुष को दो पत्नियां रखने की इजाजत दी जाती है।
प्रश्न 13.
बहु-पत्नी प्रथा।
उत्तर-
यह बहु-विवाह का एक अन्य रूप है। इस तरह के विवाह में व्यक्ति एक से अधिक पत्नियों के साथ विवाह करवाता है। रिउटर के अनुसार बहु-पत्नी विवाह विवाह का वह रूप है, जिसमें व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक पत्नियों को रख सकता है। ये प्रथा संसार के सभी समाजों में पाई जाती है। पुरुष में यौन की इच्छा और बड़े परिवार की चाह के कारण इस विवाह प्रथा को अपनाया गया।

प्रश्न 14.
बहु-पत्नी विवाह के कारण।
उत्तर-
- पुरुषों की अधिक यौन सम्बन्धों की इच्छाओं के कारण बहु विवाह होते हैं।
- बड़े परिवार की इच्छा के कारण यह विवाह होते हैं।
- लड़कियां होने पर लड़कों की इच्छा के कारण यह विवाह होते हैं।
- स्त्रियों की गणना बढ़ने के कारण भी यह विवाह होते थे।
- राजाओं, महाराजाओं की अधिक पत्नियां रखने के शौक के कारण इस प्रकार के विवाह होते थे।
प्रश्न 15.
बहु-पत्नी विवाह के गुण।
उत्तर-
- बच्चों का बढ़िया पालन-पोषण हो जाता है।
- मर्दो की अधिक यौन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है।
- सम्पत्ति घर में ही रहती है।
- सन्तान शक्तिशाली और सेहतमंद पैदा होती है।
- एक पत्नी के बीमार होने से घर के काम चलते रहते हैं।
- लिंग सम्बन्धों की पूर्ति के कारण अनैतिकता नहीं फैलती।
प्रश्न 16.
बहु-पत्नी विवाह के अवगुण।
उत्तर-
- इसके साथ स्त्रियों का दर्जा निम्न होता है।
- स्त्रियों की यौन इच्छा पूरी नहीं होती, जिसके लिये वह बाहर जाती हैं और अनैतिकता फैलती है।
- अधिक पत्नियों के कारण उनमें झगड़ा रहता है।
- परिवार में अशान्ति रहती है।
- परिवार में आर्थिक बोझ बढ़ता है।

प्रश्न 17.
कुलीन विवाह।
उत्तर-
हिन्दू समाज में बहु-पत्नी विवाह का सबसे मुख्य उदाहरण कुलीन बहु-विवाह है। सभी चाहते हैं कि उनकी लड़कियों का विवाह बड़ी जाति के लड़कों के साथ हो पर कुलीन वंश की गिनती अधिक नहीं थी। एक-एक कुलीन ब्राह्मण 100-100 लड़कियों के साथ विवाह करवाता था। इस कारण दहेज प्रथा बढ़ गई और समाज में अनैतिकता भी बढ़ गई।
प्रश्न 18.
साली विवाह।
उत्तर-
इस विवाह में पुरुष अपनी स्त्री की बहन के साथ विवाह करता है। ये विवाह दो तरह का होता है। सीमित साली विवाह, समकालीन साली विवाह, सीमित साली विवाह में पुरुष अपनी स्त्री की मौत के बाद उसकी बहन के साथ विवाह करता है। समकालीन साली विवाह में पुरुष अपनी स्त्री की सभी-बहनों को अपनी पत्नियों के समान मानता है। पहली किस्म का प्रचलन अधिक है। इनमें परिवार नहीं टूटता और बच्चों का पालन-पोषण अधिक अच्छी तरह होता है।
प्रश्न 19.
देवर विवाह।
उत्तर-
विवाह की इस प्रथा में पत्नी अपने पति की मौत के बाद उसके भाई के साथ विवाह करवाती है। इसके साथ परिवार की सम्पत्ति सुरक्षित रह जाती है। परिवार टूटने से बचता है। बच्चों का पालन-पोषण ठीक हो जाता है। इस विवाह के साथ लड़के के माता-पिता को लड़की का मूल्य वापिस नहीं करना पड़ता।

प्रश्न 20.
बहु-पति विवाह।
उत्तर-
इस विवाह में एक स्त्री बहुत से पतियों के साथ विवाह करती है। एक ही समय में वह सभी की पत्नी होती है इसके दो प्रकार हैं। भ्रात बहु-पति विवाह, जिसमें स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं और गैर-भ्रातृ बहु-पति विवाह, जिसमें स्त्री के सभी पति आपस में भाई नहीं होते। ग़रीबी और स्त्रियों की कम गिनती के कारण ये प्रथा बढ़ी।
प्रश्न 21.
भ्रातृ बहु-पति विवाह।
उत्तर-
इस विवाह की प्रथा के अनुसार स्त्री के सारे पति परस्पर भाई हुआ करते थे अथवा एक ही जाति के व्यक्ति होते थे। इस विवाह की प्रथा में सबसे बड़ा भाई एक स्त्री से विवाह करता है तथा उसके सब भाइयों का उस पर पत्नी रूप में अधिकार होता है व सारे उससे लैंगिक सम्बन्ध रखते हैं। यदि कोई छोटा भाई विवाह करता है तो उसकी भी पत्नी सब भाइयों की पत्नी होती है, जो बच्चे होते हैं वो सब बड़े भाई के नाम से माने जाते हैं व सम्पत्ति पर भी अधिकार बड़े भाई का अधिक होता है।
प्रश्न 22.
गैर-भ्रातृ बहु-पति विवाह।
उत्तर–
बहु-पति विवाह की इस प्रकार में एक औरत के पति आपस में भाई नहीं होते। यह पति सब भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते हैं। ऐसे समय में औरत निश्चित समय के लिए एक पति के पास रहती है इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे के पास। इस तरह सारा साल अलग-अलग पतियों के पास जीवन व्यतीत करती है। जिस समय एक स्त्री एक पति के पास रहती है उस समय दूसरे पतियों को उससे सम्बन्ध बनाने का अधिकार नहीं होता। बच्चा होने पर एक विशेष संस्कार अनुसार पति उसका पिता बन जाता है जो वह गर्भावस्था में स्त्री को धनुष (तीर-कमान) भेंट करता है। उसे उस बच्चे का पिता मान लिया जाता है।

प्रश्न 23.
परिवार का अर्थ।
उत्तर-
परिवार एक ऐसी संस्था है जिससे स्त्री व पुरुष समाज से मान्यता प्राप्त लिंग सम्बन्ध स्थापित करता है। परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जो एक विशेष नाम से पहचाना जाता है जिसमें पति-पत्नी के स्थाई लिंग सम्बन्ध होते हैं जिसमें सदस्यों के पालन-पोषण की पूर्ण व्यवस्था होती है जिससे सदस्यों में खून के सम्बन्ध होते हैं व इसके सदस्य एक खास निवास स्थान पर रहते हैं।
प्रश्न 24.
परिवार की विशेषताएं।
उत्तर-
- परिवार सर्वव्यापक है।
- परिवार लिंग सम्बन्धों से उत्पन्न समूह है।
- परिवार का सामाजिक आधार में केन्द्रीय स्थान होता है।
- परिवार में रक्त सम्बन्धों का बन्धन होता है।
- परिवार में सदस्यों की ज़िम्मेदारी अन्य सदस्य चुनते हैं।
- परिवार सामाजिक नियन्त्रण का आधार होता है।
प्रश्न 25.
परिवार व सामाजिक नियन्त्रण।
उत्तर-
परिवार ही बच्चों पर नियन्त्रण रखता है व उसको नियन्त्रण में रहना सिखाता है। परिवार उस पर इस प्रकार से नियन्त्रण रखता है कि उसमें ग़लत आदतें न उत्पन्न हो सकें। परिवार अपने सदस्यों के हर तरह के व्यवहार व क्रियाओं पर नियन्त्रण रखता है। इस तरह बच्चा अनुशासन में रहना सीखता जाता है। इस प्रकार परिवार बच्चे पर निगरानी रखकर एक तरह से सामाजिक नियन्त्रण रखता है।

प्रश्न 26.
परिवार व समाजीकरण।
उत्तर-
परिवार माता-पिता व बच्चों की स्थायी संस्था है, जिसका प्रथम कार्य बच्चों का समाजीकरण करना है। परिवार में बच्चा हमदर्दी, प्यार व ज़िम्मेदारी की पालना करना सीखता है। परिवार से ही वह छोटे, बराबर के व बड़ों के प्रति व्यवहार प्रकट करना सीखता है। परिवार में उसकी आदतों, अनुभवों, शिक्षाओं व कार्यों से ही आगे जाकर समाज में उसका काम व आचरण निश्चित होता है। परिवार में ही वह सामाजिक रीति-रिवाजों, रस्मों, आचरण, नियमों, सामाजिक बन्धनों की पालना इत्यादि सीखता है। इस प्रकार परिवार समाजीकरण का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है।
प्रश्न 27.
एकाकी परिवार क्या है ?
उत्तर-
इकाई परिवार वह परिवार है जिसमें पति-पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। विवाह के बाद बच्चे अपना अलग घर कायम कर लेते हैं। यह सबसे छोटे परिवार होते हैं। यह परिवार अधिक प्रगतिशील होते हैं व उनके फैसले तर्क के आधार पर होते हैं। इसमें पति-पत्नी को बराबर का दर्जा हासिल होता है। आजकल इकाई परिवार का अधिक चलन है।
प्रश्न 28.
इकाई परिवार की विशेषताएं बताओ।
उत्तर-
- केन्द्रीय परिवार या इकाई परिवार आकार में छोटा होता है।
- इकाई परिवार में सम्बन्ध सीमित होते हैं।
- परिवार के प्रत्येक सदस्य को महत्त्व मिलता है।
- परिवार की सत्ता साझी होती है।
प्रश्न 29.
इकाई परिवार के गुण (लाभ)।
उत्तर-
- इकाई परिवारों में औरतों की स्थिति ऊंची होती है।
- इसमें रहने-सहने का दर्जा उच्च वर्ग का होता है।
- व्यक्ति को मानसिक सन्तुष्टि मिलती है।
- व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है।
- सदस्यों में सहयोग की भावना होती है।

प्रश्न 30.
इकाई परिवार के अवगुण (हानियां)।
उत्तर-
- यदि माता या पिता में से कोई बीमार पड़ जाए तो घर के कामों में रुकावट आ जाती है।
- इसमें बेरोज़गार व्यक्ति का गुजारा मुश्किल से होता है।
- पति की मौत के पश्चात् यदि औरत अशिक्षित हो तो परिवार की पालना कठिन हो जाती है।
- कई बार आर्थिक मुश्किलों के कारण पति-पत्नी में लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं।
प्रश्न 31.
संयुक्त परिवार।
उत्तर-
संयुक्त परिवार एक मुखिया की ओर से शासित अनेकों पीढ़ियों के रक्त सम्बन्धियों का एक ऐसा समूह है जिनका निवास, चूल्हा व सम्पत्ति संयुक्त होते हैं। वह सब कर्तव्यों व बन्धनों में बंधे रहते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं-(1) साझा चूल्हा (2) साझा निवास (3) साझी सम्पत्ति (4) मुखिया का शासन (5) बड़ा आकार। आजकल इस प्रकार के परिवारों की बजाय केन्द्रीय परिवार चलन में आ गए हैं।
प्रश्न 32.
संयुक्त जायदाद या ‘संयुक्त सम्पत्ति’।
उत्तर-
संयुक्त परिवार में सम्पत्ति पर सभी सदस्यों का बराबर अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य अपनी सामर्थ्य अनुसार इस सम्पत्ति में अपना योगदान डालता है। जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता होती है वह उतनी सम्पत्ति खर्च कर लेता है। परिवार का कर्त्ता साझी जायदाद की देख-रेख करता है।
प्रश्न 33.
साझा रसोई-घर।
उत्तर-
संयुक्त परिवार की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके सभी सदस्य एक ही रसोई घर का इस्तेमाल करते हैं। भाव यह कि उनका खाना एक ही जगह बनता है व उसे वह इकट्ठे ही मिलकर खाते हैं। ऐसा करते समय वह अपने विचार एक-दूसरे से बांटते हैं। इससे उनका आपसी प्यार व हमदर्दी बनी रहती है।

प्रश्न 34.
साझे परिवार में कर्ता।
उत्तर-
संयुक्त परिवार में घर के मुखिया की मुख्य भूमिका होती है जिसको कर्ता कहते हैं। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य परिवार का मुखिया या कर्ता होता है। परिवार से सम्बन्धित सारे महत्त्वपूर्ण फैसले उसके द्वारा लिए जाते हैं। वह परिवार की साझी सम्पत्ति की देखभाल करता है। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। कर्ता की मृत्यु के पश्चात् परिवार की देखभाल की ज़िम्मेदारी उसके सबसे बड़े बेटे पर आ जाती है और वह परिवार का कर्ता बन जाता है।
प्रश्न 35.
संयुक्त परिवार के गुण (लाभ)।
उत्तर-
- संयुक्त परिवार संस्कृति व समाज की सुरक्षा करता है।
- संयुक्त परिवार बच्चों का पालन-पोषण करता है।
- संयुक्त परिवार सामाजिक नियन्त्रण व मनोरंजन का केन्द्र होता है।
- संयुक्त परिवार सम्पत्ति के विभाजन को रोकता है, उत्पादन में बढ़ोत्तरी व खर्च में कमी करता है।
- बुजुर्गों व बीमार सदस्यों की मदद करता है।
प्रश्न 36.
संयुक्त परिवार के अवगुण (हानियां)।
उत्तर-
- संयुक्त परिवार में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास नहीं हो पाता।
- संयुक्त परिवार में औरतों का निम्न दर्जा होता है।
- इनमें व्यक्तियों की खाली रहने की आदत पड़ जाती है।
- चिंता न होने से अधिक संतान उत्पत्ति होती है।
- लड़ाई-झगड़े अधिक होते हैं।
- पति-पत्नी को एकान्त प्राप्त नहीं होता।
प्रश्न 37.
क्यों संयुक्त परिवार टूट रहे हैं ?
उत्तर-
संयुक्त परिवारों के टूटने के कई कारण हैं; जैसे-
- धन की बढ़ती महत्ता के कारण।
- पश्चिमी प्रभाव के कारण।
- औद्योगीकरण के बढ़ने के कारण।
- सामाजिक गतिशीलता के सामने आने के कारण।
- जनसंख्या की बढ़ती दर के कारण।
- यातायात के साधनों का विकास की वजह से।
- स्वतन्त्रता व समानता के आदर्श के सामने आने से।
- औरतों के आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने से।

प्रश्न 38.
पितृ-मुखी परिवार क्या है ?
अथवा
पितृसत्तात्मक परिवार।
उत्तर-
जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है कि इस प्रकार के परिवारों की सत्ता या शक्ति पूरी तरह से पिता के हाथ में होती है। परिवार के सम्पूर्ण कार्य पिता के हाथ में होते हैं। वह ही परिवार का कर्ता होता है। परिवार के सभी छोटे या बड़े कार्यों में पिता का ही कहना माना जाता है। परिवार के सभी सदस्यों पर पिता का ही नियन्त्रण होता है। इस तरह का परिवार पिता के नाम पर ही चलता है। पिता के वंश का नाम पुत्र को मिलता है व पिता के वंश का महत्त्व होता है। आजकल इस प्रकार के परिवार मिलते हैं।
प्रश्न 39.
मातृ-वंशी परिवार।
अथवा
मातृसत्तात्मक परिवार।
उत्तर-
जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि परिवार में सत्ता या शक्ति माता के हाथ ही होती है। बच्चों पर माता के रिश्तेदारों का अधिकार अधिक होता है न कि पिता के रिश्तेदारों का। स्त्री ही मूल पूर्वज मानी जाती है। सम्पत्ति का वारिस पुत्र नहीं बल्कि मां का भाई या भांजा होता है। परिवार मां के नाम से चलता है। इस प्रकार का परिवार भारत में कुछ कबीलों में जैसे गारो, खासी आदि में मिल जाता है।
प्रश्न 40.
परिवार के मुख्य कार्य बताओ।
उत्तर-
- लैंगिक सम्बन्धों की पूर्ति करता है।
- सन्तान पैदा करना।
- सदस्यों की सुरक्षा व पालन-पोषण करता है।
- सम्पत्ति की देखभाल व आय-व्यय का प्रबन्ध करता है।
- धर्म की शिक्षा देना।
- बच्चों का समाजीकरण करता है।
- संस्कृति का संचार व विकास करता है।
- परिवार सामाजिक नियन्त्रण में मदद करता है।

प्रश्न 41.
परिवार के कार्यों में परिवर्तन।
उत्तर-
- परिवार अधिकतर प्रगतिशील हो रहे हैं।
- धार्मिक उत्तरदायित्वों की पालना की भावना कम हो रही है।
- पारिवारिक महत्त्व काफ़ी कम हो गया है।
- औरतें काम करने के लिए बाहर जाती हैं, इसलिए उनके काम बदल रहे हैं।
- संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं।
प्रश्न 42.
रक्त सम्बन्धी परिवार।
उत्तर-
इस प्रकार के परिवार में रक्त-सम्बन्ध का स्थान सर्वोच्च होता है। इनमें किसी प्रकार के लिंग सम्बन्ध नहीं होते। इसमें पति-पत्नी भी होते हैं परन्तु वह परिवार के आधार नहीं होते। इसमें सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। तलाक भी इन परिवारों को भिन्न नहीं कर सकता और यह स्थाई होते हैं।
प्रश्न 43.
पितृ स्थानीय परिवार।
उत्तर-
इस प्रकार के परिवार में लड़की विवाह के उपरान्त अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जाकर रहने लग जाती है और पति के माता-पिता व पति के साथ वहीं घर बसाती है। इस प्रकार के परिवार आमतौर से प्रत्येक समाज में मिल जाते हैं।

प्रश्न 44.
नव स्थानीय परिवार।
उत्तर-
इस प्रकार के परिवार पहली दोनों किस्मों से भिन्न हैं। इसमें पति-पत्नी कोई भी एक-दूसरे के पिता के घर जाकर नहीं रहते बल्कि वह किसी और स्थान पर जाकर नया घर बसाते हैं। इसलिए इसको नव स्थानीय परिवार कहते हैं। आजकल के औद्योगिक समाज में इस तरह के परिवार आम पाए जाते हैं।
प्रश्न 45.
नातेदारी क्या होती है ?
अथवा
नातेदारी।
उत्तर-
चार्लस विनिक के अनुसार, “नातेदारी व्यवस्था में वे सम्बन्ध शामिल किये जाते हैं जोकि कल्पित या वास्तविक वंश परम्परागत बन्धनों के ऊपर आधारित एवं समाज के द्वारा प्रभावित होते हैं।”
प्रश्न 46.
नातेदारी को कितने भागों में बांटा जा सकता है?
उत्तर-
निम्न तीन में बांटा जा सकता है-
- व्यावहारिक नातेदारी।
- सगोत्र नातेदारी।
- कल्पित या रस्मी नातेदारी।
प्रश्न 47.
सगोत्र नातेदारी क्या होती है ?
उत्तर-
वह सभी व्यक्ति जिनमें रक्त का बन्धन है, सगोत्र नातेदारी का ही भाग होते हैं। रक्त का सम्बन्ध यद्यपि वास्तविक हो या कल्पित तो ही इसी आधार के ऊपर सम्बन्धित व्यक्तियों को नातेदारी व्यवस्था में स्थान प्राप्त है यदि इसको सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है।

प्रश्न 48.
वंश समूह क्या होता है ?
उत्तर-
वंश समूह माता या पिता में से किसी एक के रक्त सम्बन्धियों से मिलकर बनता है। इन सभी सम्बन्धियों के किसी एक स्त्री या पुरुष के साथ वास्तविक वंश परम्परागत होते (Ties) हैं। सभी सदस्य वास्तविक साझे पूर्वज की सन्तान होने के कारण अपने वंश समूह में विवाह नहीं करवाते। इस प्रकार वंश समूह उन रक्त के सम्बन्धियों का समूह होता है। जो साझे पूर्वज की एक रेखकी सन्तान होते है और जिनकी पहचान को अनुरेखित किया जाता
है।
प्रश्न 49.
गोत्र क्या होते हैं ?
उत्तर-
गोत्र वंश समूह का ही विस्तृत रूप है, जोकि माता-पिता के किसी एक के अनुरेखित रक्त सम्बन्धियों से मिलकर बनता है। इस तरह गोत्र रिश्तेदारों का समूह होता है, जो किसी साझे पूर्वज की एक रेखकी सन्तान होती है। पूर्वज आमतौर पर कल्पित ही होते हैं। क्योंकि इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। यह बहिर्विवाही समूह होते हैं।
प्रश्न 50.
वैवाहिक नातेदारी।
उत्तर-
वैवाहिक नातेदारी पति-पत्नी के यौन सम्बन्धों पर आधारित होती है। यद्यपि उनमें कोई रक्त सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु उनमें विवाह के बाद सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं। विवाह के बाद व्यक्ति को पति के साथ जवाई, फूफड़, जीजा, सांदू आदि के रुतबे हासिल होते हैं। इस तरह स्त्री को भी पत्नी के साथ-साथ, देवराणी, जेठानी, चाची, ताई इत्यादि का रुतबा प्राप्त होता है। इस तरह के रुतबों को वैवाहिक नातेदारी का नाम दिया जाता है।
बड़े उत्तरों वाले प्रश्न
प्रश्न 1.
विवाह की विशेषताओं का वर्णन करें।
उत्तर-
विवाह की विशेषताओं का वर्णन नीचे दिया गया है-
1. विवाह एक सर्वव्यापक संस्था है (It is an universal insitutions)-विवाह की संस्था चाहे प्राचीन थी, चाहे आधुनिक है, सभी समाजों में पाई जाती है। यह सर्वव्यापक है। इस संस्था के बिना किसी स्थिर समाज की हम कल्पना तक नहीं कर सकते।
2. इस संस्था के द्वारा आदमी व औरत के लैंगिक सम्बन्धों को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है (Social sanction)-बिना सामाजिक मान्यता के यह सम्बन्ध गैर कानूनी करार दिए जाते हैं। इस संस्था का सदस्य बन कर व्यक्ति अपने दूसरे अधिकारों को भी जान जाता है व उसका दायरा कुछ सीमित हो जाता है।
3. दो विरोधी लिंगों का सम्बन्ध इस संस्था को जन्म देता है (Development of institution)-इससे मानव अपनी जैविक ज़रूरत को भी पूरा कर लेता है। पशुओं में भी विरोधी लिंगों का मेल होता है। लेकिन मानवों के इस मेल के द्वारा विवाह की संस्था का जन्म होता है परन्तु जानवरों का इस संस्था से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता।
4. विवाह की संस्था के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक स्थिति भी प्राप्त हो जाती है (Provide social status)-विवाह के पश्चात् पुरुष व स्त्री, पति-पत्नी के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद उनकी सामाजिक स्थिति माता-पिता से सम्बन्धित हो जाती है जिसके साथ परिवार का जन्म हो जाता है।
5. विवाह को एक समझौता भी समझा जाता है (Social Contract)—इसमें आदमी व औरत न केवल अपनी लिंग इच्छाओं की पूर्ति करते हैं बल्कि बच्चों के पालन-पोषण का बोझ भी सम्भालते हैं व पारिवारिक उत्तरदायित्वों को भी अदा किया जाता है।
6. विवाह के प्रकार अलग-अलग समाजों में अलग-अलग पाए जाते हैं (Different types in different societies)—प्रत्येक समाज की अपनी ही संस्कृति होती है जिसकी सुरक्षा से बाकी संस्थाएं जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए मुसलमानों की संस्कृति एक से अधिक विवाह की आज्ञा दे देती है परन्तु हिन्दुओं की संस्कृति इसके विपरीत है अर्थात् एक से अधिक विवाह को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती।
7. विवाह के द्वारा व्यक्ति को कानूनन मान्यता प्राप्त हो जाती है (Legal Sanction)-इससे पुरुष व स्त्री के विवाह सम्बन्ध भी स्थापित हो जाते हैं।
8. इस संस्था के द्वारा धार्मिक रीति-रिवाज भी सुरक्षित रहते हैं। चाहे आधुनिक समय में कोर्ट-मैरिज होने लगी है, परन्तु धार्मिक संस्कार अभी भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं।

प्रश्न 2.
एक विवाह का क्या अर्थ है ? इसके कारणों, लाभों तथा कमियों का वर्णन करें।
उत्तर-
आधुनिक समय में अधिकतर पाई जाने वाली विवाह का प्रकार ‘एक विवाह’ है। एक विवाह का अर्थ है जब एक आदमी, एक समय एक ही औरत से या एक औरत, एक समय, एक ही आदमी से विवाह करवाती है तो इसको एक विवाह का नाम दिया गया है। आजकल के सांस्कृतिक समाजों में इसको काफ़ी महत्ता प्राप्त है।
मैलिनोवस्की (Malinoviski) के अनुसार, “एक विवाह ही, विवाह का वास्तविक प्रकार है, जो पाई जा रही है व पाई जाती रहेगी।”
पीडीगंटन (Piddington) के अनुसार, “एक विवाह, विवाह का वह स्वरूप है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों के साथ एक ही समय पर विवाह सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता।”
वुकेनोविक के अनुसार, “उसी विवाह को एक विवाह कहना ठीक होता है, जिसमें न केवल एक व्यक्ति की पत्नी या पति हो, बल्कि किसी की भी मौत हो जाने पर दूसरा विवाह न करे। आमतौर पर एक पति या पत्नी के जीते जी किसी से न विवाह करना ही एक विवाह माना जाता है।”
भारतीय समाज में हिन्दू धर्म के अनुसार भी एक विवाह को ही आदर्श विवाह माना जाता है। प्राचीन समय से ही स्त्री के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता था। पति की मौत के साथ वह औरत आप भी सती होना बेहतर समझती थी। भारत में हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अधीन भी बहु-विवाह को समाप्त कर दिया गया व एक विवाह करने की ही स्वीकृति हो गई। आधुनिक समय में तो कानून इतने सख्त हैं कि तलाक लिए बिना आदमी व औरत दूसरा विवाह नहीं करवा सकते। कुछ हालातों में दूसरे विवाह की इजाजत दी गई जैसे सन्तान न होने की सूरत में. पति या पत्नी में कोई एक ला-इलाज बीमारी से सम्बन्धित हो आदि।
कारण (Causes)-
1. आधुनिक समाज में एक विवाह की प्रथा ही प्रचलित रही है। इस प्रथा के आने से ही हमारे समाज में भी प्रगति हुई है। जहां एक विवाह की प्रथा पाई गई उस समाज में प्रगति भी अधिक हुई। समाज की प्रगति के लिए भी एक विवाह को आवश्यक समझा गया।
2. स्त्रियों व पुरुषों की जनसंख्या की दर में बराबरी पाए जाने के कारण भी एक विवाह ही ज़रूरी समझा गया। इस अनुपात की बराबरी के कारण समाज में स्थिरता भी आ गई।
3. एकाधिकार की भावना के कारण भी एक विवाह को स्वीकृति प्राप्त हुई। आदिम समाज में जब विवाह की संस्था अधिक नियमित नहीं थी हुई तो कोई भी आदमी, किसी भी औरत से सम्बन्ध रख लेता था। कुछ देर के बाद उनमें ईर्ष्या की भावना पैदा होनी शुरू हो गई क्योंकि प्रत्येक आदमी यह इच्छा रखने लगा कि उसकी औरत, दूसरे आदमी के पास न जाए। उस समय जो आदमी शारीरिक तौर पर अधिक बलवान् थे, उन्होंने स्त्री पर एकाधिकार रखना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे आजकल के समय में आदमी व औरत दोनों के द्वारा एकाधिकार की भावना को अपनाया जाने लगा व आधुनिक समाज में एक विवाह के प्रकार को अपनाया गया।
4. प्राचीन समय में स्त्री का मूल्य रखा जाता था। जो भी पुरुष उस कीमत को अदा कर देता था उसको वह स्त्री दे दी जाती थी। इसके अतिरिक्त परिवार की स्थिरता के कारण एक पुरुष व एक स्त्री का विवाह प्रचलित था।
एक विवाह के लाभ (Advantages of Monogamy)-
1. स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन (Change in the Status of Women)–प्राचीन समय से स्त्रियों की समाज में काफ़ी निम्न स्थिति थी। पुरुष ने जिस तरह चाहा, उसी तरह का स्त्री से व्यवहार किया। यहां तक कि आश्रम व्यवस्था में स्त्री ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकती थी। उस का कार्य केवल बच्चे पैदा करना, घर का काम करना इत्यादि तक सीमित था।
इसके अतिरिक्त यदि जाति-प्रथा पर नजर डालें तो वहां भी औरत के जन्म को बुरा समझा जाता था। बिना पुरुष के उसको समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं होता था वह पति की मौत पर अपने आप को सती कर देती थी। धीरे-धीरे जब शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तो उनकी स्थिति पुरुषों के समान हो गई। इसी कारण एक विवाह की प्रथा के साथ स्त्री ने अपनी स्थिति को स्त्री के समान ही समझा। इस विवाह के प्रकार ने स्त्री की स्थिति में अधिक परिवर्तन किया।
2. बच्चों का पालन-पोषण (Up-bringing of Children)-एक विवाह के प्रकार के आधार पर जो परिवार पाया गया, उसमें बच्चों की परवरिश पहले से अधिक अच्छे ढंग से हो गई। दूसरे विवाह के प्रकारों में बच्चों में ईर्ष्या की भावना रहती थी। यहां तक कि परिवार के सभी सदस्यों में प्यार केवल दिखावा मात्र तक ही सीमित था। इस विवाह की किस्म से माता-पिता द्वारा बच्चों को सम्पूर्ण प्यार प्राप्त हुआ। उनकी हर तरह की ज़रूरतों की ओर ध्यान दिया गया। बच्चों में योग्यता व ज्ञान बढ़ा। उसके व्यक्तित्व का भी विकास हुआ।
3. परिवार की स्थिरता (Stability of Family)-एक विवाह से परिवार पहले से अधिक स्थिर हो गए। आदमी व औरत को एक-दूसरे के विचार समझने का मौका मिला। परिवार तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक पुरुष व स्त्री दोनों में सूझ-बूझ न हो। बहु-विवाह में लड़ाई-झगड़ा अधिक रहता था, न तो पुरुष स्त्री को पूरा प्यार दे सकता था न ही स्त्री पुरुष को पूरा प्यार दे सकती थी। तनाव की स्थिति तकरीबन विकसित रहती थी। इस स्थिति का प्रभाव बच्चों पर पड़ता था जिससे बच्चों का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता था। इसी कारण एक विवाह की प्रथा के द्वारा ही पारिवारिक जिन्दगी को अधिक स्थिरता प्राप्त हुई।
4. जायदाद का विभाजन (Division of Property)-जायदाद का विभाजन बहु-विवाह में एक समस्या बन जाती थी। कई बार तो भाई-भाई आपस में एक-दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते थे। परन्तु एक विवाह की प्रथा में इस समस्या का हल हो गया। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसकी जायदाद उसके बच्चों में बराबरी से विभाजित कर दी जाती थी।
5. रहन-सहन का उच्च-स्तर (Higher Standard of living)-आधुनिक समय में व्यक्ति की ज़िन्दगी प्राचीन समय से अधिक आरामदायक हो गई। एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री व एक स्त्री को केवल एक ही पुरुष की देखभाल करनी पड़ती थी। हरेक व्यक्ति अपने बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार अधिक-से-अधिक अच्छी शिक्षा दे सकता है व अपने आराम की सहूलतें भी प्राप्त कर लेता है। बहु-विवाह की प्रथा में अधिक बच्चों की परवरिश भी मुश्किल हो जाती थी। एक विवाह की प्रथा से सीमित परिवार को ज्यादातर अपनाया गया।
एक विवाह की कमियां (Demerits of Monogamy)-
1. एक विवाह की प्रथा में जब स्त्री बच्चा पैदा करने की अवस्था में होती है तो वह पुरुष को पूरा सहयोग नहीं दे सकती इसके अतिरिक्त बीमारी के समय पुरुष अपनी लैंगिक इच्छा की पूर्ति के लिए घर से बाहर जाना शुरू हो गया जिससे वेश्याओं को समाज में जगह मिल गई। कई स्थितियों में पुरुष व स्त्री को मजबूरन इकटे रहना पड़ता है चाहे उनमें आपसी प्यार न हो तो भी पुरुष व स्त्री दोनों अपनी जैविक भूख को मिटाने के लिए घर से बाहर जाने लगे हैं।
2. दूसरी कमी एक विवाह की प्रथा का कारण यह रहा कि यदि घर में पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक बीमार हो या दोनों, ऐसी स्थिति में घर बिलकुल बेहाल हो जाता है। बच्चों को खाने-पीने की समस्या का सामना करना पड़ जाता है व कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

प्रश्न 3.
बहु-विवाह की परिभाषाओं, प्रकारों, कारणों, लाभों तथा हानियों सहित व्याख्या करें।
उत्तर-
बहु-विवाह का अर्थ है जब तक एक से अधिक आदमी या औरतों से विवाह करने की स्वीकृति हो, उसको बह-विवाह का नाम दिया गया है। बलसेरा (Balsera) के अनुसार, “विवाह की वह प्रकार जिसमें पतियों व पत्नियों की बहुलता होती है, वह बहु-विवाह कहलाता है।”
बहु-विवाह के आगे भी कुछ प्रकार पाए गए हैं जो निम्नलिखित अनुसार है-
- दो-पत्नी विवाह (Bigamy)
- बहु-पत्नी विवाह (Polygyny)
- बहु-पति विवाह (Polyandry)
दो-पत्नी विवाह (Bigamy)-विवाह की इस प्रथा में एक पुरुष को केवल दो स्त्रियों से विवाह करवाने की आज्ञा होती है। विवाह का यह प्रकार पंजाब में भी प्रचलित रहा था।
बहु-पत्नी विवाह (Polygyny) विवाह के इस प्रकार का अर्थ है जब एक पुरुष का विवाह अधिक स्त्रियों से कर दिया जाता है, तो उसको बहु-पत्नी विवाह कहा जाता है।
के० एम० कपाड़िया (Kapadia) के अनुसार, “बहु-पत्नी विवाह, विवाह का वह प्रकार होता है, जिसमें पुरुष एक ही समय एक से अधिक स्त्रियां रख सकता है।”
जी० डी० मिचैल (G.D. Mitchell) के अनुसार, “एक पुरुष यदि एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करवाता है तो उसको बहु-पत्नी विवाह का नाम दिया जाता है।
यह दो प्रकार का होता है :
- प्रतिबन्धित बहु-पत्नी विवाह (Restricted Polygyny Marriage) .
- अप्रतिबन्धित बहु-पत्नी विवाह (Unrestricted Polygyny Marriage)
प्रतिबन्धित बहु-पत्नी विवाह (Restricted Polygyny)-बहु-पत्नी विवाह के इस प्रकार में पत्नियों की संख्या सीमित कर दी जाती है। व्यक्ति उस सीमा से अधिक पत्नियां व्यक्ति नहीं रख सकता। मुसलमानों में प्रतिबन्धित बहु-पत्नी विवाह की प्रथा अनुसार एक व्यक्ति के लिए पत्नियों की संख्या भी निश्चित कर दी जाती है।
अप्रतिबन्धित बहु-पत्नी विवाह (Unrestricted Polygyny)–इस प्रथा के अनुसार कोई भी पुरुष जितनी मर्जी पत्नियां रख सकता है। भारत में भी प्राचीन समय में विवाह की यह प्रथा ही प्रचलित थी।
बहु-पत्नी विवाह के कारण (Causes of Polygyny)-वैस्टर मार्क ने बहु-पत्नी विवाह के कई कारण दिए हैं जो निम्नलिखित हैं-
- स्त्रियों के पुरुषों से जल्दी बूढ़े हो जाने के कारण बहु-पत्नी विवाह प्रचलित रहा। बच्चा पैदा होने के पश्चात् स्त्रियों की सेहत भी कमजोर हो जाती थी। ऐसा अधिकतर असभ्य समाजों में पाया गया है।
- विवाह के पश्चात् कुछ समय स्त्री व पुरुष के वैवाहिक सम्बन्धों पर पाबन्दी लगा दी जाती थी। उदाहरण के तौर पर गर्भवती स्त्री के लिए भी यौन सम्बन्धों पर पाबन्दी होती थी। इस कारण भी एक से अधिक विवाह की आज्ञा दी जाती थी।
- पुरुषों में अधिक यौन सम्बन्धों की इच्छा भी इस विवाह के कारणों में मुख्य थी व कई बार पुरुषों द्वारा परिवर्तन चाहने के कारण भी बहु-पत्नी विवाह प्रचलित था।
- विशाल परिवार को प्राचीन समय में अच्छा दर्जा प्राप्त होता था। बड़े आकार के परिवार की इच्छा भी बहुपत्नी विवाह को प्रभावित करती थी।
- प्राचीन कबीले-समाजों में समाज को सम्मान प्राप्त करने के लिए भी कबीले के सरदार एक से अधिक विवाह करवाने में विश्वास रखते थे। क्योंकि लोग उसको अधिक अमीर परिवार से सम्बन्धित कर देते थे।
बहु-पत्नी विवाह के लाभ (Merits of Polygyny)-
- बहु-पत्नी विवाह की प्रथा से बच्चों का पालनपोषण बहुत बढ़िया ढंग से हो जाता था क्योंकि कई औरतें मिल कर उनकी देखभाल कर लेती थीं। यदि एक औरत बीमार हो जाती थी तो दूसरी औरत उसके बच्चों को रोटी इत्यादि दे देती थी।
- इस विवाह का लाभ यह भी था कि वेश्याओं के पास पुरुष को जाकर पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। घर में ही उसको अधिक काम इच्छा के लिए आवश्यक नवीनता भी प्राप्त हो जाती थी। इसकारण घर की सम्पत्ति भी सुरक्षित रहती थी।
- इस प्रथा से बच्चे भी स्वस्थ होते थे। क्योंकि एक स्त्री को ही अकेले बहुत बच्चों को जन्म देने के लिए उपयोग नहीं किया जाता था।
- बहु-पत्नी विवाह से जब कुलीन विवाह पाया गया तो निम्न जाति की लड़की भी उच्च जाति के लड़के से शादी करने लगी जिसके परिणामस्वरूप समाज में भाईचारे की भावना भी अधिक जागृत हुई।
बहु-पत्नी विवाह की हानियां (Demerits of Polygyny)-
- बहु-पत्नी विवाह की सबसे बड़ी कमी यह थी कि स्त्रियों का दर्जा समाज में बहुत निम्न था। क्योंकि स्त्री को केवल पुरुष के मनोरंजन के साधन रूप में ही समझा जाता था। आदमी के लिए औरत के प्रति प्यार की भावना नहीं थी बल्कि वह उसको केवल लिंग इच्छा की पूर्ति से ही सम्बन्ध रखता था। औरत की भावनाओं की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में तो औरत की कोई पहचान ही नहीं थी।
- स्त्रियां जब लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति से अधूरी रह जाती थी तो वह घर से बाहर जाकर अपने यौन सम्बन्ध कायम करने लग जाती थी क्योंकि एक पुरुष बहु-पत्नियों से विवाह करवा कर अपनी सन्तुष्टि तो कर सकता है परन्तु स्त्रियों की सन्तुष्टि नहीं हो सकती।
- परिवार में विवाह की इस प्रथा के साथ-माहौल दुःखदायक ही रह जाता था क्योंकि अधिक पत्नियां होने से आपस में लड़ाई-झगड़ा लगा रहता था।
- बहु-पत्नी विवाह की प्रथा के कारण समाज में परिवार के मुखिया पर आर्थिक बोझ अधिक होता था क्योंकि कमाने वाला एक होता था व बाकी परिवार के सभी सदस्य उस पर ही निर्भर होते थे। परिवार के रहन-सहन का दर्जा काफ़ी निम्न हो जाता था।
- बहु-पत्नी विवाह में परिवार का आकार बड़ा होता था जिस कारण मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा रहती थीं।
प्रश्न 4.
बहु-पति विवाह के प्रकारों, कारणों, लाभों तथा हानियों सहित व्याख्या करें।
उत्तर-
संसार के कई समाजों में बहु-पति विवाह की प्रथा प्रचलित है। बहु-पति विवाह का अर्थ विवाह की वह प्रथा है जिसमें एक औरत एक ही समय में एक से अधिक आदमियों से विवाह करवाए। उसको बह-पति विवाह का नाम दिया जाता है। अधिकतर यह विवाह तिब्बत (Tibet) पोलीनेशिया (Polynesia) के मार्कयूज़नीम, मालाबार के टोडा (Todas) मलायाद्वीप के कुछ कबीलों में अभी भी प्रचलित है। हिन्दू धर्म ग्रन्थों में महाभारत के अनुसार पांच पाण्डव भाइयों की भी एक ही पत्नी थी। भारत में देहरादून के खस कबीले, मध्य भारत के टोडा कबीले, केरल के कोट कबीले में भी बह-पति विवाह की प्रथा अभी भी प्रचलित है। इसके अतिरिक्त कई पहाडी कबीलों में भी इसी प्रथा को मान्यता प्राप्त हुई है। बहु-पति विवाह के बारे अलग-अलग विद्वानों के विचार नीचे दिए जा रहे हैं-
के० एम० कपाड़िया (K.M. Kapadia) के अनुसार, “बहु-पति विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें एक स्त्री के एक ही समय एक से अधिक पति होते हैं या इस प्रथा के अनुसार सभी भाइयों की सामूहिक रूप से एक पत्नी या कई पत्नियां होती हैं।” ___* जी० डी० मिचैल (G. D. Mitchell) के अनुसार, “एक स्त्री का दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह की प्रथा बहु-पति विवाह है।” इस प्रकार जिस विवाह में एक स्त्री के एक से अधिक पति हों को बहु-पति विवाह कहा जाता है।
बहु-पति विवाह के प्रकार (Types of Polyandrous Marriage)-बहु-पति विवाह के दो मुख्य रूप पाए होते हैं :
- भ्रातृ बहु-पति विवाह (Fraternal Polyandry)
- गैर-भ्रातृ बहु-पति विवाह (Non-Fraternal Polyandry)
भ्रातृ बहु-पति विवाह (Fraternal Polyandry)-बहु-पति विवाह के इस प्रकार के अनुसार स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं। बड़े भाई को बच्चे का पिता समझा जाता था व बाकी छोटे भाई उस औरत के पति होते हैं व वह अपने बड़े भाई की आज्ञा के बिना यौन सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते थे। घर में बड़े भाई की आज्ञा ही चलती थी व उसकी ही ज़िम्मेदारी होती थी कि वह बच्चों का पालन-पोषण करे। विवाह के पश्चात् यदि पति का और भाई भी जन्म लेता है तो उसको भी उस औरत का पति ही समझा जाता था। यदि बड़े के अलावा कोई और भाई भी किसी और जगह विवाह कर ले तो भी उसकी औरत के बाकी भाइयों से पत्नी वाले सम्बन्ध ही होते थे। यदि भाई इस बात को न मानें, अपनी पत्नी पर केवल अपना अधिकार ही समझे तो उसको जायदाद में से बेदखल कर दिया जाता था। भारत में नीलगिरी, लद्दाख, सिक्किम, असम इत्यादि में भी यह प्रथा पाई जाती है।
गैर-भ्रातृ बहुपति विवाह (Non-Fraternal Polyandry)-बहुपति विवाह के इस प्रकार में स्त्री के सभी पति भाई नहीं होते बल्कि वह सब अलग-अलग स्थान पर रहते हैं। औरत के लिए समय निश्चित किया जाता है कि उसने कितने समय के लिए एक पति के पास रहना है। निश्चित समय समाप्त होने पर वह दूसरे पति के साथ रहती है। इस प्रकार बारी-बारी वह सब पतियों के साथ रहती है। इस प्रकार में यदि स्त्री की मृत्यु हो जाए तो सारे पतियों को विधुर सा जीवन जीना पड़ता है। कई कबीले जिनमें यह प्रथा पाई जाती है तो सब जब स्त्री गर्भवती होती है तो गर्भ अवस्था में जो पति उसको तीरकमान भेंट करता है तो उसी को बच्चे का पिता स्वीकार कर लिया जाता है व बारी-बारी सभी पतियों को इस रस्म के अदा करने का अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रथा अनुसार यह भी नियम होता है कि एक निश्चित समय के लिए वह जिस पति के साथ रह रही होती है तो बाकी पतियों के उसके साथ लिंग सम्बन्धों की आज्ञा नहीं होती।
बहु-पति विवाह के कारण (Causes of Polyandry)-
1. प्राचीन कबीलों में रहते हुए लोगों के लिए एक व्यक्ति द्वारा पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी उठानी मुश्किल होती थी जिस कारण व्यक्ति मिल कर एक स्त्री से विवाह करवा लेते थे। डॉ० कपाड़िया के अनुसार यह प्रथा कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण भी पाई जाती थी। प्राचीन समय में रोजी रोटी के लिए व्यक्ति को बहुत लम्बा समय अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था इस कारण कुछ व्यक्ति इस काम में व्यस्त रहते थे व बाकी पुरुष परिवार की देख-रेख के लिए घर रहते थे।
2. बढ़ती हुई जनसंख्या को सीमित करने के लिए भी विवाह की यह प्रथा पाई गई। इसमें परिवार सीमित रहता है। क्योंकि बच्चे कम पैदा होते हैं।
3. कई स्थानों पर रोजी रोटी के साधन सीमित होने के कारण भी यह प्रथा पाई गई क्योंकि कमाने वालों की संख्या सीमित साधनों के कारण अधिक थी व खाने वाले कम हो जाते थे, जिससे उनमें खुशहाली भी थी।
4. कई समाज शास्त्रियों के अनुसार विवाह की इस प्रथा के प्रचलित होने का कारण औरतों की संख्या का मर्दो की संख्या से कम होना भी है। ___5. कुछ क्षेत्रों में लड़की की कीमत अदा करने पर ही उसको पत्नी बनाया जा सकता था व कई बार लड़की की कीमत इतनी अधिक होती थी कि अकेले व्यक्ति की हैसियत से बाहर होती थी। इस कारण कई व्यक्ति मिलकर उसको पत्नी बनाने के लिए कीमत अदा करने के काबिल होते थे। इसी कारण वह सभी मिलकर एक ही औरत को अपनी पत्नी स्वीकार कर लेते थे।
बहुपति विवाह के लाभ (Merits of Polyandry)-
1. बहु-पति विवाह की प्रथा से जनसंख्या सीमित की जा सकती है क्योंकि कई समाजों में ग़रीबी का कारण भी बढ़ती. आबादी द्वारा होता है, इस प्रथा से बच्चों की संख्या कम हो जाती है।
2. इस प्रथा से जैसे जनसंख्या सीमित होती है उसी तरह रहन-सहन का दर्जा ऊंचा हो जाता है, क्योंकि कमाने वाले पर परिवार का बोझ काफ़ी कम होता है। कमाने वालों की संख्या अधिक होती है जिस कारण परिवार पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।
3. संयुक्त परिवार इस प्रथा के द्वारा ही पाया जाता है व साथ ही परिवार का आकार भी सीमित होता है। इस कारण लड़ाई-झगड़े भी कम हो जाते हैं क्योंकि प्रत्येक परिवार का सदस्य, परिवार के साझे लाभ के लिए ही मेहनत करता है।
4. बहुपति विवाह की प्रथा में बच्चों का पालन-पोषण अधिक स्थिर ढंग से होता है क्योंकि बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारी परिवार के सभी सदस्यों की साझी होती है। माता व पिता का प्यार जो बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पाया जाता है, भी बच्चों को प्राप्त हो जाता है। संघर्ष की स्थिति बहुत कम पाई जाती है।
बहुपति विवाह की हानियाँ (Demerits of Polyandry)-
1. बहुपति विवाह का सबसे बड़ा नुकसान औरतों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित होता है क्योंकि एक स्त्री को कितने ही पुरुषों की लैंगिक इच्छा की पूर्ति करनी पड़ती है जिस कारण उनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता था।
2. विवाह की इस प्रथा से जन्म दर बहुत कम होती थी। यदि यह विवाह कुछ कबीलों में विकसित रहा तो आने वाले वर्षों में हो सकता है कि समाज भी समाप्त हो जाए।
3. सभी पुरुषों की काम वासना पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि औरत के लिए प्रत्येक आदमी के पास रहने का समय निश्चित किया जाता है। जब वह निश्चित समय एक आदमी के पास रह रही होती है तो बाकी आदमियों को उसके साथ सहवास करने की मनाही होती है। ऐसी स्थिति में आदमी अपनी काम इच्छा की पूर्ति के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार परिवार व समाज दोनों के बीच झगड़े से अनैतिकता में अधिकता पाई जाती है।

प्रश्न 5.
विवाह की संस्था में आ रहे परिवर्तनों का वर्णन करो।
उत्तर-
1. सरकार द्वारा लाए गए परिवर्तन-जब विवाह को एक संस्था के रूप में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुई तो इस संस्था में कई प्रकार के परिवर्तन भी लाए गए। विवाह सम्बन्धी कानून पास किए गए जिनमें हिन्दू मैरिज एक्ट सन् 1955 (Hindu Marriage Act 1955) में पास किया गया। इस कानून के तहत बहु-विवाह की प्रथा पर पाबन्दी लगा दी गई। एक विवाह को ही समाज द्वारा स्वीकारा गया व एक आदर्श विवाह भी माना गया। बाल विवाह जैसी बुराई जो बहुत समय से इस समाज में चली आ रही थी, को भी समाप्त किया गया व कानून की उल्लंघना करने वाले को कठोर सज़ा दिए जाने का भी प्रावधान बना। तलाक सम्बन्धी कानून भी पास किया ताकि आदमी व औरत की ज़िन्दगी तनाव भरपूर न रहे। पुराने समय में औरत से चाहे पति दुर्व्यवहार करे तो भी उसको अपनी सारी ज़िन्दगी बितानी पड़ती थी परन्तु अब आदमी व औरत दोनों को छूट दी गई है कि कोई भी अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि सुख से भरपूर जीवन व्यतीत कर सके।
2. विवाह को सामाजिक समझौते से सम्बन्धित किया गया-पुरानी विचारधारा के अनुसार आदमी व औरत के लिए विवाह एक धार्मिक बन्धन तक ही सीमित होता था, परन्तु आजकल की विचारधारा के अनुसार विवाह को इस बात तक सही बताया कि यदि पुरुष व स्त्री के बीच अच्छे सम्बन्ध हैं तो ठीक है, नहीं तो इस समझौते को तोड़ा भी जा सकता है। कई हालातों में जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है तो बाद में सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए पति-पत्नी के द्वारा आप भी फ़ैसला लिया जा सकता है क्योंकि दोनों के लिए नियम भी समान के बनाए जाते हैं। आधुनिक समय में विवाह को निजी खुशी से सम्बन्धित किया है ताकि परिवार में बच्चों की देखभाल भी ठीक ढंग से हो सके।
3. औरतों की स्थिति में परिवर्तन-जैसे-जैसे औरतें समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हिस्सा लेने लगी हैं वैसे-वैसे विवाह का स्वरूप भी बदल गया है। शुरू में समाज में औरत आर्थिक पक्ष से बिलकुल ही दूसरों पर आधारित होती थी। इस तरह वह हर तरह का दुःख भी बर्दाश्त कर लेती थी। परन्तु धीरे-धीरे औरत ने जब शिक्षा प्राप्त कर ली तो उससे वह आर्थिक तौर पर स्वतन्त्र हो गई। वह अपने फ़ैसले आप लेने लगी। कानूनी पक्ष से भी उसे काफ़ी मदद प्राप्त हुई। पति के जुल्म करने की स्थिति में वह उससे अलग होकर अपना जीवन अधिक अच्छी तरह गुज़ारने लगी। इस प्रकार जब औरत ने समाज में अपनी एक जगह बना ली तो विवाह की संस्था में स्वयं परिवर्तन आ गया। तलाक दर में तेजी आई। औरत की स्थिति पहले से अधिक अच्छी हो गई।
4. शिक्षा के विकास द्वारा परिवर्तन-शुरू में शिक्षा की ओर कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। इसी कारण धार्मिक संस्कार को पूरा करने के लिए विवाह की प्रथा विकसित रही। परन्तु जैसे-जैसे शिक्षा में बढ़ोत्तरी हुई तो विवाह को ज़रूरी न समझा गया व न ही छोटी उम्र में लड़की व लड़के की शादी की गई। शिक्षित बच्चे अपनी मर्जी से विवाह करवाने की इच्छा जाहिर करने लगे।
5. औद्योगीकरण के विकास द्वारा लाया परिवर्तन-पुराने समाज में विवाह सम्बन्धी नियम इतने कठोर होते थे कि हर एक व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करवाना पड़ता था। यदि वह उस नियम की उल्लंघना भी करता तो उसको सज़ा दी जाती थी। परन्तु जैसे-जैसे पैसे का महत्त्व समाज में बढ़ा तो विवाह के सम्बन्धों में परिवर्तन आ गया। प्राचीन समय की भान्ति विवाह में पवित्रता नहीं रही। आदमी व औरत ने अपने सम्बन्धों को भी काफ़ी हद तक पैसे के सुपुर्द कर दिया जिस कारण कई बार उनका एक-दूसरे पर विश्वास भी समाप्त हो जाता है व वह अलग रहना शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त औरतों व आदमियों दोनों तरफ से कुछ कमियां पैदा हो गई हैं जिनसे विवाह की संस्था की प्रबलता में भी कमी आई।
प्रश्न 6.
परिवार के मुख्य कार्यों का वर्णन करो।
उत्तर-
अलग-अलग समाजशास्त्रियों ने परिवार के कार्यों को अपने-अपने ढंग से वर्गीकृत किया। इनका वर्णन अग्रलिखित अनुसार है
I. जैविक कार्य (Biological Functions of Family)
1. लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति (Satisfaction of Sexual desire) परिवार का यह ज़रूरी कार्य तब से पाया जा रहा है जब से मानवीय समाज पाया गया है क्योंकि लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति परिवार का प्रारम्भिक कार्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति ही आदमी व औरत को लम्बे समय तक जोड़े रखती है, जिसके साथ इनमें शख्सियत का भी निर्माण होता है। यदि हम इस इच्छा को दबा देते हैं तो इससे कई ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिनसे सामाजिक सम्बन्ध भी टूट जाते हैं।
2. सन्तान उत्पत्ति (Reproduction)—मानवीय समाज को जीवित रखने के लिए भी यह ज़रूरी होता है कि हम मानवीय नस्ल को आगे से आगे बढ़ाएं। हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार व्यक्ति को तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक उसके पुत्र पैदा नहीं होता। समाज भी परिवार से बाहर पैदा हुए बच्चे को गैर-कानूनी करार दे देता है। इसी कारण परिवार को ही सन्तान उत्पत्ति का मनोरथ कहा जाता है।
3. रहने की व्यवस्था (Provision of Shelter)-परिवार के द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा का प्रबन्ध भी किया जाता है। व्यक्ति के रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाती है ताकि रोज़ाना के कार्यों से वापिस आकर वह घर में अपने परिवार सहित रह सके। आजकल के समय में क्लबों, होटलों आदि में चाहे आदमी को रहने के लिए जगह मिल जाती है परन्तु घर उसके लिए स्वर्ग के समान होता है क्योंकि जो आराम उसको घर में रहकर मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता।
4. बच्चों का पालन-पोषण (Upbringing of Children) बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी का कार्य भी परिवार का ही होता है। बच्चा पैदा करने का अर्थ यह नहीं कि उसको परिवार की ज़रूरत नहीं बल्कि बच्चे का सही विकास माता-पिता की देख-रेख में ही ठीक हो सकता है। यह ठीक है कि आधुनिक समय में औरतों के रोज़गार में आ जाने से बच्चों की सम्भाल परिवार से बाहर क्रैचों में जाकर होने लगी है, परन्तु फिर भी हम यह देखते हैं कि जो बच्चे माता-पिता की देख-रेख में बड़े होते हैं, उनमें अधिक गुणों का भी विकास हुआ होता है। हैवलॉक (Havelock) के अनुसार अमेरिका में माँ का दूध पीने वाले बच्चों के बीच मृत्यु दर, दूसरा दूध पीने वाले बच्चों से बहुत कम है। इस प्रकार परिवार की सहायता के साथ ही हम बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से कर सकते हैं व इससे ही बच्चे का सम्पूर्ण विकास भी हो सकता है।
II. आर्थिक कार्य (Economic Functions)-परिवार को शुरू से आर्थिक कार्यों का केन्द्र माना जाता रहा है क्योंकि अपने सदस्यों की आर्थिक सुरक्षा भी इसी से प्राप्त होती है। परंपरागत समाजों में तो काफ़ी चीजें घर में रहकर ही बनाई जाती थीं। परिवार के आर्थिक कार्य इस प्रकार हैं-
1. जायदाद की सुरक्षा (Protection of Property)—परिवार में व्यक्ति की जायदाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है। प्राचीन समय में अधिकतर पितृ प्रधान परिवार में जायदाद का विभाजन केवल लड़कों में ही किया जाता था परन्तु आजकल के आधुनिक समय में जायदाद का विभाजन कानून के द्वारा लड़के व लड़की दोनों के बीच किया जाने लगा है। यदि कोई व्यक्ति विवाहित नहीं होता तो उसकी मौत के बाद जायदाद के विभाजन पीछे, रिश्तेदारों के बीच भी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस प्रकार जायदाद परिवार के सदस्यों के बीच परिवार के मुखिया की इच्छा के मुताबिक विभाजित कर दी जाती है।
2. पैसे का प्रबन्ध (Provision of Money)-पैसे की ज़रूरत परिवार के सदस्यों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए होती है। इस कारण परिवार के मुखिया द्वारा ही प्राचीन समय में पैसे का प्रबन्ध किया जाता था। आजकल आदमी व औरत दोनों मिलकर मेहनत करके परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
III. परिवार के सामाजिक कार्य(Social functions of family)—
1. समाजीकरण (Socialization)-परिवार में व्यक्ति समाज के बीच रहने के तौर-तरीके सीखकर ही एक अच्छा नागरिक बनता है व परिवार के द्वारा ही बच्चे का सामाजिक सम्पर्क भी स्थापित होता है। व्यक्ति का जन्म परिवार में होता है व सबसे पहले वह अपने माता-पिता के सम्पर्क में आता है क्योंकि उसकी प्राथमिक ज़रूरतों की पूर्ति भी इन्हीं से ही होती है। स्थिति व भूमिका की प्राप्ति भी व्यक्ति के परिवार में ही रहकर होती है। प्रदत्त पद की प्राप्ति भी परिवार से ही होती है।
परिवार में रहकर ही बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। यह सामाजिक विशेषता उसको परिवार में रहकर ही प्राप्त होती है। सैण्डरसन ने व्यक्ति की पशु प्रवृत्तियों को नियन्त्रण में रखना, अच्छी आदतों का निर्माण करना, ज़िम्मेदारियों को समझना व व्यक्ति में स्वः विश्वास का विकास करना भी परिवार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। सहयोग, प्यार, कुर्बानी, अनुशासन इत्यादि जैसे गुणों का विकास भी बच्चे में परिवार के बीच रहकर ही होता है। जिस प्रकार की शिक्षा बच्चा परिवार में रहकर प्राप्त करता है, उस प्रकार का असर बच्चे में समाज के लिए भी विकसित हो जाता है। उसको हर तरह से समाज में व्यवहार करने के बारे में पता लग जाता है।
2. सामाजिक संस्कृति को सुरक्षित रखना व आगे पहुंचाना (Protection and transmission of culture)-परिवार हमारी संस्कृति को सम्भालता है व यह संस्कृति ही हमारी सामाजिक विरासत होती है। इसमें निरन्तरता बनी रहती है। प्रत्येक परिवार अपनी यह ज़िम्मेदारी समझता है कि वह नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार, आदतें, रीति-रिवाज, परम्पराएं इत्यादि प्रदान करे, बच्चा वह हर चीज़ अचेतन प्रक्रिया में ही सीखता रहता है। क्योंकि वह जो कुछ भी अपने माता-पिता को करता देखता है वही वह आप करने लग जाता है। प्रत्येक परिवार के अपने रीति-रिवाज होते हैं जिन पर वह आधारित होता है। परिवार कुछ चीजें बच्चों को चेतन रूप में भी सिखाता है ताकि बच्चा परिवार के बनाए हुए आदर्शों के मुताबिक चले। इस प्रकार इस निरन्तरता के आधार पर ही परिवार की संस्कृति सुरक्षित भी रहती है व अगली पीढ़ी तक भी पहुंच जाती है।
3. सामाजिक नियन्त्रण (Social Control)-परिवार को सामाजिक नियन्त्रण की एक एजेंसी के रूप में महत्ता प्राप्त है क्योंकि यह पहली एजेंसी होती है जिसमें बच्चे पर नियन्त्रण रखा जाता है ताकि गलत आदतों का निर्माण उसमें न हो सके। उदाहरण के लिए माता-पिता बच्चे के झूठ बोलने पर नियन्त्रण रखते हैं, बड़ों के साथ गलत व्यवहार आदि पर नियन्त्रण करते हैं ताकि बच्चा परिवार के बनाए हुए कुछ नियमों की पालना करे। प्रत्येक सदस्य परिवार के लिए ऐसा काम करना चाहता है जिससे समाज में उसके परिवार का गौरव अधिक बढ़े। परिवार अपने सदस्यों के हर तरह के व्यवहार व क्रियाओं पर नियन्त्रण रखता है। इससे बच्चा आज्ञाकारी व अनुशासन प्रिय बन जाता है। यदि घर का एक बच्चा अपने बड़े भाई बहन या माता-पिता से गलत तरीके से व्यवहार करेगा तो समाज के बाकी सदस्यों के साथ भी वह दुर्व्यवहार करने लग जाता है। जैसे चोरी करना जोकि समाज के कानूनों के द्वारा जुर्म करार दिया जाता है। उसकी आदत भी कई बार परिवार के बड़े सदस्यों को देखकर सीखी जाती है। यदि परिवार के माता-पिता बच्चे के किसी प्रकार की वस्तु चोरी करके घर लाने पर मनाही नहीं करेंगे तो बच्चा बड़ा होकर यही काम करने लगेगा। इसी तरह से परिवार बच्चे पर हर तरह की निगरानी रखकर सामाजिक नियन्त्रण रखता है।
4. स्थिति प्रदान करना (Provide Status)-परिवार में रहकर बच्चे को अपने स्थान व भूमिका का पता · चलता है। प्राचीन समाज में तो बच्चा जैसे भी परिवार में पैदा होता था उसी तरह का आदर उसको प्राप्त होने लग जाता था। जैसे अमीर परिवार, राजा-महाराजा के परिवार, जागीरदार के परिवार आदि में पैदा हुए बच्चे को उतना ही सम्मान समाज में प्राप्त होता था जितना उसके माता-पिता को। उसकी स्थिति वही होती थी। एक गरीब घर में पैदा हुए बच्चे की स्थिति भी निम्न होती थी। चाहे आजकल के समय में बच्चा समाज के बीच अपनी स्थिति परिश्रम से प्राप्त करने लगा है परन्तु फिर भी कुछ सीमा तक बच्चा जिस तरह के परिवार में जन्म लेता है उसको उसी प्रकार कम या अधिक परिश्रम करना पड़ता है।
IV. शिक्षा सम्बन्धी कार्य (Educational Function)-परिवार बच्चे की शिक्षा के लिए प्राथमिक साधन होता है क्योंकि सबसे प्रथम शिक्षा बच्चा परिवार में रहकर ही प्राप्त करता है। अच्छी आदतें सीखना व और अन्य कई गुण आदि परिवार से ही सम्बन्धित होते हैं। प्राचीन समाजों में व्यापार सम्बन्धी शिक्षा, धर्म सम्बन्धी शिक्षा, अच्छा नागरिक बनने सम्बन्धी, बच्चा परिवार में ही प्राप्त करता है। चाहे आज के समाज में बच्चे के शिक्षात्मक कार्य दूसरी संस्थाओं के पास चले गए हैं परन्तु फिर भी कुछ सीमा तक परिवार अभी भी इस शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को अदा कर रहा है।
V. राजनीतिक कार्य (Political Function)-राजनीतिक क्षेत्र के लिए परिवार को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। कनफ्यूशियस के अनुसार मनुष्य सबसे पहला सदस्य परिवार का है व बाद में राज्य का। आदिम (Primitve) समाज में परिवार की महत्ता राजनीतिक पक्ष से अधिक प्रबल होती थी। समाज अलग-अलग कबीलों में बंटा हुआ था। इन कबीलों के ऊपर सबसे बड़ी आयु वाले व्यक्तियों को मुखिया बनाया जाता था। परिवार में भी सबसे बड़ी आयु वाला मुखिया होता था व परिवार के बाकी सदस्य उसके मुताबिक चलते थे। भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली में भी परिवार के मुखिया की ही प्रतिनिधिता होती थी। यह मुखिया परिवार का दादा, पड़दादा आदि हो सकता था। परिवार के सदस्यों को अलग-अलग स्थितियां व रोल दिए जाते थे जिन्हें निभाना परिवार के प्रत्येक सदस्य का फर्ज होता था। परिवार की स्थिरता भी इसी कारण होती थी। आधुनिक समाज में परिवार के असंगठन का कारण ही परिवार के राजनीतिक कार्यों की कमी होती है। परिवार ही व्यक्ति को एक राजनीतिक व्यक्ति बनाने में मदद करता है जिससे व्यक्ति समाज का एक अच्छा नागरिक बन सकता है। यह राजनीतिक संगठन ही एक.ऐसा ताकतवर संगठन होता है जो व्यक्ति के सामाजिक सम्बन्धों को भी नियमित करता है। सो पारिवारिक संगठन ही हमारे सामाजिक संगठन के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार परिवार राजनीतिक कार्य भी अदा करता है।
VI. धार्मिक कार्य (Religious Function)-धार्मिक संस्कारों के बारे जानकारी व्यक्ति को परिवार से ही प्राप्त होती है। जैसे हिन्दू ग्रन्थों के अनुसार तब तक धार्मिक संस्कार अधूरे होते हैं जब तक पत्नी न हो। परिवार धार्मिक क्रियाओं का केन्द्र होता है। भारतीय समाज में विवाह को ही धार्मिक बन्धन का नाम दिया जाता है। धार्मिक क्रियाओं के द्वारा ही इसको पूरा किया जाता है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के धार्मिक संस्कार परिवार द्वारा अदा किए जाते हैं। व्यक्ति में नैतिकता का विकास भी धर्म के द्वारा होता है। धर्म एक प्रकार से व्यक्ति पर नियन्त्रण भी रखता है। इससे व्यक्ति में अच्छे गुणों का विकास होता है जैसे कुर्बानी अथवा त्याग की भावना, प्यार, सहयोग इत्यादि।
धर्म के आधार पर ही पारिवारिक जीवन भी निर्भर करता है। इस प्रकार धर्म अपने सदस्यों को धार्मिक आदर्शों, नियमों आदि प्रति पहचान करवाता है जिससे व्यक्तियों में एकता इत्यादि की भावना भी कायम रहती है। चाहे आजकल के समाज में लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो गया है परन्तु फिर भी परिवार धार्मिक रिवाजों को कायम रख रहा है।
VII. मनोरंजन के कार्य (Recreational Function) परिवार अपने सदस्यों के मनोरंजन के लिए भी सहूलतें प्रदान करता है। शुरू के समाज में व्यक्ति रात के समय परिवार में इकट्ठे बैठकर एक-दूसरे से अपनी रोज़ाना की बातचीत करते थे व परिवार के बुजुर्ग सदस्य अपनी बाल कथाएं आदि सुनाकर शेष का मनोरंजन करते थे। उस समय मनोरंजन के दूसरे साधन विकसित नहीं थे। इसके अतिरिक्त त्योहारों के समय भी परिवार के सदस्य इकट्ठे मिल कर नाचते, गाना गाते थे जिनसे सबका मनोरंजन होता था।

प्रश्न 7.
गोत्र के बारे में आप क्या जानते हैं ? विस्तारपूर्वक लिखें।
उत्तर-
गोत्र को वंश समूह का विस्तृत रूप कह सकते हैं। जब कोई वंश समूह विकास के कारण बढ़ जाता है तो वह गोत्र का रूप धारण कर लेता है। यह माता या पिता के अनुरेखित रक्त सम्बन्धियों को मिलाकर बनता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गोत्र रक्त के रिश्तेदारों का समूह होता है और वह सभी किसी साझे पूर्वज के एक रेखकी सन्तान होते हैं। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह साझे पूर्वज काल्पनिक होते हैं क्योंकि उनके बारे में किसी को पता नहीं होता है।
गोत्र किसी ऐसे व्यक्ति या पूर्वज से शुरू होता है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। क्योंकि यह माना जाता है कि उसने ही परिवार को या उस गोत्र को शुरू किया था इसलिए उसको संस्थापक मान लिया जाता है। उस गोत्र का नाम भी उसके पूर्वज के नाम के साथ रख लिया जाता है। गोत्र हमेशा एक तरफ को चलती है मतलब किसी बच्चे के माता-पिता के गोत्र एक नहीं हो सकते वह हमेशा अलग-अलग होंगे। यह एक पक्ष का ही होता है। इसका यह अर्थ है कि माता की गोत्र अलग परिवारों का इकट्ठ है और पिता की गोत्र भिन्न परिवारों का इकट्ठ है। इस तरह यह गोत्र बाहर व्यक्ति का समूह होता है। एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता।
परिभाषाएं (Definitions) –
(1) मजूमदार (Majumdar) के अनुसार, “एक क्लैन या सिब अक्सर कुछ वंश समूहों का जुट होता है जोकि आपसी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं जोकि मनुष्य या मनुष्य की तरह, पशु, वृक्ष, पौधा या निर्जीव वस्तु हो सकता है।”
(“A clan or sib is often the combination of a few lineages and descent into may be ultimately traced to a mythical ancestor, who may be human, human like, animal, plant or even in animate.”)
(2) पिंडिगटन (Pidington) के अनुसार, “एक गोत्र जिसको कभी-कभी कुल (Sib) भी कहते हैं, एक बाहर विवाही सामाजिक समूह है जिसके सदस्य अपने आपको एक-दूसरे के साथ सम्बन्धित समझते हैं, जो आमतौर पर अपनी उत्पत्ति एक काल्पनिक वंशानुक्रम द्वारा किसी बड़े-बूढ़ों से मानते हैं।”
(“A clan some times called sib is an exogamous social group whose members regard themselves as being related to each other usually by functional descent from a common ancestor.”)
(3) रिवर्ज़ (Rivers) के अनुसार, “गोत्र में कबीले का एक बाहर विवाहित विभाजन है जिसके सदस्य अपने ही कुछ बन्धनों द्वारा एक-दूसरे के साथ सम्बन्धित रहते हैं। इस बन्धन का आकार एक साझे पूर्वज की सन्तान या वंश होने में विश्वास एक साझा टोटम या एक साझे भू-भाग में निवास हो सकता है।”(“Clan is an exogamous division of tribe the members of which are held to be related to one another by same common lies, it may be descent from a common ancestor, possession of a common totom or hibitationed of a common territory.”) .
इन परिभाषाओं को देखकर हम कह सकते हैं कि गोत्र एक काफ़ी बड़ा रक्त समूह होता है जोकि एक वंश के सिद्धान्त पर आधारित होता है। गोत्र अपने आप में एक पूरा सामाजिक संगठन है जोकि एक समाज की अलगअलग गोत्रों को एक खास रूप अर्थात् और काम प्रदान करती है। गोत्र या तो मातृ वंशी होती है या फिर पितृ वंशी, मतलब कि बच्चे या तो पिता की गोत्र के सदस्य होते हैं या फिर माता की गोत्र के सदस्य । एक गोत्र बाहरी समूह होता है अर्थात् विवाह गोत्र से बाहर होना चाहिए है। इसलिए माता-पिता के गोत्र अलग-अलग होने चाहिए।
गोत्र की विशेषताएं (Characteristics of Clan) –
1. गोत्र की सदस्यता वंश पर आधारित होती है (Membership of Clan depends upon Lineage)गोत्र की सदस्यता वंश परम्परा पर आधारित होती है। यह चाहे पितृ वंशी या मातृ वंशी हो सकता है जोकि उस समाज पर निर्भर करता है। व्यक्ति की गोत्र उसके हाथ में नहीं होती। यह उसकी इच्छा पर भी आधारित नहीं होती। यह तो जन्म पर आधारित होता है। व्यक्ति जिस गोत्र में जन्म लेता है उसका सदस्य बन जाता है। व्यक्ति जिस गोत्र में जन्म लेता है, उसमें ही बड़ा होता है और उसमें ही मर जाता है।
2. हर गोत्र का नाम होता है (Each clan has a name)-हर गोत्र का एक खास नाम होता है। चाहे यह नाम, पशु, वृक्ष, किसी प्राकृतिक वस्तु आदि से भी लिया जा सकता है। यह चार प्रकार के होते हैं-भू-भागी नाम, टोटम वाले नाम, उपनाम, ऋषि नाम।
3. एक पक्ष (Unilateral)–गोत्र हमेशा एक पक्ष का होता है। यह कभी भी दो पक्ष की नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि गोत्र या पितृ वंशी समूह होगा या मातृ वंशी समूह। पितृ वंशी समूह से मतलब है कि वह बच्चा पिता के वंश का सदस्य होगा और मातृ वंशी से मतलब है कि वह माता के वंश का सदस्य होगा। इस तरह सिर्फ एक पक्ष होगा दोनों तरफ से नहीं।
4. गोत्र के सदस्य एक स्थान पर नहीं रहते (Member of a clan do not live at one place)-गोत्र के सदस्यों में खून का सम्बन्ध होता है पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक ही स्थान पर रहते हों। इनका निवास स्थान साझा नहीं होता।
5. साझा पूर्वज (Common Ancestor)—गोत्र का एक साझा पूर्वज होता है चाहे उस पूर्वज के बारे में किसी को पता नहीं होता। यह साझा पूर्वज हमेशा कल्पना पर आधारित होता है। चाहे वह पूर्वज असल में भी हो सकते हैं पर यह आमतौर पर कल्पित भी हो सकता है।
6. बर्हिविवाही समूह (Exogamous group)-गोत्र एक बर्हिविवाही समूह है। इसका मतलब है कि कोई भी एक ही गोत्र में विवाह नहीं करवा सकता। यह वर्जित होता है। यह इस वज़ह के कारण होता है क्योंकि गोत्र के सारे सदस्य एक साझे असली या कल्पित पूर्वज की पैदावार होते हैं और उन सभी में खून के सम्बन्ध होते हैं। इस वज़ह के कारण उस रिश्ते में बहन-भाई हुए और इनमें वर्जित है। विवाह अपनी गोत्र से बाहर ही करवाया जा सकता है

विवाह, परिवार तथा नातेदारी PSEB 11th Class Sociology Notes
- प्रत्येक समाज ने अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया होता है। संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक ढांचा है जो एक समुदाय के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करती है। यह विशेष प्रकार की आवश्यकता को पूर्ण करती है जो समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
- संस्थाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे कि यह विशेष आवश्यकताएं पूर्ण करती हैं, यह नियमों का एक गुच्छा हैं, यह अमूर्त व सर्वव्यापक होती हैं, यह स्थायी होती हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं आते, इनमें प्रकृति सामाजिक होती है इत्यादि।
- विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है। यह समाज की एक मौलिक संस्था . है। विवाह से दो विरोधी लिंगों के व्यक्तियों को पति-पत्नी के रूप में इकट्ठे रहने की आज्ञा मिल जाती है। वह लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं तथा समाज के आगे बढ़ने में योगदान देते हैं।
- वैसे तो समाज में विवाह के कई प्रकार मिलते हैं परन्तु एक विवाह तथा बहु विवाह ही प्रमुख हैं। बहुविवाह आगे दो भागों में विभाजित हैं-बहुपति विवाह तथा बहुपत्नी विवाह । बहुपति विवाह कई जनजातीय समाजों में प्रचलित है तथा बहुपत्नी विवाह पहले हमारे समाजों में प्रचलित था।
- हमारे समाज में जीवन साथी के चुनाव के कई तरीके प्रचलित हैं जिनमें से अन्तर्विवाह (Endogamy) तथा बहिर्विवाह (Exogamy) प्रमुख हैं। अन्तर्विवाह में व्यक्ति को एक निश्चित समूह के अंदर ही विवाह करना पड़ता है तथा बहिर्विवाह में व्यक्ति को एक निश्चित समूह से बाहर विवाह करवाना पड़ता है।
- विवाह की संस्था में पिछले कुछ समय में कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों के कई मुख्य कारण हैं जैसे कि औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, नए कानूनों का बनना, स्त्रियों की स्वतन्त्रता, पश्चिमी समाजों का प्रभाव इत्यादि।
- परिवार एक ऐसी सर्वव्यापक संस्था है जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में मौजद है। व्यक्ति केजीवन में परिवार नामक संस्था का काफ़ी अधिक प्रभाव है तथा इसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता।
- परिवार के कई विशेषताएं होती हैं जैसे कि यह सर्वव्यापक संस्था है, इसका भावात्मक आधार होता है, इसका आकार छोटा होता है यह स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार का होता है, यह व्यक्ति के व्यवहार को नियन्त्रित करता है इत्यादि।
- परिवार के कई प्रकार होते हैं तथा इनके रहने के स्थान, सत्ता, सदस्यों इत्यादि के आधार पर कई भागों में विभाजित किया जा सकता है।
- पिछले कुछ समय में परिवार नामक संस्था में कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं जैसे कि आकार का छोटा होना, परिवारों का टूटना, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, नातेदारी के संबंधों का कमज़ोर होना, कार्यों में परिवर्तन इत्यादि।
- नातेदारी व्यक्ति के रिश्तों की व्यवस्था है। इसमें कई प्रकार के रिश्ते आते हैं। नातेदारी को दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। वह दो आधार हैं-रक्त संबंध तथा विवाह।
- नज़दीकी तथा दूरी के आधार पर तीन प्रकार के रिश्तेदार पाए जाते हैं-प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के रिश्तेदार। प्राथमिक रिश्तेदार माता-पिता, बहन-भाई होते हैं। द्वितीय रिश्तेदार हमारे प्राथमिक रिश्तेदारों के प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं जैसे पिता का पिता-दादा। तृतीय प्रकार के रिश्तेदार द्वितीय रिश्तेदारों के प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं जैसे-चाचा का पुत्र-चचेरा भाई।
- पितृसत्तात्मक (Patriarchal)-वह परिवार जहाँ पिता की सत्ता चलती हो तथा उसका ही नियन्त्रण हो।
- मातृसत्तात्मक (Matriarchal)—वह परिवार जहाँ माता की सत्ता चलती हो तथा उसका ही नियन्त्रण हो।
- एकाकी परिवार (Nuclear Family)—वह परिवार जहाँ पति, पत्नी व उनके बिन ब्याहे बच्चे रहते हों।
- संयुक्त परिवार (Joint Family)-वह परिवार जिसमें दो या अधिक पीढ़ियों के सदस्य इकट्ठे रहते हों तथा एक ही रसोई में से खाना खाते हों।
- अन्तर्विवाह (Endogamy)-एक निश्चित समूह, जैसे कि जाति में ही विवाह करवाना।
- बहिर्विवाह (Exogamy)-एक निश्चित समूह, जैसे कि गोत्र या परिवार से बाहर विवाह करवाना।
- एक विवाह (Monogamy)-जब एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह हो उसे एक विवाह कहते हैं।
- बहु विवाह (Polygamy)-जब एक पुरुष या स्त्री दो या अधिक विवाह करवाएं तो उसे बहुविवाह कहते है।
- विवाह मूलक नातेदारी (Affinal Kinship)—वह रिश्तेदारी जो व्यक्ति के विवाह के पश्चात् बनती है जैसे कि जमाई, जीजा, इत्यादि।
- रक्त मूलक नातेदारी (Consanguineous Kinship)—वह नातेदारी जो व्यक्ति के जन्म के पश्चात् ही बन जाती है जैसे-पुत्र, पुत्री, माता, पिता, भाई, बहन इत्यादि।
- नातेदारी (Kinship)-सामाजिक संबंध जो वास्तविक या काल्पनिक आधारों पर रक्त या विवाह के अनुसार बनते हों।
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()